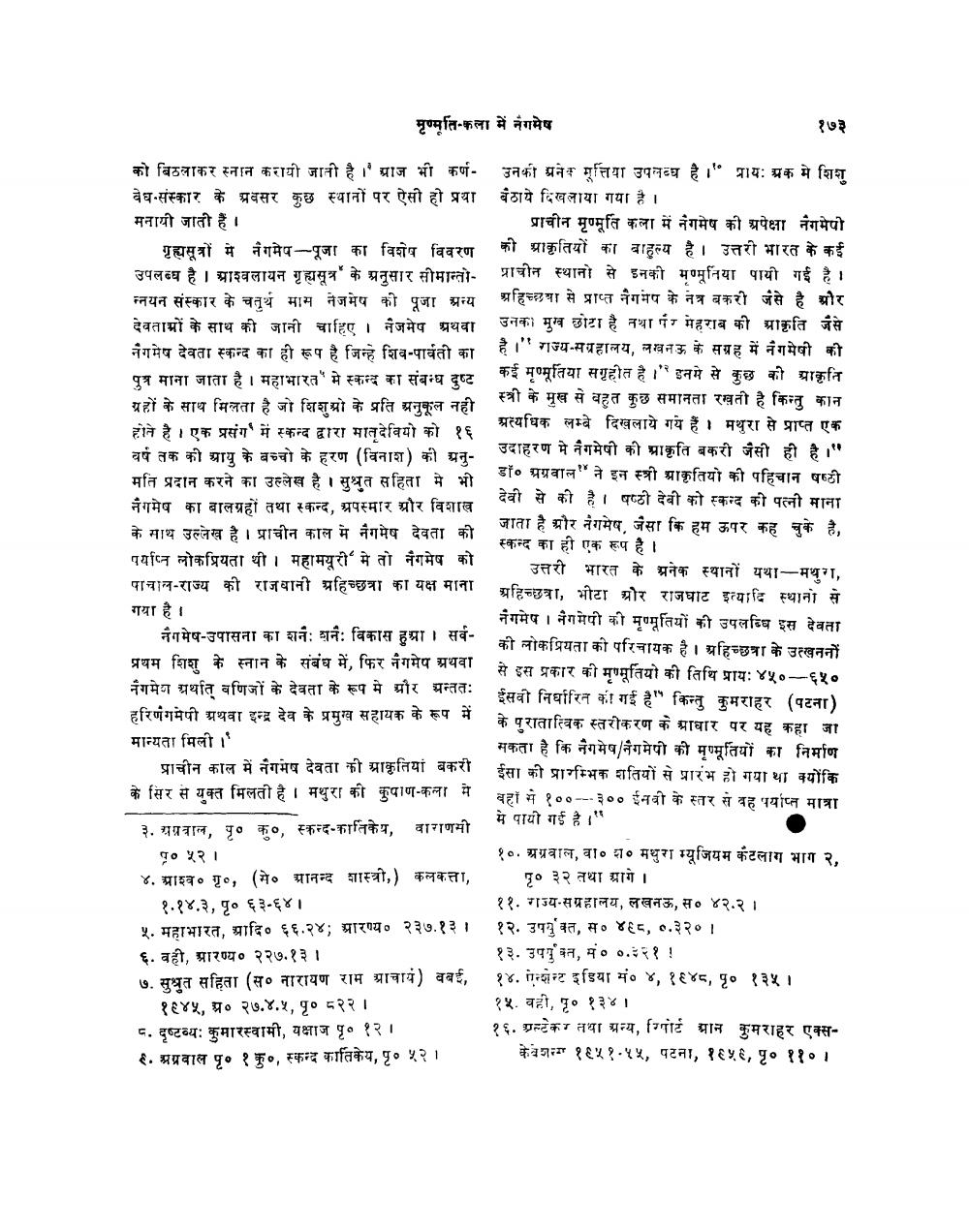________________
मृण्मृति-कला में नंगमेष
१७३
को बिठलाकर स्नान करायी जाती है। प्राज भी कर्ण- उनकी अनेक मूत्तिया उपलब्ध है। प्रायः प्रक मे शिशु वेध-संस्कार के अवसर कुछ स्थानों पर ऐसी हो प्रथा बंठा ये दिखलाया गया है। मनायी जाती हैं।
प्राचीन मृण्मूर्ति कला में नेगमेष की अपेक्षा नंगमेपी _गृह्यसूत्रों में नैगमेप-पूजा का विशेष विवरण की प्राकृतियों का बाहुल्य है। उत्तरी भारत के कई उपलब्ध है । प्राश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार सीमान्तो- प्राचीन स्थानो से इनकी मृणमूनिया पायी गई है। न्नयन संस्कार के चतुर्थ माम नेजमेष की पूजा अन्य अहिच्या से प्राप्त नैगमेप के नेत्र बकरी जैसे है और देवतामों के साथ की जानी चाहिए । नेजमेष अथवा उनका मुख छोटा है तथा पर मेहराब की प्राकृति जैसे नंग मेष देवता स्कन्द का ही रूप है जिन्हें शिव-पार्वती का है। 'गज्य-संग्रहालय, लखनऊ के सग्रह में नंगमेषी की पुत्र माना जाता है । महाभारत मे स्कन्द का संबन्ध दुष्ट
कई मृण्मूर्तिया सगृहीत है। इनमे से कुछ की प्राकृति ग्रहों के साथ मिलता है जो शिशुमो के प्रति अनुकूल नही
स्त्री के मुख से बहुत कुछ समानता रखती है किन्तु कान होते है । एक प्रसंग में स्कन्द द्वारा मात देवियो को १६
अत्यधिक लम्बे दिखलाये गये हैं। मथुरा से प्राप्त एक वर्ष तक की आयु के बच्चो के हरण (विनाश) की अनु
उदाहरण मे नगमेषी की प्राकृति बकरी जैसी ही है।"
डॉ० अग्रवाल" ने इन स्त्री प्राकृतियो की पहिचान षष्ठी मति प्रदान करने का उल्लेख है । सुश्रुत सहिता मे भी नंगमेष का बालग्रहों तथा स्कन्द, अपस्मार और विशाख
देवी से की है। षष्ठी देवी को स्कन्द की पत्नी माना
जाता है और नेगमेष, जैसा कि हम ऊपर कह चुके है, के माथ उल्लेख है। प्राचीन काल में नैगमेष देवता की
स्कन्द का ही एक रूप है। पर्याप्त लोकप्रियता थी। महामयूरी मे तो नैगमेष को
उत्तरी भारत के अनेक स्थानों यथा-मथुग, पाचाल-राज्य की राजधानी अहिच्छत्रा का यक्ष माना
अहिच्छवा, भीटा और राजघाट इत्यादि स्थानों से गया है।
नंगमेष । नेगमेपी की मृण्मूर्तियों की उपलब्धि इस देवता नंगमेष-उपासना का शनैः शनैः विकास हुआ। सर्व
की लोकप्रियता की परिचायक है । अहिच्छत्रा के उत्खननों प्रथम शिशु के स्नान के संबंध में, फिर नगमेप अथवा
से इस प्रकार की मृण्मूर्तियो की तिथि प्रायः ४५०-६५० नंगमेग अर्थात वणिजों के देवता के रूप मे और अन्ततः ।
ईसवी निर्धारित की गई है किन्तु कुमराहर (पटना) हरिणगमेपी अथवा इन्द्र देव के प्रमुख सहायक के रूप में
के पुरातात्विक स्तरीकरण के आधार पर यह कहा जा मान्यता मिली।
मकता है कि नेगमेष/नगमेपी की ममूर्तियों का निर्माण प्राचीन काल में नंगमेष देवता की प्राकृतियां बकरी
ईसा की प्रारम्भिक शतियों से प्रारंभ हो गया था क्योंकि के सिर से युक्त मिलती है । मथुरा की कुषाण-कला मे बानी
बहाँ मे १०० ---३०० ईनवी के स्तर से वह पर्याप्त मात्रा ३. अग्रवाल, पृ० कु०, स्कन्द-कार्तिकेय, वाराणसी में पायी गई है। १० ५२।
१०. अग्रवाल, वा०२० मथुरा म्यूजियम कैटलाग भाग २, ४. पाश्व गृ०, (मे० आनन्द शास्त्री,) कलकत्ता,
पृ० ३२ तथा प्रागे । १.१४.३, पृ० ६३.६४ ।
११. गज्य-संग्रहालय, लखनऊ, स० ४२.२ । ५. महाभारत, पादि०६६.२४; प्रारण्य० २३७.१३ । १२. उपयुक्त, स० ४६८, ०.३२० । ६. वही, पारण्य० २२७.१३ ।
१३. उपर्युक्त, मं० ०.३२१ ! ७. सुश्रुत सहिता (स० नारायण राम प्राचार्य) बबई, १४. शेन्ट इडिया मं० ४,१९४८, पृ० १३५॥ १९४५, अ० २७.४.५, पृ० ८२२ ।
१५. वही, पृ० १३४ । ८. दृष्टव्यः कुमारस्वामी, यक्षाज पृ० १२ ।
१६. पल्टेकर तथा अन्य, रिपोर्ट प्रान कुमराहर एक्स६. अग्रवाल पृ० १ कु०, स्कन्द कार्तिकेय, पृ० ५२ । के वशम १९५१-५५, पटना, १६५६, पृ० ११०।