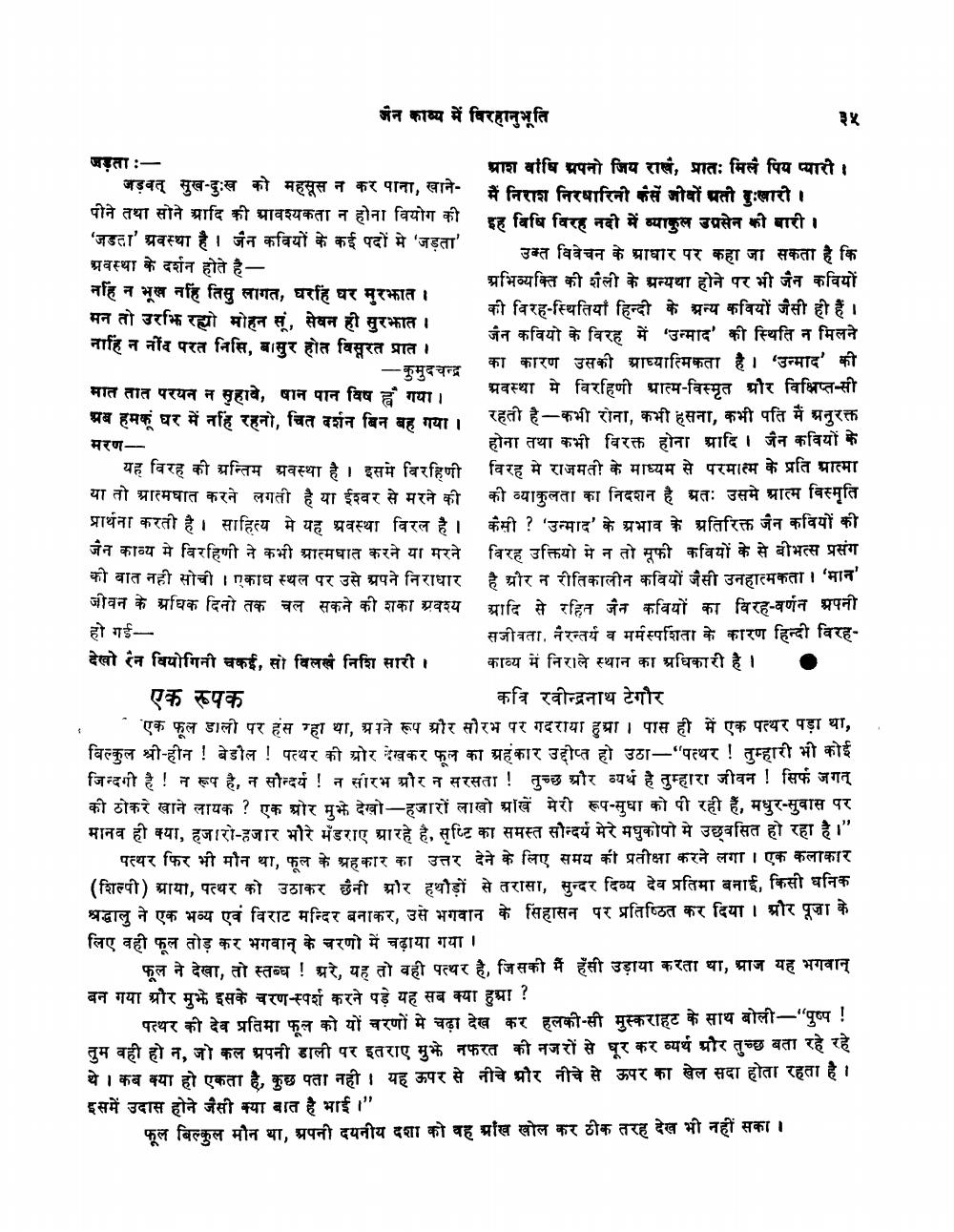________________
जैन काव्य में विरहानुभूति
जड़ता:
प्राश बांधि अपनो जिय राखं, प्रातः मिल पिय प्यारी। त् सुख-दुःख का महसूस न कर पाना, खान- मैं निराश निरषारिनी कैसें जीवों प्रती दुःखारी। पीने तथा सोने आदि की पावश्यकता न होना वियोग की इह विषि विरह नदी में व्याकूल उग्रसेन की बारी। 'जडता' अवस्था है। जैन कवियों के कई पदों में 'जड़ता'
उक्त विवेचन के प्राधार पर कहा जा सकता है कि अवस्था के दर्शन होते है
अभिव्यक्ति की शैली के अन्यथा होने पर भी जैन कवियों नहि न भूख नहिं तिसु लागत, घरहिं घर मुरझात । मन तो उझि रह्यो मोहन सू, सेवन ही सुरझात ।
की विरह-स्थितियाँ हिन्दी के अन्य कवियों जैसी ही हैं । नाहिं न नींव परत निसि, बासुर होत विसरत प्रात ।
जैन कवियो के विरह में 'उन्माद' की स्थिति न मिलने -कुमुदचन्द्र
का कारण उसकी आध्यात्मिकता है। 'उन्माद' की मात तात परयन न सहावे, षान पान विष ह गया।
अवस्था मे विरहिणी प्रात्म-विस्मृत और विक्षिप्त-सी अब हमकू घर में नहि रहनो, चित वर्शन बिन बह गया।
रहती है-कभी रोना, कभी हसना, कभी पति मैं अनुरक्त मरण
होना तथा कभी विरक्त होना प्रादि । जैन कवियों के यह विरह की अन्तिम अवस्था है। इसमें विरहिणी विरह मे राजमती के माध्यम से परमात्म के प्रति प्रात्मा या तो प्रात्मघात करने लगती है या ईश्वर से मरने की की व्याकुलता का निदशन है अतः उसमे प्रात्म विस्मृति प्रार्थना करती है। साहित्य मे यह अवस्था विरल है। कैसी? 'उन्माद' के प्रभाव के अतिरिक्त जैन कवियों की जैन काव्य मे विरहिणी ने कभी अात्मघात करने या मरने विरह उक्तियो में न तो मुफी कवियों के से बीभत्स प्रसंग की बात नही सोची । एकाध स्थल पर उसे अपने निराधार है और न रीतिकालीन कवियों जैसी उनहात्मकता। 'मान' जीवन के अधिक दिनो तक चल सकने की शका अवश्य प्रादि से रहित जैन कवियों का विरह-वर्णन अपना हो गई
सजीवता, नैरन्तर्य व मर्मस्पशिता के कारण हिन्दी विरहदेखो रेन वियोगिनी चकई, सो विलख निशि सारी। काव्य में निराले स्थान का अधिकारी है । एक रूपक
कवि रवीन्द्रनाथ टेगौर । एक फूल डाली पर हंस रहा था, अपने रूप और सौरभ पर गदराया हुमा। पास ही में एक पत्थर पड़ा था, . बिल्कुल श्री-हीन ! बेडौल ! पत्थर की ओर देखकर फल का अहंकार उद्दीप्त हो उठा-"पत्थर ! तुर जिन्दगी है ! न रूप है, न सौन्दर्य ! न सौरभ और न सरसता ! तुच्छ और व्यर्थ है तुम्हारा जीवन ! सिर्फ जगत् की ठोकरे खाने लायक ? एक ओर मुझे देखो-हजारों लाखो ऑखें मेरी रूप-सुधा को पी रही हैं, मधुर-सुवास पर मानव ही क्या, हजारो-हजार भौरे मँडराए प्रारहे है, सष्टि का समस्त सौन्दर्य मेरे मघुकोषो मे उछ्वसित हो रहा है।"
पत्थर फिर भी मौन था, फूल के अहकार का उत्तर देने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक कलाकार (शिल्पी) पाया, पत्थर को उठाकर छैनी और हथौड़ों से तरासा, सुन्दर दिव्य देव प्रतिमा बनाई, किसी धनिक श्रद्धालु ने एक भव्य एवं विराट मन्दिर बनाकर, उसे भगवान के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। और पूजा के लिए वही फूल तोड़ कर भगवान के चरणो में चढ़ाया गया ।
फूल ने देखा, तो स्तब्ध ! अरे, यह तो वही पत्थर है, जिसकी मैं हँसी उड़ाया करता था, पाज यह भगवान् बन गया और मुझे इसके चरण स्पर्श करने पड़े यह सब क्या हुआ ?
पत्थर की देव प्रतिमा फूल को यों चरणों में चढ़ा देख कर हलकी-सी मुस्कराहट के साथ बोली-"पुष्प ! तुम वही हो न, जो कल अपनी डाली पर इतराए मुझे नफरत की नजरों से घूर कर व्यर्थ और तुच्छ बता रहे रहे थे । कब क्या हो एकता है, कुछ पता नही। यह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का खेल सदा होता रहता है। इसमें उदास होने जैसी क्या बात है भाई।"
फूल बिल्कुल मौन था, अपनी दयनीय दशा को वह प्रांख खोल कर ठीक तरह देख भी नहीं सका।