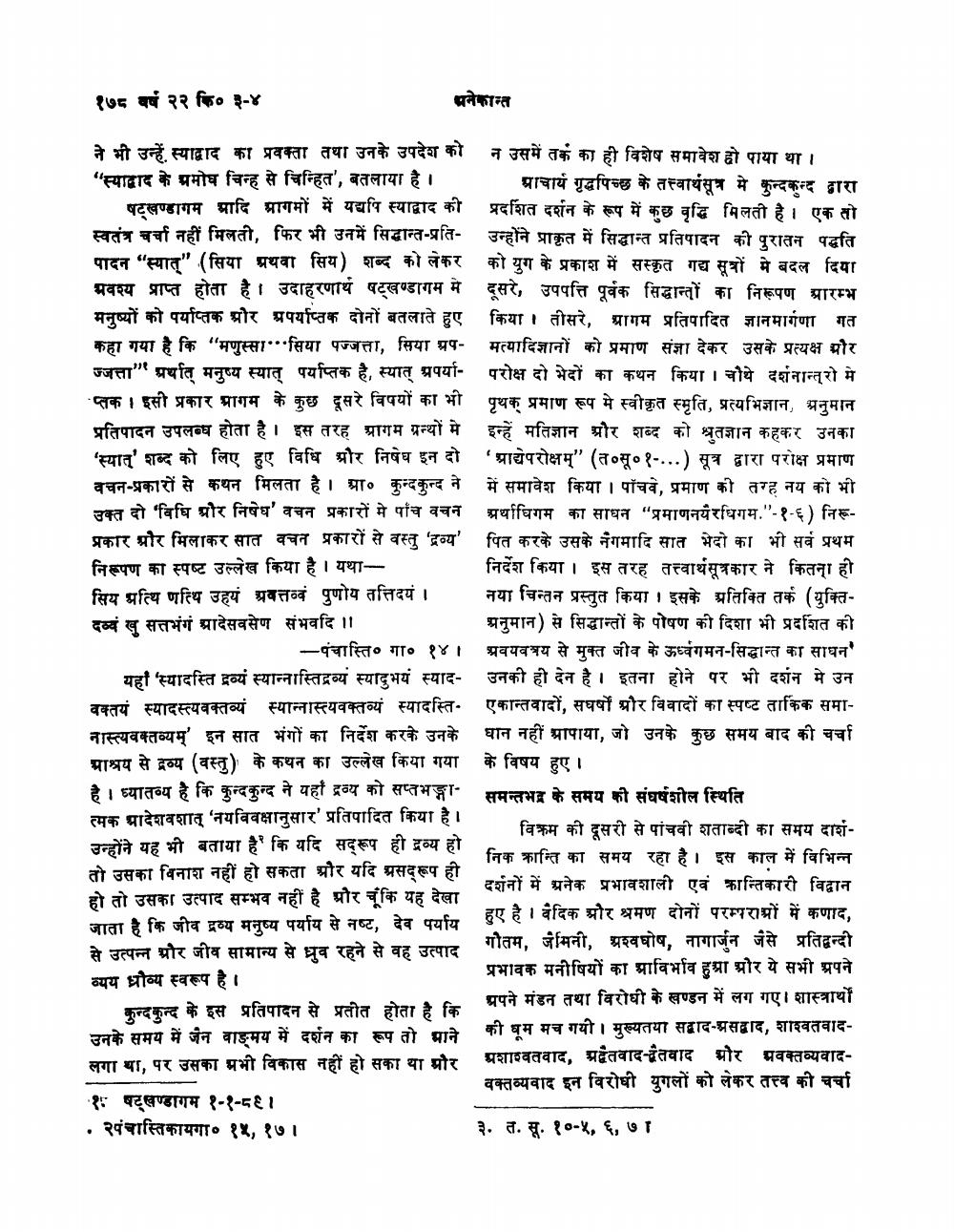________________
१७८ वर्ष २२ कि० ३-४
अनेकान्त
ने भी उन्हें. स्याद्वाद का प्रवक्ता तथा उनके उपदेश को न उसमें तक का ही विशेष समावेश हो पाया था। "स्यावाद के प्रमोघ चिन्ह से चिन्हित', बतलाया है।
प्राचार्य गृद्धपिच्छ के तत्वार्थसूत्र मे कुन्दकुन्द द्वारा षटखण्डागम मादि मागमों में यद्यपि स्याद्वाद की प्रदर्शित दर्शन के रूप में कुछ वृद्धि मिलती है। एक तो स्वतंत्र चर्चा नहीं मिलती, फिर भी उनमें सिद्धान्त-प्रति- उन्होंने प्राकृत में सिद्धान्त प्रतिपादन की पुरातन पद्धति पादन "स्यात" (सिया अथवा सिय) शब्द को लेकर को युग के प्रकाश में सस्कृत गद्य सूत्रों में बदल दिया अवश्य प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ षट्खण्डागम में दूसरे, उपपत्ति पूर्वक सिद्धान्तों का निरूपण प्रारम्भ मनुष्यों को पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों बतलाते हुए किया। तीसरे, प्रागम प्रतिपादित ज्ञानमार्गणा गत कहा गया है कि "मणुस्सा.."सिया पज्जत्ता, सिया अप- मत्यादिज्ञानों को प्रमाण संज्ञा देकर उसके प्रत्यक्ष पौर ज्जत्ता अर्थात मनुष्य स्यात् पर्याप्तक है, स्यात् अपर्या- परोक्ष दो भेदों का कथन किया। चौथे दर्शनान्तरो मे प्तक । इसी प्रकार मागम के कुछ दूसरे विषयों का भी पृथक् प्रमाण रूप मे स्वीकृत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान प्रतिपादन उपलब्ध होता है। इस तरह पागम ग्रन्थों मे इन्हें मतिज्ञान और शब्द को श्रुतज्ञान कहकर उनका 'स्यात्' शब्द को लिए हुए विधि और निषेध इन दो 'प्राद्यपरोक्षम्" (त०सू०१-...) सूत्र द्वारा परोक्ष प्रमाण वचन-प्रकारों से कथन मिलता है। प्रा० कुन्दकुन्द ने में समावेश किया। पाँचवे, प्रमाण की तरह नय को भी उक्त दो विधि और निषेध' वचन प्रकारों मे पाँच वचन अधिगम का साधन "प्रमाणनयरधिगम."-१-६) निरूप्रकार और मिलाकर सात वचन प्रकारों से वस्तु 'द्रव्य' पित करके उसके नंगमादि सात भेदो का भी सर्व प्रथम निरूपण का स्पष्ट उल्लेख किया है । यथा
निर्देश किया। इस तरह तत्त्वार्थसूत्रकार ने कितना ही सिय पत्थि णत्थि उहयं अवत्तव्वं पुणोय तत्तिदयं । नया चिन्तन प्रस्तुत किया। इसके अतिक्ति तर्क (युक्तिदव्यं खु सत्तभंग प्रादेसवसेण संभवदि ।।
अनुमान) से सिद्धान्तों के पोषण की दिशा भी प्रदर्शित की -पंचास्ति गा० १४। अवयवत्रय से मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन-सिद्धान्त का साधन' यहाँ 'स्यादस्ति द्रव्यं स्यान्नास्तिद्रव्यं स्यादुभयं स्याद- उनकी ही देन है। इतना होने पर भी दर्शन मे उन वक्तयं स्यादस्त्यवक्तव्यं स्यान्नास्त्यवक्तव्यं स्यादस्ति. एकान्तवादों, सघर्षों और विवादों का स्पष्ट तार्किक समानास्त्यवक्तव्यम्' इन सात भंगों का निर्देश करके उनके धान नहीं आपाया, जो उनके कुछ समय बाद की चर्चा माश्रय से द्रव्य (वस्तु) के कथन का उल्लेख किया गया के विषय हुए। है। ध्यातव्य है कि कुन्दकुन्द ने यहाँ द्रव्य को सप्तभङ्गाः समन्तभद्र के समय की संघर्षशील स्थिति त्मक मादेशवशात् 'नयविवक्षानुसार' प्रतिपादित किया है।
विक्रम की दूसरी से पांचवी शताब्दी का समय दार्शउन्होंने यह भी बताया है कि यदि सद्रूप ही द्रव्य हो
निक क्रान्ति का समय रहा है। इस काल में विभिन्न तो उसका विनाश नहीं हो सकता और यदि असद्रूप ही
दर्शनों में अनेक प्रभावशाली एवं क्रान्तिकारी विद्वान हो तो उसका उत्पाद सम्भव नहीं है और चूंकि यह देखा
हए है । वैदिक और श्रमण दोनों परम्परामों में कणाद, जाता है कि जीव द्रव्य मनुष्य पर्याय से नष्ट, देव पर्याय से उत्पन्न और जीव सामान्य से ध्रुव रहने से वह उत्पाद
गौतम, जैमिनी, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे प्रतिद्वन्दी व्यय ध्रौव्य स्वरूप है।
प्रभावक मनीषियों का आविर्भाव हुआ और ये सभी अपने कुन्दकुन्द के इस प्रतिपादन से प्रतीत होता है कि
अपने मंडन तथा विरोधी के खण्डन में लग गए। शास्त्रार्थों उनके समय में जैन वाङ्मय में दर्शन का रूप तो भाने की धूम मच गयी। मुख्यतया सद्वाद-असद्वाद, शाश्वतवादलगा था, पर उसका अभी विकास नहीं हो सका था और
प्रशाश्वतवाद, अद्वैतवाद-द्वैतवाद और प्रवक्तव्यवाद
वक्तव्यवाद इन विरोधी युगलों को लेकर तत्त्व की चर्चा १ षट्खण्डागम १-१-८६। .२पंचास्तिकायगा०१५,१७।
३. त. सू. १०-५, ६, ७॥