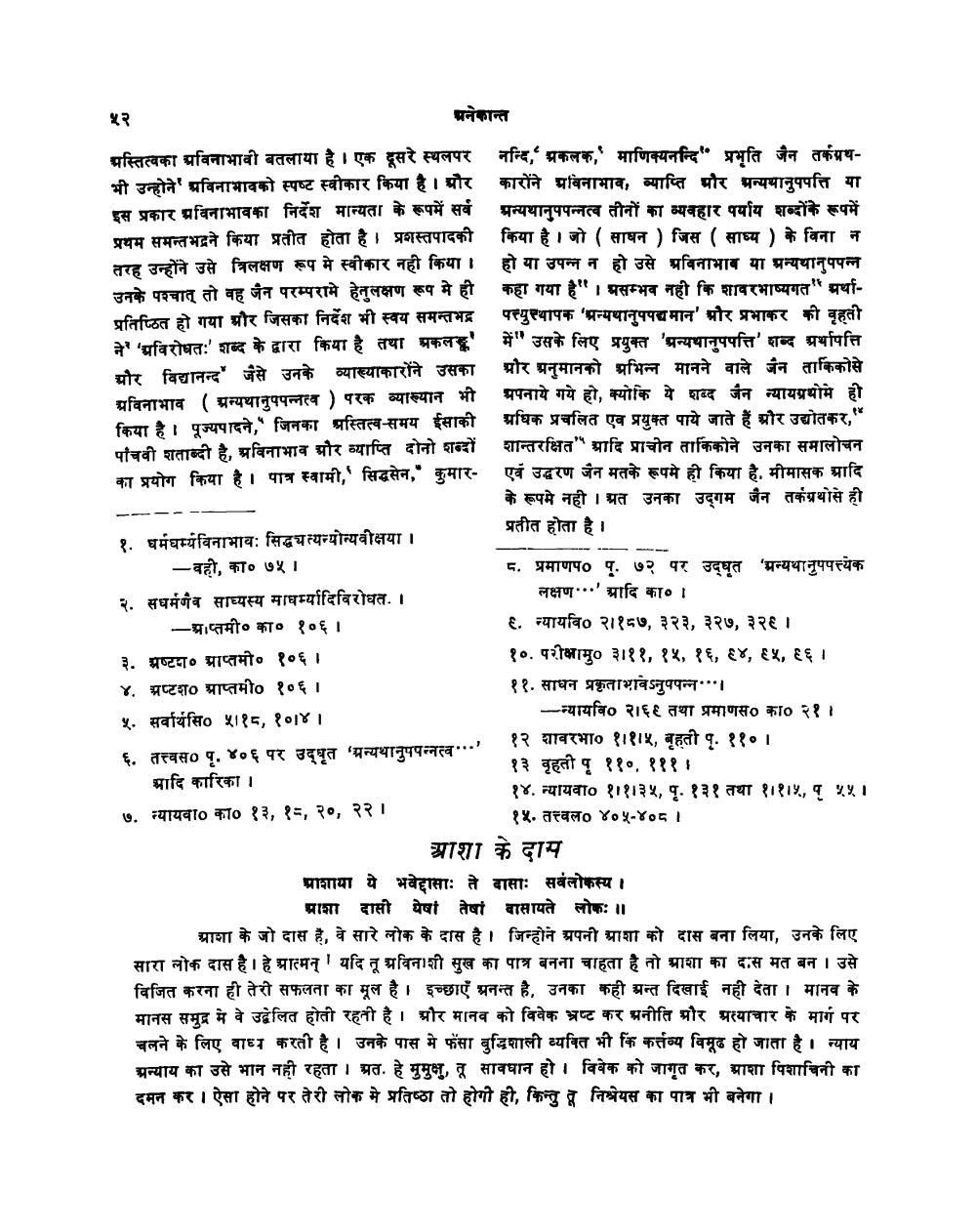________________
अनेकान्त
अस्तित्वका अविनाभावी बतलाया है। एक दूसरे स्थलपर नन्दि, प्रकलक, माणिक्यनन्दि" प्रभति जैन तर्कप्रथभी उन्होने अविनाभावको स्पष्ट स्वीकार किया है। और कारोंने प्रविनाभाव, व्याप्ति और अन्यथानुपपत्ति या इस प्रकार प्रविनाभावका निर्देश मान्यता के रूपमें सर्व अन्यथानुपपन्नत्व तीनों का व्यवहार पर्याय शब्दोंके रूपमें प्रथम समन्तभद्रने किया प्रतीत होता है। प्रशस्तपादकी किया है । जो ( साधन ) जिस ( साध्य ) के विना न तरह उन्होंने उसे विलक्षण रूप मे स्वीकार नहीं किया। हो या उपन्न न हो उसे अविनाभाव या अन्यथानुपपन्न उनके पश्चात् तो वह जैन परम्परामे हेतुलक्षण रूप मे ही कहा गया है"। असम्भव नही कि शावरभाष्यगत"मर्थाप्रतिष्ठित हो गया और जिसका निर्देश भी स्वय समन्तभद्र पत्युस्थापक 'अन्यथानुपपद्यमान' और प्रभाकर की वृहती
'विरोधतः' शब्द के द्वारा किया है तथा प्रकलङ्क' में" उसके लिए प्रयुक्त 'अन्यथानुपपत्ति' शब्द अर्थापत्ति और विद्यानन्द' जैसे उनके व्याख्याकारोंने उसका और अनुमानको अभिन्न मानने वाले जैन तार्किकोसे अविनाभाव ( अन्यथानुपपन्नत्व) परक व्याख्यान भी अपनाये गये हो, क्योकि ये शब्द जैन न्यायग्रथोमे ही किया है। पूज्यपादने, जिनका अस्तित्व-समय ईसाकी अधिक प्रचलित एवं प्रयुक्त पाये जाते हैं और उद्योतकर," पांचवी शताब्दी है, अविनाभाव और व्याप्ति दोनो शब्दों शान्तरक्षित" आदि प्राचीन तार्किकोने उनका समालोचन का प्रयोग किया है। पात्र स्वामी, सिद्धसेन,' कुमार एवं उद्धरण जैन मतके रूपमे ही किया है. मीमासक आदि
के रूपमे नही । अत उनका उद्गम जैन तर्कग्रथोसे ही - - --
प्रतीत होता है। १. धर्मघयविनाभावः सिद्धयत्यन्योन्यवीक्षया । -वही, का० ७५ ।
८. प्रमाणप० पु. ७२ पर उद्घत 'मन्यथानुपपत्त्येक २. सधर्मणव साध्यस्य माधादिविरोधत. ।
लक्षण...' आदि का। -प्राप्तमी० का० १०६ ।
६. न्यायवि० २।१८७, ३२३, ३२७, ३२६ । ३. अष्टग प्राप्तमी० १०६ ।
१०. परीक्षामु० ३।११, १५, १६, ६४, ६५, ६६ । ४. अप्टश प्राप्तमी० १०६ ।
११. साधन प्रकृताभावऽनुपपन्न। ५. सर्वार्थसि० ५।१८, १०।४।
-न्यायवि० २०६६ तथा प्रमाणस० का० २१ ।
., १२ शावरभा० १११५, बृहती पृ. ११० । ६. तत्त्वस० पृ. ४०६ पर उद्धृत 'अन्यथानुपपन्नत्व""
१३ वृहती पृ ११०, १११ । आदि कारिका ।
१४. न्यायवा० ११२३५, पृ. १३१ तथा १।११५, पृ ५५ । ७. न्यायवा० का० १३, १८, २०, २२ ।
१५. तत्त्वल० ४०५-४०८ ।
आशा के दाय प्राशाया ये भवेद्दासाः ते दासाः सर्वलोकस्य ।
पाशा दासी येषां तेषां वासायते लोकः ॥ आशा के जो दास है, वे सारे लोक के दास है। जिन्होंने अपनी पाशा को दास बना लिया, उनके लिए सारा लोक दास है । हे पात्मन् । यदि तू अविनाशी सुख का पात्र बनना चाहता है तो प्राशा का दास मत बन । उसे विजित करना ही तेरी सफलता का मूल है। इच्छाएँ अनन्त है, उनका कही अन्त दिखाई नहीं देता। मानव के मानस समुद्र में वे उद्वेलित होती रहती है। और मानव को विवेक भ्रष्ट कर अनीति और अत्याचार के मार्ग पर चलने के लिए वाध करती है। उनके पास में फंसा बुद्धिशाली व्यक्ति भी कि कर्तव्य विमूढ हो जाता है। न्याय अन्याय का उसे भान नहीं रहता। प्रत. हे मुमुक्षु, तू सावधान हो। विवेक को जागृत कर, आशा पिशाचिनी का दमन कर । ऐसा होने पर तेरी लोक मे प्रतिष्ठा तो होगी ही, किन्तु तू निश्रेयस का पात्र भी बनेगा।