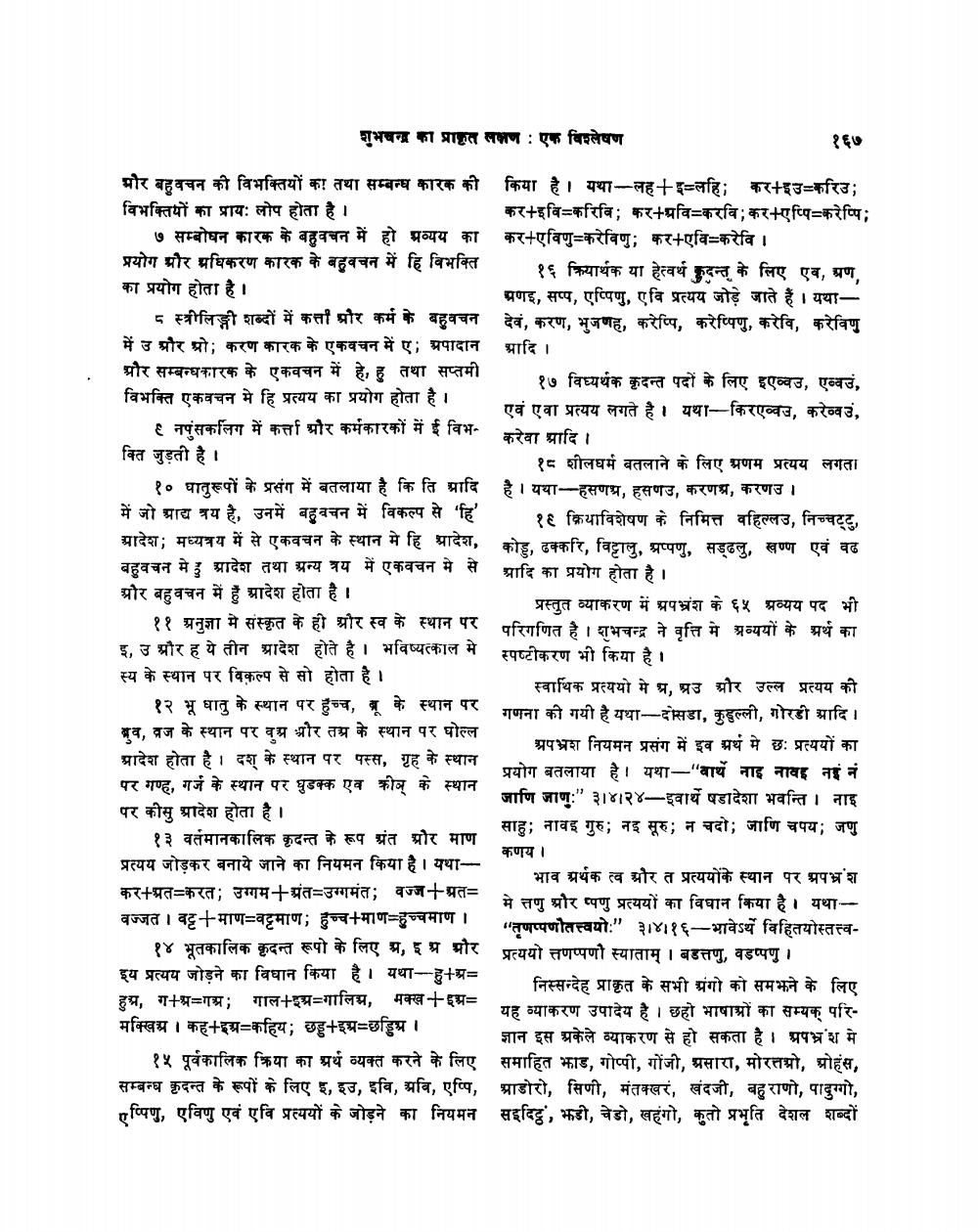________________
शुभचन्द्र का प्राकृत लक्षण : एक विश्लेषण
१६७
मौर बहुवचन की विभक्तियों का तथा सम्बन्ध कारक की किया है। यथा-लह+इ-लहिः कर+इउ-करिउ; विभक्तियों का प्रायः लोप होता है।
___ कर+इवि-करिवि ; कर+प्रवि-करवि; कर+एप्पि-करेप्पि; ७ सम्बोधन कारक के बहुवचन में हो अव्यय का कर+एविणु-करेविणु; कर+एविकरेवि । प्रयोग और अधिकरण कारक के बहुवचन में हि विभक्ति
१६ क्रियार्थक या हेत्वर्थ कुदन्त के लिए एव, अण का प्रयोग होता है।
प्रणइ, सप्प, एप्पिणु, एवि प्रत्यय जोड़े जाते हैं । यथा८ स्त्रीलिङ्गी शब्दों में कर्ता और कर्म के बहुवचन देवं, करण, भुजणह, करेप्पि, करेप्पिणु, करेवि, करेविणु में उ और प्रो; करण कारक के एकवचन में ए; अपादान आदि । और सम्बन्धकारक के एकवचन में हे, हु तथा सप्तमी
१७ विध्यर्थक कृदन्त पदों के लिए इएव्वउ, एव्वलं, विभक्ति एकवचन मे हि प्रत्यय का प्रयोग होता है।
एवं एवा प्रत्यय लगते है। यथा-किरएव्वउ, करेव्वउ, ___ नपुंसकलिंग में कर्ता और कर्मकारकों में ई विभ
• करेवा प्रादि। क्ति जुड़ती है।
१८ शीलधर्म बतलाने के लिए अणम प्रत्यय लगता १० धातुरूपों के प्रसंग में बतलाया है कि ति प्रादि है। यथा-हसणग्र, हसणउ, करण, करणउ । में जो प्राद्य त्रय है, उनमें बहुवचन में विकल्प से "हि
किया विशेष निमिन टिल आदेश; मध्यत्रय में से एकवचन के स्थान मे हि प्रादेश, कोड, ढक्करि, विट्टालु, अप्पणु, सड्ढलु, खण्ण एवं बढ बहवचन मेड प्रादेश तथा अन्य त्रय में एकवचन मे से प्राटि का प्रयोग होता और बहुवचन में हैं आदेश होता है।
प्रस्तुत व्याकरण में अपभ्रंश के ६५ अव्यय पद भी ११ अनज्ञा मे संस्कृत के ही और स्व के स्थान पर परिगणित है।शभचन्द्र ने वत्ति मे अव्ययों के अर्थ का इ, उ और ह ये तीन आदेश होते है। भविष्यत्काल में स्पष्टीकरण भी किया है। स्य के स्थान पर विकल्प से सो होता है।
स्वार्थिक प्रत्ययो मे अ, अउ और उल्ल प्रत्यय की १२ भू धातु के स्थान पर हुँच्च, ब्रू के स्थान पर
गणना की गयी है यथा-दोसडा, कुडल्ली, गोरडी आदि । बुव, व्रज के स्थान पर वन और तप के स्थान पर घोल्ल
अपभ्रश नियमन प्रसंग में इव अर्थ मे छ: प्रत्ययों का आदेश होता है। दश् के स्थान पर पस्स, गृह के स्थान
प्रयोग बतलाया है। यथा-"वार्थे नाइ नावह नई नं पर गण्ह, गर्ज के स्थान पर धुडक्क एव कीञ् के स्थान
जाणि जाणुः" ३।४।२४-इवार्थे षडादेशा भवन्ति । नाइ पर कीसु प्रादेश होता है।
साहु; नावइ गुरु; नइ सूरु; न चदो; जाणि चपय; जणु १३ वर्तमानकालिक कृदन्त के रूप अंत और माण
कणय। प्रत्यय जोड़कर बनाये जाने का नियमन किया है। यथा
भाव अर्थक त्व और त प्रत्ययोंके स्थान पर अपभ्रंश कर+प्रत-करत; उग्गम+अंत-उग्गमंत; वज्ज+प्रत=
मे तणु और प्पणु प्रत्ययों का विधान किया है। यथावज्जत । बट्ट+माण वट्टमाण; हुँच्च+माण हुँच्चमाण ।
"तृणप्पणीतत्त्वयोः" ३।४।१६-भावेऽर्थे विहितयोस्तत्त्व१४ भतकालिक कृदन्त रूपो के लिए अहम भोर प्रत्ययो त्तणप्पणौ स्याताम् । बडत्तणु, वडप्पणु । इय प्रत्यय जोड़ने का विधान किया है। यथा-हु+प्र=
निस्सन्देह प्राकृत के सभी अंगो को समझने के लिए हुअ, ग+प्रगगाल+इअगालिन, मक्ख+इ=
यह व्याकरण उपादेय है । छहो भाषाओं का सम्यक् परिमक्खिय। कह+इ=कहिय; छड्ड+इप्र-छड्डिप्र ।।
ज्ञान इस अकेले व्याकरण से हो सकता है। अपभ्रश मे १५ पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ व्यक्त करने के लिए समाहित झाड, गोप्पी, गोंजी, प्रसारा, मोरत्तो, मोहंस, सम्बन्ध कृदन्त के रूपों के लिए इ, इउ, इवि, अवि, एप्पि, प्राडोरो, सिणी, मंतक्खरं, खंदजी, बहुराणो, पादुग्गो, प्पिणु, एविणु एवं एवि प्रत्ययों के जोड़ने का नियमन सइदिट्ठ, झडी, चेडो, खहंगो, कुतो प्रभृति देशल शब्दों