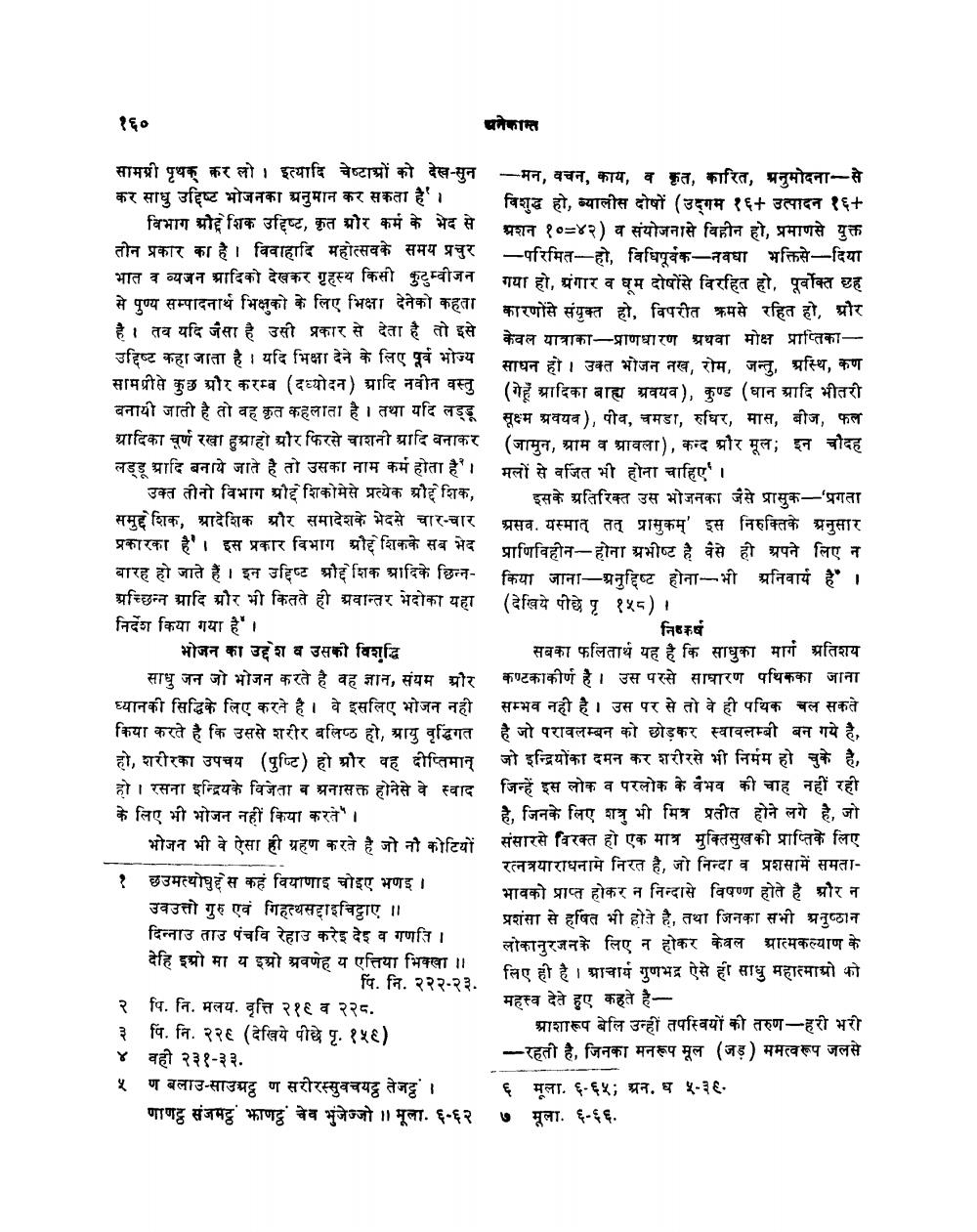________________
१६०
अनेकान्त
सामग्री पृथक कर लो। इत्यादि चेष्टाओं को देख-सुन -मन, वचन, काय, व कृत, कारित, अनुमोदना-से कर साधु उद्दिष्ट भोजनका अनुमान कर सकता है। विशुद्ध हो, ब्यालीस दोषों (उद्गम १६+ उत्पादन १६+
विभाग भौशिक उद्दिष्ट, कृत और कर्म के भेद से प्रशन १०४२) व संयोजनासे विहीन हो, प्रमाणसे युक्त तीन प्रकार का है। विवाहादि महोत्सवके समय प्रचुर -परिमित-हो, विधिपूर्वक-नवधा भक्तिसे-दिया भात व व्यजन आदिको देखकर गृहस्थ किसी कुटुम्वाजन गया हो, अंगार व घूम दोषोंसे विरहित हो, पूर्वोक्त छह से पुण्य सम्पादनार्थ भिक्षुको के लिए भिक्षा देनेको कहता
कारणोंसे संयुक्त हो, विपरीत क्रमसे रहित हो, और है। तब यदि जैसा है उसी प्रकार से देता है तो इसे
केवल यात्राका-प्राणधारण अथवा मोक्ष प्राप्तिकाउद्दिष्ट कहा जाता है। यदि भिक्षा देने के लिए पूर्व भोज्य
दिन क लिए पूर्व भाज्य साधन हो। उक्त भोजन नख, रोम, जन्तु, अस्थि, कण सामग्रास कुछ और करम्ब (दध्यादन) आदि नवान वस्तु (गेहूँ आदिका बाह्य अवयव), कुण्ड (धान आदि भीतरी
या जाता है ता वह कृत कहलाता ह । तथा याद ला सूक्ष्म अवयव), पीव, चमडा, रुधिर, मास, बीज, फल अादिका चूर्ण रखा हुअाहो और फिरसे चाशनी आदि बनाकर (जामुन, आम व पावला), कन्द और मूल; इन चौदह लड्डू प्रादि बनाये जाते है तो उसका नाम कर्म होता है। मलों से वजित भी होना चाहिए।
उक्त तीनो विभाग प्रौद्देशिकोमेसे प्रत्येक प्रौद्देशिक, इसके अतिरिक्त उस भोजनका जैसे प्रासुक-'प्रगता समूह शिक, प्रादेशिक और समादेशके भेदसे चार-चार प्रसव. यस्मात् तत् प्रासुकम्' इस निरुक्तिके अनुसार प्रकारका है। इस प्रकार विभाग प्रौद्द शिकके सब भेद प्राणिविहीन-होना अभीष्ट है वैसे ही अपने लिए न बारह हो जाते हैं । इन उद्दिष्ट अोद्द शिक प्रादिके छिन्न- किया जाना—अनहिष्ट होना भी अनिवार्य है । अस्छिन्न आदि और भी कितते ही अवान्तर भेदोका यहा (देखिये पीछे ए १५८)। निर्देश किया गया है।
निष्कर्ष भोजन का उद्देश व उसको विशुद्धि
सबका फलितार्थ यह है कि साधुका मार्ग अतिशय साधु जन जो भोजन करते है वह ज्ञान, संयम और कण्टकाकीर्ण है। उस परसे साधारण पथिकका जाना ध्यानकी सिद्धि के लिए करते है। वे इसलिए भोजन नही सम्भव नही है। उस पर से तो वे ही पथिक चल सकते किया करते है कि उससे शरीर बलिष्ठ हो, आयु वृद्धिंगत है जो परावलम्बन को छोड़कर स्वावलम्बी बन गये है, हो, शरीरका उपचय (पुष्टि) हो और वह दीप्तिमान् जो इन्द्रियोंका दमन कर शरीरसे भी निर्मम हो चुके है, हो । रसना इन्द्रियके विजेता व अनासक्त होनेसे वे स्वाद जिन्हें इस लोक व परलोक के वैभव की चाह नहीं रही के लिए भी भोजन नहीं किया करते।
है, जिनके लिए शत्रु भी मित्र प्रतीत होने लगे है, जो भोजन भी वे ऐसा ही ग्रहण करते है जो नौ कोटियों संसारसे विरक्त हो एक मात्र मुक्तिसुखकी प्राप्तिके लिए
रत्नत्रयाराधनामे निरत है, जो निन्दा व प्रशसामें समताछउमत्थोघुद्देस कहं वियाणाइ चोइए भणइ ।
भावको प्राप्त होकर न निन्दासे विषण्ण होते है और न उवउत्तो गुरु एवं गिहत्थसद्दाइचिट्ठाए ।
प्रशंसा से हर्षित भी होते है, तथा जिनका सभी अनुष्ठान दिन्नाउ ताउ पंचवि रेहाउ करेइ देइ व गणति ।
लोकानुरजनके लिए न होकर केवल प्रात्मकल्याण के देहि इम्रो मा य इमो अवणेह य एत्तिया भिक्खा ॥
लिए ही है। प्राचार्य गुणभद्र ऐसे ही साधु महात्मामो को
पिं. नि. २२२-२३. २ पि. नि. मलय. वृत्ति २१६ व २२८.
महस्व देते हुए कहते है३ पि. नि. २२६ (देखिये पीछे पृ. १५६)
आशारूप बेलि उन्हीं तपस्वियों की तरुण-हरी भरी ४ वही २३१-३३.
-रहती है, जिनका मनरूप मूल (जड़) ममत्वरूप जलसे ५ ण बलाउ-साउट्ठ ण सरीरस्सुवचय? तेजट्ट। ६ मूला. ६.६५; अन. ध ५-३६.
णाणट्ठ संजमट्ठ भाणटुं चेव भुंजेज्जो ॥ मूला. ६.६२ ७ मूला. ६-६६.