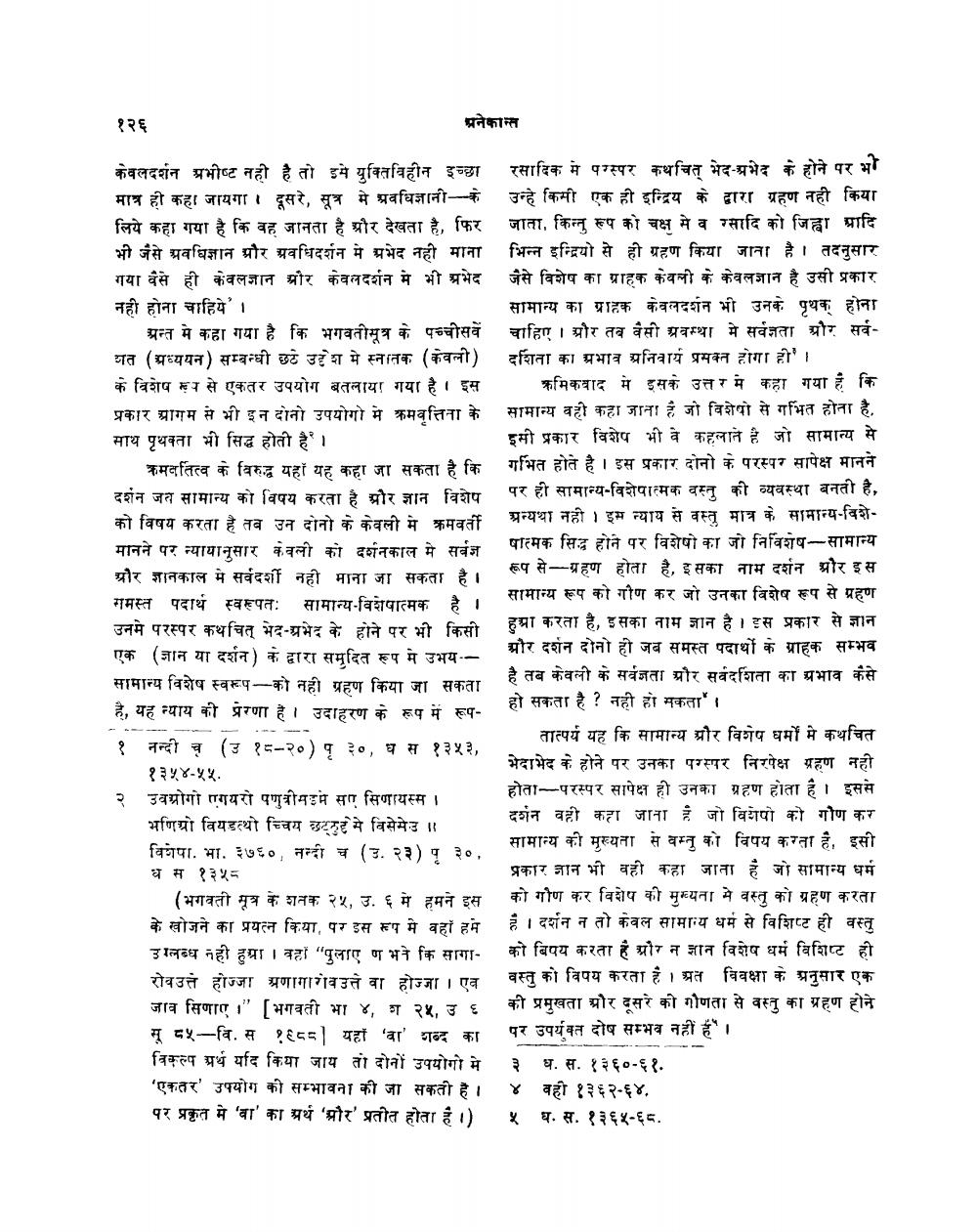________________
१२६
अनेकान्त
केवलदर्शन अभीष्ट नही है तो इसे युक्तिविहीन इच्छा रसादिक में परस्पर कथचित् भेद-अभेद के होने पर भी मात्र ही कहा जायगा। दूसरे, सूत्र मे अवधिज्ञानी-के उन्हे किमी एक ही इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया लिये कहा गया है कि वह जानता है और देखता है, फिर जाता, किन्तु रूप को चक्ष मे व रसादि को जिह्वा प्रादि भी जैसे अवधिज्ञान और अवधिदर्शन में अभेद नही माना भिन्न इन्द्रियो से ही ग्रहण किया जाता है। तदनुसार गया वैसे ही केवलज्ञान और केवलदर्शन में भी अभेद जैसे विशेष का ग्राहक केवली के केवलज्ञान है उसी प्रकार नहीं होना चाहिये।
सामान्य का ग्राहक केवलदर्शन भी उनके पृथक् होना अन्त में कहा गया है कि भगवतीसूत्र के पच्चीसवें चाहिए । और तब वैसी अवस्था मे सर्वज्ञता और सर्वगत (अध्ययन) सम्बन्धी छठे उद्देश मे स्नातक (केवली) दर्शिता का प्रभाव अनिवार्य प्रसक्त होगा ही। के विशेष रूप से एकतर उपयोग बतलाया गया है । इस क्रमिकबाद में इसके उत्तर में कहा गया है कि प्रकार प्रागम से भी इन दोनो उपयोगो में क्रमवत्तिता के सामान्य वही कहा जाता है जो विशेषो से गभित होता है, साथ पृथक्ता भी सिद्ध होती है।
इसी प्रकार विशेष भी वे कहलाते है जो सामान्य से क्रमदतित्व के विरुद्ध यहाँ यह कहा जा सकता है कि गभित होते है। इस प्रकार दोनो के परस्पर सापेक्ष मानने दशन जव सामान्य को विषय करता है और ज्ञान विशेष पर हा सामान्य-विशेषात्मक वस्तु की व्यवस्था बनता ह, को विषय करता है तब उन दोनो के केवली में क्रमवर्ती
अन्यथा नही । इम न्याय से वस्तु मात्र के सामान्य-विशेमानने पर न्यायानमार वलीको नाम षात्मक सिद्ध होने पर विशेषो का जो निविशेष-सामान्य और ज्ञानकाल मे सर्वदर्शी नही माना जा सकता है।
रूप से-ग्रहण होता है, इसका नाम दर्शन और इस गमस्त पदार्थ स्वरूपतः सामान्य विशेषात्मक है ।।
सामान्य रूप को गीण कर जो उनका विशेष रूप से ग्रहण उनमे परस्पर कथचित् भेद-अभेद के होने पर भी किसी
हमा करता है, इसका नाम ज्ञान है। इस प्रकार से ज्ञान एक (ज्ञान या दर्शन) के द्वारा समृदित रूप में उभय--
और दर्शन दोनो ही जब समस्त पदार्थों के ग्राहक सम्भव सामान्य विशेष स्वरूप-को नही ग्रहण किया जा सकता
है तब केवली के सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता का प्रभाव कैसे है, यह न्याय की प्रेरणा है। उदाहरण के रूप में रूप
हो सकता है ? नहीं हो सकता। १ नन्दी च (उ १८-२०)पृ ३०, घ स १३५३,
___ तात्पर्य यह कि सामान्य और विशेष धर्मों में कथचित
भेदाभेद के होने पर उनका परस्पर निरपेक्ष ग्रहण नही १३५४-५५. उवनोगो गयरो पणुवीमइमे सा सिणायस्स ।
होता-परस्पर सापेक्ष ही उनका ग्रहण होता है। इससे भणियो वियडत्थो च्चिय छठु मे विसेमे उ ।।
दर्शन वही कहा जाता है जो विगंपो को गौण कर विशेषा. भा. ३७६०, नन्दी च (उ. २३) पू ३०,
सामान्य की मुख्यता से वस्तु को विषय करता है, इसी ध स १३५६
प्रकार ज्ञान भी वही कहा जाता है जो सामान्य धर्म (भगवती मूत्र के शतक २५, उ. ६ में हमने इस को गोण कर विशेष की मुम्यता मे वस्तु को ग्रहण करता के खोजने का प्रयत्न किया, पर इस रूप में वहाँ हमे है । दर्शन न तो केवल सामान्य धर्म से विशिष्ट ही वस्तू उपलब्ध नही हया । वहाँ "पूलाए ण भने कि सागा- को बिपय करता है और न ज्ञान विशेष धर्म विशिष्ट ही रोव उत्तं होज्जा प्रणागागंव उत्ते वा होज्जा । एव वस्तु को विपय करता है । अत विवक्षा के अनुसार एक जाव सिणाए।" [भगवती भा ४, २५, उ ६ की प्रमुखता और दूसरे को गौणता से वस्तु का ग्रहण होने सू ८५-वि. स १९८८] यहाँ 'वा' शब्द का पर उपयुक्त दोष सम्भव नहीं हैं। विकल्प अर्थ यदि किया जाय तो दोनों उपयोगो मे ३ घ. स. १३६०-६१. 'एकतर' उपयोग की सम्भावना की जा सकती है। ४ वही १३६२-६४. पर प्रकृत मे 'वा' का अर्थ 'और' प्रतीत होता है।) ५ घ. स. १३६५-६८.