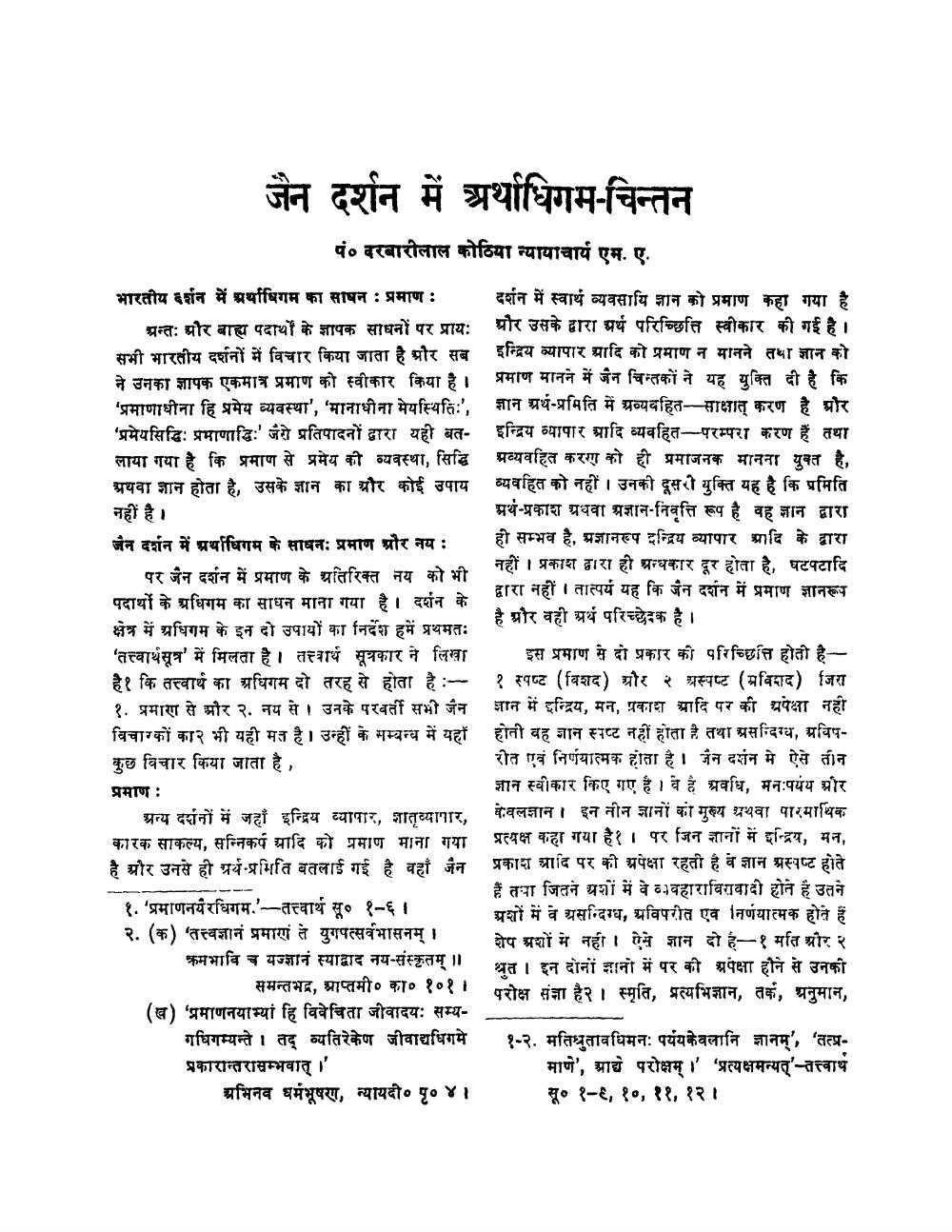________________
जैन दर्शन में अर्थाधिगम-चिन्तन
पं० दरबारीलाल कोठिया न्यायाचार्य एम. ए.
भारतीय दर्शन में अर्थाधिगम का साधन : प्रमाण :
अन्तः और बाह्य पदार्थों के ज्ञापक साधनों पर प्रायः सभी भारतीय दर्शनों में विचार किया जाता है और सब ने उनका ज्ञापक एकमात्र प्रमाण को स्वीकार किया है । 'प्रमाणाधीना हि प्रमेय व्यवस्था', 'मानाधीना मेयस्थितिः', 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाडि' जैसे प्रतिपादनों द्वारा यही बत लाया गया है कि प्रमाण से प्रमेय की व्यवस्था, सिद्धि अथवा ज्ञान होता है, उसके ज्ञान का और कोई उपाय नहीं है।
जैन दर्शन में अर्थाधिगम के साधनः प्रमाण और नय :
पर जैन दर्शन में प्रमाण के अतिरिक्त नय को भी पदार्थों के अधिगम का साधन माना गया है । दर्शन के क्षेत्र में अधिगम के इन दो उपायों का निर्देश हमें प्रथमतः 'तत्त्वार्थ सूत्र' में मिलता है । तत्त्वार्थ सूत्रकार ने लिखा है कि तत्त्वार्थ का अधिगम दो तरह से होता है १. प्रमारण से और २. नय से । उनके परवर्ती सभी जैन विचारकों का भी यही मत है उन्हीं के सम्बन्ध में यहाँ कुछ विचार किया जाता है,
प्रमाण :
अन्य दर्शनों में जहाँ पद्रिय व्यापार, व्यापार कारक साकल्य, सन्निकर्ष आदि को प्रमाण माना गया है और उनसे ही ग्रर्थ प्रमिति बतलाई गई है वहाँ जैन
१. 'प्रमाणनयेरधिगम तत्त्वार्थ सू० १-६। २. (क) 'तत्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम् ।
*मभावि च यज्ञानं स्याद्वाद नय-संस्कृतम् ॥ समन्तभद्र, प्राप्तमी० का० १०१ । (ख) प्रमाणनयाभ्यां हि विवेचिता जीवादयः सम्प गधिगम्यन्ते । तद् व्यतिरेकेण जीवाद्यधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात् ।'
अभिनव धर्मभूषण, न्यायदी० पृ० ४।
दर्शन में स्वार्थ व्यवसायि ज्ञान को प्रमाण कहा गया है और उसके द्वारा अर्थ परिच्छित्ति स्वीकार की गई है। इन्द्रिय व्यापार आदि को प्रमाण न मानने तथा ज्ञान को प्रमाण मानने में जैन चिन्तकों ने यह युक्ति दी है कि ज्ञान अर्थ- प्रमिति में अव्यवहित- साक्षात् करण है और इन्द्रिय व्यापार आदि व्यवहितपरम्परा करण हैं तथा मव्यवहित करण को ही प्रमाजनक मानना युक्त है, दहित को नहीं। उनकी दूसरी मुक्ति यह है कि प्रमिति अर्थ- प्रकाश अथवा अज्ञान-निवृत्ति रूप है वह ज्ञान द्वारा ही सम्भव है, प्रज्ञानरूप दन्द्रिय व्यापार आदि के द्वारा नहीं । प्रकाश द्वारा ही अन्धकार दूर होता है, घटपटादि द्वारा नहीं । तात्पर्य यह कि जैन दर्शन में प्रमाण ज्ञानरूप है और वही सर्व परिच्छेदक है।
इस प्रमाण से दो प्रकार की परिहित होती है१ स्पष्ट ( विशद ) और २ स्पष्ट (मविदाद) जिरा ज्ञान में इन्द्रिय, मन, प्रकाश आदि पर की अपेक्षा नही होती वह ज्ञान पष्ट नहीं होता है तथा असन्दिग्ध, मविप रीत एवं निर्णयात्मक होता है। जैन दर्शन में ऐसे तीन ज्ञान स्वीकार किए गए हैं। ये अवधि मन:पर्यय मौर केवलज्ञान । इन तीन ज्ञानों की मुख्य अथवा पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा गया है । पर जिन ज्ञानों में इन्द्रिय, मन, प्रकाश आदि पर की अपेक्षा रहती है व ज्ञान असष्ट होते हैं तथा जितने यों में वे व्यवहाराविरावादी होते हैं उसने शों में वे सन्दिग्ध, प्रविपरीत एव निर्णयात्मक होते हैं। शेष अशों में नहीं। ये ज्ञान दो-१ मति और २ श्रुत। इन दोनों ज्ञानों में पर की अपेक्षा होने से उनकी परोक्ष संज्ञा है२ । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, धनुमान,
१-२ मतिश्रुतावधिमनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्', 'तत्प्रमाणे', आद्ये परोक्षम् ' 'प्रत्यक्षमन्यत्तस्या सू० १-२, १०, ११, १२ ।