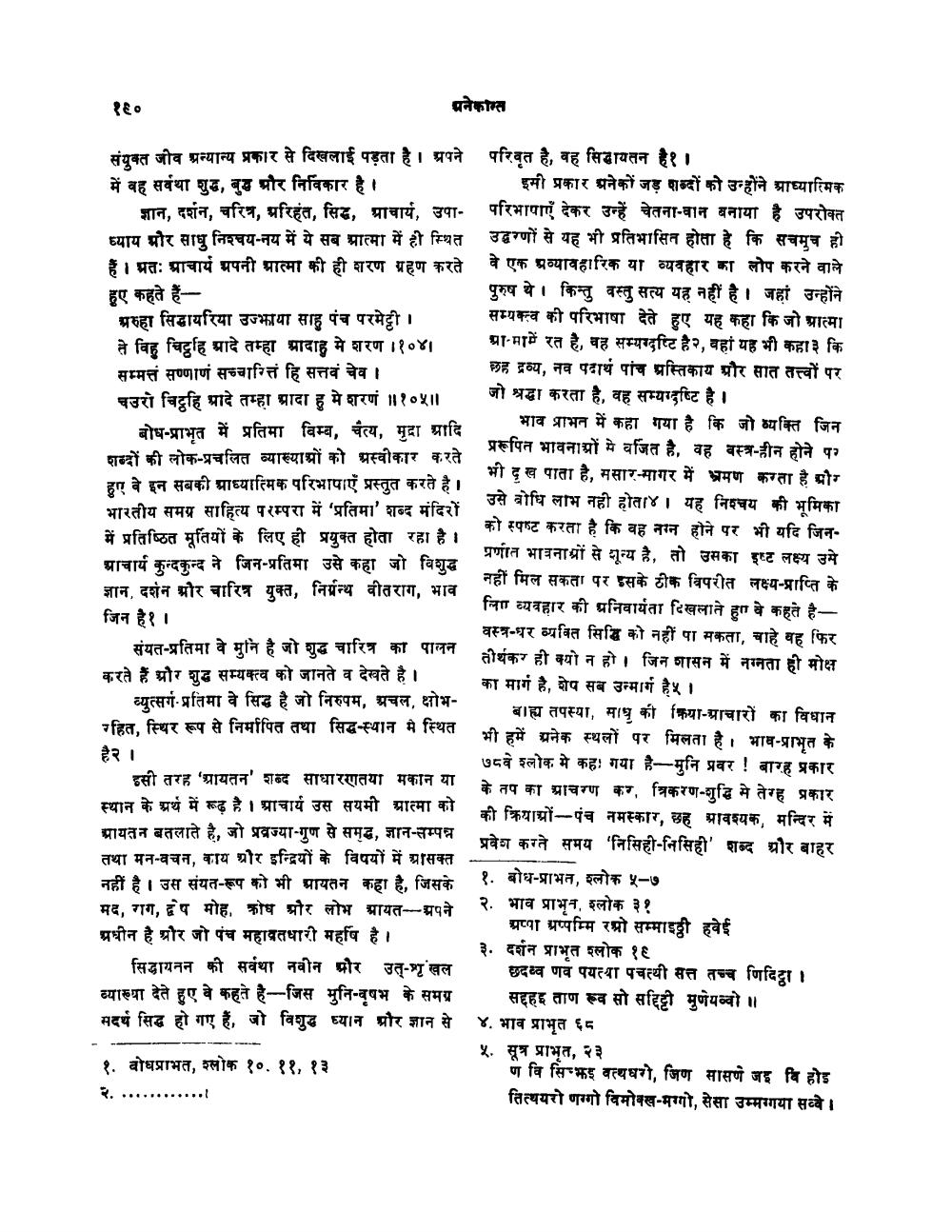________________
१६०
अनेकान्त
संयुक्त जीव अन्यान्य प्रकार से दिखलाई पड़ता है। अपने परिवृत है, वह सिखायतन है। में वह सर्वथा शुद्ध, बुद्ध और निर्विकार है।
इसी प्रकार अनेकों जड़ शब्दों को उन्होंने प्राध्यात्मिक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, अरिहंत, सिद्ध, प्राचार्य, उपा- परिभाषाएँ देकर उन्हें चेतना-वान बनाया है उपरोक्त ध्याय और साधु निश्चय-नय में ये सब प्रात्मा में ही स्थित उद्धरणों से यह भी प्रतिभासित होता है कि सचमुच ही हैं। प्रतः प्राचार्य अपनी आत्मा की ही शरण ग्रहण करते वे एक अव्यावहारिक या व्यवहार का लोप करने वाले हुए कहते हैं
पुरुष थे। किन्तु वस्तु सत्य यह नहीं है। जहां उन्होंने प्राहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेट्टी। सम्यक्त्व की परिभाषा देते हए यह कहा कि जो प्रात्मा ते विह चिहि प्रादे तम्हा प्रादाहु मे शरण ।१०४।
प्रा-मामें रत है, वह सम्यग्दष्टि है २, वहां यह भी कहा कि सम्मत्तं सण्णाणं सच्चारित्तं हि सत्तवं चेव ।
छह द्रव्य, नव पदार्थ पांच प्रस्तिकाय और सात तत्त्वों पर चउरो चिट्ठहि प्रादे तम्हा प्रादा हु मे शरणं ॥१०॥ जो श्रद्धा करता है, वह सम्यग्दष्टि है।
भाव प्राभत में कहा गया है कि जो व्यक्ति जिन बोध-प्राभूत में प्रतिमा बिम्ब, चैत्य, मुद्रा आदि
प्ररूपित भावनाओं मे वजित है, वह वस्त्र-हीन होने पर शब्दों की लोक-प्रचलित व्याख्याओं को अस्वीकार करते
भी दुख पाता है, मसार-मागर में भ्रमण करता है और हए वे इन सबकी प्राध्यात्मिक परिभाषाएँ प्रस्तुत करते है।
उसे बोधि लाभ नही होता४। यह निश्चय की भूमिका भारतीय समग्र साहित्य परम्परा में 'प्रतिमा' शब्द मंदिरों
को स्पष्ट करता है कि वह नग्न होने पर भी यदि जिनमें प्रतिष्ठित मूर्तियों के लिए ही प्रयुक्त होता रहा है।
प्रणीत भावनामों से शून्य है, तो उसका इष्ट लक्ष्य उमे प्राचार्य कुन्दकुन्द ने जिन-प्रतिमा उसे कहा जो विशुद्ध
नहीं मिल सकता पर इसके ठीक विपरीत लक्ष्य-प्राप्ति के ज्ञान, दर्शन और चारित्र युक्त, निम्रन्थ वीतराग, भाव
लिा व्यवहार की अनिवार्यता दिखलाते हुए वे कहते हैजिन है।
वस्त्र-धर व्यक्ति सिद्धि को नहीं पा मकता, चाहे वह फिर संयत-प्रतिमा वे मुनि है जो शुद्ध चारित्र का पालन
तीर्थकर ही क्यो न हो। जिन शासन में नग्नता ही मोक्ष करते हैं और शुद्ध सम्यक्त्व को जानते व देखते है।
का मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है५ । व्युत्सर्ग-प्रतिमा वे सिद्ध है जो निरुपम, अचल, क्षोभ
बाह्य तपस्या, माधु की क्रिया-पाचारों का विधान रहित, स्थिर रूप से निर्मापित तथा सिद्ध-स्थान में स्थित
भी हमें अनेक स्थलों पर मिलता है। भाव-प्राभूत के है२ ।
७८वे श्लोक मे कहा गया है-मुनि प्रवर ! बारह प्रकार इसी तरह 'पायतन' शब्द साधारणतया मकान या
के तप का प्राचरण कर, त्रिकरण-शुद्धि मे तेरह प्रकार स्थान के अर्थ में रूढ़ है। प्राचार्य उस सयमी आत्मा को
की क्रियाओं-पंच नमस्कार, छह प्रावश्यक, मन्दिर में आयतन बतलाते है, जो प्रव्रज्या-गुण से समृद्ध, ज्ञान-सम्पन्न
प्रवेश करते समय 'निसिही-निसिही' शब्द और बाहर तथा मन-वचन, काय और इन्द्रियों के विषयों में प्रासक्त नहीं है। उस संयत-रूप को भी पायतन कहा है. जिसके १. बोध-प्राभत, श्लोक ५-७ मद, गग, द्वेष मोह, क्रोध और लोभ आयत-अपने २. भाव प्राभन, श्लोक ३१
अप्पा अप्पम्मि रमो सम्माइठ्ठी हवेई अधीन है और जो पंच महाव्रतधारी महर्षि है।
३. दर्शन प्राभूत श्लोक १९ सिद्धायनन की सर्वथा नवीन और उत्-शृखल छदव्व णव पयत्या पचत्यी सत्त तच्च णिदिट्ठा। व्याख्या देते हुए वे कहते है-जिस मुनि-वषभ के समग्र सद्दहइ ताण रूव सो सट्टिी मुणयन्वो॥ मदर्थ सिद्ध हो गए हैं, जो विशुद्ध ध्यान और ज्ञान से ४. भाव प्राभूत ६८
५. सूत्र प्राभृत, २३ १. बोधप्राभत, श्लोक १०. ११, १३
ण वि सिंन्झइ वत्थधगे, जिण सासणे जइ वि होड तित्थयरोणग्गो विमोक्ख-मग्गो, सेसा उम्मग्गया सव्वे ।