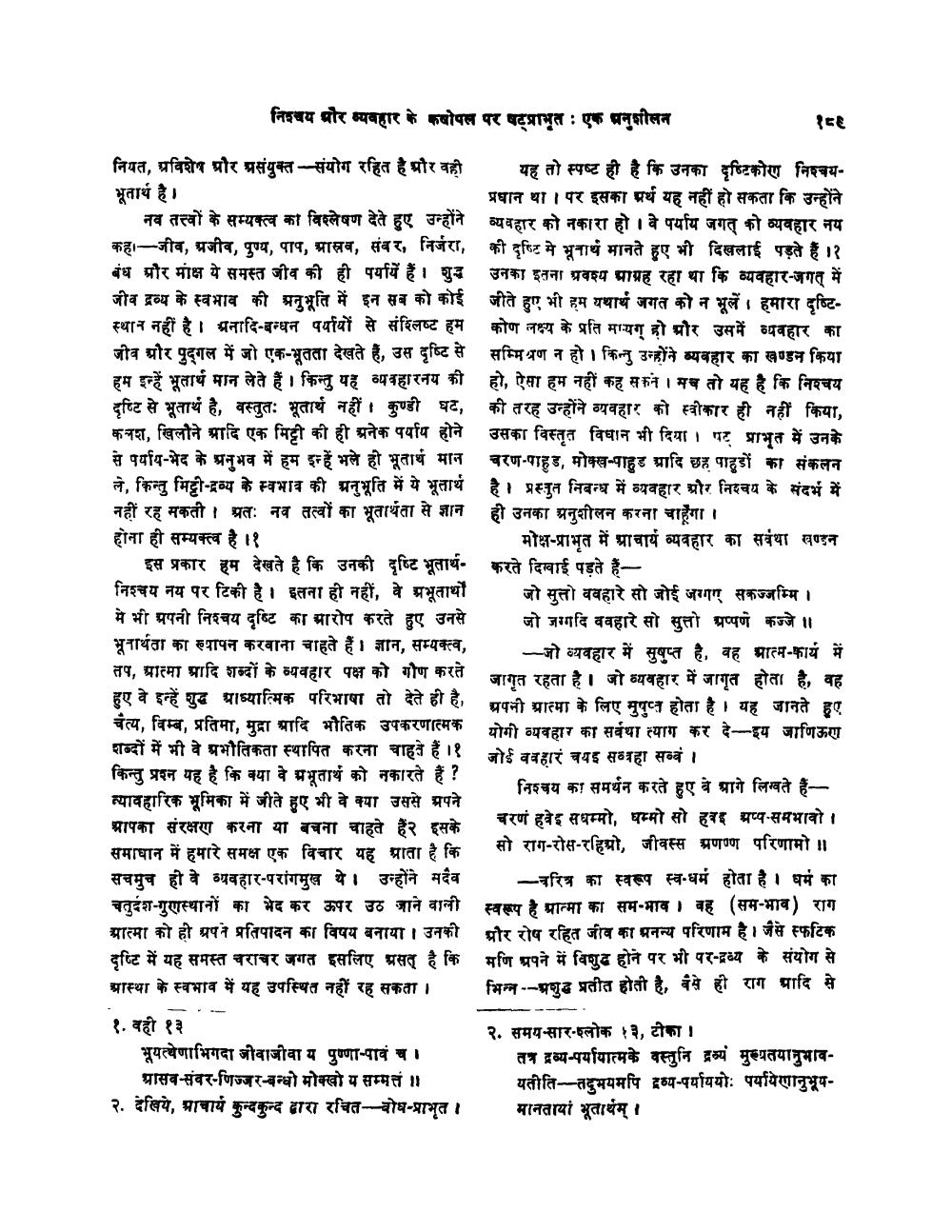________________
निश्चय और व्यवहार के कषोपल पर षट्प्राभूत : एक अनुशीलन
१८६
नियत, प्रविशेष और प्रसंयुक्त-संयोग रहित है और वही यह तो स्पष्ट ही है कि उनका दृष्टिकोण निश्चयभूतार्थ है।
प्रधान था। पर इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उन्होंने नव तत्त्वों के सम्यक्त्व का विश्लेषण देते हुए उन्होंने व्यवहार को नकारा हो । वे पर्याय जगत् को व्यवहार नय कहा-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, पासव, संवर, निर्जरा, की दृष्टि मे भूनार्थ मानते हुए भी दिखलाई पड़ते हैं। बंध और माक्ष ये समस्त जीव की ही पर्यायें हैं। शुद्ध उनका इतना अवश्य प्राग्रह रहा था कि व्यवहार-जगत् में जीव द्रव्य के स्वभाव की अनुभूति में इन सब को कोई जीते हुए भी हम यथार्थ जगत को न भूलें। हमारा दृष्टिस्थान नहीं है। अनादि-बन्धन पर्यायों से संश्लिष्ट हम कोण लक्ष्य के प्रति मायग् हो और उसमें व्यवहार का जीव और पुद्गल में जो एक-भूतता देखते हैं, उस दृष्टि से सम्मिश्रण न हो। किन्तु उन्होंने व्यवहार का खण्डन किया हम इन्हें भूतार्थ मान लेते हैं । किन्तु यह व्यवहारनय की हो, ऐसा हम नहीं कह सकने । मच तो यह है कि निश्चय दृष्टि से भूतार्थ है, वस्तुतः भूतार्थ नहीं। कुण्डी घट, की तरह उन्होंने व्यवहार को स्वीकार ही नहीं किया, कलश, खिलौने आदि एक मिट्टी की ही अनेक पर्याय होने उसका विस्तृत विधान भी दिया। पट प्राभूत में उनके से पर्याय-भेद के अनुभव में हम इन्हें भले ही भूतार्थ मान चरण-पाहुड, मोक्ख-पाहुड आदि छह पाहुडों का संकलन ले, किन्तु मिट्टी-द्रव्य के स्वभाव की अनुभूति में ये भूतार्थ है। प्रस्तुत निबन्ध में व्यवहार और निश्चय के संदर्भ में नहीं रह सकती। प्रतः नव तत्वों का भूतार्थता से ज्ञान ही उनका अनुशीलन करना चाहेगा। होना ही सम्यक्त्व है।
मोक्ष-प्राभूत में प्राचार्य व्यवहार का सर्वथा खण्डन इस प्रकार हम देखते है कि उनकी दृष्टि भूतार्थ- करते दिखाई पड़ते हैंनिश्चय नय पर टिकी है। इतना ही नहीं, वे अभूतार्थों जो सुतो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि । मे भी अपनी निश्चय दृष्टि का आरोप करते हुए उनसे जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे ।। भूनार्थता का ख्यापन करवाना चाहते हैं। ज्ञान, सम्यक्त्व,
जो व्यवहार में सुषुप्त है, वह प्रात्म-कार्य में तप, प्रात्मा प्रादि शब्दों के व्यवहार पक्ष को गौण करते
जागृत रहता है। जो व्यवहार में जागृत होता है, वह हुए वे इन्हें शुद्ध पाध्यात्मिक परिभाषा तो देते ही है,
अपनी प्रात्मा के लिए मुषुप्त होता है। यह जानते हुए चंत्य, विम्ब, प्रतिमा, मुद्रा आदि भौतिक उपकरणात्मक योगी व्यवहार का सर्वथा त्याग कर दे-डय जाणिऊण शब्दों में भी वे प्रभौतिकता स्थापित करना चाहते हैं ।१
जोई ववहारं चयइ सधहा सव्वं ।। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या वे प्रभूतार्थ को नकारते हैं ?
निश्चय का समर्थन करते हुए बे आगे लिखते हैंव्यावहारिक भूमिका में जीते हुए भी वे क्या उससे अपने आपका संरक्षण करना या बचना चाहते हैं२ इसके
चरणं हवेइ सधम्मो, धम्मो सो हवद अप्प-समभावो। समाधान में हमारे समक्ष एक विचार यह पाता है कि सा राग-रास-राहमा, जावस्स अण सचमुच ही वे व्यवहार-परांगमुख थे। उन्होंने मदेव -चरित्र का स्वरूप स्व-धर्म होता है। धर्म का चतुर्दश-गुणस्थानों का भेद कर ऊपर उठ जाने वाली स्वरूप है प्रात्मा का सम-भाव। वह (सम-भाव) राग आत्मा को ही अपने प्रतिपादन का विषय बनाया। उनकी और रोष रहित जीव का अनन्य परिणाम है। जैसे स्फटिक दृष्टि में यह समस्त चराचर जगत इसलिए असत् है कि मणि अपने में विशुद्ध होने पर भी पर-द्रव्य के संयोग से प्रास्था के स्वभाव में यह उपस्थित नहीं रह सकता। भिन्न--अशुद्ध प्रतीत होती है, वैसे ही राग मादि से १. वही १३
२. समय-सार-श्लोक १३, टीका। भूयत्वेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णा-पावं च ।
तत्र द्रव्य-पर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावपासव-संवर-णिज्जर-बन्धो मोक्खो य सम्मत्तं ॥
यतीति-तदुभयमपि द्रव्य-पर्याययोः पर्यायेणानुभूय२. देखिये, प्राचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित-बोध-प्राभृत। मानतायां भूतार्थम् ।