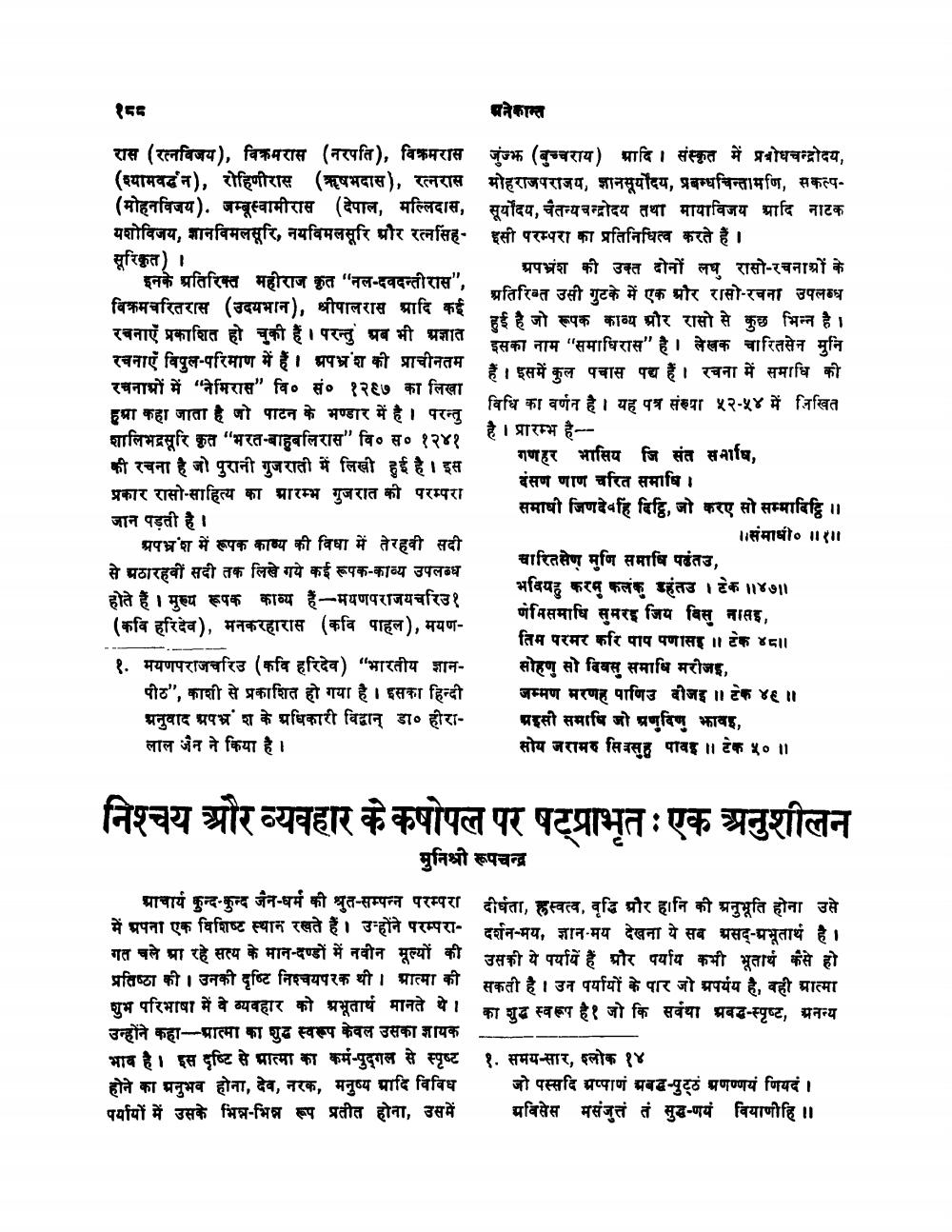________________
१८.
भनेकान्त
रास (रत्नविजय), विक्रमरास (नरपति), विक्रमरास जंज्झ (बच्चराय) मादि । संस्कृत में प्रबोधचन्द्रोदय, (श्यामवर्टन), रोहिणीरास (ऋषभदास), रत्नरास मोहराजपराजय, ज्ञानसूर्योदय, प्रबन्धचिन्तामणि, सकल्प(मोहनविजय). जम्बूस्वामीरास (देपाल, मल्लिदास, सूर्योदय, चैतन्यचन्द्रोदय तथा मायाविजय प्रादि नाटक यशोविजय, ज्ञानविमलसूरि, नयविमलसूरि पौर रत्नसिंह- इसी परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं । सूरिकृत)।
अपभ्रंश की उक्त दोनों लप रासो-रचनात्रों के - इनके अतिरिक्त महीराज कृत "नल-दवदन्तीरास",
अतिरिक्त उसी गुटके में एक और रासो-रचना उपलब्ध विक्रमचरितरास (उदयभान), श्रीपालरास आदि कई
हुई है जो रूपक काव्य और रासो से कुछ भिन्न है। रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। परन्तु अब भी अज्ञात
इसका नाम "समाधिरास" है। लेखक चारितसेन मुनि रचनाएं विपुल-परिमाण में हैं। अपभ्रंश की प्राचीनतम
हैं। इसमें कुल पचास पद्य हैं। रचना में समाधि की रचनामों में "नेमिरास" वि० सं० १२९७ का लिखा हमा कहा जाता है जो पाटन के भण्डार में है। परन्तु
विधि का वर्णन है। यह पत्र संख्या ५२-५४ में लिखित शालिभद्रसूरि कृत "भरत-बाहुबलिरास" वि० स० १२४१
है । प्रारम्भ है--
गणहर भासिय जि संत समाधि, की रचना है जो पुरानी गुजराती में लिखी हुई है। इस
बंसण णाण चरित समाधि। प्रकार रासो-साहित्य का प्रारम्भ गुजरात की परम्परा
समाधी जिणदेवहि दिदि, जो करए सो सम्माविति।। जान पड़ती है।
समाधी० ॥॥ अपभ्रश में रूपक काव्य की विधा में तेरहवी सदी
चारितसेण मुणि समाधि पढंतउ, से पठारहवीं सदी तक लिखे गये कई रूपक-काव्य उपलब्ध
भवियहु करमु कलंक हंतउ । टेक ॥४७॥ होते हैं । मुख्य रूपक काव्य हैं-मयणपराजयचरिउ१
मिसमाधि समरइ जिय विसु नासह, (कवि हरिदेव), मनकरहारास (कवि पाहल), मयण
तिम परमर करि पाप पणासह ॥ टेक ४८॥ १. मयणपराजचरिउ (कवि हरिदेव) "भारतीय ज्ञान- सोहणु सो विवस समाधि मरीजइ,
पीठ", काशी से प्रकाशित हो गया है। इसका हिन्दी जम्मण मरणह पाणिउ बीजह ॥ टेक ४६॥ अनुवाद अपभ्रंश के अधिकारी विद्वान् डा० हीरा- प्राइसी समाधि जो अणुविष्णु झावइ, लाल जैन ने किया है।
सोय जरामा सिवसह पावइ ॥ टेक ५०॥
निश्चय और व्यवहार के कषोपल पर षट्प्राभतः एक अनुशीलन
मुनिश्री रूपचन्द्र
प्राचार्य कुन्द-कुन्द जैन-धर्म की श्रुत-सम्पन्न परम्परा दीर्घता, हस्वत्व, वद्धि और हानि की अनुभूति होना उसे में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने परम्परा- दर्शन-मय, ज्ञान-मय देखना ये सब असद-प्रभूतार्थ है। गत चले पा रहे सत्य के मान-दण्डों में नवीन मूल्यों की उसकी ये पर्यायें हैं और पर्याय कभी भतार्थ कैसे हो प्रतिष्ठा की। उनकी दृष्टि निश्चयपरक थी। प्रात्मा की सकती है। उन पर्यायों के पार जो अपर्यय है, वही प्रात्मा शुभ परिभाषा में वे व्यवहार को प्रभूतार्थ मानते थे। का शुद्ध स्वरूप है। जो कि सर्वथा प्रबद्ध-स्पृष्ट, अनन्य उन्होंने कहा-मात्मा का शुद्ध स्वरूप केवल उसका शायक भाव है। इस दृष्टि से मात्मा का कर्म-पुद्गल से स्पृष्ट १. समय-सार, श्लोक १४ होने का अनुभव होना, देव, नरक, मनुष्य मादि विविध जो पस्सदि अप्पाणं मबद्ध-पुढें अणण्णय णियदं । पर्यायों में उसके भिन्न-भिन्न रूप प्रतीत होना, उसमें मविसेस मसंजुत्तं तं सुख-णयं वियाणीहि ।।