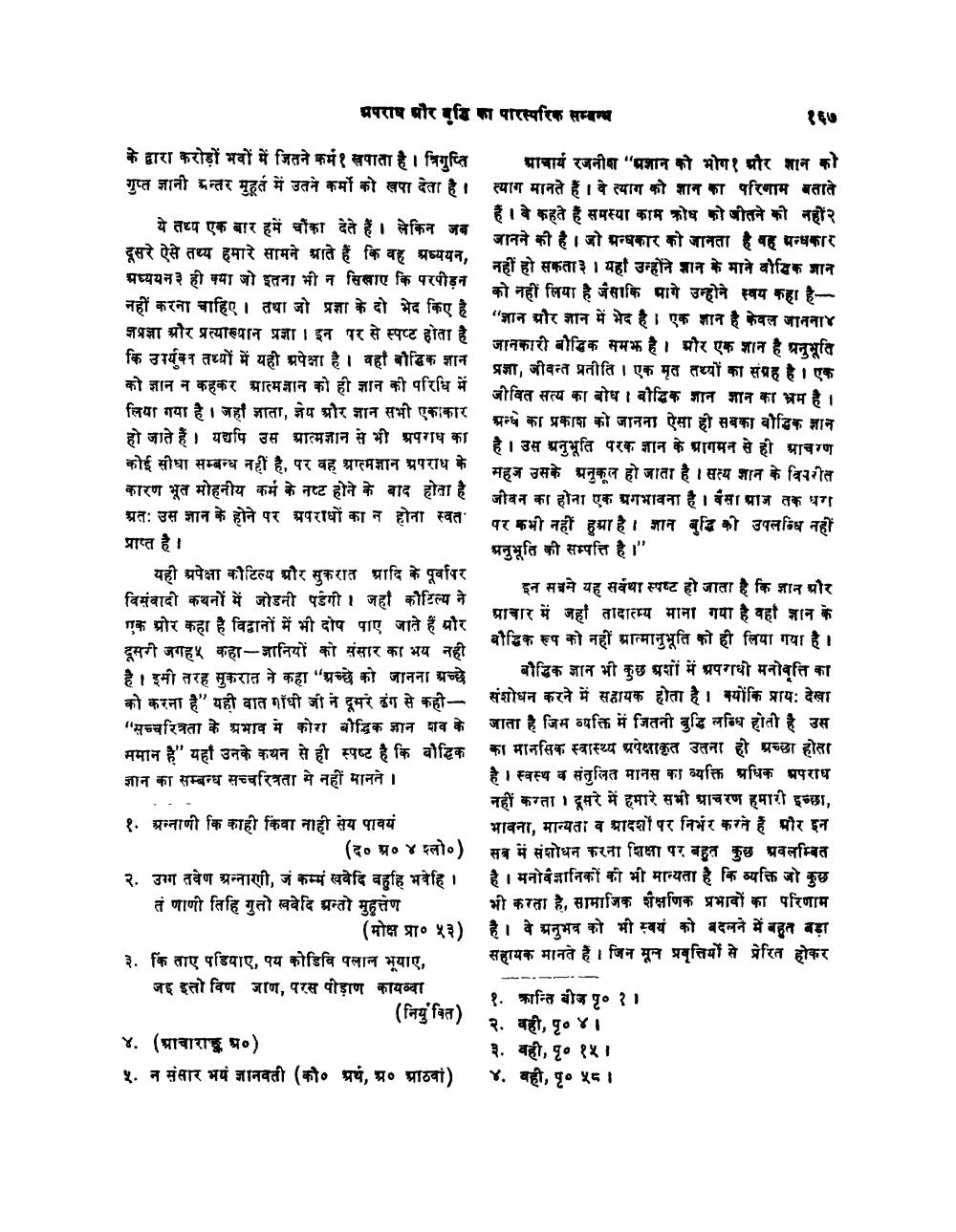________________
अपराध और बुद्धि का पारस्परिक सम्बन्ध
१६७
के द्वारा करोड़ों भवों में जितने कर्म१ खपाता है। त्रिगुप्ति प्राचार्य रजनीश "प्रज्ञान को भोग और शान को गुप्त ज्ञानी मन्तर मुहूर्त में उतने कर्मों को खपा देता है। त्याग मानते हैं। वे त्याग को ज्ञान का परिणाम बताते
हैं । वे कहते हैं समस्या काम क्रोध को जीतने को नहीं२ ये तथ्य एक बार हमें चौंका देते हैं। लेकिन जब दूसरे ऐसे तथ्य हमारे सामने पाते हैं कि वह अध्ययन,
जानने की है । जो अन्धकार को जानता है वह पन्धकार
नहीं हो सकता३ । यहाँ उन्होंने ज्ञान के माने बोधिक जान अध्ययन३ ही क्या जो इतना भी न सिखाए कि परपीड़न
को नहीं लिया है जैसाकि मागे उन्होने स्वय कहा हैनहीं करना चाहिए। तथा जो प्रज्ञा के दो भेद किए है
"ज्ञान और ज्ञान में भेद है। एक ज्ञान है केवल जानना४ ज्ञप्रज्ञा और प्रत्याख्यान प्रज्ञा । इन पर से स्पष्ट होता है
जानकारी बौद्धिक समझ है। मोर एक ज्ञान है अनुभूति कि उपर्युक्त तथ्यों में यही अपेक्षा है। वहाँ बौद्धिक ज्ञान
प्रज्ञा, जीवन्त प्रतीति । एक मृत तथ्यों का संग्रह है। एक को ज्ञान न कहकर आत्मज्ञान को ही ज्ञान की परिधि में
जीवित सत्य का बोध । बौद्धिक ज्ञान ज्ञान का भ्रम है। लिया गया है। जहाँ ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान सभी एकाकार
अन्धे का प्रकाश को जानना ऐसा ही सबका बौद्धिक ज्ञान हो जाते हैं। यद्यपि उस आत्मज्ञान से भी अपराध का
है। उस अनुभूति परक ज्ञान के प्रागमन से ही आचरण कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर वह अात्मज्ञान अपराध के
महज उसके अनुकूल हो जाता है । सत्य ज्ञान के विपरीत कारण भूत मोहनीय कर्म के नष्ट होने के बाद होता है
जीवन का होना एक अगभावना है। सामाज तक धग अतः उस ज्ञान के होने पर अपराधों का न होना स्वतः
पर कभी नहीं हुआ है। ज्ञान बुद्धि की उपलब्धि नहीं प्राप्त है।
अनुभूति की सम्पत्ति है।" यही अपेक्षा कौटिल्य और सुकरात प्रादि के पूर्वापर
इन सबने यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान और विसंवादी कथनों में जोडनी पड़ेगी। जहाँ कौटिल्य ने एक प्रोर कहा है विद्वानों में भी दोप पाए जाते हैं पौर
प्राचार में जहाँ तादात्म्य माना गया है वहाँ ज्ञान के
बौद्धिक रूप को नहीं प्रात्मानुभूति को ही लिया गया है। दूसरी जगह५ कहा-ज्ञानियों को संसार का भय नही है। इसी तरह सुकरात ने कहा “अच्छे को जानना अच्छे
बौद्धिक ज्ञान भी कुछ प्रशों में अपगधी मनोवृत्ति का को करना है" यही बात गाँधी जी ने दूसरे ढंग से कही- संशोधन करने में सहायक होता है। क्योंकि प्राय: देखा "सच्चरित्रता के प्रभाव में कोरा बौद्धिक ज्ञान शव के जाता है जिस व्यक्ति में जितनी बुद्धि लब्धि होती है उस ममान है" यहाँ उनके कथन से ही स्पष्ट है कि बौद्धिक का मानसिक स्वास्थ्य अपेक्षाकृत उतना ही अच्छा होता ज्ञान का सम्बन्ध सच्चरित्रता मे नहीं मानने ।
है । स्वस्थ व संतुलित मानस का व्यक्ति अधिक अपराध
नहीं करता। दूसरे में हमारे सभी प्राचरण हमारी इच्छा, १. अन्नाणी कि काही किंवा नाही सेय पावयं
भावना, मान्यता व आदर्शों पर निर्भर करते हैं और इन
(द० प्र० ४ श्लो०) सब में संशोधन करना शिक्षा पर बहुत कुछ अवलम्बित २. उग्ग तवेण अन्नाणी, जं कम्म खवेदि वहहि भवेहि। है। मनोवैज्ञानिकों की भी मान्यता है कि व्यक्ति जो कुछ तं णाणी तिहि गुतो खवेदि अन्तो मुहुत्तेण
भी करता है, सामाजिक शैक्षणिक प्रभावों का परिणाम
(मोक्ष प्रा०५३) है। वे अनुभव को भी स्वयं को बदलने में बहुत बड़ा ३. किं ताए पडियाए, पय कोडिवि पलाल भूयाए,
सहायक मानते हैं । जिन मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जइ इत्तो विण जाण, परस पीड़ाण कायदा
१. क्रान्ति बीज पृ०१।
(नियुक्ति)
२. वही, पृ०४।
४. (प्राचाराङ्कप्र०) ५. न संसार भयं ज्ञानवती (को० अर्थ, प्र० पाठवां)
३. वही, पृ०१५। ४. वही, पृ०५८