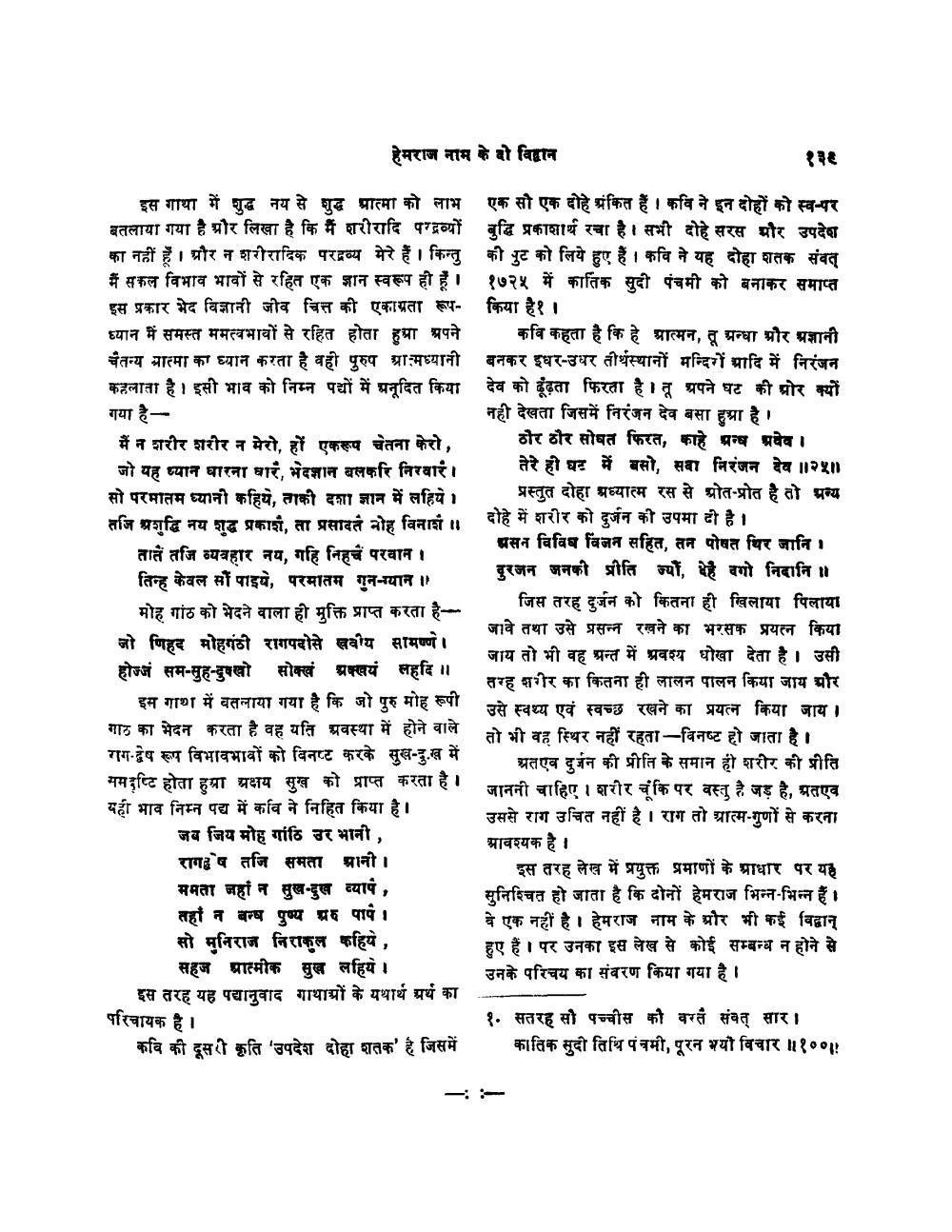________________
हेमराज नाम के दो विद्वान
इस गाथा में शुद्ध नय से शुद्ध प्रात्मा को लाभ एक सौ एक दोहे अंकित हैं । कवि ने इन दोहों को स्व-पर बतलाया गया है और लिखा है कि मैं शरीरादि परद्रव्यों बुद्धि प्रकाशार्थ रचा है। सभी दोहे सरस मोर उपदेश का नहीं हैं। और न शरीरादिक परद्रव्य मेरे हैं । किन्तु की गुट को लिये हुए हैं। कवि ने यह दोहा शतक संवत् मैं सकल विभाव भावों से रहित एक ज्ञान स्वरूप ही हूँ। १७२५ में कार्तिक सुदी पंचमी को बनाकर समाप्त इस प्रकार भेद विज्ञानी जीव चित्त की एकाग्रता रूप- किया है। ध्यान में समस्त ममत्वभावों से रहित होता हया अपने कवि कहता है कि हे पात्मन, तू अन्धा और अज्ञानी चैतन्य प्रात्मा का ध्यान करता है वही पुरुप प्रा.मध्यानी बनकर इधर-उधर तीर्थस्थानों मन्दिरों आदि में निरंजन कहलाता है। इसी भाव को निम्न पद्यों में अनूदित किया देव को ढूंढ़ता फिरता है। तू अपने घट की पोर क्यों गया है
नहीं देखता जिसमें निरंजन देव बसा हुआ है। मैं न शरीर शरीर न मेरो, हों एकरूप चेतना केरो,
ठोर ठौर सोधत फिरत, काहे अन्ध प्रवेव । जो यह ध्यान धारना धार, भेदज्ञान बलकरि निरवार।
तेरे ही घट में बसो, सवा निरंजन देव ॥२५॥ सो परमातम ध्यानी कहिये, ताकी दशा ज्ञान में लहिये।
प्रस्तुत दोहा अध्यात्म रस से प्रोत-प्रोत है तो अन्य तजि अशुद्धि नय शुद्ध प्रकाश, ता प्रसाद नोह विनाश॥ दोहे में शरीर को दुर्जन की उपमा दी है।
असन विविध विजन सहित, तन पोषत थिर जानि । ताते तजि व्यवहार नय, गहि निहचे परवान।
दुरजन जनकी प्रीति ज्यों, देह वगो निदानि । तिन्ह केवल सौं पाइये, परमातम गुनन्यान॥ मोह गांठ को भेदने वाला ही मुक्ति प्राप्त करता है
__जिस तरह दुर्जन को कितना ही खिलाया पिलाया
जावे तथा उसे प्रसन्न रखने का भरसक प्रयत्न किया जो णिहद मोहगंठी रागपदोसे खवीय सामण्णे।
जाय तो भी वह अन्त में अवश्य धोखा देता है। उसी होज्जं सम-सुह-दुक्खो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥
तरह शरीर का कितना ही लालन पालन किया जाय और इस गाण में बतलाया गया है कि जो पुरु मोह रूपी
उसे स्वथ्य एवं स्वच्छ रखने का प्रयत्न किया जाय। गाठ का भेदन करता है वह यति अवस्था में होने वाले
तो भी वह स्थिर नहीं रहता-विनष्ट हो जाता है। गग-द्वेष रूप विभावभावों को विनष्ट करके सुख-दु.ख में
अतएव दुर्जन की प्रीति के समान ही शरीर की प्रीति मम दृष्टि होता हुमा अक्षय सुख को प्राप्त करता है।
जाननी चाहिए । शरीर चूंकि पर वस्तु है जड़ है, अतएव यही भाव निम्न पद्य में कवि ने निहित किया है।
उससे राग उचित नहीं है । राग तो प्रात्म-गुणों से करना जब जिय मोह गांठि उर भानी,
आवश्यक है। रागढष तजि समता पानी।
इस तरह लेख में प्रयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह ममता जहां न सुख-दुख व्याप ,
सुनिश्चित हो जाता है कि दोनों हेमराज भिन्न-भिन्न हैं। तहाँ न बन्ध पुण्य अरु पापै ।
वे एक नहीं है। हेमराज नाम के और भी कई विद्वान् सो मनिराज निराकुल कहिये ,
हए हैं। पर उनका इस लेख से कोई सम्बन्ध न होने से सहज प्रात्मीक सुख लहिये ।
उनके परिचय का संवरण किया गया है। इस तरह यह पद्यानुवाद गाथानों के यथार्थ अर्थ का परिचायक है।
१. सतरह सौ पच्चीस को वरतै संवत् सार। कवि की दूसरी कृति 'उपदेश दोहा शतक' है जिसमें कातिक सुदी तिथि पंचमी, पूरन भयौ विचार ॥१०॥