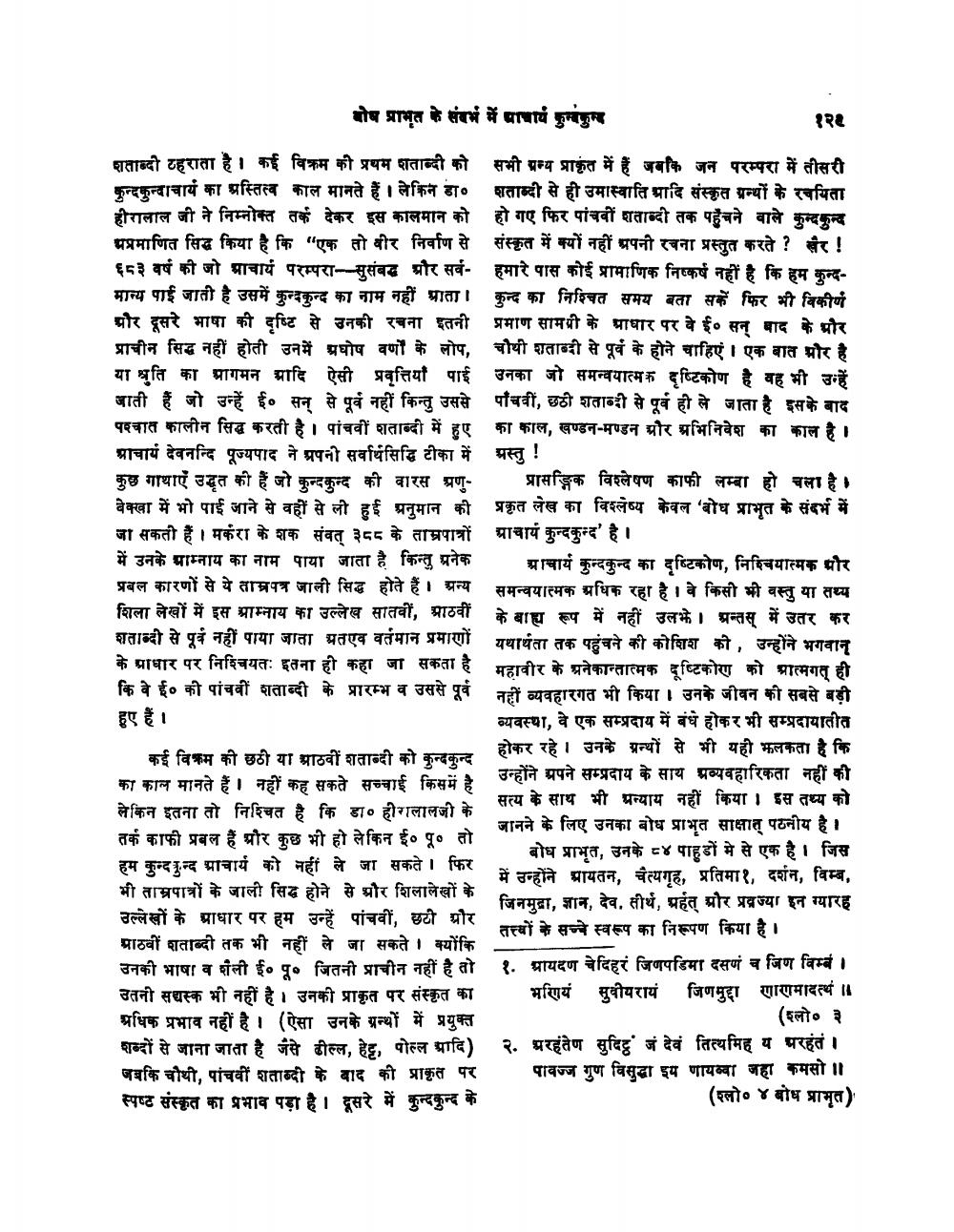________________
बोध प्राभूत के संदर्भ में प्राचार्य कुनकुन
१२९
शताब्दी ठहराता है। कई विक्रम की प्रथम शताब्दी को सभी अन्य प्राकृत में हैं जबकि जन परम्परा में तीसरी कन्दकन्दाचार्य का अस्तित्व काल मानते हैं । लेकिन डा. शताब्दी से ही उमास्वाति प्रादि संस्कृत ग्रन्थों के रचयिता हीरालाल जी ने निम्नोक्त तर्क देकर इस कालमान को हो गए फिर पांचवीं शताब्दी तक पहुँचने वाले कुन्दकुन्द भप्रमाणित सिद्ध किया है कि "एक तो वीर निर्वाण से संस्कृत में क्यों नहीं अपनी रचना प्रस्तुत करते ? खैर ! ६५३ वर्ष की जो प्राचार्य परम्परा-सुसंबद्ध और सर्व- हमारे पास कोई प्रामाणिक निष्कर्ष नहीं है कि हम कुन्दमान्य पाई जाती है उसमें कुन्दकुन्द का नाम नहीं पाता। कुन्द का निश्चित समय बता सकें फिर भी विकीर्ण और दूसरे भाषा की दृष्टि से उनकी रचना इतनी प्रमाण सामग्री के आधार पर वे ई० सन् बाद के और प्राचीन सिद्ध नहीं होती उनमें प्रघोष वर्गों के लोप, चौथी शताब्दी से पूर्व के होने चाहिएं । एक बात और है या श्रुति का प्रागमन आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ पाई उनका जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण है वह भी उन्हें जाती हैं जो उन्हें ई. सन से पूर्व नहीं किन्तु उससे पांचवीं, छठी शताब्दी से पूर्व ही ले जाता है इसके बाद पश्चात कालीन सिद्ध करती है। पांचवीं शताब्दी में हुए का काल, खण्डन-मण्डन और अभिनिवेश का काल है। प्राचार्य देवनन्दि पूज्यपाद ने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीका में प्रस्तु ! कुछ गाथाएँ उद्धृत की हैं जो कुन्दकुन्द की वारस अणु- प्रासङ्गिक विश्लेषण काफी लम्बा हो चला है। वेक्खा में भो पाई जाने से वहीं से ली हई अनुमान की प्रकृत लेख का विश्लेष्य केवल 'बोध प्राभूत के संदर्भ में जा सकती हैं । मर्करा के शक संवत् ३८८ के ताम्रपात्रों प्राचार्य कुन्दकुन्द' है। में उनके पाम्नाय का नाम पाया जाता है किन्तु अनेक प्राचार्य कुन्दकुन्द का दृष्टिकोण, निश्चियात्मक और प्रबल कारणों से ये ताम्रपत्र जाली सिद्ध होते हैं। अन्य समन्वयात्मक अधिक रहा है। वे किसी भी वस्तु या तथ्य शिला लेखों में इस आम्नाय का उल्लेख सातवी, आठवीं
के बाह्य रूप में नहीं उलझे । अन्तस् में उतर कर शताब्दी से पूर्व नहीं पाया जाता प्रतएव वर्तमान प्रमाणों यथार्थता तक पहुंचने की कोशिश की, उन्होंने भगवान के प्राधार पर निश्चियतः इतना ही कहा जा सकता है महावीर के अनेकान्तात्मक दृष्टिकोण को प्रात्मगत् ही कि वे ई० की पांचवीं शताब्दी के प्रारम्भ व उससे पूर्व नहीं व्यवहारगत भी किया। उनके जीवन की सबसे बड़ी हुए हैं।
व्यवस्था, वे एक सम्प्रदाय में बंधे होकर भी सम्प्रदायातीत
होकर रहे। उनके ग्रन्थों से भी यही झलकता है कि कई विक्रम की छठी या आठवीं शताब्दी को कुन्दकुन्द
उन्होंने अपने सम्प्रदाय के साथ अव्यवहारिकता नहीं की का काल मानते हैं। नहीं कह सकते सच्चाई किसमें है
सत्य के साथ भी अन्याय नहीं किया। इस तथ्य को लेकिन इतना तो निश्चित है कि डा. हीगलालजी के
जानने के लिए उनका बोध प्राभूत साक्षात् पठनीय है। तर्क काफी प्रबल हैं और कुछ भी हो लेकिन ई०पू० तो
बोध प्राभूत, उनके ८४ पाहूडों में से एक है। जिस हम कुन्दकुन्द आचार्य को नहीं ले जा सकते । फिर
में उन्होंने प्रायतन, चैत्यगृह, प्रतिमा१, दर्शन, विम्ब, भी ताम्रपात्रों के जाली सिद्ध होने से और शिलालेखों के
जिनमुद्रा, ज्ञान, देव. तीर्थ, प्रर्हत् और प्रव्रज्या इन ग्यारह उल्लेखों के आधार पर हम उन्हें पांचवीं, छठी और
तत्त्वों के सच्चे स्वरूप का निरूपण किया है। पाठवीं शताब्दी तक भी नहीं ले जा सकते। क्योंकि उनकी भाषा व शैली ई०पू० जितनी प्राचीन नहीं है तो १. प्रायदण चेदिहरं जिणपडिमा दसणं च जिण विम्ब । उतनी सद्यस्क भी नहीं है। उनकी प्राकृत पर संस्कृत का भरिणयं सुवीयरायं जिणमुद्दा णाणमादत्थं ॥ अधिक प्रभाव नहीं है। (ऐसा उनके ग्रन्थों में प्रयुक्त
(श्लो० ३ शब्दों से जाना जाता है जैसे ढील्ल, हेट्ट, पोल्ल आदि) २. परहंतेण सुदिटुंजं देवं तित्यमिह य परहंतं । जबकि चौथी, पांचवीं शताब्दी के बाद की प्राकृत पर पावज्ज गुण विसुद्धा इय णायव्या जहा कमसो॥ स्पष्ट संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। दूसरे में कुन्दकुन्द के
(श्लो० ४ बोध प्राभृत)