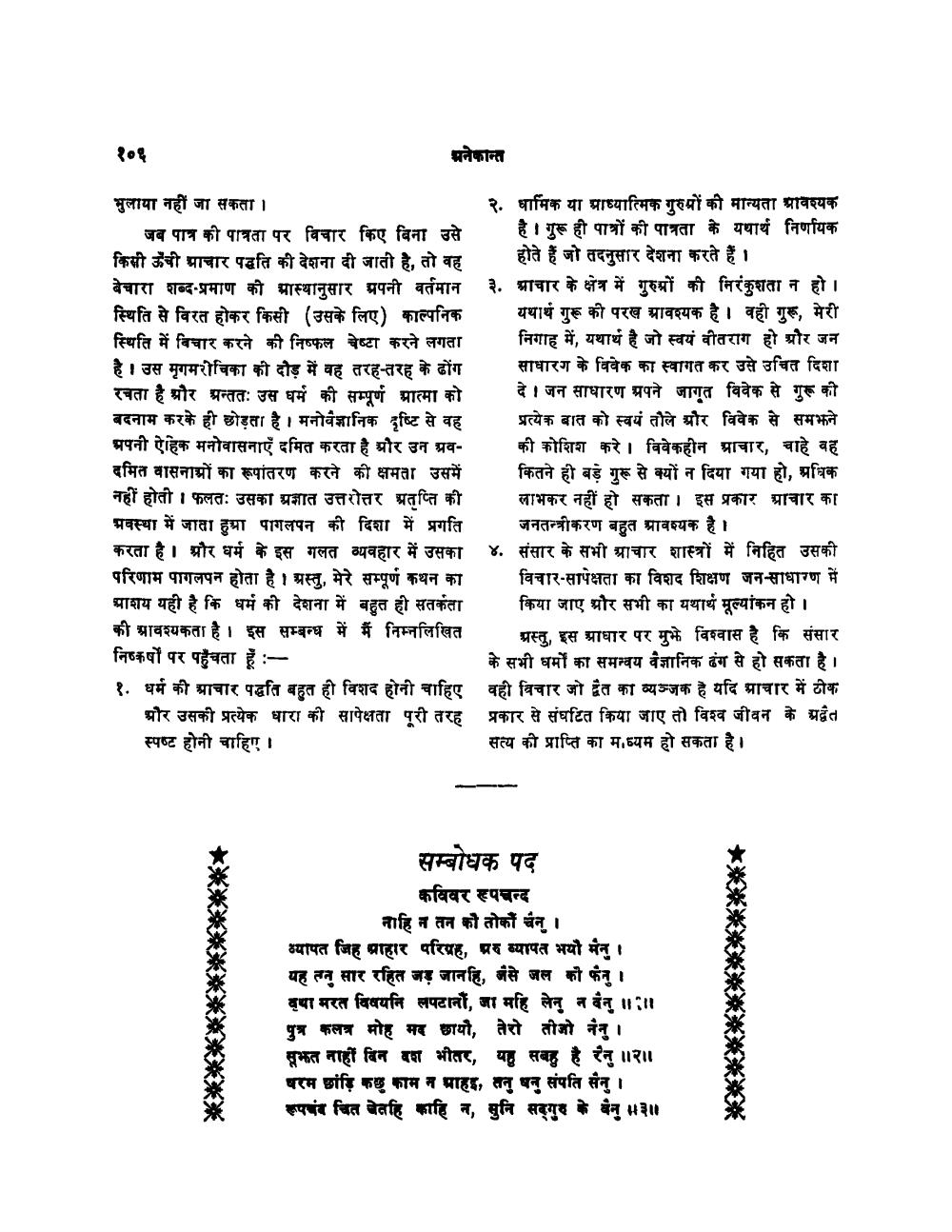________________
२०६
भुलाया नहीं जा सकता ।
जब पात्र की पात्रता पर विचार किए बिना उसे किसी ऊँची आाचार पद्धति की देशना दी जाती है, तो वह बेचारा शब्द प्रमाण को प्रास्वानुसार अपनी वर्तमान स्थिति से विरत होकर किसी ( उसके लिए ) काल्पनिक स्थिति में विचार करने की निष्फल चेष्टा करने लगता है। उस मृगमरीचिका की दौड़ में वह तरह-तरह के ढोंग रचता है धौर अन्ततः उस धर्म की सम्पूर्ण धात्मा को बदनाम करके ही छोड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वह अपनी ऐहिक मनोवासनाएँ दमित करता है और उन सब दमित वासनाओं का रूपांतरण करने की क्षमता उसमें नहीं होती। फलतः उसका अज्ञात उत्तरोत्तर प्रप्ति की अवस्था में जाता हुआ पागलपन की दिशा में प्रगति करता है । और धर्म के इस गलत व्यवहार में उसका परिणाम पागलपन होता है मस्तु मेरे सम्पूर्ण कथन का आशय यही है कि धर्म की देशना में बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित निष्कर्षो पर पहुँचता हूँ :
अनेकान्त
१. धर्म की प्राचार पद्धति बहुत ही विशद होनी चाहिए और उसकी प्रत्येक धारा की सापेक्षता पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए।
*************
२. धार्मिक या प्राध्यात्मिक गुरुमों की मान्यता द्यावश्यक है। गुरू ही पात्रों की पात्रता के यथार्थ निर्णायक होते हैं जो तदनुसार देशना करते हैं।
२.
प्राचार के क्षेत्र में गुरुधों की निरंकुशता न हो। यथार्थ गुरु की परख आवश्यक है। वही गुरू, मेरी निगाह में, यथार्थ है जो स्वयं वीतराग हो धौर जन साधारण के विवेक का स्वागत कर उसे उचित दिशा दे । जन साधारण अपने जागृत विवेक से गुरू की प्रत्येक बात को स्वयं तौले धौर विवेक से समझने की कोशिश करे। विवेकहीन प्राचार, चाहे वह कितने ही बड़े गुरू से क्यों न दिया गया हो, अधिक लाभकर नहीं हो सकता। इस प्रकार ग्राचार का जनतन्त्रीकरण बहुत श्रावश्यक है।
संसार के सभी आचार शास्त्रों में निहित उसकी विचार - सापेक्षता का विशद शिक्षण जन साधारण में किया जाए और सभी का यथार्थ मूल्यांकन हो ।
४.
अस्तु, इस आधार पर मुझे विश्वास है कि संसार के सभी धर्मों का समन्वय वैज्ञानिक ढंग से हो सकता है। वही विचार जो द्वैत का व्यञ्जक है यदि भाचार में ठीक प्रकार से संघटित किया जाए तो विश्व जीवन के अद्वैत सत्य की प्राप्ति का माध्यम हो सकता है ।
सम्बोधक पद
कविवर रूपचन्द नाहि न तन को तोकों चनु ।
व्यापत हि बाहार परिग्रह, मद व्यापत भयो मेनु ।
तीनो नंनु ।
यह नुसार रहित जड़ जानहि, जैसे जल को फैनु । वृथा मरत विषयनि लपटानों, जा महि लेनु न वैनु ॥२॥ पुत्र कलत्र मोह मद छायो सुमत नाहीं दिन दश भीतर चरम छांड़ि कछु काम न ग्राह रूपचंद चित चेतहि काहि न
तेरो यह सबहू है रंनु ॥ २॥ तनु धन संपति सेनु । सुनि सद्गुव के बेनु ॥३॥
*************