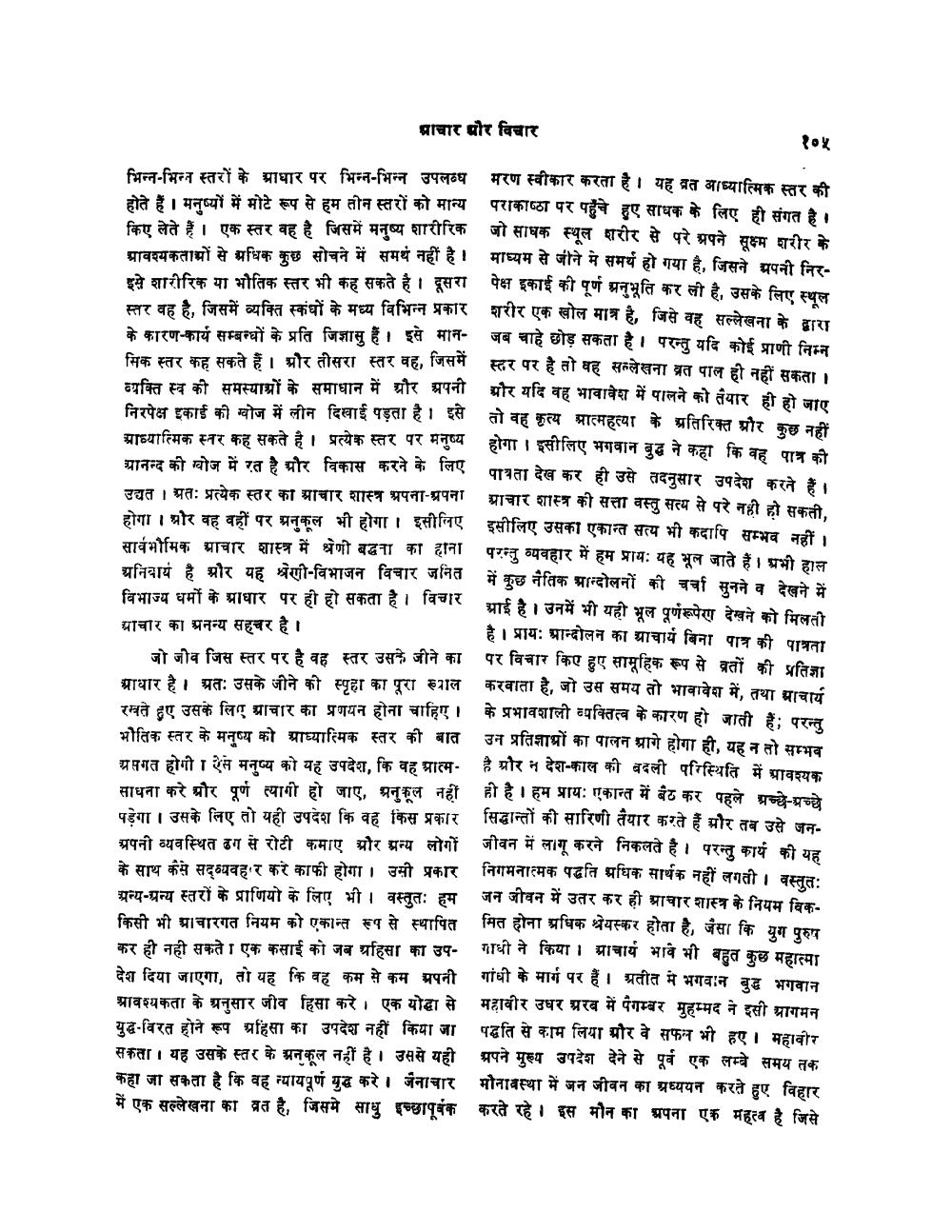________________
प्राचार और विचार
भिन्न-भिन्न स्तरों के आधार पर भिन्न-भिन्न उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों में मोटे रूप से हम तीन स्तरों को मान्य किए लेते हैं । एक स्तर वह है जिसमें मनुष्य शारीरिक मावश्यकताओं से अधिक कुछ सोचने में समर्थ नहीं है। इसे शारीरिक या भौतिक स्तर भी कह सकते है । दूसरा स्तर वह है, जिसमें व्यक्ति स्कंधों के मध्य विभिन्न प्रकार के कारण कार्य सम्बन्धों के प्रति जिज्ञासु हैं। इसे मानमिक स्तर कह सकते हैं और तीसरा स्तर वह जिसमें व्यक्ति स्व की समस्याओं के समाधान में और अपनी निरपेक्ष इकाई की ग्वोज में लीन दिखाई पड़ता है । इसे आध्यात्मिक स्तर कह सकते है प्रत्येक स्तर पर मनुष्य ग्रानन्द की खोज में रत है और विकास करने के लिए उद्यत । अतः प्रत्येक स्तर का आचार शास्त्र अपना-अपना होगा । श्रौर वह वहीं पर अनुकूल भी होगा । इसीलिए सार्वभौमिक आचार शास्त्र में श्रेणी बढना का होना अनिवार्य है और यह श्रेणी - विभाजन विचार जनित विभाज्य धर्मो के आधार पर ही हो सकता है। विचार प्रचार का अनन्य सहचर है ।
।
जो जीव जिस स्तर पर है वह स्तर उसके जीने का आधार है । अतः उसके जीने की स्पृहा का पूरा रूवाल रखते हुए उसके लिए प्रचार का प्रणयन होना चाहिए । भौतिक स्तर के मनुष्य को साध्यात्मिक स्तर की बात
जगत होगी। ऐसे मनुष्य को यह उपदेश, कि यह प्रात्मसाधना करे और पूर्ण त्यागी हो जाए, अनुकूल नहीं पड़ेगा। उसके लिए तो यही उपदेश कि वह किस प्रकार अपनी व्यवस्थित ढंग से रोटी कमाए और अन्य लोगों के साथ कैसे सद्व्यवहार करे काफी होगा उसी प्रकार धन्य-धन्य स्तरों के प्राणियों के लिए भी वस्तुतः हम किसी भी प्राचारगत नियम को एकान्त रूप से स्थापित कर ही नही सकते एक कसाई को जब पहिया का उपदेश दिया जाएगा, तो यह कि वह कम से कम अपनी श्रावश्यकता के अनुसार जीव हिसा करे। एक योद्धा से युद्धविरत होने रूप हिंसा का उपदेश नहीं किया जा सकता। यह उसके स्तर के अनुकूल नहीं है। उससे यही कहा जा सकता है कि वह न्यायपूर्ण युद्ध करे जैनाचार में एक सल्लेखना का व्रत है, जिसमे साधु इच्छापूर्वक
।
१०५
मरण स्वीकार करता है। यह व्रत आध्यात्मिक स्तर की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए साधक के लिए ही संगत है । जो साधक स्थूल शरीर से परे अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जीने में समर्थ हो गया है, जिसने अपनी निर पेक्ष इकाई की पूर्ण अनुभूति कर ली है, उसके लिए स्थूल शरीर एक खोल मात्र है, जिसे वह सल्लेखना के द्वारा जब चाहे छोड़ सकता है। परन्तु यदि कोई प्राणी निम्न स्तर पर है तो वह सल्लेखना व्रत पाल ही नहीं सकता । और यदि वह भावावेश में पालने को तैयार ही हो जाए तो वह कृत्य आत्महत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा । इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि वह पात्र की पापता देख कर ही उसे अदनुसार उपदेश करते हैं। आचार शास्त्र की सत्ता वस्तु सत्य से परे नही हो सकती, इसीलिए उसका एकान्त सत्य भी कदापि सम्भव नहीं । परन्तु व्यवहार में हम प्रायः यह भूल जाते हैं। अभी हाल में कुछ नैतिक आन्दोलनों की चर्चा सुनने व देखने में आई है। उनमें भी यही भूल पूर्णरूपेण देखने को मिलती है। प्रायः आन्दोलनका प्राचार्य बिना पात्र की प पर विचार किए हुए सामूहिक रूप से व्रतों की प्रतिज्ञा करवाता है, जो उस समय तो भावावेश में, तथा प्राचार्य के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण हो जाती है परन्तु उन प्रतिज्ञानों का पालन प्रागे होगा ही, यह न तो सम्भव है पर देश-काल की बदली परिस्थिति में मावश्यक ही है । हम प्रायः एकान्त में बैठ कर पहले अच्छे-अच्छे सिद्धान्तों की सारिणी तैयार करते हैं और तब उसे जन
4
जीवन में लागू करने निकलते हैं। परन्तु कार्य की यह निगमनात्मक पद्धति अधिक सार्थक नहीं लगती । वस्तुत: जन जीवन में उतर कर ही आचार शास्त्र के नियम विकमित होना अधिक श्रेयस्कर होता है, जैसा कि युग पुरुष साथी ने किया। प्राचार्य भावे भी बहुत कुछ महात्मा गांधी के मार्ग पर हैं । अतीत में भगवान बुद्ध भगवान महावीर उधर अरब में पैगम्बर मुहम्मद ने इसी श्रागमन पद्धति से काम लिया और वे सफल भी हुए। महावीर अपने मुख्य उपदेश देने से पूर्व एक लम्बे समय तक मोनावस्था में जन जीवन का अध्ययन करते हुए बिहार करते रहे। इस मौन का अपना एक महत्व है जिसे