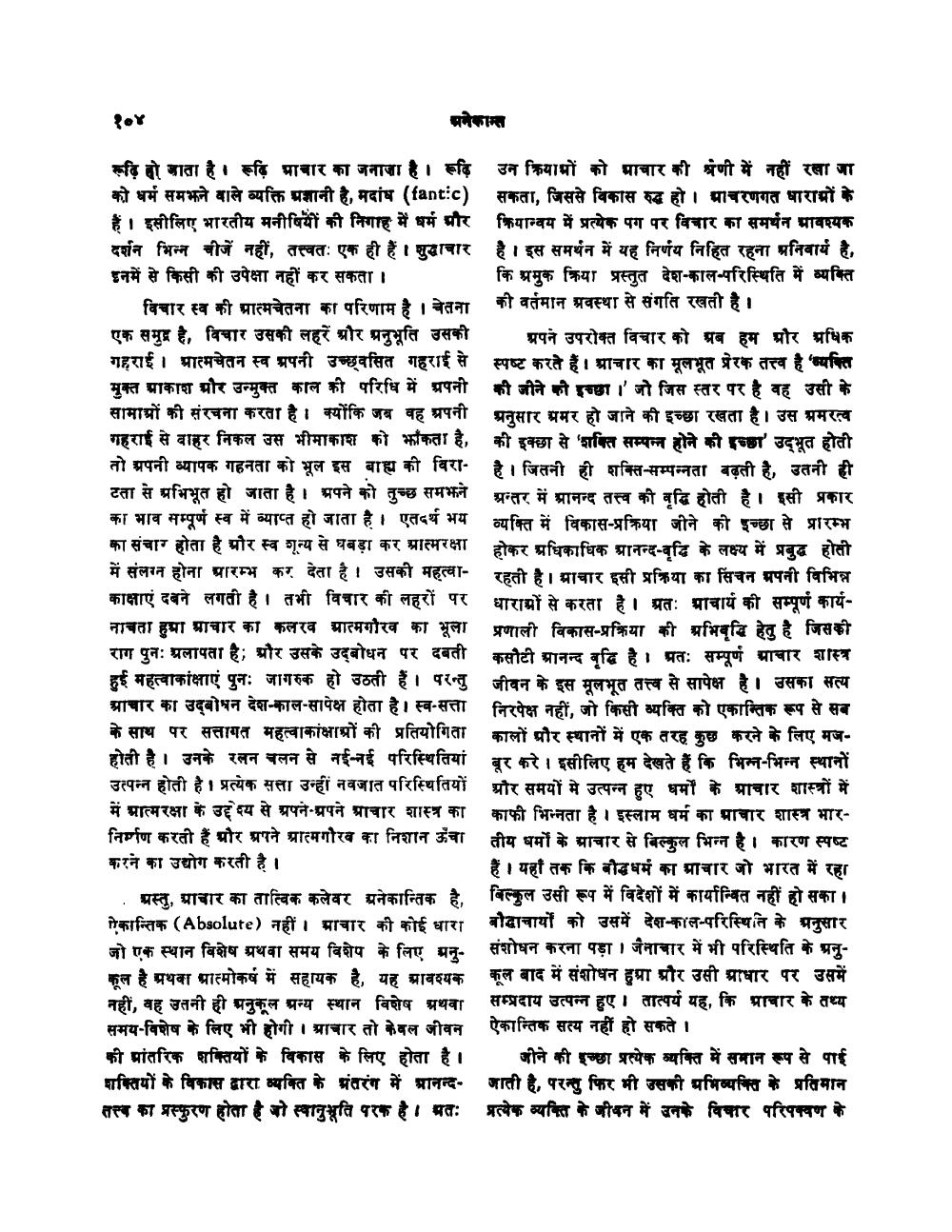________________
१०४
अनेकान्त
रूढ़ि हो जाता है। रूढ़ि माचार का जनाजा है। रूढ़ि उन क्रियामों को प्राचार की श्रेणी में नहीं रखा जा को धर्म समझने वाले व्यक्ति प्रज्ञानी है, मदांध (fantic) सकता, जिससे विकास रुद्ध हो। पाचरणगत धारामों के हैं। इसीलिए भारतीय मनीषियों की निगाह में धर्म और क्रियान्वय में प्रत्येक पग पर विचार का समर्थन मावश्यक दर्शन भिन्न चीजें नहीं, तस्वतः एक ही हैं। शुद्धाचार है। इस समर्थन में यह निर्णय निहित रहना अनिवार्य है, इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकता।
कि अमुक क्रिया प्रस्तुत देश-काल-परिस्थिति में व्यक्ति विचार स्व की प्रात्मचेतना का परिणाम है। चेतना की वर्तमान अवस्था से संगति रखती है। एक समुद्र है, विचार उसकी लहरें और अनुभूति उसकी अपने उपरोक्त विचार को अब हम और अधिक गहराई। प्रात्मचेतन स्व अपनी उच्छ्वसित गहराई से स्पष्ट करते हैं। प्राचार का मूलभूत प्रेरक तत्त्व है 'व्यक्ति मुक्त पाकाश और उन्मुक्त काल की परिधि में अपनी की जीने की इच्छा ।' जो जिस स्तर पर है वह उसी के सामानों की संरचना करता है। क्योंकि जब वह अपनी अनुसार अमर हो जाने की इच्छा रखता है। उस अमरत्व गहराई से बाहर निकल उस भीमाकाश को झाँकता है, की इक्छा से 'शक्ति सम्पन्न होने की इच्छा' उद्भूत होती तो अपनी व्यापक गहनता को भूल इस बाह्य की विरा- है। जितनी ही शक्ति-सम्पन्नता बढ़ती है, उतनी ही टता से अभिभूत हो जाता है। अपने को तुच्छ समझने अन्तर में प्रानन्द तत्व की वद्धि होती है। इसी प्रकार का भाव मम्पूर्ण स्व में व्याप्त हो जाता है। एतदर्थ भय व्यक्ति में विकास प्रक्रिया जीने की इच्छा से प्रारम्भ का संचार होता है और स्व शून्य से घबड़ा कर प्रात्मरक्षा होकर अधिकाधिक प्रानन्द-वदि के लक्ष्य में प्रबुद्ध होती में संलग्न होना प्रारम्भ कर देता है। उसकी महत्वा- रहती है। प्राचार इसी प्रक्रिया का सिंचन प्रपनी विभिन्न काक्षाएं दबने लगती है। तभी विचार की लहरों पर धारामों से करता है। अतः प्राचार्य की सम्पूर्ण कार्यनाचता हुमा प्राचार का कलरव प्रात्मगौरव का भूला प्रणाली विकास-प्रक्रिया की अभिवृद्धि हेतु है जिसकी राग पुनः प्रलापता है; और उसके उद्बोधन पर दबती कसौटी आनन्द वृद्धि है। अतः सम्पूर्ण प्राचार शास्त्र हई महत्वाकांक्षाएं पुनः जागरुक हो उठती हैं। परन्तु जीवन के इस मुलभत तत्त्व से सापेक्ष है। उसका सत्य प्राचार का उद्बोधन देश-काल-सापेक्ष होता है। स्व-सत्ता निरपेक्ष नहीं. जो किसी व्यक्ति को एकान्तिक रूप से सब के साथ पर सत्तागत महत्वाकांक्षाओं की प्रतियोगिता कालों और स्थानों में एक तरह कुछ करने के लिए मजहोती है। उनके रलन चलन से नई-नई परिस्थितियां बर करे । इसीलिए हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न स्थानों उत्पन्न होती है। प्रत्येक सत्ता उन्हीं नवजात परिस्थितियों और समयों में उत्पन्न हए धर्मों के प्राचार शास्त्रों में में मात्मरक्षा के उद्देश्य से अपने-अपने प्राचार शास्त्र का काफी भिन्नता है । इस्लाम धर्म का प्राचार शास्त्र भारनिर्माण करती हैं और अपने प्रात्मगौरव का निशान ऊँचा तीय धर्मों के प्राचार से बिल्कुल भिन्न है। कारण स्पष्ट करने का उद्योग करती है।
हैं। यहाँ तक कि बौद्धधर्म का प्राचार जो भारत में रहा .. प्रस्तु, प्राचार का तात्विक कलेवर अनेकान्तिक है, बिल्कुल उसी रूप में विदेशों में कार्यान्वित नहीं हो सका। कान्तिक (Absolute) नहीं। माचार की कोई धारा बौद्धाचार्यों को उसमें देश-काल-परिस्थिति के अनुसार जो एक स्थान विशेष अथवा समय विशेष के लिए मनू- सशाषन करना पड़ा। जनाचार म भा पारास्थात क अनुकूल है अथवा प्रात्मोकर्ष में सहायक है, यह आवश्यक कूल बाद में संशोधन हुप्रा और उसी आधार पर उसमें नहीं, वह उतनी ही अनुकूल अन्य स्थान विशेष अथवा सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। तात्पर्य यह, कि प्राचार के तथ्य समय-विशेष के लिए भी होगी। प्राचार तो केवल जीवन ऐकान्तिक सत्य नहीं हो सकते। की प्रांतरिक शक्तियों के विकास के लिए होता है। जीने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से पाई शाक्तियों के विकास द्वारा व्यक्ति के अंतरंग में प्रानन्द- जाती है, परन्तु फिर भी उसकी अभिव्यक्ति के प्रतिमान तत्व का प्रस्फुरण होता है जो स्वानुभूति परक है। प्रतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उनके विचार परिपक्वण के