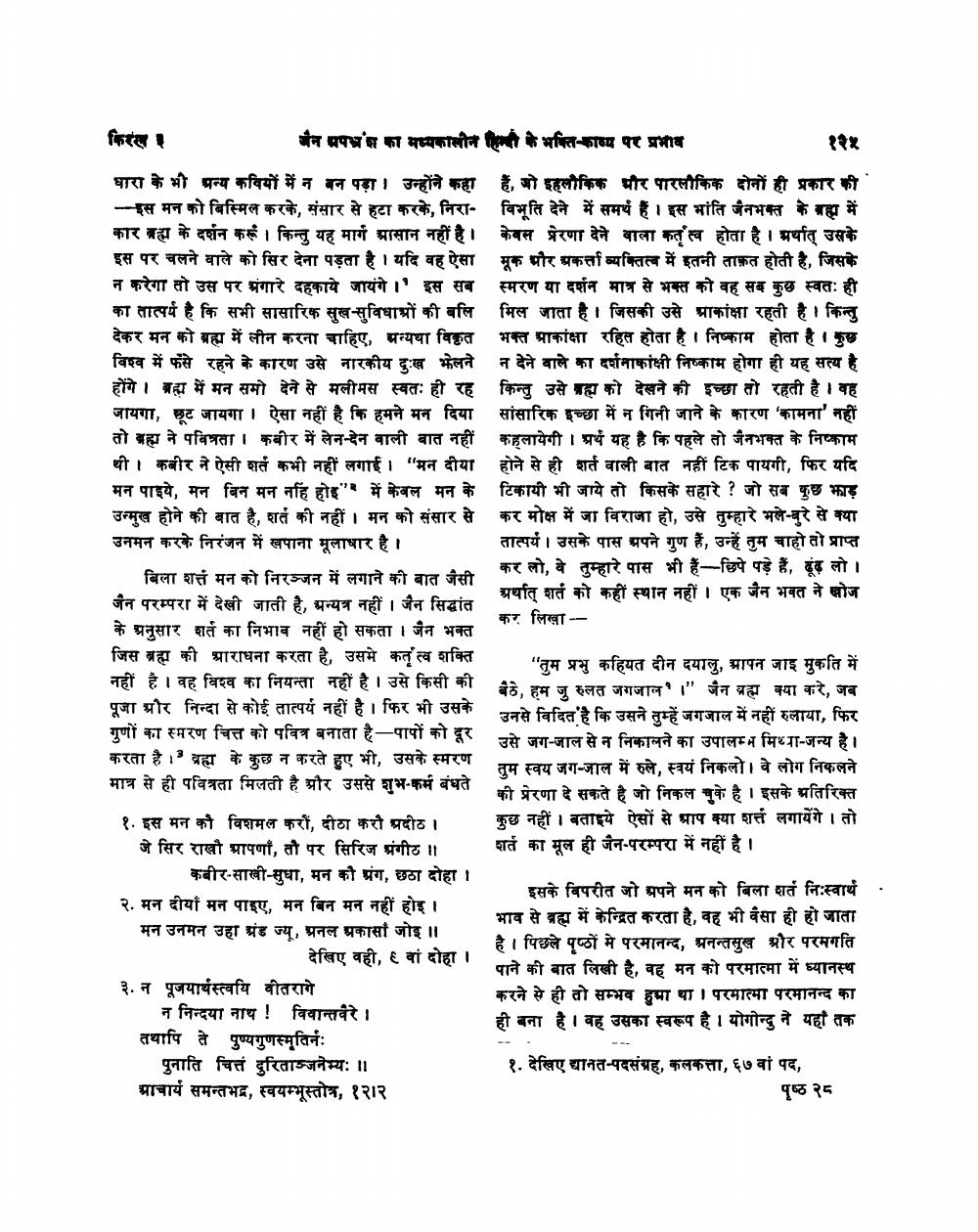________________
किर
धारा के भी अन्य कवियों में न बन पड़ा। उन्होंने कहा - इस मन को बिस्मिल करके, संसार से हटा करके, निराकार ब्रह्म के दर्शन करूं । किन्तु यह मार्ग आसान नहीं है। इस पर चलने वाले को सिर देना पड़ता है। यदि वह ऐसा न करेगा तो उस पर अंगारे दहकाये जायंगे।' इस सब का तात्पर्य है कि सभी सासारिक सुख-सुविधाओं की बलि देकर मन को ब्रह्म में लीन करना चाहिए, अन्यथा विकृत विश्व में फँसे रहने के कारण उसे नारकीय दुःख झेलने होगे। ब्रह्म में मन समो देने से मलीमस स्वतः ही रह जायगा छूट जायगा । ऐसा नहीं है कि हमने मन दिया तो ब्रह्म ने पवित्रता। कबीर में लेन-देन वाली बात नहीं थी। कबीर ने ऐसी शर्त कभी नहीं लगाई। "मन दीया मन पाइये, मन बिन मन नहि होइ" में केवल मन के उन्मुख होने की बात है, शर्त की नहीं। मन को संसार से उनमन करके निरंजन में खपाना मूलाधार है ।
जैन ' का मध्यकालीन हिन्दी के भक्ति-काव्य पर प्रभाव
बिला शतं मन को निरञ्जन में लगाने की बात जैसी जैन परम्परा में देखी जाती है, अन्यत्र नहीं । जैन सिद्धांत के अनुसार शर्त का निभाव नहीं हो सकता । जैन भक्त जिस ब्रह्म की आराधना करता है, उसमे कर्तृत्व शक्ति नहीं है । वह विश्व का नियन्ता नहीं है । उसे किसी की पूजा और निन्दा से कोई तात्पर्य नहीं है। फिर भी उसके गुणों का स्मरण चित्त को पवित्र बनाता है-पापों को दूर करता है । 3 ब्रह्म के कुछ न करते हुए भी, उसके स्मरण मात्र से ही पवित्रता मिलती है और उससे शुभ कर्म बंधते
१. इस मन को विशमल करों, दीठा करौ प्रदीठ । जे सिर राखौ प्रापणां, तो पर सिरिज अंगीठ ॥
कबीर- साखी - सुधा, मन को अंग, छठा दोहा । २. मन दीयाँ मन पाइए, मन बिन मन नहीं होइ । मन उनमन उहा अंड ज्यू, अनल अकासाँ जोइ ॥ देखिए वही, ६ वां दोहा ।
३. न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे
न निन्दया नाथ ! विवान्तरे। तथापि ते पुण्यगुणस्मूतिर्नः
पुनाति चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥ प्राचार्य समन्तभद्र, स्वयम्भूस्तोत्र, १२१२
१९५
हैं, जो इहलौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की विभूति देने में समर्थ हैं । इस भांति जैनभक्त के ब्रह्म में केवल प्रेरणा देने वाला कर्तृत्व होता है । अर्थात् उसके मूक धौर धकर्ता व्यक्तित्व में इतनी ताकत होती है, जिसके स्मरण या दर्शन मात्र से भक्त को वह सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। जिसकी उसे धाकांक्षा रहती है। किन्तु भक्त प्राकांक्षा रहित होता है । निष्काम होता है । कुछ न देने वाले का दर्शनाकांक्षी निष्काम होगा ही यह सत्य है। किन्तु उसे ब्रह्म को देखने की इच्छा तो रहती है। वह सांसारिक इच्छा में न गिनी जाने के कारण 'कामना' नहीं कहलायेगी धर्म यह है कि पहले तो जैनभक्त के निष्काम होने से ही शर्त वाली बात नहीं टिक पायगी, फिर यदि टिकायी भी जाये तो किसके सहारे ? जो सब कुछ भा कर मोक्ष में जा विराजा हो, उसे तुम्हारे भले-बुरे से क्या तात्पर्य । उसके पास अपने गुण हैं, उन्हें तुम चाहो तो प्राप्त कर लो वे तुम्हारे पास भी है-छिपे पड़े हैं, ढूंढ लो। अर्थात् शर्त को कहीं स्थान नहीं । एक जैन भवत ने खोज कर लिखा
――
"तुम प्रभु कहियत दीन दयालु, आपन जाइ मुकति में बैठे, हम जु रुलत जगजाल ।" जैन ब्रह्म क्या करे, जब उनसे विदित है कि उसने तुम्हें जगजाल में नहीं रुलाया, फिर उसे जग-जाल से न निकालने का उपालम्भ मिश्रा-जन्य है । तुम स्वय जग-जाल में रुले, स्वयं निकलो। वे लोग निकलने की प्रेरणा दे सकते है जो निकल चुके है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बताइये ऐसों से धाप क्या शर्त लगायेंगे तो शर्त का मूल ही जैन परम्परा में नहीं है ।
इसके विपरीत जो अपने मन को बिला दातं निःस्वार्थ भाव से ब्रह्म में केन्द्रित करता है, वह भी वैसा ही हो जाता है । पिछले पृष्ठों मे परमानन्द, अनन्तसुख और परमगति पाने की बात लिखी है, वह मन को परमात्मा में ध्यानस्थ करने से ही तो सम्भव हुआ था । परमात्मा परमानन्द का ही बना है। वह उसका स्वरूप है। योगीन्दु ने यहाँ तक
१. देखिए द्यानत-पदसंग्रह, कलकत्ता, ६७ वां पद,
पृष्ठ २८