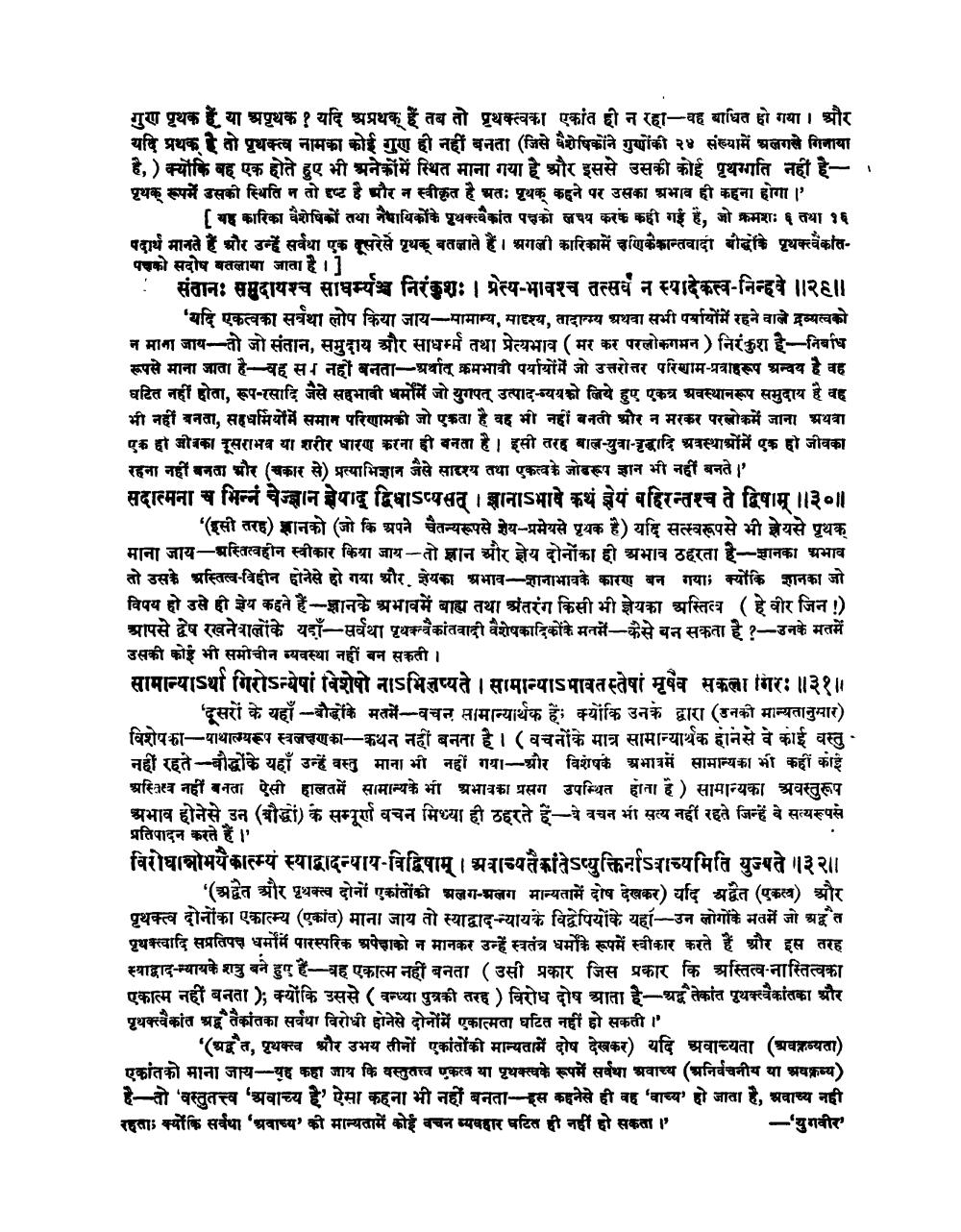________________
गुण पृथक हैं, या अपृथक ? यदि अप्रथक हैं तब तो पृथक्त्वका एकांत ही न रहा- वह बाधित हो गया । और यदि प्रथक है तो पृथक्त्व नामका कोई गुण हो नहीं बनता (जिसे वैशेषिकोंने गुणोंकी २४ संख्यामें अलग गिनाया है ) क्योंकि वह एक होते हुए भी अनेकों में स्थित माना गया है और इससे उसकी कोई पृथग्गति नहीं हैपृथक् रूपमें उसकी स्थिति न तो दृष्ट है और न स्वीकृत है अतः पृथक् कहने पर उसका प्रभाव ही कहना होगा ।'
[ यह कारिका वैशेषिकों तथा नैयायिकों के पृथक्त्वैकांत पक्षको लक्ष्य करके कही गई है, जो क्रमशः ६ तथा १६ पदार्थ मानते हैं और उन्हें सर्वथा एक दूसरेसे पृथक् बतलाते हैं। अगली कारिकामें क्षणिकान्तवादी बौद्धोंके पृथक्त्वकांत
।
संतानः समुदायश्च साधर्म्यश्च निरंकुशः । प्रेत्य भावश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्व - निन्दवे ॥२६॥ 'यदि एकत्वका सर्वथा लोप किया जाय - पामाम्य, मादृश्य, तादात्म्य अथवा सभी पर्यायोंमें रहने वाले द्रव्यत्वको न माना जाय तो जो संतान, समुदाय और साधर्म्म तथा प्रेत्यभाव ( मर कर परलोकगमन ) निरंकुश है - निबंध रूपसे माना जाता है-वह स नहीं बनता - प्रर्थात् क्रमभावी पर्यायों में जो उत्तरोत्तर परिणाम प्रवाहरूप अन्वय है वह घटित नहीं होता, रूप-रसादि जैसे सहभावी धर्मोंमें जो युगपत् उत्पाद-व्ययको लिये हुए एकत्र अवस्थानरूप समुदाय है वह भी नहीं बनता, सहधर्मियों में समान परिणामको जो एकता है वह भी नहीं बनती और न मरकर परलोकमें जाना अथवा एक हो जीवका दूसराभव या शरीर धारण करना ही बनता है। इसी तरह बाल-युवा-वृद्धादि अवस्थाओं में एक हो जीवका रहना नहीं बनता और (चकार से) प्रत्याभिज्ञान जैसे सादृश्य तथा एकत्वके जोढरूप ज्ञान भी नहीं बनते ।' सदात्मना च भिन्नं चेज्ज्ञान ज्ञेयाद् द्विधाऽप्यसत् । ज्ञानाऽभावे कथं ज्ञेयं वहिरन्तश्च ते द्विषाम् ||३०|| ' (इसी तरह) ज्ञानको (जो कि अपने चैतन्यरूपसे शेय- प्रमेयसे पृथक है) यदि सत्स्वरूपसे भी ज्ञेयसे पृथक् माना जाय - अस्तित्वहीन स्वीकार किया जाय - तो ज्ञान और ज्ञेय दोनोंका हो अभाव ठहरता है - ज्ञानका अभाव तो उसके अस्तित्व-विहीन होनेसे हो गया और शेयका अभाव - ज्ञानाभावके कारण बन गया; क्योंकि ज्ञानका जो विषय हो उसे ही ज्ञेय कहते हैं - ज्ञानके अभाव में बाह्य तथा अंतरंग किसी भी ज्ञेयका अस्तित्व ( हे वीर जिन !) आपसे द्वेष रखनेवालोंके यहाँ — सर्वथा पृथक्त्वैकांतवादी वैशेषकादिकों के मनमें— कैसे बन सकता है ? --उनके मतमें उसकी कोई भी समीचीन व्यवस्था नहीं बन सकती ।
सामान्याऽर्था गिरोऽन्येषां विशेषो नाऽभिलप्यते । सामान्याऽपावतस्तेषां मृषैव सकला गिरः ॥ ३१ ॥ 'दूसरों के यहाँ - बौद्धों मतमें - वचन सामान्यार्थक हैं; क्योंकि उनके द्वारा (उनकी मान्यतानुसार) विशेषका - याथात्म्यरूप स्वलक्षणका - कथन नहीं बनता है । ( वचनों के मात्र सामान्यार्थक होने से वे कोई वस्तु - नहीं रहते - बौद्धों के यहाँ उन्हें वस्तु माना भी नहीं गया और विशेषके अभाव में सामान्यका भी कहीं कोई aer नहीं बनता ऐसी हालत में सामान्यके भी प्रभावका प्रसंग उपस्थित होता है ) सामान्यका अवस्तुरूप अभाव होने से उन (बौद्धों) के सम्पूर्ण वचन मिध्या ही ठहरते हैं - ये वचन भी सत्य नहीं रहते जिन्हें वे सत्यरूपसे प्रतिपादन करते हैं ।" विरोधानोभयैकात्म्यं स्याद्वादन्याय-विद्विषाम् । श्रवाच्यतैकां तेऽप्युक्तिर्नाऽवाच्यमिति युज्यते ॥ ३२ ॥
' (अद्वैत और पृथक्त्व दोनों एकांतोंकी अलग-अलग मान्यतामें दोष देखकर) यदि अद्वैत (एक) और पृथक्त्व दोनोंका एकात्म्य (एकांत) माना जाय तो स्याद्वाद न्याय के विद्वेषियों के यहाँ उन लोगोंके मतमें जो पृथक्त्वादि सप्रतिपक्ष धर्मोमें पारस्परिक अपेक्षाको न मानकर उन्हें स्वतंत्र धर्मोंके रूपमें स्वीकार करते हैं और इस तरह स्याद्वाद न्यायके शत्रु बने हुए हैं वह एकात्म नहीं बनता ( उसी प्रकार जिस प्रकार कि अस्तित्व- नास्तित्वका एकात्म नहीं बनता ); क्योंकि उससे (वन्ध्या पुत्रकी तरह ) विरोध दोष आता है - श्रद्व तेकांत पृथक्त्वैकांतका और पृथक्त्वकांत कांता सर्वथा विरोधी होनेसे दोनों में एकात्मता घटित नहीं हो सकती ।"
'(अद्वैत, पृथक्त्व और उभय तीनों एकांतोंकी मान्यतामें दोष देखकर ) यदि अवाच्यता (अवक्रन्यता ) एकांत को माना जाय -- यह कहा जाय कि वस्तुतत्त्व एकत्व या पृथक्त्वके रूपमें सर्वथा अवाच्य (अनिर्वचनीय या श्रवक्रव्य है - तो 'वस्तुतत्त्व 'अवाच्य है' ऐसा कहना भी नहीं बनता - इस कहनेसे ही वह 'वाच्य' हो जाता है, अवाच्य नही रहताः क्योंकि सर्वथा 'अवाच्य' की मान्यतामें कोई वचन व्यवहार घटित ही नहीं हो सकता ।" — 'युगवीर'