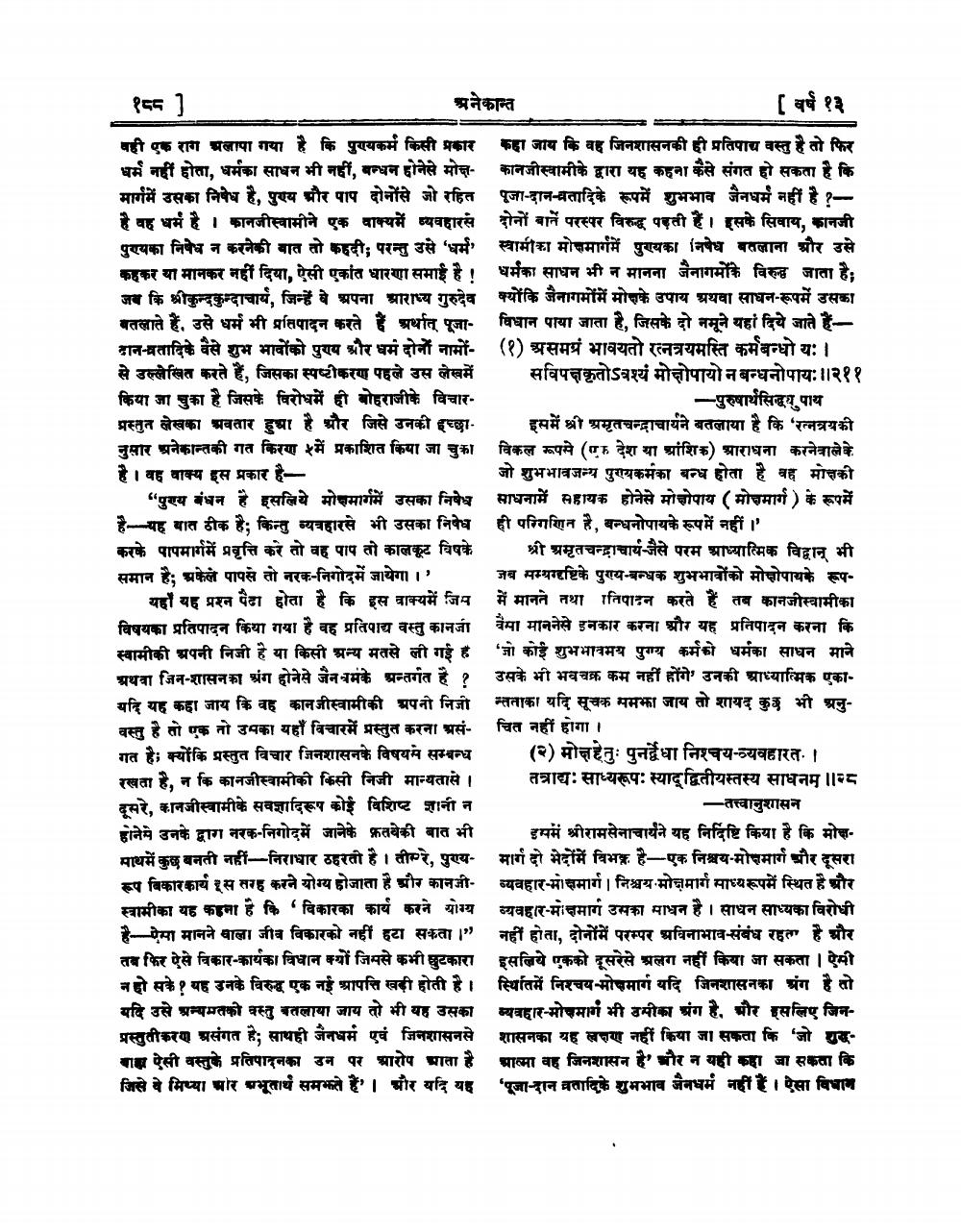________________
१८८]
श्रनेकान्त
[ वर्ष १३
वही एक राग अलापा गया है कि पुण्यकर्म किसी प्रकार धर्म नहीं होता, धर्मका साधन भी नहीं, बन्धन होनेसे मोल मार्ग में उसका निषेध है, पुरुष और पाप दोनोंसे रहित है वह धर्म है । कानजीस्वामीने एक वाक्यमें व्यवहारसे पुण्यका निषेध न करनेकी बात तो कहदी; परन्तु उसे 'धर्म' कहकर या मानकर नहीं दिया, ऐसी एकांत धारणा समाई है! जब कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य, जिन्हें वे अपना श्राराध्य गुरुदेव बताते हैं, उसे धर्म भी प्रतिपादन करते हैं अर्थात् पूजादान-यतादिके वैसे शुभ भावोंको पुण्य और धर्म दोनों नामोंसे उल्लेखित करते हैं, जिसका स्पष्टीकरया पहले उसमें किया जा चुका है जिसके विरोध में ही बोहराजीके विचारप्रस्तुत लेखका अवतार हुआ है और जिसे उनकी इच्छानुसार अनेकान्तकी गत किरण श्में प्रकाशित किया जा चुका है। वह वाक्य इस प्रकार है
कहा जाय कि वह जिनशासनकी ही प्रतिपाद्य वस्तु है तो फिर कानजीस्वामीके द्वारा यह कहना कैसे संगत हो सकता है कि पूजा-दान-यतादिके रूपमें शुभभाव जैनधर्म नहीं है जो ?दोनों बातें परस्पर विरुद्ध पड़ती हैं। इसके सिवाय, कानजी स्वामीका मोक्षमार्गमें पुण्यका निषेध बतलाना और उसे धर्मका साधन भी न मानना जैनागमोंके विरुद्ध जाता है; क्योंकि जैनागमोंमें मोक्षके उपाय श्रथवा साधन रूपमें उसका विधान पाया जाता है, जिसके दो नमूने यहां दिये जाते हैं(१) असमत्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः ।
विपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ।। २११ - पुरुषार्थसिद्धय पाय
इसमें श्री अमृतचन्द्राचार्यने बतलाया है कि 'रत्नत्रय की विकल रूपसे (एक देश या आंशिक) श्राराधना करनेवाले के जो शुभभावजन्य पुरायकर्मका बन्ध होता है वह मोकी साधनायें सहायक होनेसे मोहोपाय (मोमार्ग) के रूपमें ही परिगहिन है, बन्धनोपायके रूपमें नहीं ।'
"पुश्य बंधन है इसलिये मोषमार्गमें उसका निषेध है—यह बात ठीक है; किन्तु व्यवहारसे भी उसका निषेध करके पापमार्ग में प्रवृत्ति करे तो वह पाप तो कालकूट विषके समान है; अकेले पाप तो नरक-निगोदा
यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि इस वाक्य जय विषयका प्रतिपादन किया गया है वह प्रतिपाद्य वस्तु कानजी स्वामीकी अपनी निजी है या किसी अन्य मतसे ली गई है अथवा जिनशासनका भंग होनेसे जैन चमके अन्तर्गत है? यदि यह कहा जाय कि वह कानजीस्वामी की अपनी निजी वस्तु है तो एक तो उसका यहाँ विचारमें प्रस्तुत करना असंगत है; क्योंकि प्रस्तुत विचार जिनशासनके विषय सम्बन्ध रखता है, न कि कानजीस्वामीको किसी निजी मान्यतासे । दूसरे, कानजीस्वामीके सवज्ञादिरूप कोई विशिष्ट ज्ञानी न होनेमे उनके द्वारा नरक-निगोद में जानेके की बात भी माथमें कुछ बनती नहीं— निराधार ठहरती है। तीसरे, पुण्यरूप विकारकार्य इस तरह करने योग्य होजाता है और कानजीस्वामीका यह कहना है कि 'विकारका कार्य करने योग्य
-ऐसा मानने वाला जीव विकारको नहीं हटा सकता ।” तब फिर ऐसे विकार - कार्यका विधान क्यों जिम्मसे कभी छुटकारा न हो सके ? यह उनके विरुद्ध एक नई श्रापति खड़ी होती है। यदि उसे श्रन्यमको वस्तु बतलाया जाय तो भी यह उसका प्रस्तुतीकरण असंगत है; साथही जैनधर्म एवं जिनशासन से बाह्य ऐसी वस्तुके प्रतिपादनका उन पर आरोप आता है जिसे वे मिथ्या और अभूतार्थं समझते हैं'। और यदि यह
श्री अमृतचन्द्राचार्य जैसे परम आध्यात्मिक विद्वान् भी जय सम्पष्टिके पुण्य-बन्धक शुभभावोंको मोोपायके रूपमें मानते तथा तिपादन करते हैं तब कानजीस्वामीका वैसा मानने से इनकार करना और यह प्रतिपादन करना कि 'जो कोई शुभभावमय पुण्य कर्मको धर्मका साधन माने उसके भी भवन कम नहीं होंगे उनकी आध्यात्मिक एकातताका यदि सूचक समझा जाय तो शायद कुछ भी अनुचित नहीं होगा।
(२) मोक्ष हेतुः पुनर्द्वैधा निश्चय व्यवहारतः । तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद्वितीयस्तस्य साधनम् ॥८
-तत्त्वानुशासन
हमें श्रीरामसेनाचार्यने यह निर्दिष्ट किया है कि मोलमार्ग दो भेदोंमें विभक्त हैमार्ग दो मेरो भिन्न है-एक नियमोपमार्ग और दूसरा व्यवहार-मांसमार्ग निश्चय योषमार्ग माध्यरूपमें स्थित है और 1 व्यवहार-मोक्षमार्ग उसका साधन है। साधन साध्यका विरोधी नहीं होता, दोनों में परम्पर अविनाभाव-संबंध रहता है और इसलिये एकको दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता | ऐसी स्थितमें निश्चय मोक्षमार्ग यदि जिनशासनका चंग है तो व्यवहार-मोषमार्ग भी उमीका अंग है, और इसलिए जिन शासनका यह लक्षण नहीं किया जा सकता कि 'जो शुद्धश्रात्मा वह जिनशासन है' और न यही कहा जा सकता कि 'पूजा-दानवतादि शुभभाव जैनधर्म नहीं है। ऐसा विभाग