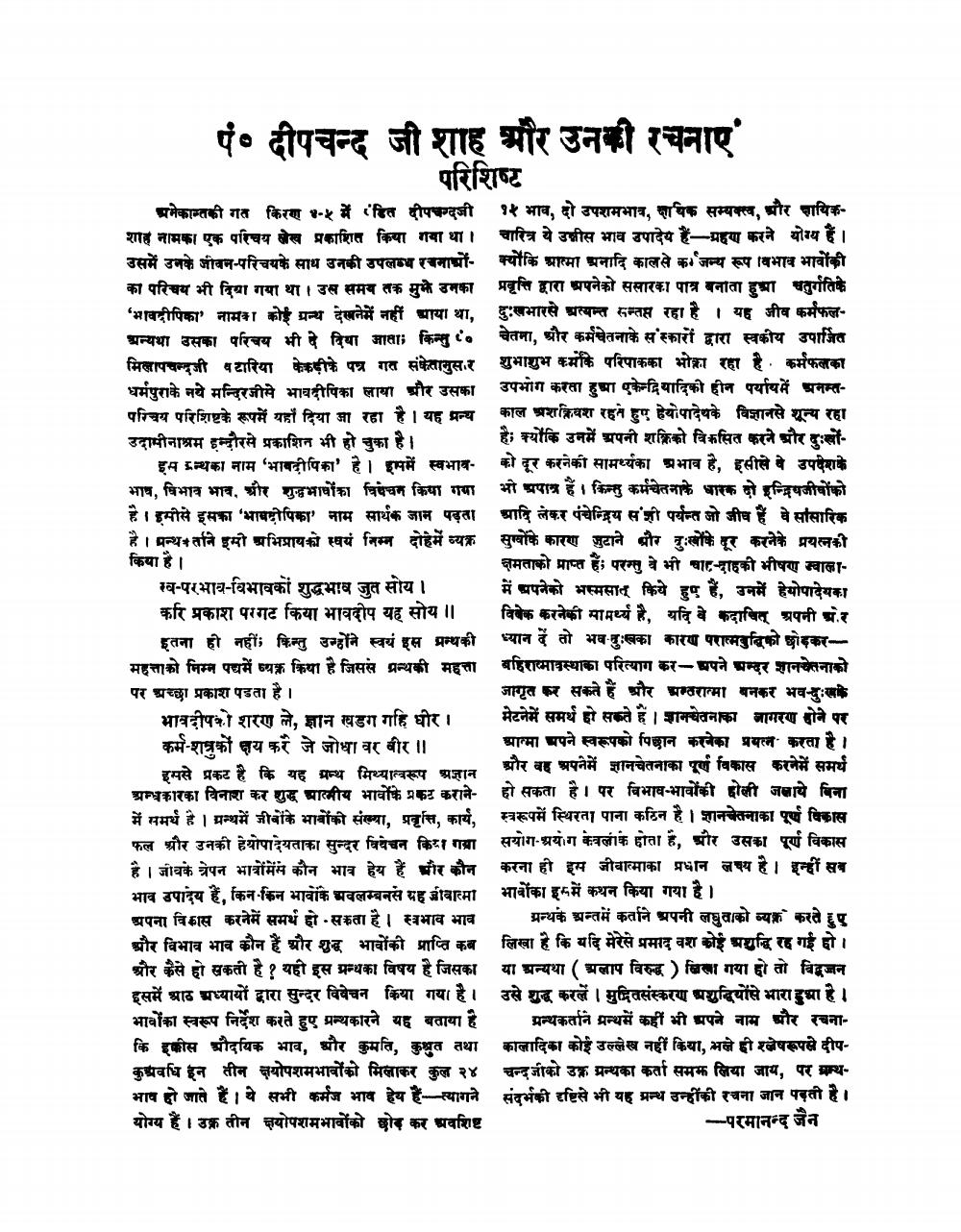________________
पं० दीपचन्द जी शाह और उनकी रचनाए परिशिष्ट
अनेकान्तकी गत किरया ४-५ में डित दीपदवी शाह नामका एक परिचय लेख प्रकाशित किया गया था । उसमें उनके जीवन-परिचयके साथ उनकी उपलब्ध रचनाओंका परिचय भी दिया गया था। उस समय तक मुझे उनका 'भावदीपिका' नामका कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आया था, अन्यथा उसका परिचय भी दे दिया जाता; किन्तु ० मिलापचन्दजी मिलची बटारिया केकड़ी पत्र गत संकेतानुसार धर्मपुरा के नये मन्दिरजीसे भावदीपिका लाया और उसका परिचय परिशिष्टके रूपमें यहाँ दिया जा रहा है। यह प्रन्य उदामीनाश्रम इन्दौर से प्रकाशित भी हो चुका है।
इस ग्रन्थका नाम 'भावदीपिका' है। इसमें स्वभावभाव, विभाव भाव, चीर सुभाषका विवेचन किया गया है। इसीसे इसका 'भावशेषिका' नाम सार्थक जान पड़ता हे मन्याने इमी अभिप्रायको स्वयं निम्न दोहे में व्यक्र । किया है।
स्व-परभाव-विभावकों शुद्धभाव जुत सोय । करि प्रकाश परगट किया भावदोप यह सोय ।।
इतना ही नहीं; किन्तु उन्होंने स्वयं इस प्रन्थकी महलाको निम्न पथमें व्यक्र किया है जिससे ग्रन्थकी महत्ता पर अच्छा प्रकाश पडता है ।
भावदीपको शरण ने ज्ञान खडग गहि धीर कर्म-शत्रुक्षय करें जे जोधा वर बीर ॥
इससे प्रकट है कि यह ग्रन्थ मिथ्यात्वरूप अज्ञान अन्धकारका विनाश कर शुद्ध आत्मीय भावके प्रकट करानेमें समर्थ है। ग्रन्थ जीव भावोंकी संख्या, प्रश कार्य फल और उनकी हेयोपादेयताका सुन्दर विवेचन किया गया हे जीवके प्रेपन भावमिंग कीन भाव हेम है और कौन
I
१५ भाव, दो उपशमभाव, क्षायिक सम्यक्त्व, ' और शायिकचारित्रये उनीस भाव उपादेय है— ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि आत्मा अनादि कालसे कजन्य रूप विभाव भावोंकी प्रवृत्ति द्वारा अपनेको ससारका पात्र बनाता हुआ चतुर्गतिके दुःखभारसे अत्यन्त सन्तप्त रहा है । यह जीव कर्मफलचेतना, और कर्मचेतनाके संस्कारों द्वारा स्वकीय उपार्जित शुभाशुभकर्मक परिपाकका भोका रहा है. कर्म कर्मफलका उपभोग करता हुआ एकेन्द्रियादिको हीन पर्याय में अनन्तकाजक्रिय रहने हुए हेयोपादेयके विज्ञानसे शून्य रहा है क्योंकि उनमें अपनी शक्रिको विकसित करने और दुःखोंको दूर करने की सामर्थ्यका अभाव है, इसीसे वे उपदेश भी पात्र हैं। किन्तु कर्मचेतना धारक दो इन्द्रियोंको आदि लेकर पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्यन्त जो जीव हैं वे सांसारिक सुम्बकि कारण गटाने और दुःखोंके दूर करनेके प्रयत्नकी क्षमताको प्राप्त है। परन्तु वे भी चाट- दाइकी भीषया ज्याठामें अपनेको भस्मसात किये हुए हैं, उनमें हेयोपादेयका विवेक करनेकी मात्र है, यदि वे कदाचित् अपनी र ध्यान दें तो भव-दुःखका कारण परात्मबुद्धिको छोड़करबहिरामादस्थाका परित्याग कर अपने अन्दर ज्ञानतनाको जागृत कर सकते हैं और अन्तरात्मा बनकर भव-दुःखके मेटने में समर्थ हो सकते हैं। ज्ञानचेतनाका जागरण होने पर आत्मा अपने स्वरूपको पिछान करनेका प्रयत्न करता है । और वह अपने ज्ञानचेतनाका पूर्ण विकास करनेमें समर्थ हो सकता है । पर विभाव-भावोंकी होली जलाये बिना स्वरूपमें स्थिरता पाना कठिन है। शानचेतनाका पूर्व विकास योगयोग होता है, और उसका पूर्व विकास करना ही इस जीवात्माका प्रधान लक्ष्य है। इन्हीं सब
भाव उपादेय है, किन-किन भावेकि अवलम्बनसे यह जीवभावका इसमें कथन किया गया है।
.
अपना विकास करने में समर्थ हो सकता है । स्वभाव भाव और विभाव भाव कौन हैं और शुद्ध भावोंकी प्राप्ति कब और कैसे हो सकती है ? यही इस ग्रन्थका विषय है जिसका इसमें आठ अध्यायों द्वारा सुन्दर विवेचन किया गया है । भाका स्वरूप निर्देश करते हुए प्रन्धकारने यह बताया है कि इक्कीस औदायिक भाव, और कुमति, कुश्रुत तथा कुअवधि इन तीन क्षयोपशमभावों को मिलाकर कुल २४ भाव हो जाते हैं। ये सभी कर्मज भाव व है—स्थाने हेय योग्य हैं। उक्त तीन क्षयोपशमभावोंको छोड़ कर अवशिष्ट
प्रथम कर्ताने अपनी लघुताको व्यक्त करते हुए जिला है कि यदि मेरेसे प्रमाद यश कोई अशुद्धि रह गई हो। या अन्यथा ( अलाप विरुद्ध ) लिखा गया हो तो विद्वज्जन उसे शुद्ध करलें । मुद्रितसंस्करण अशुद्धियोंसे भारा हुआ है ।
ग्रन्थकर्ताने ग्रन्थमें कहीं भी अपने नाम और रचनाकालादिका कोई उल्लेख नहीं किया, भले ही श्लेषरूपले दीपचन्दजीको उक्त ग्रन्थका कर्ता समझ लिया जाय, पर ग्रन्थसंदर्भकी दृष्टिसे भी यह प्रन्ध उन्हींकी रचना जान पड़ती है। परमानन्द जैन