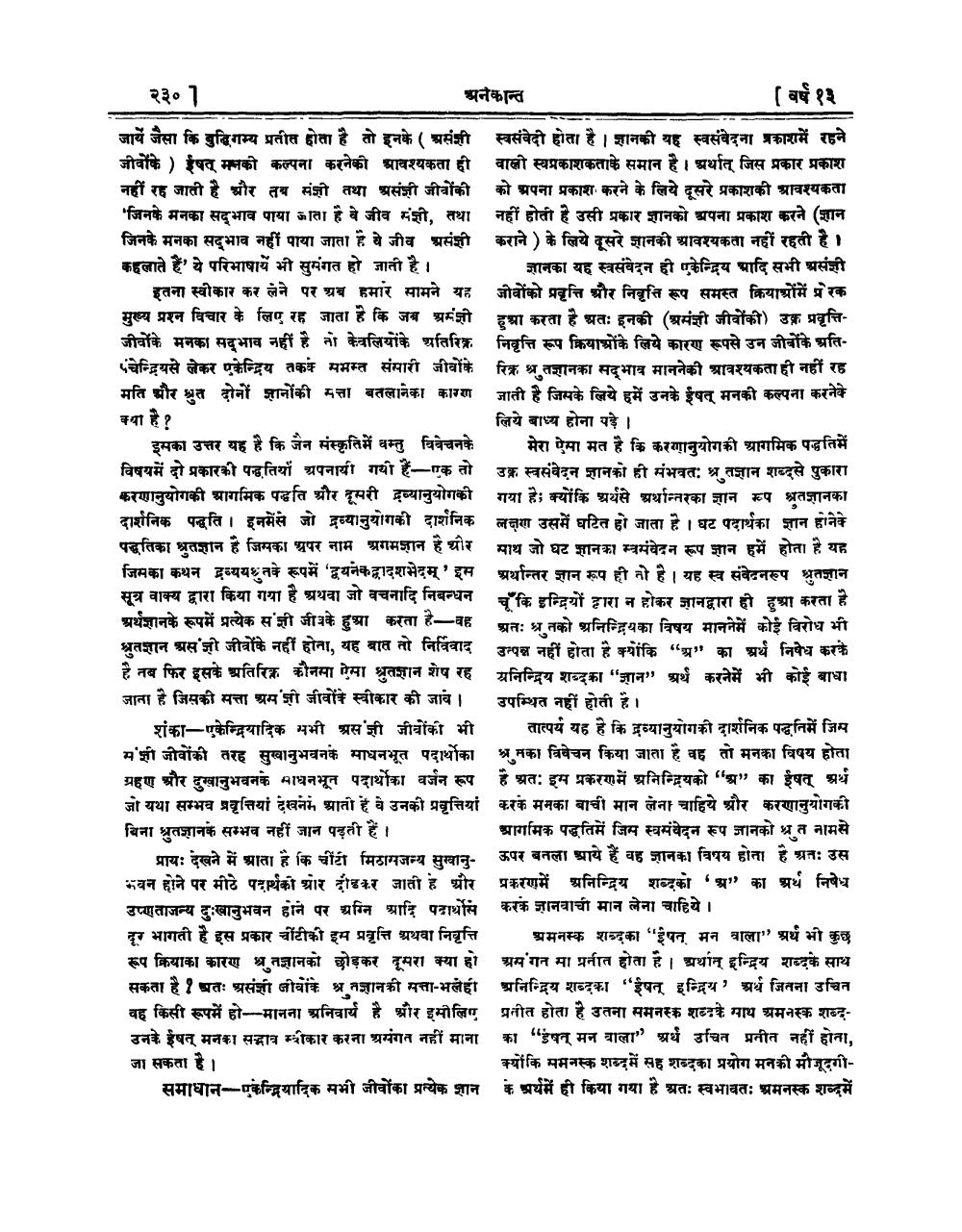________________
२३०]
अनेकान्त
(वर्ष १३
जायें जैसा कि बुद्धिगम्य प्रतीत होता है तो इनके (असंही स्वसंवेदी होता है । ज्ञानकी यह स्वसंवेदना प्रकाशमें रहने जीवोंके ) ईषत् मनको कल्पना करनेको आवश्यकता ही वाली स्वप्रकाशकताके समान है। अर्थात् जिस प्रकार प्रकाश नहीं रह जाती है और तब संज्ञी तथा असंज्ञी जीवोंकी को अपना प्रकाश करने के लिये दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता 'जिनके मनका सद्भाव पाया जाता है वे जीव मंज्ञी, तथा नहीं होती है उसी प्रकार ज्ञानको अपना प्रकाश करने (ज्ञान जिनके मनका सद्भाव नहीं पाया जाता है ये जीव असंज्ञी कराने) के लिये दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती है। कहलाते हैं। ये परिभाषायें भी सुसंगत हो जाती है।
ज्ञानका यह स्वसंवेदन ही एकेन्द्रिय आदि सभी असंज्ञी इतना स्वीकार कर लेने पर अब हमारे सामने यह जीवोंको प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप समस्त क्रियाओं में प्रेरक मुख्य प्रश्न विचार के लिए रह जाता है कि जब अमंज्ञो हा करता है अतः इनकी (अमंज्ञी जीवोंकी) उक प्रवृत्तिजीवोंके मनका सद्भाव नहीं है ना केवलियोंके अतिरिक्र. निवृत्ति रूप क्रियाओं के लिये कारण रूपसे उन जीवोंके अतिपंचेन्द्रियसे लेकर एकेन्द्रिय तक ममम्त संपारी जीवोंके रिक श्र तज्ञानका सदभाव माननेकी आवश्यकता ही नहीं रह मति और श्रुत दोनों ज्ञानोंकी मत्ता बतलानेका कारण जाती है जिसके लिये हमें उनके ईषत् मनकी कल्पना करनेके क्या है?
लिये बाध्य होना पड़े। इसका उत्तर यह है कि जैन संस्कृति में वस्तु विवेचनके मेरा ऐसा मत है कि करणानुयोगकी श्रागमिक पद्धतिमें विषयमें दो प्रकारकी पद्धतियों अपनायी गयी हैं-एक तो उक्त स्वसंवेदन ज्ञानको ही संभवतः श्र तज्ञान शब्दसे पुकारा करणानुयोगकी आगमिक पद्धति और दूसरी द्रव्यानुयोगकी गया है। क्योंकि अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञान रूप श्रुतज्ञानका दार्शनिक पद्धति । इनमेंसे जो द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक लक्षण उसमें घटित हो जाता है। घट पदार्थका ज्ञान होनेके पद्धतिका श्रुतज्ञान है जिम्मका अपर नाम अगमज्ञान है और माथ जो घट ज्ञानका म्नमवेदन रूप ज्ञान हमें होता है यह जिमका कथन द्रव्ययशुनके रूपमें 'द्वयनकद्वादशभेदम् ' इस अर्थान्तर ज्ञान रूप ही तो है। यह स्व संवेदनरूप श्रुतज्ञान सन वाक्य द्वारा किया गया है अथवा जो वचनादि निबन्धन चकि इन्द्रियों द्वारा न होकर ज्ञानद्वारा ही हुआ करता है अर्थज्ञानके रूपमें प्रत्येक संज्ञी जीवके हुआ करता है-वह
अतः श्रुतको अनिन्द्रियका विषय माननेमें कोई विरोध भी श्रतज्ञान असंज्ञी जीवोंके नहीं होता, यह बात तो निर्विवाद नीता
राके है नब फिर इसके अतिरिक्र कौनमा ऐसा श्रुतज्ञान शेष रह ग्रनिन्द्रिय शब्दका "ज्ञान" अर्थ करने में भी कोई बाधा जाना है जिसकी सत्ता अमज्ञी जीवोंके स्वीकार की जावे। उपस्थित नहीं होती है।
शंका-एकेन्द्रियादिक मभी असशी जीवोंकी भी तात्पर्य यह है कि द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धनिमें जिम्म मज्ञी जीवोंकी तरह सुखानुभवनक माधनभूत पदार्थोका श्रु नका विवेचन किया जाता है वह तो मनका विषय होता ग्रहण और दुखानुभवनके माधनभून पदार्थोका वर्जन रूप है अत: इस प्रकरण में अनिन्द्रियको "अ" का ईषत् अर्थ जो यथा सम्भव प्रवृत्तियां देखनम पाती हे वे उनकी प्रवृत्तियां करके ममका बाची मान लेना चाहिये और करणानुयोगकी बिना श्रुतज्ञान सम्भव नहीं जान पड़ती हैं।।
प्रागमिक पद्धतिमें जिम स्वसंवेदन रूप जानको श्रत नामसे प्रायः देखने में आता है कि चींटी मिठामजन्य सुग्वानु- ऊपर बनला पाये हैं वह ज्ञानका विषय होता है अतः उस भवन होने पर मीठे पदार्थको प्रार दौडकर जाती है और प्रकरणमें अनिन्द्रिय शब्दको '" का अर्थ निषेध उप्णताजन्य दुःखानुभवन होने पर अग्नि आदि पदार्थोस करके ज्ञानवाची मान लेना चाहिये। दूर भागती है इस प्रकार चींटीकी इस प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति अमनस्क शब्दका "ईषत् मन वाला" अर्थ भी कुछ रूप क्रियाका कारण श्रु तज्ञानको छोड़कर दूसरा क्या हो अमंगत मा प्रतीत होता है। अर्थात् इन्द्रिय शब्दके साथ सकता है । अतः असंज्ञी जीवोंके अ तज्ञानकी पत्ता-भलेही अनिन्द्रिय शब्दका “ईषत् इन्द्रिय' अर्थ जितना उचित वह किसी रूपमें हो-मानना अनिवार्य है और इसीलिए प्रतीत होता है उतना समनस्क शब्द के साथ अमनस्क शब्दउनके ईषत् मनका सद्भाव म्बीकार करना असंगत नहीं माना का “ईषत् मन बाला" अर्थ उचित प्रतीत नहीं होता, जा सकता है।
क्योंकि ममनस्क शब्दमें सह शब्दका प्रयोग मनकी मौजूदगीसमाधान-एकन्द्रियादिक मभी जीवोंका प्रत्येक ज्ञान के अर्थ में ही किया गया है अतः स्वभावतः अमनस्क शब्दमें