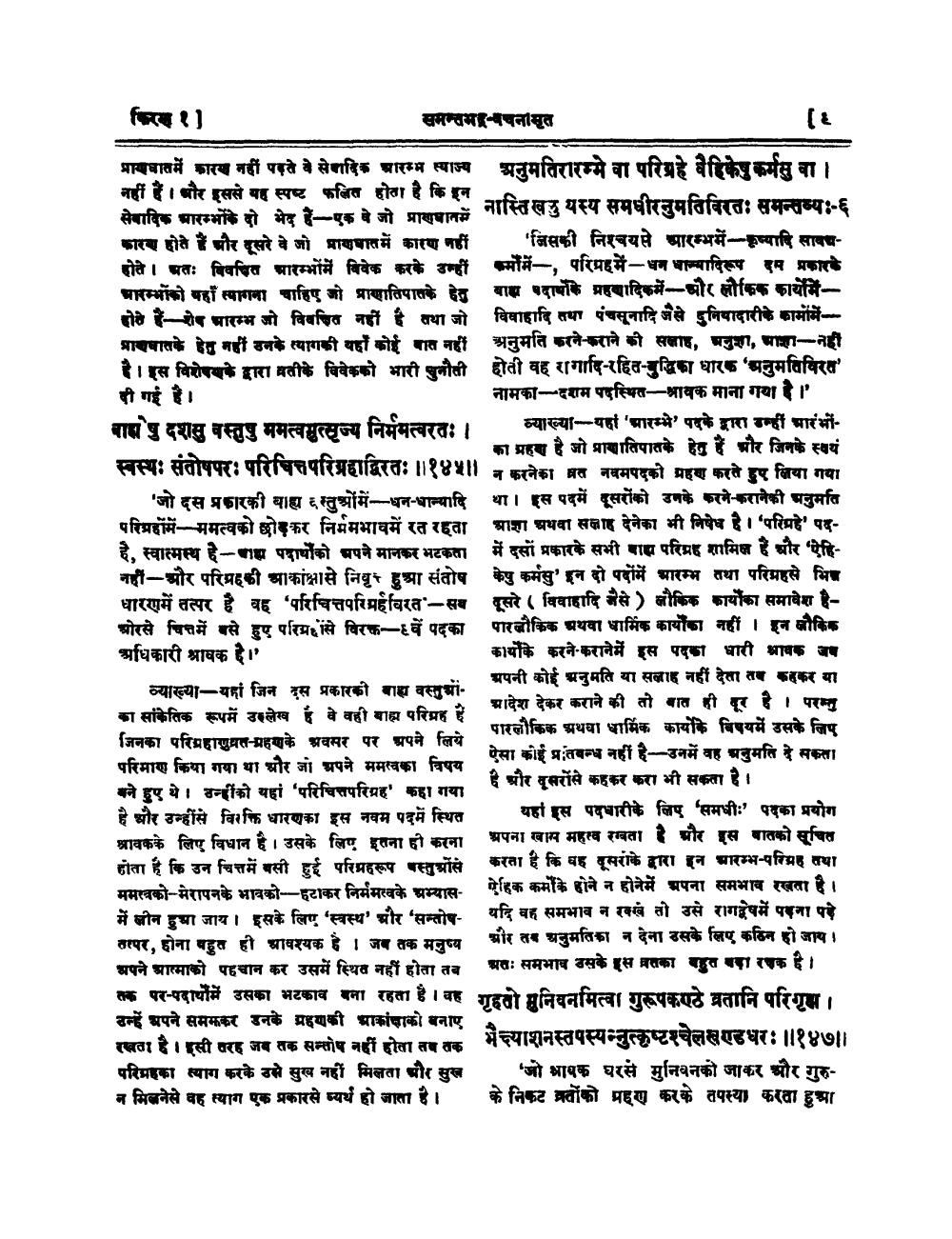________________
फिर ११
प्राणघात कारण नहीं पढ़ते वे सेवादिक धारम्भ स्याज्य नहीं हैं। और इससे यह स्पष्ट फलित होता है कि इन सेवादिक आरम्भोंके दो भेद हैं- एक वे जो प्राणघातले कारव्य होते हैं और दूसरे वे जो प्रायघात में कारण नहीं होते | wतः विवचित चारम्भों में विवेक करके उन्हीं आरम्भको यहाँ त्यागना चाहिए जो प्राणातिपातके हेतु होते हैं—शेष भारम्भ जो विवक्षित नहीं है तथा जो प्राणघातके हेतु नहीं उनके त्यागकी यहाँ कोई बात नहीं है। इस विशेषसके द्वारा प्रतीके विवेकको भारी चुनौती दी गई है।
बाह्य ेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः । स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद्विरतः || १४५||
समन्तभद्र-वचनामृत
'जो दस प्रकारकी बाह्य वस्तुओं में धन-धान्यादि परिग्रहोंमें - ममत्वको छोड़कर निर्ममभावमें रत रहता हे, स्वात्मस्थ है-पास पदार्थोंको अपने मानकर भटकता नहीं - और परिग्रहकी आकांक्षा से निवृ हुआ संतोष धारणमें तत्पर है वह 'परिचिप्तपरिग्रहविरत' - सब ओरसे में बसे हुए परिप्रशंसे विरक्त - ६ वें पदका अधिकारी श्रावक है।"
[ε
अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा । नास्ति खत्रु यस्य समधीरनुमतिविरतः समन्तव्यः-६
व्याख्या - यहां जिन दस प्रकारको बाह्य वस्तुओंका सांकेतिक रूपमें उल्लेख है वे वही बाह्य परिग्रह है जिनका परिग्रहात ग्रहण के अवसर पर अपने लिये परिमाण किया गया था और जो अपने ममत्वका विषय बने हुए थे। उन्हींको यहां 'परिचितपरिग्रह' कहा गया है और उन्हींसे विरक्ति धारणका इस नवम पदमें स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही करना होता है कि उन चित्त में बसी हुई परिग्रहरूप वस्तुसे ममरत्रको - मेरापन के भावको हटाकर निर्ममत्वके अभ्यासमें लीन हुआ जाय। इसके लिए 'स्वस्थ' और 'सन्तोषतत्पर होना बहुत ही आवश्यक है । जब तक मनुष्य अपने आत्माको पहचान कर उसमें स्थित नहीं होता तब
तक पर-पदार्थोंमें उसका भटकाव बना रहता है । वह
उन्हें अपने समझकर उनके ग्रहयकी आकांक्षाको बनाए रखता है। इसी तरह जब तक सन्तोष नहीं होता तब तक परिग्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता और सुख न मिलनेले वह त्याग एक प्रकारसे व्यर्थ हो जाता है।
'जिसकी निश्चयसे आरम्भ में कृष्यादि सावधकमोंमें, परिग्रह में धन धान्यादिरूप दम प्रकारके बाझ पदार्थोंके महयादिक में और लौकिक कार्योंमेंविवाहादि तथा पंचसूनादि जैसे दुनियादारीके कामों में-अनुमति करने-कराने की सलाह, अनुशा, पाहा - नहीं होती वह रागादि-रहित- बुद्धिका धारक 'अनुमतिविरत' नामका - दशम पदस्थित - श्रावक माना गया है ।"
व्याख्या- यहां 'आरम्भे' पदके द्वारा उन्हीं आरंभीका ग्रहण है जो प्राथातिपातके हेतु हैं और जिनके स्वयं न करनेका प्रत नवमपदको ग्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमें दूसरोंको उनके करने-कराने की अनुमति आशा अथवा सलाह देनेका भी निषेध है । 'परिग्रहे' पदमें दसों प्रकारके सभी बाह्य परिग्रह शामिल हैं और 'ऐहिकेषु कर्मसु' इन दो पदोंमें आरम्भ तथा परिग्रहले भिन दूसरे ( विवाहादि जैसे ) लौकिक कार्योंका समावेश हैपारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योंका नहीं । इन लौकिक कार्योंके करने-कराने में इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर कराने की तो बात ही दूर है। परन्तु पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योंके विषयमें उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है उनमें वह अनुमति दे सकता है और दूसरोंसे कहकर करा भी सकता है।
यहां इस पदधारीके लिए 'समधी:' पदका प्रयोग अपना खास महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि वह दूसरोंके द्वारा इन प्रारम्भ-परिग्रह तथा ऐहिक कम होने न होनेमें अपना समभाव रखता । यदि वह समभाव न रक्खे तो उसे रागद्वेषमें पढ़ना पड़े और तब अनुमतिका न देना उसके लिए कठिन हो जाय । अतः समभाव उसके इस व्रतका बहुत बड़ा रक्षक है। गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृक्ष । भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेल ख एडधरः || १४७||
'जो श्रावक घरसे मुनिवनको जाकर और गुरुके निकट व्रतोंको प्रहण करके तपस्या करता हुआ