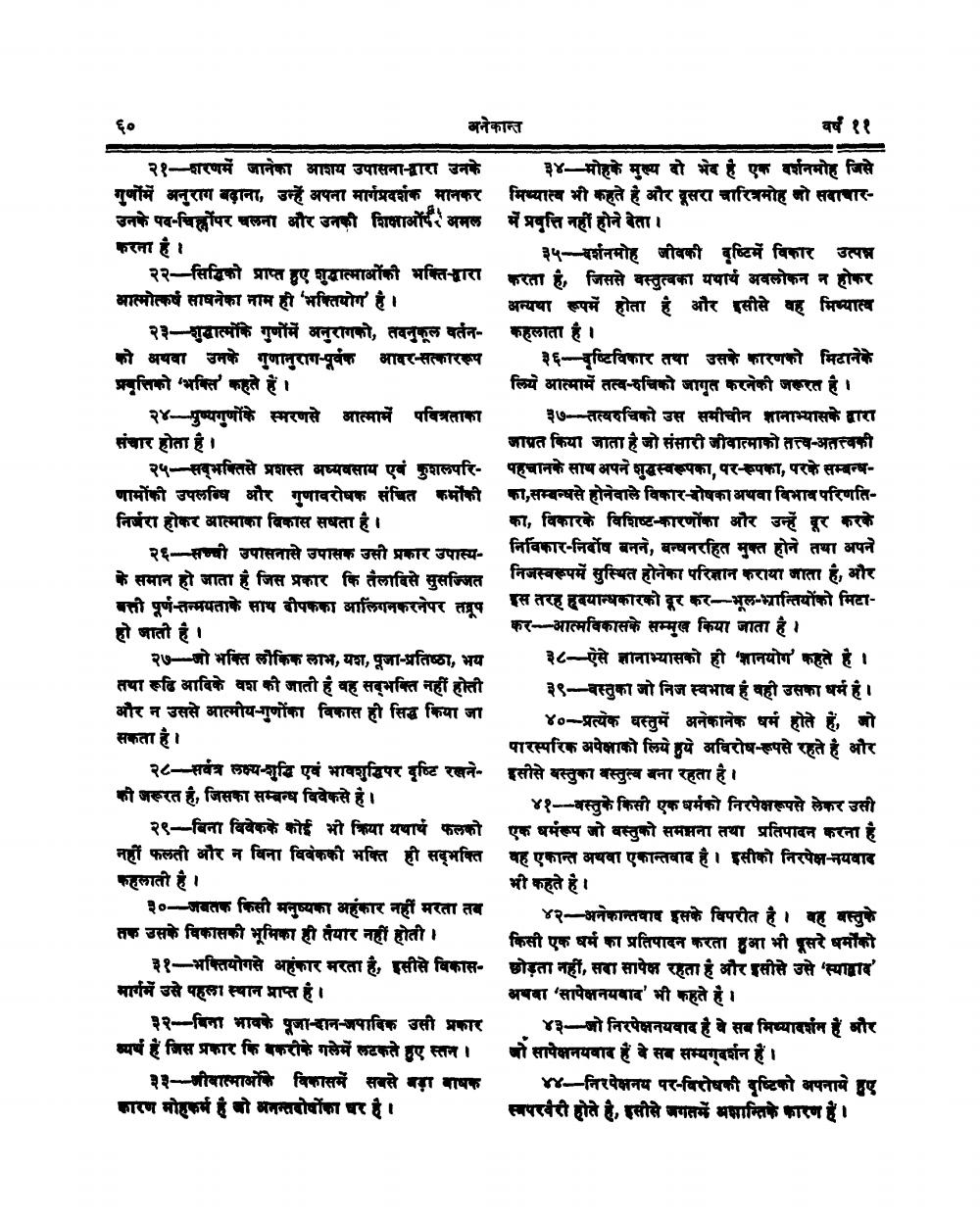________________
६०
अनेकान्त
२१- शरणमें जानेका आशय उपासना-द्वारा उनके गुणोंमें अनुराग बढ़ाना, उन्हें अपना मार्गप्रदर्शक मानकर उनके पदचिह्नों पर चलना और उनकी शिक्षाओंदर अमल करना है ।
२२- सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओंकी भक्ति द्वारा आत्मोत्कर्ष साधनेका नाम ही 'भक्तियोग' है।
२३- शुद्धात्मोंके गुणोंमें अनुरागको तवनुकूल वर्तनको अथवा उनके गुणानुराग- पूर्वक आवर-सत्काररूप प्रवृत्तिको 'भक्ति' कहते हैं ।
२४ -- पुष्पगुणोंके स्मरणसे आत्मामें पवित्रताका संचार होता है।
२५ - सद्भक्तिसे प्रशस्त अध्यवसाय एवं कुशलपरिणामोंकी उपलब्धि और गुणावरोधक संचित कर्मोकी निर्जरा होकर आत्माका विकास सकता है ।
२६- सच्ची उपासनासे उपासक उसी प्रकार उपास्यके समान हो जाता है जिस प्रकार कि तैलाविसे सुसज्जित बत्ती पूर्ण तन्मयता के साथ दीपकका आलिंगनकरनेपर तद्रूप हो जाती है ।
२७ - जो भक्ति लौकिक लाभ, यश, पूजा-प्रतिष्ठा, भय तथा रूढि आदिके वश की जाती है वह सद्भक्ति नहीं होती और न उससे आत्मीय गुणोंका विकास ही सिद्ध किया जा सकता है।
२८- सर्वत्र लक्ष्य-शुद्धि एवं भावशुद्धिपर दृष्टि रखनेकी जरूरत है, जिसका सम्बन्ध विवेकसे है।
२९ -- बिना विवेकके कोई भी क्रिया यथार्थ फलको नहीं फलती और न विना विवेककी भक्ति ही सद्भक्ति कहलाती है ।
३० - जबतक किसी मनुष्यका अहंकार नहीं मरता तब तक उसके विकासकी भूमिका ही तैयार नहीं होती।
३१ - भक्तियोगसे अहंकार मरता है, इसीसे विकासमार्ग में उसे पहला स्थान प्राप्त है।
३२ -- बिना भावके पूजा-दान-जपाविक उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार कि बकरीके गलेमें लटकते हुए स्तन ।
वर्ष ११
३४ – मोहके मुख्य दो भेद है एक दर्शनमोह जिसे मिथ्यात्व भी कहते है और दूसरा चारित्रमोह जो सदाचारमें प्रवृत्ति नहीं होने देता ।
३३- जीवात्माओंके विकासमें सबसे बड़ा बाधक कारण मोहकर्म है जो अनन्तदोषोंका घर है।
३५ - दर्शनमोह जीवकी दृष्टिमें विकार उत्पन्न करता है, जिससे वस्तुत्वका यथार्थ अवलोकन न होकर अन्यथा रूपमें होता है और इसीसे वह मिथ्यात्व कहलाता है ।
३६- दृष्टिविकार तथा उसके कारणको मिटानेके लिये आत्मामें तत्व-दचिको जागृत करनेकी जरूरत है
३७ -- तत्वदचिको उस समीचीन ज्ञानाभ्यासके द्वारा जाग्रत किया जाता है जो संसारी जीवात्माको तत्त्व-अतस्त्वकी पहचानके साथ अपने शुद्धस्वरूपका, पर-रूपका, परके सम्बन्धका, सम्बन्धसे होनेवाले विकार-दोषका अथवा विभाव परिणतिका, विकारके विशिष्ट कारणोंका और उन्हें दूर करके निर्विकार - निर्दोष बनने, बन्धनरहित मुक्त होने तथा अपने निजस्वरूपमें सुस्थित होनेका परिज्ञान कराया जाता है, और इस तरह हृदयान्धकारको दूर कर -- भूल-भ्रान्तियोंको मिटाकर -- आत्मविकासके सम्मुख किया जाता है ।
३८ - ऐसे ज्ञानाभ्यासको ही 'ज्ञानयोग' कहते है । ३९ -- वस्तुका जो निज स्वभाव है वही उसका धर्म है । ४० -- प्रत्येक वस्तुमें अनेकानेक धर्म होते हैं, जो पारस्परिक अपेक्षाको लिये हुये अविरोध-रूपसे रहते है और इसीसे वस्तुका वस्तुत्व बना रहता है।
४१ -- वस्तुके किसी एक धर्मको निरपेक्षरूपसे लेकर उसी एक धर्मरूप जो वस्तुको समझना तथा प्रतिपादन करना वह एकान्त अथवा एकान्तवाद है। इसीको निरपेक्ष-नयवाद भी कहते है ।
४२ -- अनेकान्तवाद इसके विपरीत है। वह वस्तुके किसी एक धर्म का प्रतिपादन करता हुआ भी दूसरे धर्मोको छोड़ता नहीं, सबा सापेक्ष रहता है और इसीसे उसे 'स्याद्वाद' अथवा 'सापेक्षनयवाद' भी कहते है ।
४३ - जो निरपेक्षनयवाद है वे सब मिथ्यादर्शन हैं और जो सापेक्षनयवाद हैं वे सब सम्यग्दर्शन हैं।
४४ - निरपेक्षनय पर विरोधकी दृष्टिको अपनाये हुए स्वपरवरी होते है, इसीसे जगतमें अशान्तिके कारण हैं।