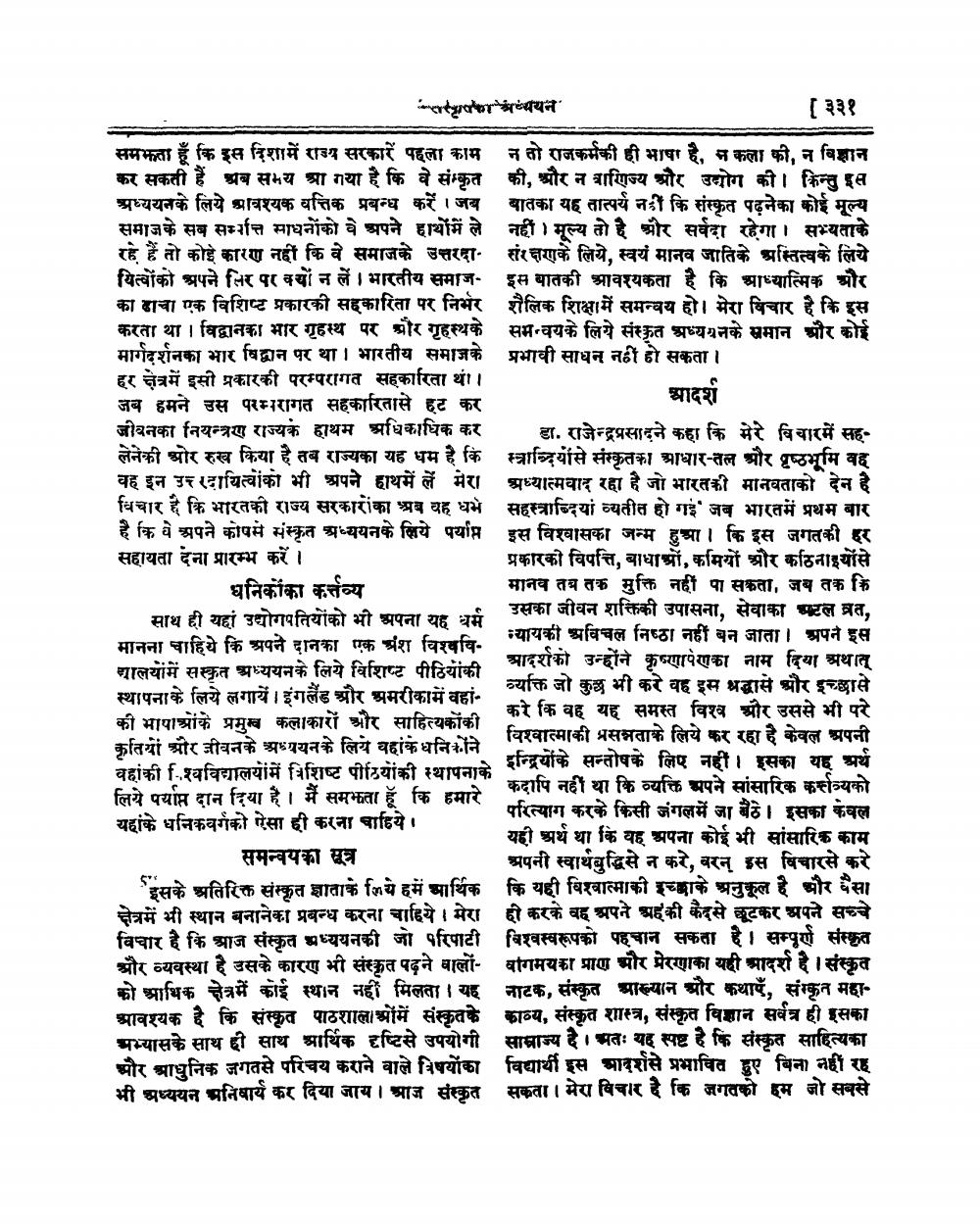________________
समझता हूँ कि इस दिशा में राज्य सरकारें पहला काम कर सकती हैं अब समय आ गया है कि वे संस्कृत अध्ययनके लिये श्रावश्यक वत्तिक प्रबन्ध करें । जब समाज के सब सति साधनोंको वे अपने हाथोंमें ले रहे हैं तो कोई कारण नहीं कि वे समाजके उत्तरदायित्वों को अपने सिर पर क्यों न लें। भारतीय समाजका ढाचा एक विशिष्ट प्रकारकी सहकारिता पर निर्भर करता था । विद्वानका भार गृहस्थ पर और गृहस्थ के मार्गदर्शनका भार विद्वान पर था । भारतीय समाज के हर क्षेत्र में इसी प्रकार की परम्परागत सहकारिता थी । जब हमने उस परम्परागत सहकारितासे हट कर जीवनका नियन्त्रण राज्यकं हाथम अधिकाधिक कर लेने की ओर रुख किया है तब राज्यका यह धम है कि वह इन उपरदायित्वों को भी अपने हाथमें लें मेरा विचार है कि भारतकी राज्य सरकारोंका अब यह धर्म है कि वे अपने कोपसे संस्कृत अध्ययन के लिये पर्याप्त सहायता देना प्रारम्भ करें ।
धनिकों का कर्त्तव्य
साथ ही यहां उद्योगपतियोंको भी अपना यह धर्म मानना चाहिये कि अपने दानका एक अंश विश्वविद्यालयोंमें संस्कृत अध्ययनके लिये विशिष्ट पीठियांकी स्थापना के लिये लगायें। इंगलैंड और अमरीका में वहांकी भाषाओंके प्रमुख कलाकारों और साहित्यकोंकी कृतियों और जीवनके अध्ययन के लिये वहांके धनिकोंने वहांकी f·श्वविद्यालयोंमें त्रिशिष्ट पीटियों की स्थापनाके लिये पर्याप्त दान दिया है । मैं समझता हूँ कि हमारे यहांके धनिकवर्गको ऐसा ही करना चाहिये । समन्वयका सूत्र
"इसके अतिरिक्त संस्कृत ज्ञाताके लिये हमें आर्थिक क्षेत्र में भी स्थान बनानेका प्रबन्ध करना चाहिये। मेरा विचार है कि आज संस्कृत अध्ययनकी जो परिपाटी और व्यवस्था है उसके कारण भी संस्कृत पढ़ने वालोंको आर्थिक क्षेत्र में कोई स्थान नहीं मिलता। यह आवश्यक है कि संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृतके अभ्यासके साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिसे उपयोगी और आधुनिक जगतसे परिचय कराने वाले त्रिषयोंका भी अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाय। आज संस्कृत
अध्ययन'
[ ३३१
न तो राजकर्मकी ही भाषा है, न कला की, न विज्ञान की, और न वाणिज्य और उद्योग की । किन्तु इस बातका यह तात्पर्य नहीं कि संस्कृत पढ़नेका कोई मूल्य नहीं। मूल्य तो है और सर्वदा रहेगा। सभ्यताके संरक्षण के लिये, स्वयं मानव जाति के अस्तित्व के लिये इस बातकी आवश्यकता है कि आध्यात्मिक और शैलिक शिक्षा में समन्वय हो । मेरा विचार है कि इस समन्वय के लिये संस्कृत अध्ययनके समान और कोई प्रभावी साधन नहीं हो सकता ।
आदर्श
डा. राजेन्द्रप्रसाद ने कहा कि मेरे विचार में सहस्त्राब्दियोंसे संस्कृतका आधार-तल और पृष्ठभूमि वह अध्यात्मवाद रहा है जो भारतकी मानवताको देन है सहस्त्राब्दियां व्यतीत हो गई जब भारतमें प्रथम बार इस विश्वासका जन्म हुआ। कि इस जगतकी हर प्रकारको विपत्ति, बाधाओं, कमियों और कठिनाइयों से मानव तब तक मुक्ति नहीं पा सकता, जब तक कि उसका जीवन शक्तिकी उपासना, सेवाका घटल व्रत, न्यायकी अविचल निष्ठा नहीं बन जाता। अपने इस व्यक्ति जो कुछ भी करे वह इस श्रद्धा और इच्छा आदर्शको उन्होंने कृष्णार्पणका नाम दिया अथात् करे कि वह यह समस्त विश्व और उससे भी परे विश्वात्मा की प्रसन्नता के लिये कर रहा है केवल अपनी इन्द्रियोंके सन्तोषके लिए नहीं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं था कि व्यक्ति अपने सांसारिक कर्त्तव्यको परित्याग करके किसी जंगलमें जा बैठे। इसका केवल यही अर्थ था कि वह अपना कोई भी सांसारिक काम अपनी स्वार्थबुद्धिसे न करे, वरन् इस विचारसे करे कि यही विश्वात्माकी इच्छा के अनुकूल है और पैसा ही करके वह अपने अहंकी कैद से छूटकर अपने सच्चे विश्वस्वरूपको पहचान सकता है। सम्पूर्ण संस्कृत वांगमयका प्राण और प्रेरणाका यही आदर्श है । संस्कृत नाटक, संस्कृत आख्यान और कथाएँ, संस्कृत महाकाव्य, संस्कृत शास्त्र, संस्कृत विज्ञान सर्वत्र ही इसका साम्राज्य है। अतः यह स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्यका विद्यार्थी इस आदर्शसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मेरा विचार है कि जगतको हम जो सबसे