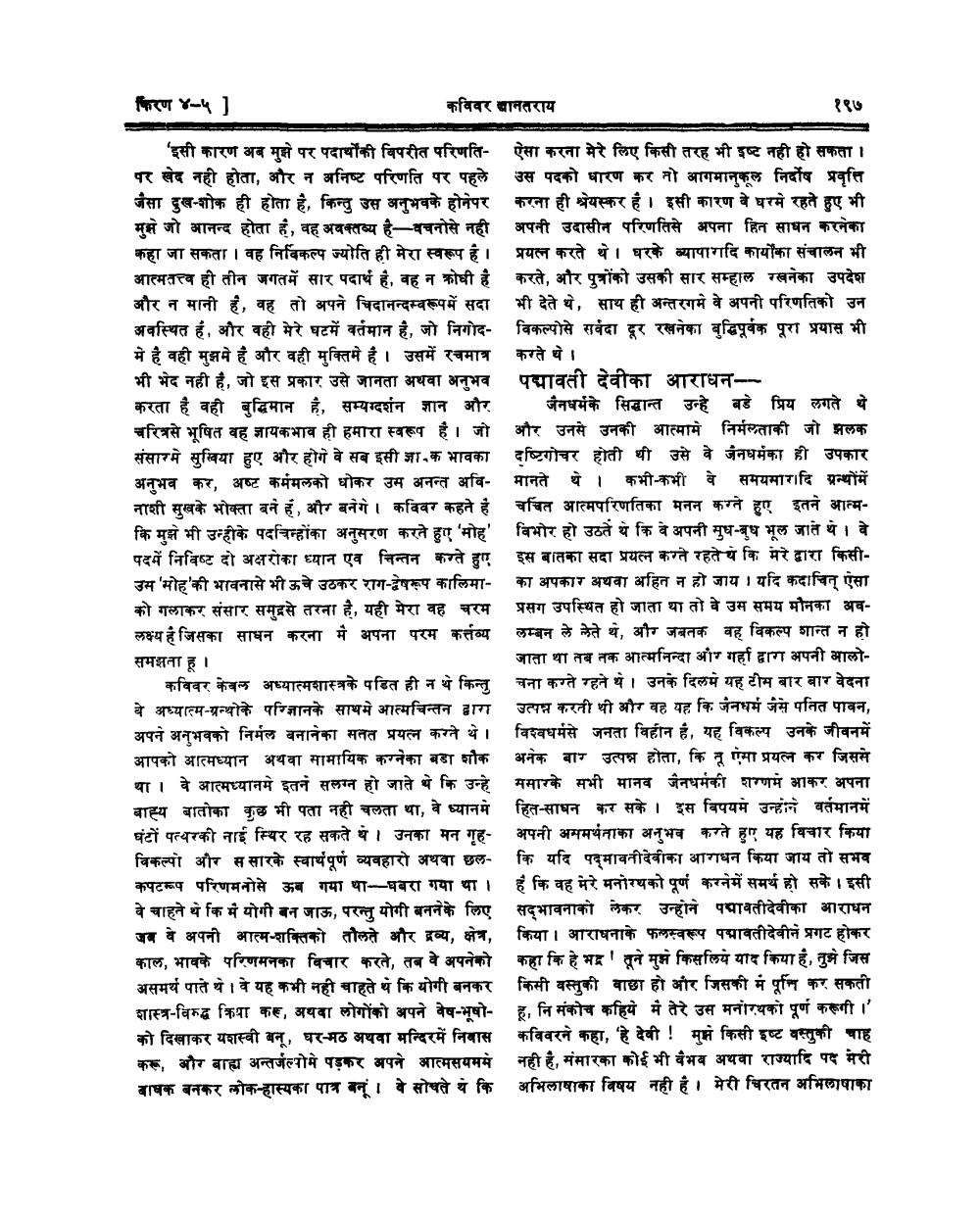________________
किरण ४-५ ]
I
'इसी कारण अब मुझे पर पदार्थोंकी विपरीत परिणति पर खेद नही होता, और न अनिष्ट परिणति पर पहले जैसा दुख-शोक ही होता है, किन्तु उस अनुभव होनेपर मुझे जो आनन्द होता है, वह अवक्तव्य है-वचनोसे नही कहा जा सकता । वह निर्विकल्प ज्योति ही मेरा स्वरूप है । आत्मतत्त्व ही तीन जगतमें सार पदार्थ है. वह न श्रोषी है और न मानी है, वह तो अपने चिदानन्दम्बरूप में सदा अवस्थित है, और वही मेरे घटमें वर्तमान है, जो निगोदमे है वही मुझमे हैं और वही मुक्तिमे है उसमें रवमात्र भी भेद नही है, जो इस प्रकार उसे जानता अथवा अनुभव करता है नही बुद्धिमान है, सम्यग्दर्शन ज्ञान और चरित्र भूषित वह ज्ञायकभाव ही हमारा स्वरूप है । जो संसार मे सुखिया हुए और होगे वे सब इसी ज्ञा.क भावका अनुभव कर, अष्ट कर्ममलको धोकर उस अनन्त अविनाशी सुखके भोक्ता बने हैं, और बनेगे । कविवर कहते है कि मुझे भी उन्ही के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए 'मोह' पदमें निविष्ट दो अक्षरोका ध्यान एव चिन्तन करते हुए उम 'मोह' की भावनासे भी ऊचे उठकर राग-द्वेषरूप कालिमाको गलाकर संसार समुद्रसे तरना है, यही मेरा वह चरम लक्ष्य है जिसका साधन करना में अपना परम कर्तव्य समझता हू ।
कविवर केवल अध्यात्मशास्त्र के पडित ही न थे किन्तु वे अध्यात्म-ग्रन्थोके परिज्ञानके साथ मे आत्मचिन्तन द्वारा अपने अनुभवको निर्मल बनानेका सतत प्रयत्न करते थे । आपको आत्मध्यान अथवा सामायिक करनेका बडा शौक था । वे आत्मध्यानमे इतनं सलग्न हो जाते थे कि उन्हें बाह्य बातोका कुछ भी पता नही चलता था, वे ध्यान मे घंटों पत्थरकी नाई स्थिर रह सकते थे। उनका मन गृह विकल्पों और ससारके स्वायंपूर्ण व्यवहारो अथवा छलकपटरूप परिणमनोसे ऊब गया था -- घबरा गया था ।
वे चाहते थे कि में योगी बन जाऊ, परन्तु योगी बनने के लिए जब वे अपनी आत्म-शक्तिको तौलते और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके परिणमनका विचार करते, तब वे अपने को असमर्थ पाते थे । वे यह कभी नही चाहते थे कि योगी बनकर शास्त्र विरुद्ध किया कह अथवा लोगोंको अपने वेष-भूषो को दिखाकर यशस्वी बनू, घर- मठ अथवा मन्दिरमें निवास करू, और बाह्य अन्तर्जल्पोमे पड़कर अपने आत्मसयममे बाचक बनकर लोक-हास्यका पात्र बनूं। वे सोचते थे कि
कविवर खानतराय
१९७
ऐसा करना मेरे लिए किसी तरह भी इष्ट नही हो सकता । उस पदको धारण कर तो आगमानुकूल निर्दोष प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है। इसी कारण वे घरमे रहते हुए भी अपनी उदासीन परिणतिसे अपना हित साधन करनेका प्रयत्न करते थे । घरके व्यापारादि कार्योका संचालन भी करते और पुत्रोंको उसकी सार सम्हाल रखनेका उपदेश भी देते थे, साथ ही अन्तरगमे वे अपनी परिणतिको उन विकल्पोसे सर्वदा दूर रखनेका बुद्धिपूर्वक पूरा प्रयास भी करते थे ।
पद्मावती देवीका आराधन---
जैनधर्मके सिद्धान्त उन्हें बड़े प्रिय लगते थे और उनसे उनकी आत्मामे निर्मलताकी जो झलक दृष्टिगोचर होती थी उसे वे जनधर्मका ही उपकार मानते थे । कभी-कभी वे समयमारदि ग्रन्थोंमें चर्चित आत्मपरिणतिका मनन करते हुए इतने आत्मविभोर हो उठते थे कि वे अपनी सुध-बुध भूल जाते थे। वे इस बात का सदा प्रयत्न करते रहते थे कि मेरे द्वारा किसीSat अपकार अथवा अहित न हो जाय । यदि कदाचित् ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता था तो वे उस समय मौनका अवलम्बन ले लेते थे, और जबतक वह विकल्प शान्त न हो जाता था तब तक आत्मनिन्दा और गढ़ द्वारा अपनी आलोचना करते रहते थे। उनके दिलमे यह टीम बार बार वेदना उत्पन्न करती थी और वह यह कि जैनधर्म जैसे पतित पावन, विश्वधर्मसे जनता विहीन है. यह विकस्य उनके जीवनमें अनेक बार उत्पन्न होता, कि तू ऐसा प्रयत्न कर जिसमे ममारके सभी मानव जैनधर्मकी शरणमं आकर अपना हित-साधन कर सके। इस विपयमे उन्होंने वर्तमानमें अपनी असमर्थताका अनुभव करते हुए यह विचार किया कि यदि पद्मावतीदेवीका आगमन किया जाय तो समय हैं कि वह मेरे मनोरथको पूर्ण करने में समर्थ हो सके। इसी सद्भावनाको लेकर उन्होंने पद्मावतीदेवीका आराधन किया। आराधनाके फलस्वरूप पद्मावतीदेवीनं प्रगट होकर कहा कि हे म तूने मुझे किसलिये याद किया है, तुझे जिस किमी वस्तुकी बाछा हो और जिसकी में पूर्ति कर सकती हू नि संकोच कहिये मे तेरे उस मनोरथको पूर्ण करूंगी।' कविवरने कहा, 'हे देवी! मुझे किसी इष्ट वस्तुकी चाह नही है, संसारका कोई भी वैभव अथवा राज्यादि पद मेरी अभिलाषाका विषय नही है। मेरी चिरतन अभिलाषाका
1