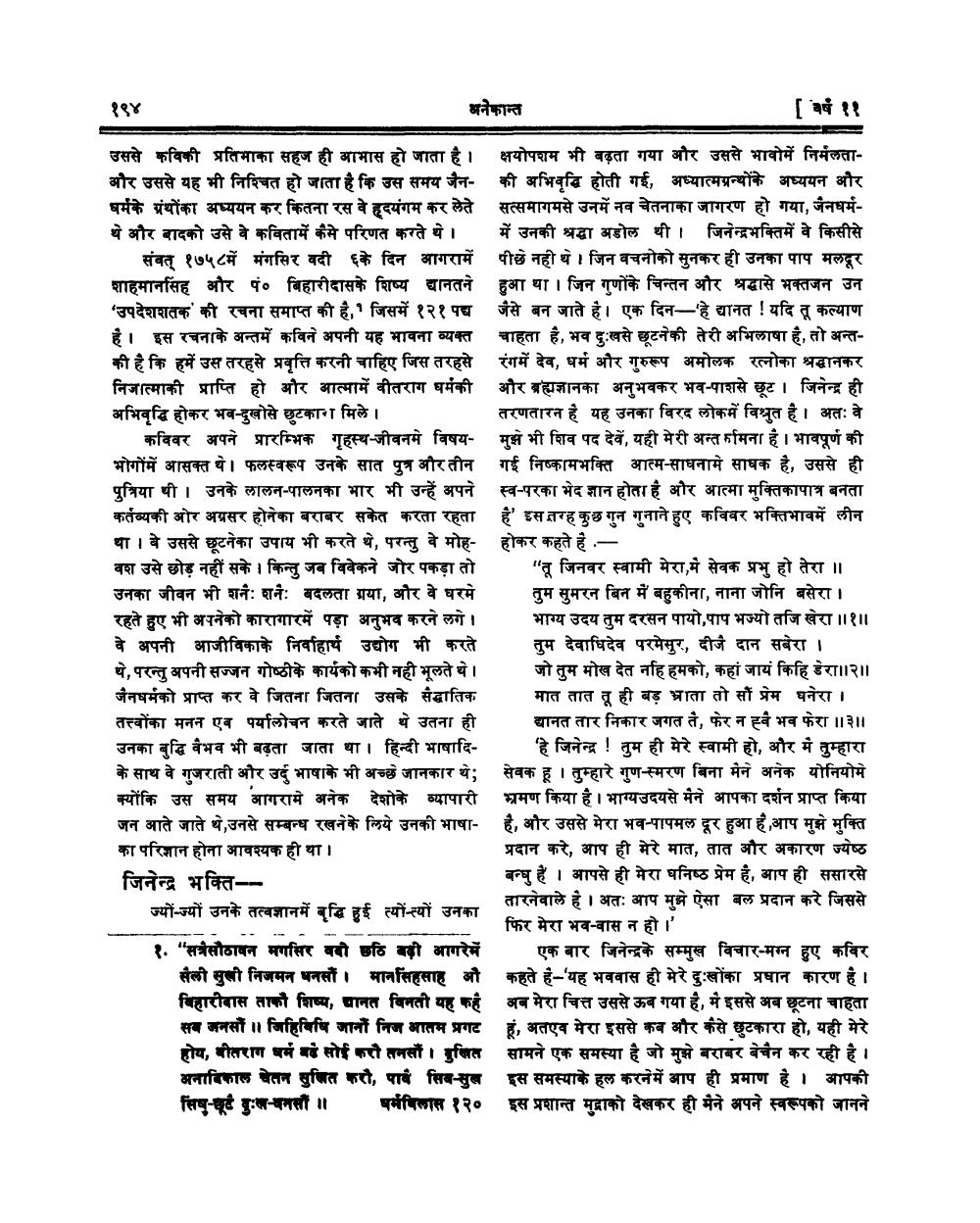________________
अनेकान्त
१९४
उससे कविकी प्रतिभाका सहज ही आभास हो जाता है । और उससे यह भी निश्चित हो जाता है कि उस समय जैनधर्म ग्रंथोंका अध्ययन कर कितना रस वे हृदयंगम कर लेते थे और बादको उसे वे कवितायें कैसे परिणत करते थे। संवत् १७५८में मंगसिर यदी के दिन आगरामें शाहमानसिंह और पं० बिहारीदासके शिष्य चानतने 'उपदेशशतक' की रचना समाप्त की है, जिसमें १२१ पद्म है । इस रचना के अन्तमें कविने अपनी यह भावना व्यक्त की है कि हमें उस तरहसे प्रवृत्ति करनी चाहिए जिस तरहसे निजात्माकी प्राप्ति हो और मात्मामें वीतराग धर्मकी अभिवृद्धि होकर भव-दुखोटा मिले।
।
कविवर अपने प्रारम्भिक गृहस्थ जीवनमे विषय भोगों में आसक्त थे। फलस्वरूप उनके सात पुत्र और तीन पुत्रिया थी । उनके लालन-पालनका भार भी उन्हें अपने कर्तव्यकी ओर अग्रसर होनेका बराबर सकेत करता रहता था। वे उससे छूटने का उपाय भी करते थे, परन्तु वे मोह वश उसे छोड़ नहीं सके। किन्तु जब विवेकने जोर पकड़ा तो उनका जीवन भी शनैः शनैः बदलता गया, और वे घरमे रहते हुए भी अपनेको कारागारमें पड़ा अनुभव करने लगे । वे अपनी आजीविकाके निर्वाहार्थ उद्योग भी करते थे, परन्तु अपनी सज्जन गोष्ठीके कार्यको कभी नही भूलते थे। जैनधर्मको प्राप्त कर वे जितना जितना उसके सैद्धातिक तत्त्वोंका मनन एवं पर्यालोचन करते जाते थे उतना ही उनका बुद्धि वैभव भी बढ़ता जाता था। हिन्दी भाषादिके साथ वे गुजराती और उर्दु भाषाके भी अच्छे जानकार थे; क्योंकि उस समय आगरामे अनेक देशोके व्यापारी जन आते जाते थे, उनसे सम्बन्ध रखनेके लिये उनकी भाषाका परिशान होना आवश्यक ही था । जिनेन्द्र भक्ति-
ज्यों-क्यों उनके तत्वज्ञानमें वृद्धि हुई त्यों-त्यों उनका
[ वर्ष ११
क्षयोपशम भी बढ़ता गया और उससे भावोमें निर्मलताकी अभिवृद्धि होती गई, अध्यात्मग्रन्थोंके अध्ययन और सत्समागमसे उनमें नव चेतनाका जागरण हो गया, जैनधर्ममें उनकी श्रद्धा अडोल थी । जिनेन्द्रभक्तिमें वे किसीसे पीछे नही थे। जिन वचनोको सुनकर ही उनका पाप मलदूर हुआ था। जिन गुणोंके चिन्तन और श्रद्धासे भक्तजन उन जैसे बन जाते हैं। एक दिन - 'हे द्यानत ! यदि तु कल्याण चाहता है, भव दुःखसे छूटने की तेरी अभिलाषा है, तो अन्तरंगमें देव, धर्म और गुरुरूप अमोलक रत्नोका श्रद्धानकर और ब्रह्मज्ञानका अनुभवकर भव-पाशसे छूट । जिनेन्द्र ही तरणतारन है यह उनका विरद लोकमें विश्रुत है । अतः वे मुझे भी शिव पद देवें, यही मेरी अन्त कमिना है। भावपूर्ण की गई निष्कामभक्ति आत्म-साधनामे साधक है, उससे ही स्व-परका भेद ज्ञान होता है और आत्मा मुक्तिकापात्र बनता है इस तरह कुछ गुन गुनाते हुए कविवर भक्तिभावमें लीन होकर कहते हैं
-- .
" तू जिनवर स्वामी मेरा मे सेवक प्रभु हो तेरा ॥ तुम सुमरन बिन में बहुकीना, नाना जोनि बसेरा । भाग्य उदय तुम दरसन पायो, पाप भज्यो तजि खेरा ॥ १ ॥ तुम देवाधिदेव परमेसुर, दीजै दान सबेरा । जो तुम मोल देत नहि हमको, कहां जायं किहि डेरा || २ || मात तात तू ही बड़ भ्राता तो सौं प्रेम घनेरा । द्यानत तार निकार जगत तं, फेर न वै भव फेरा ॥ ३ ॥ 'हे जिनेन्द्र ! तुम ही मेरे स्वामी हो, और में तुम्हारा सेवक हू । तुम्हारे गुण-स्मरण बिना मैने अनेक योनियोमे भ्रमण किया है। भाग्यउदयसे मैने आपका दर्शन प्राप्त किया है, और उससे मेरा भव-पापमल दूर हुआ है, आप मुझे मुक्ति प्रदान करे, आप ही मेरे मात, तात और अकारण ज्येष्ठ बन्धु हैं। आपसे ही मेरा घनिष्ठ प्रेम है, आप ही ससारसे तारनेवाले है । अतः आप मुझे ऐसा बल प्रदान करे जिससे फिर मेरा भव-वास न हो ।'
१. " सत्रेसौठावन मगसिर वदी छठि बढ़ी आगरेमें सैको सुखी निजमन घनसौं मानसिहसाह मौ बिहारीबास ताकी शिष्य, धानत विनती यह कहे सब जनसों ॥ जिहिविधि जानौं निज आतम प्रगट होय, बीतराग धर्म बढे सोई करी तमसाँ दुखित अनादिकाल चेतन सूचित करो, पार्व सिव-सुख सि- दुःख-बनसी ॥
१२०
एक बार जिनेन्द्रके सम्मुख विचार-मग्न हुए कविर कहते है-'वह भववास ही मेरे दुःखोंका प्रधान कारण है। अब मेरा पित्त उससे ऊब गया है, में इससे अब छूटना चाहता हूं, अतएव मेरा इससे कब और कैसे छुटकारा हो, यही मेरे सामने एक समस्या है जो मुझे बराबर बेचैन कर रही है। इस समस्याके हल करने में आप ही प्रमाण है । आपकी इस प्रशान्त मुद्राको देखकर ही मैने अपने स्वरूपको जानने