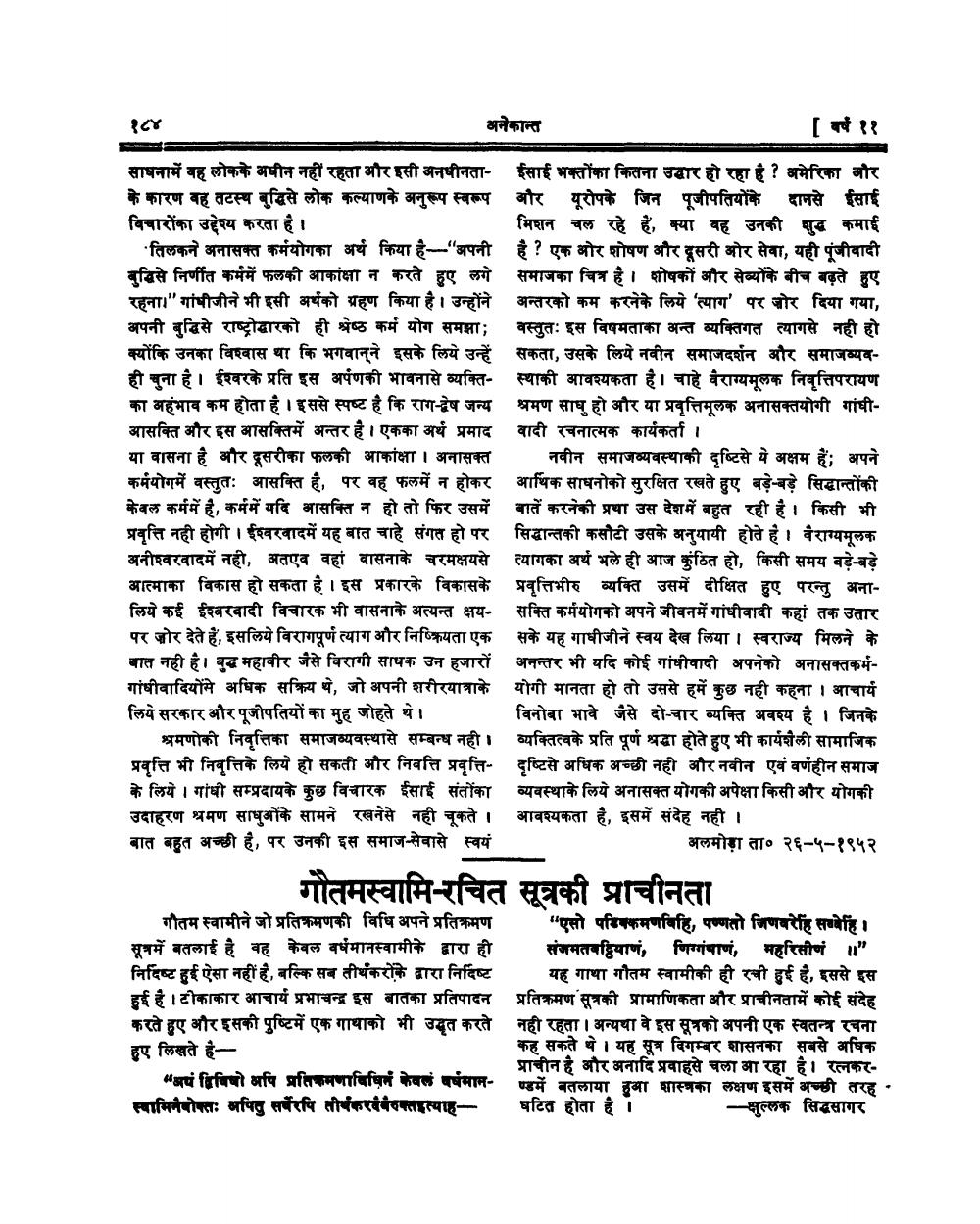________________
अनेकान्त
[ वर्ष ११ साधनामें वह लोकके अधीन नहीं रहता और इसी अनधीनता- ईसाई भक्तोंका कितना उबार हो रहा है ? अमेरिका और के कारण वह तटस्थ बुद्धिसे लोक कल्याणके अनुरूप स्वरूप और यूरोपके जिन पूजीपतियोंके दामसे ईसाई विचारोंका उद्देश्य करता है।
मिशन चल रहे हैं, क्या वह उनकी शुद्ध कमाई __ 'तिलकने अनासक्त कर्मयोगका अर्थ किया है-"अपनी है? एक ओर शोषण और दूसरी ओर सेवा, यही पूंजीवादी बुद्धिसे निर्णीत कर्ममें फलकी आकांक्षा न करते हुए लगे समाजका चित्र है। शोषकों और सेव्योंके बीच बढ़ते हुए रहना।" गांधीजीने भी इसी अर्थको ग्रहण किया है। उन्होंने अन्तरको कम करनेके लिये 'त्याग' पर जोर दिया गया, अपनी बुद्धिसे राष्ट्रोद्धारको ही श्रेष्ठ कर्म योग समझा; वस्तुतः इस विषमताका अन्त व्यक्तिगत त्यागसे नही हो क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान्ने इसके लिये उन्हें सकता, उसके लिये नवीन समाजदर्शन और समाजव्यवही चुना है। ईश्वरके प्रति इस अर्पणकी भावनासे व्यक्ति- स्थाकी आवश्यकता है। चाहे वैराग्यमूलक निवृत्तिपरायण का अहंभाव कम होता है। इससे स्पष्ट है कि राग-द्वेष जन्य श्रमण साधु हो और या प्रवृत्तिमूलक अनासक्तयोगी गांधीआसक्ति और इस आसक्तिमें अन्तर है। एकका अर्थ प्रमाद वादी रचनात्मक कार्यकर्ता । या वासना है और दूसरीका फलकी आकांक्षा । अनासक्त नवीन समाजव्यवस्थाकी दृष्टिसे ये अक्षम हैं; अपने कर्मयोगमें वस्तुत: आसक्ति है, पर वह फलमें न होकर आर्थिक साधनोको सुरक्षित रखते हुए बड़े-बड़े सिद्धान्तोंकी केवल कर्ममें है, कर्ममें यदि आसक्ति न हो तो फिर उसमें बातें करनेकी प्रथा उस देश में बहुत रही है। किसी भी प्रवृत्ति नही होगी। ईश्वरवादमें यह बात चाहे संगत हो पर सिद्धान्तकी कसौटी उसके अनुयायी होते है। वैराग्यमूलक अनीश्वरवादमें नही, अतएव वहां वासनाके चरमक्षयसे त्यागका अर्थ भले ही आज कुंठित हो, किसी समय बड़े-बड़े आत्माका विकास हो सकता है । इस प्रकारके विकासके प्रवृत्तिभीरु व्यक्ति उसमें दीक्षित हुए परन्तु अनालिये कई ईश्वरवादी विचारक भी वासनाके अत्यन्त क्षय- सक्ति कर्मयोगको अपने जीवन में गांधीवादी कहां तक उतार पर जोर देते हैं, इसलिये विरागपूर्ण त्याग और निष्क्रियता एक सके यह गाधीजीने स्वय देख लिया। स्वराज्य मिलने के बात नही है। बुद्ध महावीर जैसे विरागी साधक उन हजारों अनन्तर भी यदि कोई गांधीवादी अपनेको अनासक्तकर्मगांधीवादियोंमे अधिक सक्रिय थे, जो अपनी शरीरयात्राके योगी मानता हो तो उससे हमें कुछ नही कहना । आचार्य लिये सरकार और पूजीपतियों का मुह जोहते थे। विनोबा भावे जैसे दो-चार व्यक्ति अवश्य है । जिनके
श्रमणोको निवृत्तिका समाजव्यवस्थासे सम्बन्ध नही। व्यक्तित्वके प्रति पूर्ण श्रद्धा होते हुए भी कार्यशैली सामाजिक प्रवृत्ति भी निवृत्तिके लिये हो सकती और निवत्ति प्रवृत्ति- दृष्टिसे अधिक अच्छी नहीं और नवीन एवं वर्णहीन समाज के लिये । गांधी सम्प्रदायके कुछ विचारक ईसाई संतोंका व्यवस्थाके लिये अनासक्त योगकी अपेक्षा किसी और योगकी उदाहरण श्रमण साधुओंके सामने रखनेसे नहीं चूकते। आवश्यकता है, इसमें संदेह नही । बात बहुत अच्छी है, पर उनकी इस समाज-सेवासे स्वयं
अलमोड़ा ता० २६-५-१९५२
गौतमस्वामि-रचित सूत्रकी प्राचीनता
गौतम स्वामीने जो प्रतिक्रमणकी विधि अपने प्रतिक्रमण "एसो परिक्कमणविहि, पणतो जिणवरेहि सम्वेहि। सूत्र में बतलाई है वह केवल वर्धमानस्वामीके द्वारा ही संजमतवद्रियाणं, जिग्गंगाणं, महरितीणं ॥" निर्दिष्ट हुई ऐसा नहीं है, बल्कि सब तीर्थंकरोंके द्वारा निर्दिष्ट यह गाथा गौतम स्वामीकी ही रची हुई है, इससे इस हुई है । टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्र इस बातका प्रतिपादन प्रतिक्रमण सूत्रकी प्रामाणिकता और प्राचीनतामें कोई संदेह करते हुए और इसकी पुष्टिमें एक गाथाको भी उद्धृत करते नही रहता । अन्यथा वे इस सूत्रको अपनी एक स्वतन्त्र रचना हुए लिखते है
कह सकते थे। यह सूत्र दिगम्बर शासनका सबसे अधिक
प्राचीन है और अनादि प्रवाहसे चला आ रहा है। रत्नकर"बघ विाषषा आप प्रातक्रमणावाषन कवल पषमान- ण्डमें बतलाया हुमा शास्त्रका लक्षण इसमें अच्छी तरह . स्वामिनयोक्तः अपितु सरपि तीकरवरक्तइत्याह- घटित होता है ।
-क्षुल्लक सिद्धसागर