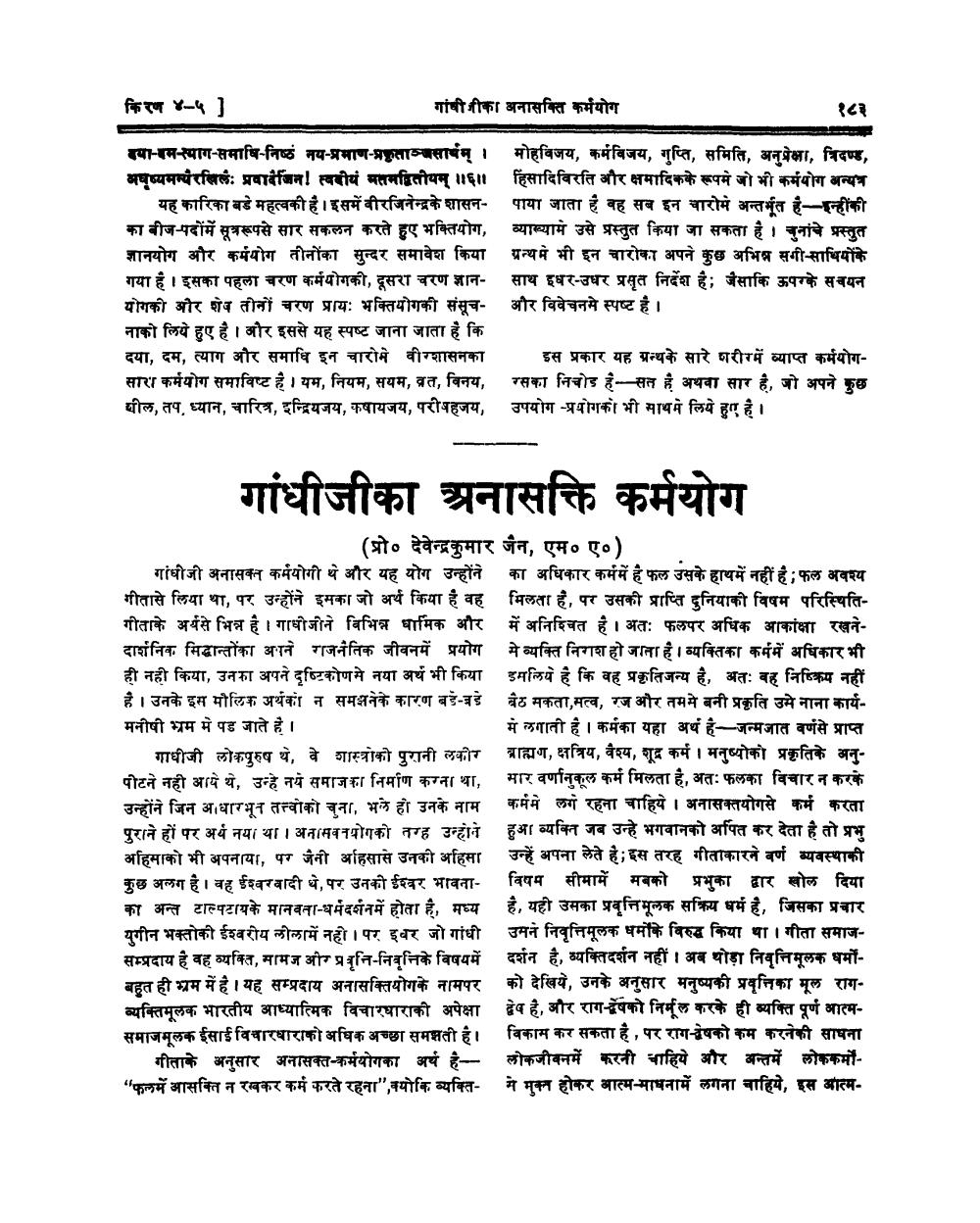________________
किरण ४-५ ]
दया-बम-माग- समाधि-निष्ठं नय-प्रमाण प्रकृतासार्थम् । अवृष्यमन्यैरखिलं : प्रवादेजिन ! त्वदीयं मतमद्वितीयम् ॥६॥
यह कारिका बड़े महत्वकी है। इसमें वीरजिनेन्द्रके शासनका बीज - पदोंमें सूत्ररूपसे सार सकलन करते हुए भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग तीनोंका सुन्दर समावेश किया गया है । इसका पहला चरण कर्मयोगकी, दूसरा चरण ज्ञानयोगकी और शेष तीनों चरण प्रायः भक्तियोगकी संसूचनाको लिये हुए है । और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि दया, दम, त्याग और समाधि इन चारोमे वीरशासनका सारा कर्मयोग समाविष्ट है। यम, नियम, सयम, व्रत, विनय, थील, तप, ध्यान, चारित्र, इन्द्रियजय, कषायजय, परीषहजय,
गांधीजीका अनासक्ति कर्मयोग
गांधीजी अनासक्त कर्मयोगी थे और यह योग उन्होंने गीतासे लिया था, पर उन्होंने इसका जो अर्थ किया है वह गीताके अर्थसे भिन्न है । गाधीजीने विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्तोंका अपने राजनैतिक जीवनमें प्रयोग ही नहीं किया, उनका अपने दृष्टिकोण से नया अर्थ भी किया है । उनके इस मौलिक अर्थको न समझनेके कारण बड़े-बड़े मनीषी भ्रम में पड जाते है ।
१८३
मोहविजय, कर्मविजय, गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, त्रिदण्ड, हिंसादिविरति और क्षमादिकके रूपमे जो भी कर्मयोग अन्यत्र पाया जाता है वह सब इन चारो अन्तर्भूत है-- इन्हींकी व्याख्यामं उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। चुनांचे प्रस्तुत ग्रन्थ मे भी इन चारोका अपने कुछ अभिन सगी-साथियोंके साथ इधर-उधर प्रसृत निर्देश है; जैसाकि ऊपरके सचयन और विवेचनमे स्पष्ट है ।
गांधीजीका अनासक्ति कर्मयोग
(प्रो० देवेन्द्रकुमार जैन, एम० ए० )
गाधीजी लोकपुरुष थे, वे शास्त्रोको पुरानी लकीर पीटने नही आये थे, उन्हें नये समाजका निर्माण करना था, उन्होंने जिन आधारभूत तत्त्वोको चुना, भले ही उनके नाम पुराने हों पर अर्थ नया था । अनासवनयोगको तरह उन्होंने अहमको भी अपनाया, पर जैनी अहसासे उनकी अहिसा कुछ अलग है । वह ईश्वरवादी थे, पर उनकी ईश्वर भावनाका अन्त टाल्टायके मानवता धर्मदर्शन में होता है, मध्य युगीन भक्तोकी ईश्वरीय लीलामें नही । पर इबर जो गांधी सम्प्रदाय है वह व्यक्ति, मामज और प्रवृति-निवृत्तिके विषय में बहुत ही भ्रम में है । यह सम्प्रदाय अनासक्तियोग के नामपर व्यक्तिमूलक भारतीय आध्यात्मिक विचारधाराकी अपेक्षा समाजमूलक ईसाई विचारधाराको अधिक अच्छा समझती है।
गीताके अनुसार अनासक्त-कर्मयोगका अर्थ है-"फलमें आसक्ति न रखकर कर्म करते रहना", क्योकि व्यक्ति
इस प्रकार यह ग्रन्थके सारे शरीर में व्याप्त कर्मयोगरसका निचोड है-सत है अथवा सार है, जो अपने कुछ उपयोग - प्रयोगको भी साथ मे लिये हुए हैं।
का अधिकार कर्ममें है फल उसके हाथमें नहीं है; फल अवश्य मिलता है, पर उसकी प्राप्ति दुनियाकी विषम परिस्थितिमें अनिश्चित है । अतः फलपर अधिक आकांक्षा रखने
व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्तिका कर्म में अधिकार भी इसलिये है कि वह प्रकृतिजन्य है, अतः वह निष्क्रिय नहीं बैठ सकता, सत्व, रज और तम मे बनी प्रकृति उसे नाना कार्यमें लगाती है । कर्मका यहा अर्थ है-जन्मजात वर्णसे प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म । मनुष्योको प्रकृतिके अनुमार वर्णानुकूल कर्म मिलता है, अतः फलका विचार न करके कर्ममे लगे रहना चाहिये । अनासक्तयोगसे कर्म करता हुआ व्यक्ति जब उन्हे भगवानको अर्पित कर देता है तो प्रभु उन्हें अपना लेते है; इस तरह गीताकारने वर्ण व्यवस्थाकी विषम सीमामें मबको प्रभुका द्वार खोल दिया है, यही उसका प्रवृत्तिमूलक सक्रिय धर्म है, जिसका प्रचार उसने निवृत्तिमूलक धर्मोके विरुद्ध किया था। गीता समाजदर्शन है, व्यक्तिदर्शन नहीं । अब थोड़ा निवृत्तिमूलक धर्मोको देखिये, उनके अनुसार मनुष्यकी प्रवृत्तिका मूल रागद्वेष है, और राग-द्वेषको निर्मूल करके ही व्यक्ति पूर्ण आत्मविकास कर सकता है, पर राग-द्वेषको कम करनेकी साधना लोकजीवनमें करनी चाहिये और अन्तमें लोककर्मोंमे मुक्त होकर आत्म-माघनामें लगना चाहिये, इस आत्म