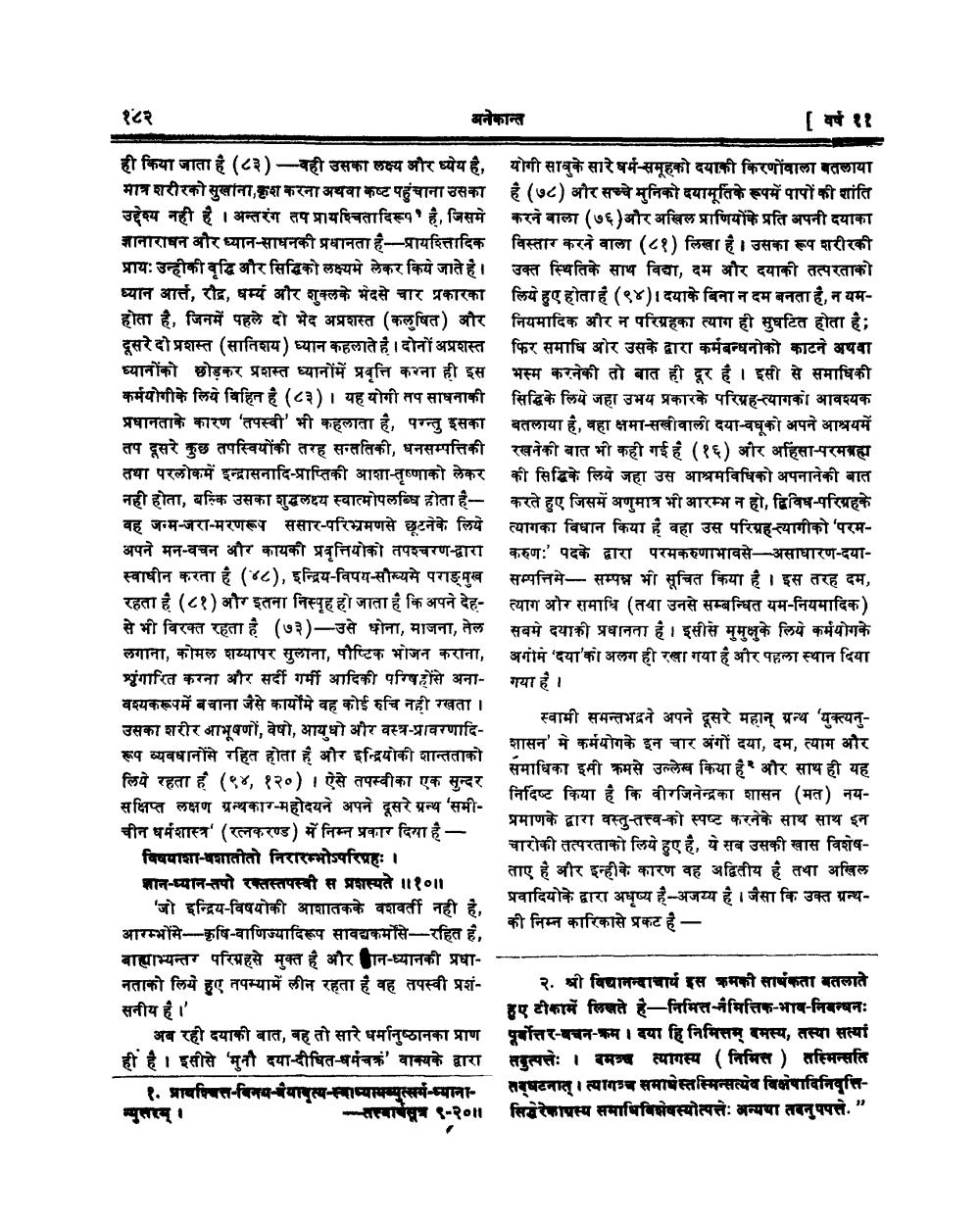________________
१८२
बनेकान्त
[वर्ष ११
ही किया जाता है (८३)-वही उसका लक्ष्य और ध्येय है, योगी सावुके सारे धर्म-समूहको दयाकी किरणोंवाला बतलाया मात्र शरीरको सुखाना,कृश करना अथवा कष्ट पहुंचाना उसका है (७८) और सच्चे मुनिको दयामूर्तिके रूपमें पापों की शांति उद्देश्य नही है । अन्तरंग तप प्रायश्चितादिरूप' है, जिसमे करने वाला (७६)और अखिल प्राणियों के प्रति अपनी दयाका ज्ञानाराधन और ध्यान-साधनकी प्रधानता है-प्रायश्त्तिादिक विस्तार करने वाला (८१) लिखा है। उसका रूप शरीरकी प्रायः उन्हीकी वृद्धि और सिद्धिको लक्ष्यमे लेकर किये जाते है। उक्त स्थितिके साथ विद्या, दम और दयाकी तत्परताको ध्यान आर्त, रौद्र, धम्यं और शुक्लके भेदसे चार प्रकारका लिये हुए होता है (९४)। दयाके बिना न दम बनता है, न यमहोता है, जिनमें पहले दो भेद अप्रशस्त (कलुषित) और नियमादिक और न परिग्रहका त्याग ही सुघटित होता है। दूसरे दो प्रशस्त (सातिशय) ध्यान कहलाते हैं। दोनों अप्रशस्त फिर समाधि और उसके द्वारा कर्मबन्धनोको काटने अथवा ध्यानोंको छोड़कर प्रशस्त ध्यानोंमें प्रवृत्ति करना ही इस भस्म करनेकी तो बात ही दूर है। इसी से समाधिकी कर्मयोगीके लिये विहित है (८३)। यह योगी तप साधनाकी सिद्धिके लिये जहा उभय प्रकारके परिग्रह-त्यागको आवश्यक प्रधानताके कारण 'तपस्वी' भी कहलाता है, परन्तु इसका बतलाया है, वहा क्षमा-सखीवाली दया-वधूको अपने आश्रयमें तप दूसरे कुछ तपस्वियोंकी तरह सन्ततिकी, धनसम्पत्तिकी रखनेकी बात भी कही गई है (१६) और अहिंसा-परमब्रह्म तथा परलोकमें इन्द्रासनादि-प्राप्तिकी आशा-तृष्णाको लेकर की सिद्धिके लिये जहा उस आश्रमविधिको अपनानेकी बात नहीं होता, बल्कि उसका शुद्धलक्ष्य स्वात्मोपलब्धि होता है- करते हुए जिसमें अणुमात्र भी आरम्भ न हो, द्विविध-परिग्रहके वह जन्म-जरा-मरणरूप ससार-परिभ्रमणसे छूटनेके लिये त्यागका विधान किया है वहा उस परिग्रह-त्यागीको 'परमअपने मन-वचन और कायकी प्रवृत्तियोको तपश्चरण-द्वारा करुणः' पदके द्वारा परमकरुणाभावसे-असाधारण-दयास्वाधीन करता है (४८), इन्द्रिय-विषय-सौख्यमे पराङ्मुख सम्पनिमे- सम्पन्न भी सूचित किया है। इस तरह दम, रहता है (८१) और इतना निस्पृह हो जाता है कि अपने देह- त्याग और समाधि (तथा उनसे सम्बन्धित यम-नियमादिक) से भी विरक्त रहता है (७३)-उसे धोना, माजना, तेल सबमे दयाकी प्रधानता है। इसीसे मुमुक्षुके लिये कर्मयोगके लगाना, कोमल शय्यापर सुलाना, पौष्टिक भोजन कराना, अगोम 'दया'को अलग ही रखा गया है और पहला स्थान दिया श्रृंगारित करना और सर्दी गर्मी आदिकी परिषहोंसे अना- गया है। वश्यकरूपमें बचाना जैसे कार्योंमे वह कोई रुचि नहीं रखता।
स्वामी समन्तभद्रने अपने दूसरे महान् ग्रन्थ 'युक्त्यनुउसका शरीर आभूषणों, वेषो, आयुधो और वस्त्र-प्रावरणादि
शासन' में कर्मयोगके इन चार अंगों दया, दम, त्याग और रूप व्यवधानोंसे रहित होता है और इन्द्रियोकी शान्तताको
समाधिका इमी क्रमसे उल्लेख किया है और साथ ही यह लिये रहता है (९४, १२०) । ऐसे तपस्वीका एक सुन्दर
निर्दिष्ट किया है कि वीरजिनेन्द्रका शासन (मत) नयसक्षिप्त लक्षण ग्रन्थकार-महोदयने अपने दूसरे ग्रन्थ 'समीचीन धर्मशास्त्र' (रलकरण्ड) में निम्न प्रकार दिया है
प्रमाणके द्वारा वस्तु-तत्त्व-को स्पष्ट करनेके साथ साथ इन
चारोकी तत्परताको लिये हुए है, ये सब उसकी खास विशेषविषयाशा-शातीतो निरारम्भोऽपरिप्रहः ।
ताए है और इन्हीके कारण वह अद्वितीय है तथा अखिल मान-ध्यान-तपो रक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥
प्रवादियोके द्वारा अधृष्य है-अजय्य है । जैसा कि उक्त ग्रन्थ'जो इन्द्रिय-विषयोकी आशातकके वशवर्ती नही है, आरम्भोंसे-कृषि-वाणिज्यादिरूप सावद्यकर्मोसे-रहित है,
की निम्न कारिकासे प्रकट है - बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त है और पान-ध्यानकी प्रधा- - -- नताको लिये हुए नपम्यामें लीन रहता है वह तपस्वी प्रशं- २. श्री विद्यानन्दाचार्य इस क्रमकी सार्थकता बतलाते सनीय है।'
ए टीकामें लिखते है-निमित्तमित्तिक-भाव-निबन्धनः ____ अब रही दयाकी बात, वह तो सारे धर्मानुष्ठानका प्राण पूर्वोत्तर-वचन-क्रम । बया हि निमित्तम् बमस्य, तस्या सत्या ही है । इसीसे 'मुनी दया-दीषित-धर्मचक्रं' वाक्यके द्वारा तदुत्पत्तेः । बमञ्च त्यागस्य (निमित्त ) तस्मिन्सति १. प्रायश्चित्त-विनय-यावृत्य-स्वाध्यायव्यत्सर्ग-प्याना- तपटनात् । त्यागश्च समाघेस्तस्मिन्सत्येव विक्षेपाविनिवृत्ति
-सस्वासूत्र ९-२०॥ सिरेकापस्य समाधिविशेषस्योत्पत्तेः अन्यथा तनुपपत्ते."