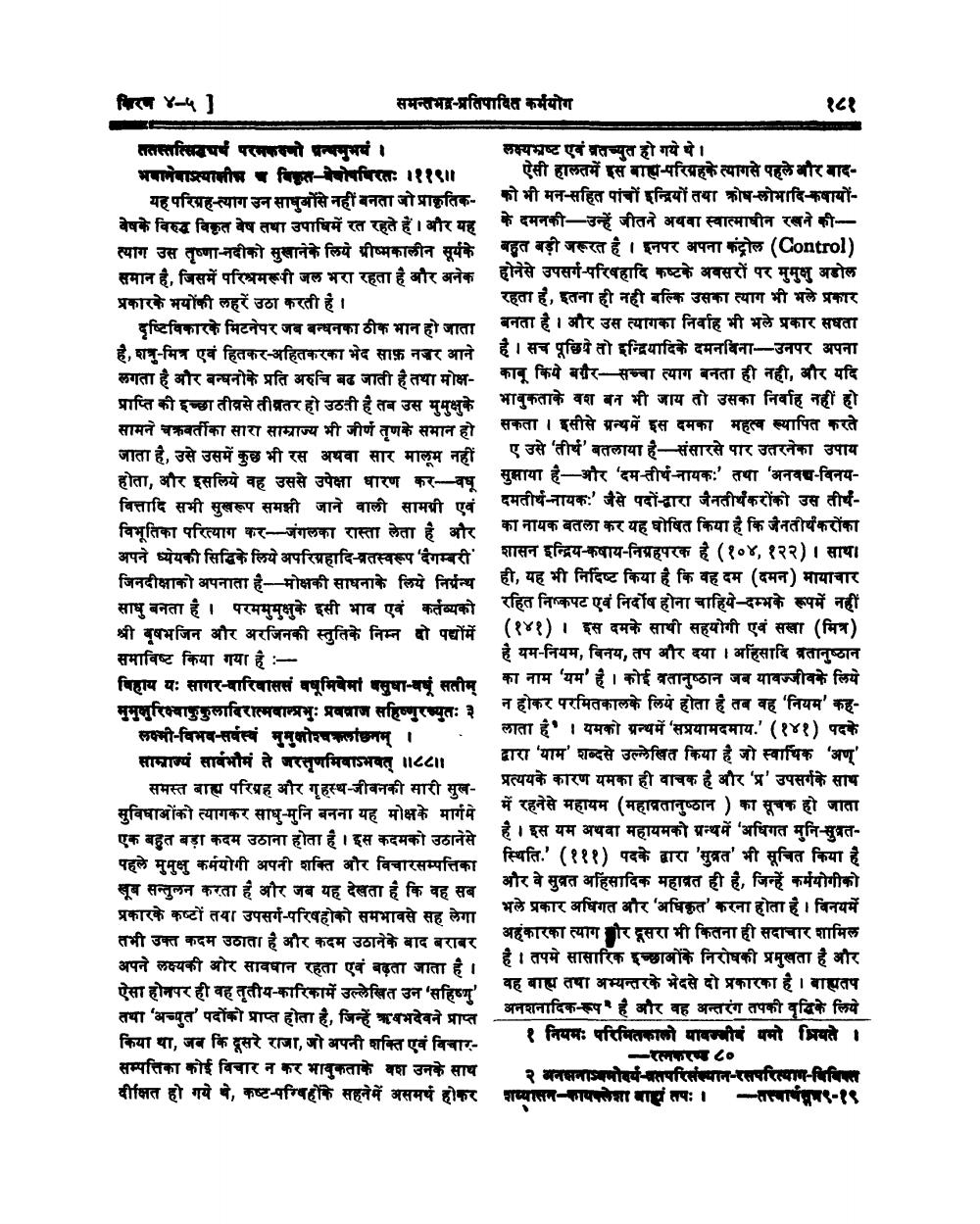________________
किरण ४-५]
समन्तभव-प्रतिपावित कर्मयोग
१८१
ततस्तसिवाय परमकरणो पन्यमुभवं ।
लक्ष्यभष्ट एवं व्रतच्युत हो गये थे। भवानेवाण्यातील विकृत-वोपपिरतः ॥११९॥ ऐसी हालतमें इस बाह्य-परिग्रहके त्यागसे पहले बीर बाद
यह परिग्रह-त्याग उन साधुओंसे नहीं बनता जोप्राकृतिक- को भी मन-सहित पांचों इन्द्रियों तथा कोष-लोभादि-कषायोंवेषके विरुद्ध विकृत वेष तथा उपाधिमें रत रहते हैं। और यह के दमनकी-उन्हें जीतने अथवा स्वात्माधीन रखने कीत्याग उस तृष्णा नदीको सुखानेके लिये ग्रीष्मकालीन सूर्यके बहुत बड़ी जरूरत है । इनपर अपना कंट्रोल (Control) समान है, जिसमें परिश्रमरूपी जल भरा रहता है और अनेक होनेसे उपसर्ग-परिषहादि कष्टके अवसरों पर मुमुक्ष अडोल प्रकारके भयोंकी लहरें उठा करती है।
रहता है, इतना ही नही बल्कि उसका त्याग भी भले प्रकार दृष्टिविकारके मिटनेपर जब बन्धनका ठीक भान हो जाता बनता है । और उस त्यागका निर्वाह भी भले प्रकार सघता है, शत्रु-मित्र एवं हितकर-अहितकरका भेद साफ़ नजर आने है। सच पूछिये तो इन्द्रियादिके दमनविना-उनपर अपना लगता है और बन्धनोके प्रति अरुचि बढ जाती है तथा मोक्ष- काबू किये बगैर-सच्चा त्याग बनता ही नहीं, और यदि प्राप्ति की इच्छा तीवसे तीव्रतर हो उठती है तब उस ममक्षके भावुकताके वश बन भी जाय तो उसका निर्वाह नहीं हो सामने चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य भी जीर्ण तृणके समान हो
सकता । इसीसे ग्रन्थमें इस दमका महत्व ख्यापित करते जाता है, उसे उसमें कुछ भी रस अथवा सार मालम नहीं ए उसे 'तीर्थ' बतलाया है-संसारसे पार उतरनेका उपाय होता, और इसलिये वह उससे उपेक्षा धारण कर-वधू सुलाया
सुझाया है-और 'दम-तीर्थ-नायकः' तथा 'अनवच-विनयवित्तादि सभी सुखरूप समझी जाने वाली सामग्री एवं दमताथनायकः' जैसे पदो-द्वारा जैनतीर्थंकरोंको उस तीर्थविभूतिका परित्याग कर-जंगलका रास्ता लेता है और का नायक बतला कर यह घोषित किया है कि जैनतीर्थंकरोंका अपने ध्येयकी सिद्धिके लिये अपरिग्रहादि-प्रतस्वरूप 'दैगम्बरी शासन इन्द्रिय-कषाय-निग्रहपरक है (१०४,१२२) । साथ। जिनदीक्षाको अपनाता है-मोक्षकी साधनाके लिये निम्रन्थ ही, यह भा निदिष्ट किया है कि वह दम (वमन) मायाचार साधु बनता है। परममुमुक्षुके इसी भाव एवं कर्तव्यको रहित निष्कपट एवं निर्दोष होना चाहिये-दम्भके रूपमें नहीं श्री वृषभजिन और अरजिनकी स्तुतिके निम्न वो पधोंमें (१४१) । इस दमके साथी सहयोगी एवं सखा (मित्र) समाविष्ट किया गया है :
है यम-नियम, विनय, तप और दया । अहिंसादि व्रतानुष्ठान विहाय यः सागर-बारिवाससं वधूमिवेमा बसुषा-वधू सतीम् ।
का नाम 'यम' है । कोई व्रतानुष्ठान जब यावज्जीवके लिये मुमुलरिक्वाकुकुलादिरात्मवाप्रभुः प्रववाज सहिष्णुरव्युतः ३
न होकर परमितकालके लिये होता है तब वह 'नियम' कहलक्मी-विभव-सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्रलांछनम् ।
लाता है' । यमको ग्रन्थमें 'सप्रयामदमाय.' (१४१) पदके साम्राज्यं सार्वभौम ते जरतृणमिवाऽभवत् ॥८॥
द्वारा 'याम' शब्दसे उल्लेखित किया है जो स्वार्षिक 'अण' समस्त बाह्य परिग्रह और गृहस्थ-जीवनकी सारी सुख
प्रत्ययके कारण यमका ही वाचक है और 'प्र' उपसर्गके साथ सुविधाओंको त्यागकर साधु-मुनि बनना यह मोक्षके मार्गमे म रहनस महायम (महावतानुष्ठान ) का सूचक हो जाता एक बहुत बड़ा कदम उठाना होता है । इस कदमको उठानेसे
है। इस यम अथवा महायमको ग्रन्थमें 'अधिगत मुनि-सुव्रतपहले मुमुक्षु कर्मयोगी अपनी शक्ति और विचारसम्पत्तिका
स्थिति.' (१११) पदके द्वारा 'सुव्रत' भी सूचित किया है खूब सन्तुलन करता है और जब यह देखता है कि वह सब
और वे सुव्रत अहिंसादिक महाव्रत ही है, जिन्हें कर्मयोगीको प्रकारके कष्टों तया उपसर्ग-परिषहोको समभावसे सह लेगा
भले प्रकार अधिगत और 'अधिकृत' करना होता है । विनयमें तभी उक्त कदम उठाता है और कदम उठानेके बाद बराबर
अहंकारका त्याग और दूसरा भी कितना ही सदाचार शामिल अपने लक्ष्यकी ओर सावधान रहता एवं बढ़ता जाता है।
है। तपमे सासारिक इच्छाओंके निरोधकी प्रमुखता है और ऐसा होनपर ही वह तृतीय-कारिकामें उल्लेखित उन 'सहिष्णु'
वह बाह्य तथा अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । बाह्यतप तथा 'अच्युत' पदोंको प्राप्त होता है, जिन्हें ऋषभदेवने प्राप्त
__ अनशनादिक-रूप' है और वह अन्तरंग तपकी वृद्धिके लिये किया था, जब कि दूसरे राजा, जो अपनी शक्ति एवं विचार
१नियमः परिमितकालो यावन्नीवं यमो प्रियते । सम्पत्तिका कोई विचार न कर भावुकताके वश उनके साथ अनसनानोरातपरिसंस्थान-रसपरित्याग-विविक्त वीक्षित हो गये थे, कष्ट पग्विहोंके सहने में असमर्थ होकर शव्यासन-कायपलेशाबाई तपः। -तत्वावर-१९