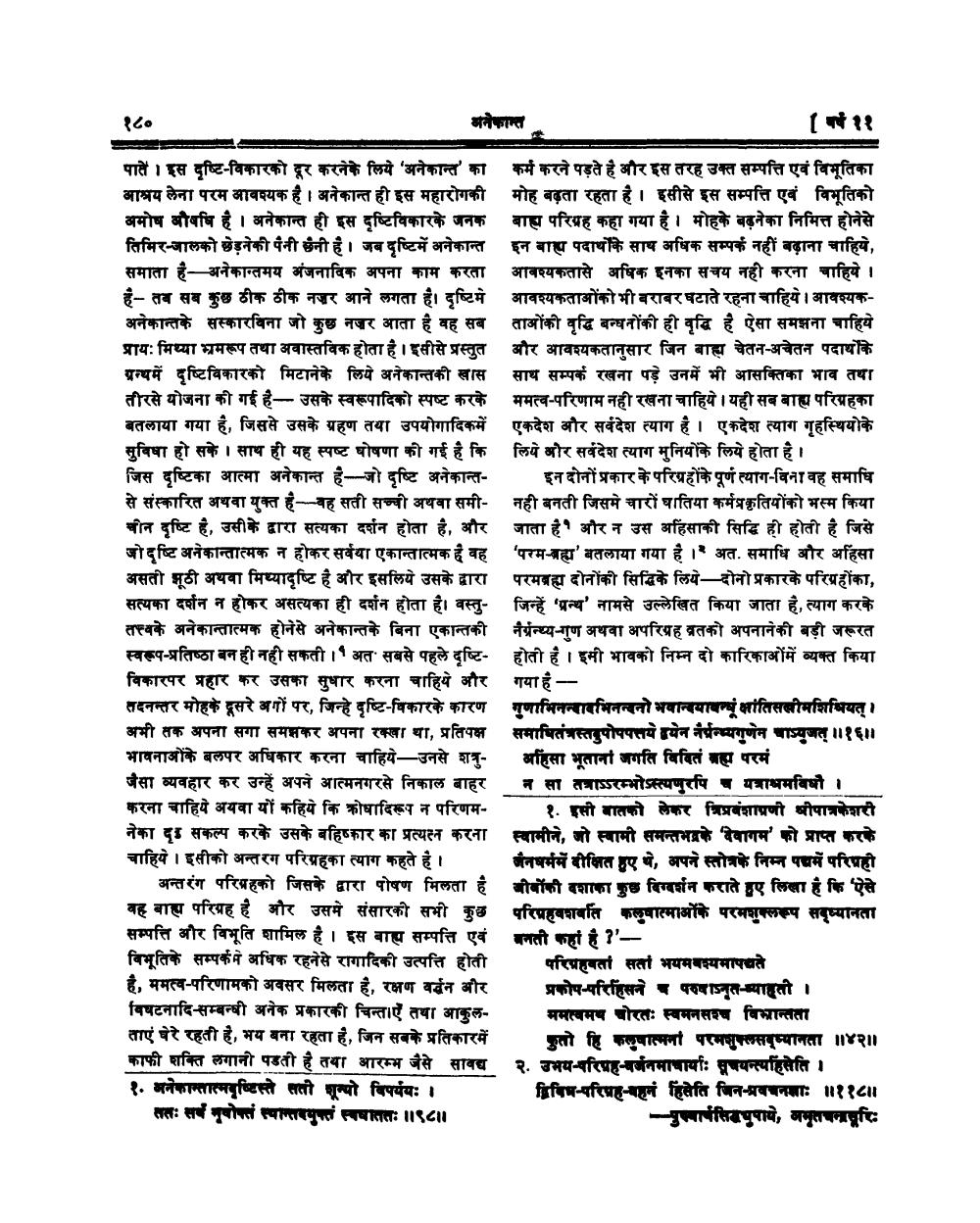________________
१८०
पायें इस दृष्टि-विकारको दूर करनेके लिये 'अनेकान्त' का आश्रय लेना परम आवश्यक है। अनेकान्त ही इस महारोगकी अमोष औषधि है । अनेकान्त ही इस दृष्टिविकारके जनक तिमिर - जालको छेड़नेकी पनी छैनी है। जब दृष्टिमें अनेकान्त समाता है— अनेकान्तमय अंजनाविक अपना काम करता हैं - तब सब कुछ ठीक ठीक नजर आने लगता है। दृष्टिमे अनेकान्तके संस्कारविना जो कुछ नजर आता है वह सब प्रायः मिथ्या भ्रमरूप तथा अवास्तविक होता है। इसीसे प्रस्तुत ग्रन्थ में दृष्टिविकारको मिटानेके लिये अनेकान्तकी लास तीरसे योजना की गई है उसके स्वरूपादिको स्पष्ट करके बतलाया गया है, जिससे उसके ग्रहण तथा उपयोगादिकमें सुविधा हो सके। साथ ही यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि जिस दृष्टिका आत्मा अनेकान्त है जो दृष्टि अनेकान्तसे संस्कारित अथवा युक्त है-वह सती सच्ची अथवा समीचीन दृष्टि है, उसीके द्वारा सत्यका दर्शन होता है, और जो दृष्टि अनेकान्तात्मक न होकर सर्वया एकान्तात्मक है वह असती झूठी अथवा मिध्यादृष्टि है और इसलिये उसके द्वारा सत्यका दर्शन न होकर असत्यका ही दर्शन होता है। वस्तुतवके अनेकान्तात्मक होनेसे अनेकान्तके बिना एकान्तकी स्वरूप प्रतिष्ठा बन ही नहीं सकती। 1 अत सबसे पहले दृष्टि विकारपर प्रहार कर उसका सुधार करना चाहिये और तदनन्तर मोहके दूसरे अगों पर, जिन्हे दृष्टि-विकारके कारण अभी तक अपना सगा समझकर अपना रक्खा था, प्रतिपक्ष भावनाओंके बलपर अधिकार करना चाहिये — उनसे शत्रुजैसा व्यवहार कर उन्हें अपने आत्मनगरसे निकाल बाहर करना चाहिये अथवा यों कहिये कि क्रोषादिरूप न परिणमनेका दृड सकल्प करके उसके बहिष्कार का प्रत्यस्न करना चाहिये। इसीको अन्तरंग परिग्रहका त्याग कहते हैं।
अन्तरंग परिग्रहको जिसके द्वारा पोषण मिलता है वह बाह्य परिग्रह है और उसमे संसारकी सभी कुछ सम्पत्ति और विभूति शामिल है। इस बाह्य सम्पत्ति एवं विभूतिके सम्पर्कमे अधिक रहनेसे रागादिकी उत्पत्ति होती है. ममत्व-परिणामको अवसर मिलता है, रक्षण वर्धन बीर विषनादि-सम्बन्धी अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ तथा आकुलताएं घेरे रहती है, भय बना रहता है, जिन सबके प्रतिकार में काफी शक्ति लगानी पड़ती है तथा आरम्भ जैसे सावध १. अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः ।
ततः सर्व वोक्तं स्यान्तवमुक्तं स्वघाततः ॥९८॥
अनेकान्त
[११
कर्म करने पड़ते है और इस तरह उक्त सम्पत्ति एवं विभूतिका मोह बढ़ता रहता है । इसीसे इस सम्पत्ति एवं विभूतिको बाह्य परिग्रह कहा गया है। मोहके बढ़नेका निमित्त होनेसे इन बाह्य पदार्थों के साथ अधिक सम्पर्क नहीं बढ़ाना चाहिये, आवश्यकतासे अधिक इनका समय नहीं करना चाहिये। आवश्यकताओंको भी बराबर घटाते रहना चाहिये। आवश्यकताकी वृद्धि बन्धनोंकी ही वृद्धि है ऐसा समझना चाहिये और आवश्यकतानुसार जिन बाह्य चेतन-अचेतन पदार्थक साथ सम्पर्क रखना पड़े उनमें भी आसक्तिका भाव तथा ममत्व - परिणाम नही रखना चाहिये । यही सब बाह्य परिग्रहका एकदेश और सर्वदेश त्याग है । एकदेश त्याग गृहस्थियो के लिये और सर्वदेश रवान मुनियोंक लिये होता है।
इन दोनों प्रकार के परिग्रहोंके पूर्ण त्याग विना वह समाषि नही बनती जिसमे चारों पातिया कर्मप्रकृतियोंको भस्म किया जाता है और न उस महिलाकी सिद्धि ही होती है जिसे 'परम- बड़ा बतलाया गया है। अत समाधि और अहिंसा परमब्रह्म दोनोंकी सिद्धिके लिये —दोनो प्रकारके परिग्रहोंका, जिन्हें 'ग्रन्थ' नामसे उल्लेखित किया जाता है, त्याग करके नैर्ग्रन्थ्य-गुण अथवा अपरिग्रह व्रतको अपनाने की बड़ी जरूरत होती है। इसी भावको निम्न दो कारिकाओं में व्यक्त किया गया है
गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्वयाबन्धं शांतिसलीमशिश्रियत् । समाधितंत्रस्तपोपपत्तये द्वयेन मैन्यगुणेन चात् ।। १६ ।। अहिंसा भूतानां जगत विदितं ब्रह्म परमं न सा तमारम्भोत्यनुरपि च यत्राश्रमविधी ।
१. इसी बात को लेकर त्रिप्रवंशाग्रणी श्रीपात्रकेशरी स्वामीने, जो स्वामी समन्तभद्रके 'वैवागम' को प्राप्त करके जैनधर्म में दीक्षित हुए थे, अपने स्तोत्रके निम्न पक्षमें परिग्रही बीबाँकी दशाका कुछ दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि ऐसे परिप्रक्वति कलुवात्माओं के परममुक्तरूप सयानता बनती कहाँ है ?'
परिग्रहवतां सतां भयमवश्यमापचते प्रकोप - परिहिंसने च परुषानृत-व्याहती । ममत्वमय चोरतः स्वमनसश्च विभ्रान्तता कुतो हि कलुषात्मनां परमशुक्लसध्यानता ॥ ४२ ॥ २. उभय-परिवर्तनमाचार्याः सूचयन्त्यहितेति । द्विविध-परिग्रह-बहन हिंसेति जिन-प्रवचनशाः ॥११८॥ -पुरुषार्थसिद्धभुषाये, अमृतचन्द्रि