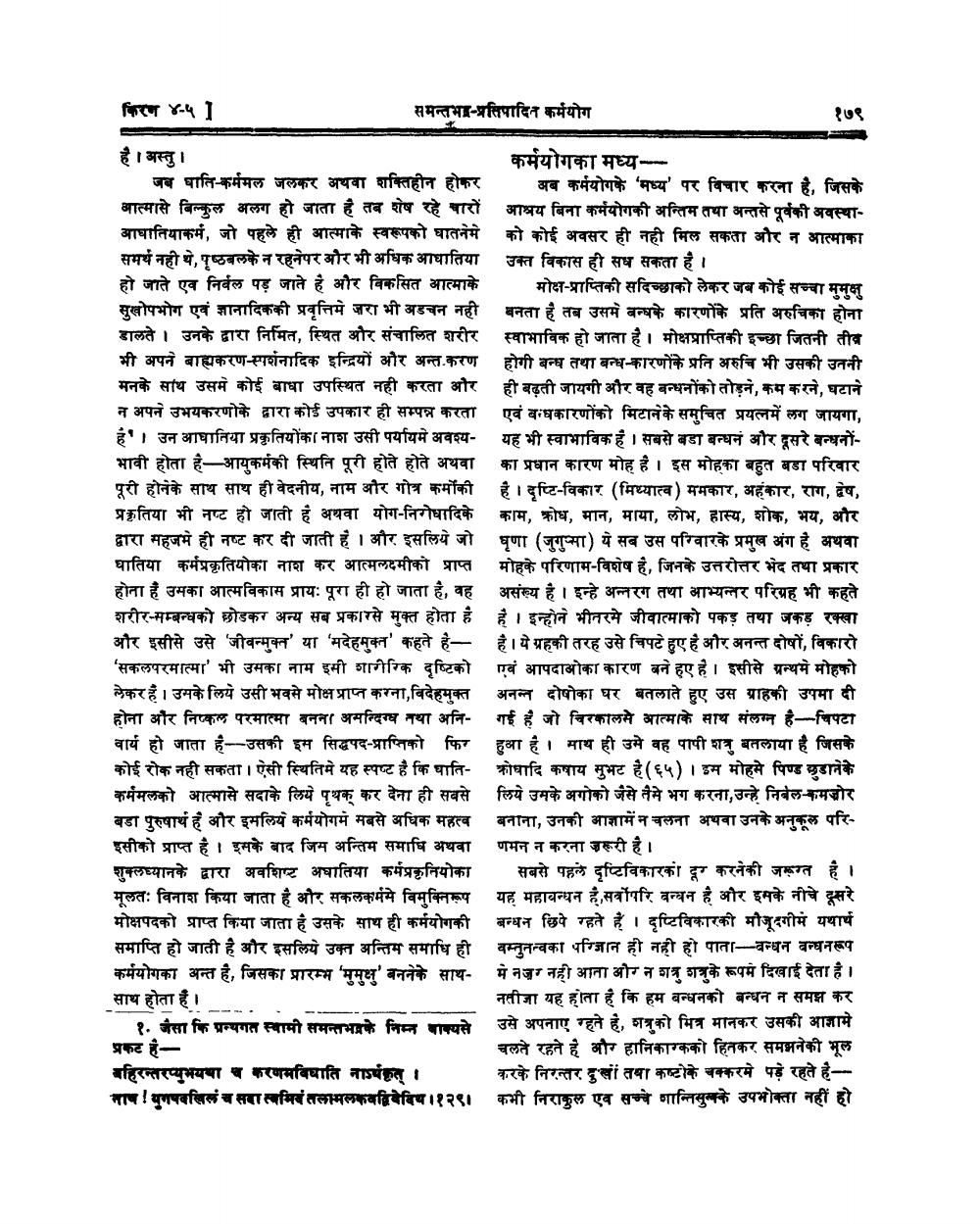________________
किरण ४-५]
समन्तभाव-प्रतिपादित कर्मयोग
है । अस्तु।
कर्मयोगका मध्यजब घाति-कर्ममल जलकर अथवा शक्तिहीन होकर अब कर्मयोगके 'मध्य' पर विचार करना है, जिसके आत्मासे बिल्कुल अलग हो जाता है तब शेष रहे चारों आश्रय बिना कर्मयोगकी अन्तिम तथा अन्तसे पूर्वकी अवस्थाआघातियाकर्म, जो पहले ही आत्माके स्वरूपको घातनेमे को कोई अवसर ही नही मिल सकता और न आत्माका समर्थ नही थे, पुष्ठबलके न रहनेपर और भी अधिक आघातिया उक्त विकास ही सध सकता है। हो जाते एव निर्बल पड़ जाते है और विकसित आत्माके मोक्ष-प्राप्तिकी सदिच्छाको लेकर जब कोई सच्चा मुमुक्षु सुखोपभोग एवं ज्ञानादिककी प्रवृत्तिमे जरा भी अडचन नहीं बनता है तब उसमे बन्धके कारणोंके प्रति अरुचिका होना डालते। उनके द्वारा निर्मित, स्थित और संचालित शरीर स्वाभाविक हो जाता है। मोक्षप्राप्तिकी इच्छा जितनी तीव्र भी अपने बाह्यकरण-स्पर्शनादिक इन्द्रियों और अन्तःकरण होगी बन्ध तथा बन्ध-कारणोंके प्रति अरुचि भी उसकी उतनी मनके साथ उसमे कोई बाधा उपस्थित नहीं करता और ही बढ़ती जायगी और वह बन्धनोंको तोड़ने, कम करने, घटाने न अपने उभयकरणोके द्वारा कोई उपकार ही सम्पन्न करता एवं बन्धकारणोंको मिटाने के समुचित प्रयत्नमें लग जायगा, है'। उन आघानिया प्रकृतियोंका नाश उसी पर्यायमे अवश्य- यह भी स्वाभाविक है। सबसे बडा बन्धनं और दूसरे बन्धनोंभावी होता है-आयुकर्मकी स्थिति पूरी होते होते अथवा का प्रधान कारण मोह है । इस मोहका बहुत बड़ा परिवार पूरी होनेके साथ साथ ही वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मोकी है। दृष्टि-विकार (मिथ्यात्व) ममकार, अहंकार, राग, द्वेष, प्रकृतिया भी नष्ट हो जाती है अथवा योग-निगेधादिके काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय, और द्वारा महजमे ही नष्ट कर दी जाती है । और इसलिये जो घृणा (जुगुप्मा) ये सब उस परिवारके प्रमुख अंग है अथवा घातिया कर्मप्रकृतियोका नाश कर आत्मलक्ष्मीको प्राप्त मोहके परिणाम-विशेष है, जिनके उत्तरोत्तर भेद तथा प्रकार होता है उमका आत्मविकास प्रायः पूरा ही हो जाता है, वह असंख्य है। इन्हे अन्नरग तथा आभ्यन्तर परिग्रह भी कहते शरीर-सम्बन्धको छोडकर अन्य सब प्रकारसे मुक्त होता है है। इन्होने भीतरमे जीवात्माको पकड़ तथा जकड़ रक्खा
और इसीसे उसे 'जीवन्मुक्त' या 'मदेहमुक्त' कहते है- है। ये ग्रहकी तरह उसे चिपटे हुए है और अनन्त दोषों, विकारो 'सकलपरमात्मा' भी उसका नाम इसी शारीरिक दृष्टिको एवं आपदाओका कारण बने हुए है। इसीसे ग्रन्थमे मोहको लेकर है। उसके लिये उसी भवसे मोक्षप्राप्त करना,विदेहमुक्त अनन्त दोषोका घर बतलाते हुए उस ग्राहकी उपमा दी होना और निष्कल परमात्मा बनना अमन्दिग्ध नथा अनि- गई है जो चिरकालमे आत्माके साथ संलग्न है-चिपटा वार्य हो जाता है-उसकी इस सिद्धपद-प्राप्तिको फिर हुआ है। माथ ही उमे वह पापी शत्रु बतलाया है जिसके कोई रोक नहीं सकता। ऐसी स्थितिमे यह स्पष्ट है कि घाति- क्रोधादि कषाय सुभट है (६५) । इम मोहमे पिण्ड छुडानेके कर्ममलको आत्मासे सदाके लिये पृथक् कर देना ही सबसे लिये उमके अगोको जैसे तैसे भग करना,उन्हे निबेल-कमजोर बडा पुरुषार्थ है और इमलिये कर्मयोगर्म मबसे अधिक महत्व बनाना, उनकी आज्ञा न चलना अथवा उनके अनुकूल परिइसीको प्राप्त है। इसके बाद जिम अन्तिम समाधि अथवा णमन न करना जरूरी है। शुक्लध्यानके द्वारा अवशिष्ट अघातिया कर्मप्रकृनियोका सबसे पहले दृष्टिविकारको दूर करनेकी जरूरत है। मूलतः विनाश किया जाता है और सकलकर्ममे विमुक्तिरूप यह महाबन्धन है,सर्वोपरि बन्धन है और इसके नीचे दूसरे मोक्षपदको प्राप्त किया जाता है उसके साथ ही कर्मयोगकी __ बन्धन छिपे रहते है । दृष्टिविकारकी मौजूदगीम यथार्थ समाप्ति हो जाती है और इसलिये उक्त अन्तिम समाधि ही वस्तुनन्वका पग्जिान ही नहीं हो पाता-बन्धन बन्धनरूप कर्मयोगका अन्त है, जिसका प्रारम्भ 'मुमुक्षु' बननेके साथ- में नजर नहीं आता और न शत्रु शत्रुके रूपमे दिखाई देता है। साथ होता है।
नतीजा यह होता है कि हम बन्धनको बन्धन न समझ कर १. जैसा कि प्रन्यगत स्वामी समन्तभनके निम्न वाक्यसे उसे अपनाए रहते है, शत्रुको मित्र मानकर उसकी आज्ञामे प्रकट है
चलते रहते है और हानिकारकको हितकर समझनेकी भूल बहिरन्तरप्युभयया च करणमविघाति नायकृत् । करके निरन्तर दुखों तथा कष्टोके चक्करमे पड़े रहते हैनापी युगपदखिलं च सदास्वमिवंतलामलकवद्विवेविष।१२९॥ कभी निराकुल एव सच्चे शान्तिसुनके उपभोक्ता नहीं हो