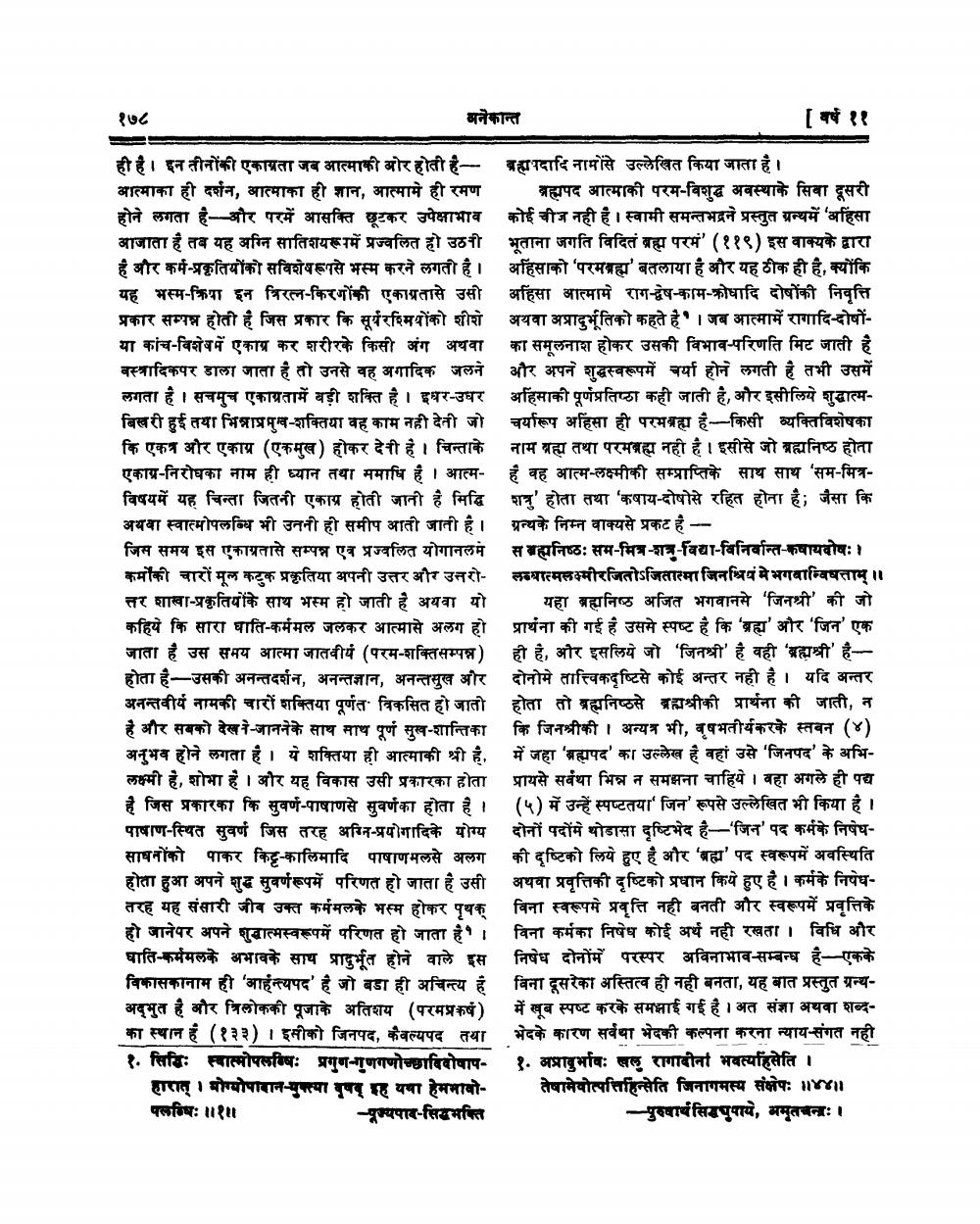________________
१७८
बनेकान्त
[वर्ष ११
-
ही है। इन तीनोंकी एकाग्रता जब आत्माकी ओर होती है- ब्रह्मपदादि नामोंसे उल्लेखित किया जाता है। आत्माका ही दर्शन, आत्माका ही ज्ञान, आत्मामे ही रमण ब्रह्मपद आत्माकी परम-विशुद्ध अवस्थाके सिवा दूसरी होने लगता है और परमें आसक्ति छूटकर उपेक्षाभाव कोई चीज नही है। स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत ग्रन्थमें 'अहिंसा आजाता है तब यह अग्नि सातिशयरूपमें प्रज्वलित हो उठनी भूताना जगति विदितं ब्रह्म परम' (११९) इस वाक्यके द्वारा है और कर्म-प्रकृतियोंको सविशेषरूपसे भस्म करने लगती है। अहिंसाको परमब्रह्म' बतलाया है और यह ठीक ही है, क्योंकि यह भस्म-क्रिया इन त्रिरत्न-किरणोंकी एकाग्रतासे उसी अहिंसा आत्मामे राग-द्वेष-काम-क्रोधादि दोषोंकी निवृत्ति प्रकार सम्पन्न होती है जिस प्रकार कि सूर्यरश्मियोंको शीशे अथवा अप्रादुर्भूतिको कहते है' । जब आत्मामें रागादि-दोषोंया कांच-विशेष में एकाग्र कर शरीरके किसी अंग अथवा का समूलनाश होकर उसकी विभाव-परिणति मिट जाती है वस्त्रादिकपर डाला जाता है तो उनसे वह अगादिक जलने और अपने शुद्धस्वरूपमें चर्या होने लगती है तभी उसमें लगता है । सचमुच एकाग्रतामें बड़ी शक्ति है । इधर-उधर अहिंमाकी पूर्णप्रतिष्ठा कही जाती है, और इसीलिये शुद्धात्मबिखरी हुई तया भिन्नाप्रमुख-शक्तिया वह काम नही देती जो चर्यारूप अहिंसा ही परमब्रह्म है--किसी व्यक्तिविशेषका कि एकत्र और एकाग्र (एकमुख) होकर देती है। चिन्ताके नाम ब्रह्म तथा परमब्रह्म नही है । इसीसे जो ब्रह्मनिष्ठ होता एकाग्र-निरोधका नाम ही ध्यान तथा ममाधि है । आत्म- है वह आत्म-लक्ष्मीकी सम्प्राप्तिके साथ साथ 'सम-मित्रविषयमें यह चिन्ता जितनी एकाग्र होती जाती है मिद्धि शत्रु' होता तथा 'कषाय-दोषोसे रहित होता है। जैसा कि अथवा स्वात्मोपलब्धि भी उतनी ही समीप आती जाती है। ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रकट है - जिस समय इस एकाग्रतासे सम्पन्न एव प्रज्वलित योगानलमे सब्रह्मनिष्ठः सम-मित्र-शत्र-विद्या-विनिर्वान्त-कवायदोषः। कर्मोकी चारों मूल कटुक प्रकृतिया अपनी उत्तर और उनरो- लग्यात्मलक्मीरजितोऽजितात्मा जिनश्रियं मे भगवान्विषत्ताम् ॥ तर शाखा-प्रकृतियोंके साथ भस्म हो जाती है अथवा यो यहा ब्रह्मनिष्ठ अजित भगवानमे 'जिनश्री' की जो कहिये कि सारा घाति-कर्ममल जलकर आत्मासे अलग हो प्रार्थना की गई है उसमे स्पष्ट है कि 'ब्रह्म' और 'जिन' एक जाता है उस समय आत्मा जातवीर्य (परम-शक्तिसम्पन्न) ही है, और इसलिये जो 'जिनश्री' है वही 'ब्रह्मश्री' हैहोता है-उसकी अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और दोनोमे तात्त्विकदृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। यदि अन्तर अनन्तवीर्य नामकी चारों शक्तिया पूर्णत विकसित हो जातो होता तो ब्रह्मनिष्ठसे ब्रह्मश्रीकी प्रार्थना की जाती, न है और सबको देखने-जाननेके साथ माथ पूर्ण सुख-शान्तिका कि जिनश्रीकी । अन्यत्र भी, वृषभतीर्यकरके स्तवन (४) अनुभव होने लगता है। ये शक्तिया ही आत्माकी श्री है, में जहा 'ब्रह्मपद' का उल्लेख है वहां उसे 'जिनपद' के अभिलक्ष्मी है, शोभा है । और यह विकास उसी प्रकारका होता प्रायसे सर्वथा भिन्न न समझना चाहिये । वहा अगले ही पद्य है जिस प्रकारका कि सुवर्ण-पाषाणसे सुवर्णका होता है। (५) में उन्हें स्पष्टतया जिन' रूपसे उल्लेखित भी किया है। पाषाण-स्थित सुवर्ण जिस तरह अग्नि-प्रयोगादिके योग्य दोनों पदोंमे थोडासा दृष्टिभेद है-'जिन' पद कर्मके निषेधसाधनोंको पाकर किट्ट-कालिमादि पाषाणमलसे अलग की दृष्टिको लिये हुए है और 'ब्रह्म' पद स्वरूपमें अवस्थिति होता हुआ अपने शुद्ध सुवर्णरूपमें परिणत हो जाता है उसी अथवा प्रवृत्तिकी दृष्टिको प्रधान किये हुए है । कर्मके निषेधतरह यह संसारी जीव उक्त कर्ममलके भस्म होकर पृथक् विना स्वरूपमे प्रवृत्ति नहीं बनती और स्वरूपमें प्रवृत्तिके हो जानेपर अपने शुवात्मस्वरूपमें परिणत हो जाता है। विना कर्मका निषेध कोई अर्थ नही रखता। विधि और घाति-कर्ममलके अभावके साथ प्रादुर्भत होने वाले इस निषेध दोनोंमें परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध है-एकके विकासकानाम ही 'आर्हन्त्यपद' है जो बडा ही अचिन्त्य है विना दूसरेका अस्तित्व ही नही बनता, यह बात प्रस्तुत ग्रन्थअद्भुत है और त्रिलोककी पूजाके अतिशय (परमप्रकर्ष) में खूब स्पष्ट करके समझाई गई है । अत संज्ञा अथवा शब्दका स्थान है (१३३) । इसीको जिनपद, कैवल्यपद तथा भेदके कारण सर्वथा भेदकी कल्पना करना न्याय-संगत नही १. सिडिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुण-गणगणोच्छादिदोषाप- १. मप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति ।
हारात् । योग्योपादान-युक्त्या वृषबह यथा हेमभावो- तेषामेवोत्पत्तिहिन्सेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥४॥ पलग्षिः ॥१॥ -पूज्यपाद-सिटमक्ति
-पुरुषार्थसिमपुपाये, अमृतचनः।