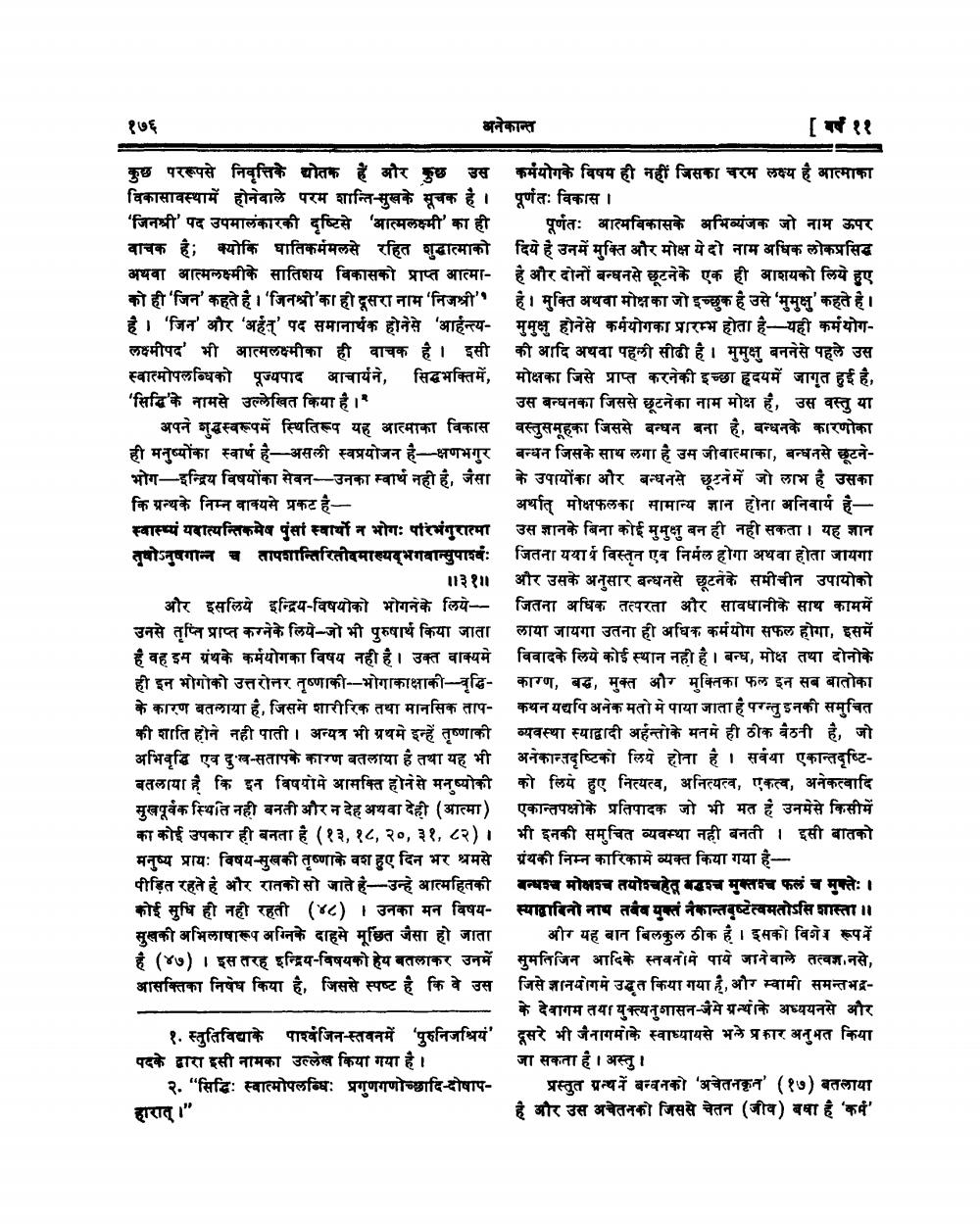________________
अनेकान्त
[वर्ष ११
कुछ पररूपसे निवृत्तिके द्योतक हैं और कुछ उस कर्मयोगके विषय ही नहीं जिसका चरम लक्ष्य है आत्माका विकासावस्थामें होनेवाले परम शान्ति-सुखके सूचक है। पूर्णतः विकास । 'जिनश्री' पद उपमालंकारकी दृष्टिसे 'आत्मलक्ष्मी' का ही पूर्णतः आत्मविकासके अभिव्यंजक जो नाम ऊपर वाचक है; क्योकि घातिकर्ममलसे रहित शुद्धात्माको दिये है उनमें मुक्ति और मोक्ष ये दो नाम अधिक लोकप्रसिद्ध अथवा आत्मलक्ष्मीके सातिशय विकासको प्राप्त आत्मा- है और दोनों बन्धनसे छूटनेके एक ही आशयको लिये हुए को ही 'जिन' कहते है। जिनश्री'का ही दूसरा नाम 'निजश्री' है। मुक्ति अथवा मोक्षका जो इच्छुक है उसे 'मुमुक्षु' कहते है। है। 'जिन' और 'अर्हत' पद समानार्थक होनेसे 'आर्हन्त्य- मुमुक्षु होनेसे कर्मयोगका प्रारम्भ होता है-यही कर्मयोगलक्ष्मीपद' भी आत्मलक्ष्मीका ही वाचक है। इसी की आदि अथवा पहली सीढी है। मुमुक्षु बननेसे पहले उस स्वात्मोपलब्धिको पूज्यपाद आचार्यने, सिद्धभक्तिमें, मोक्षका जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा हृदयमें जागृत हुई है, "सिद्धि के नामसे उल्लेखित किया है।
उस बन्धनका जिससे छूटनेका नाम मोक्ष है, उस वस्तु या __ अपने शुद्धस्वरूपमें स्थितिरूप यह आत्माका विकास वस्तुसमूहका जिससे बन्धन बना है, बन्धनके कारणोका ही मनुष्योंका स्वार्थ है-असली स्वप्रयोजन है-क्षणभगुर बन्धन जिसके साथ लगा है उस जीवात्माका, बन्धनसे छूटनेभोग-इन्द्रिय विषयोंका सेवन-उनका स्वार्थ नही है, जैसा के उपायोंका और बन्धनसे छूटने में जो लाभ है उसका कि ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रकट है
अर्थात् मोक्षफलका सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य हैस्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा उस ज्ञानके बिना कोई मुमुक्षु बन ही नहीं सकता। यह ज्ञान तुषोऽनुषगान्न च तापशान्तिरितीवमात्यद्भगवान्सुपाश्वः जितना ययार्थ विस्तृत एव निर्मल होगा अथवा होता जायगा
॥३१॥ और उसके अनुसार बन्धनसे छूटनेके समीचीन उपायोको और इसलिये इन्द्रिय-विषयोको भोगनेके लिये- जितना अधिक तत्परता और सावधानीके साथ काममें उनसे तृप्ति प्राप्त करनेके लिये-जो भी पुरुषार्थ किया जाता लाया जायगा उतना ही अधिक कर्मयोग सफल होगा, इसमें है वह इस ग्रंथके कर्मयोगका विषय नही है। उक्त वाक्यमे विवादके लिये कोई स्थान नहीं है। बन्ध, मोक्ष तथा दोनोके ही इन भोगोको उत्तरोनर तृष्णाकी-भोगाकाक्षाकी वृद्धि- कारण, बद्ध, मुक्त और मुक्तिका फल इन सब बातोका के कारण बतलाया है, जिसमे शारीरिक तथा मानसिक ताप- कथन यद्यपि अनेक मतो मे पाया जाता है परन्तु इनकी समुचित की शाति होने नही पाती। अन्यत्र भी ग्रथमे इन्हें तृष्णाकी व्यवस्था स्याद्वादी अर्हन्तोके मनमे ही ठीक बैठनी है, जो अभिवृद्धि एव दुःख-सतापके कारण बतलाया है तथा यह भी अनेकान्तदृष्टिको लिये होता है । सर्वथा एकान्तदृष्टिबतलाया है कि इन विषयोमे आसक्ति होनेसे मनुष्योकी को लिये हुए नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्वादि सुखपूर्वक स्थिति नही बनती और न देह अथवा देही (आत्मा) एकान्तपक्षोके प्रतिपादक जो भी मत है उनमेसे किसीमें का कोई उपकार ही बनता है (१३, १८, २०, ३१, ८२)। भी इनकी समुचित व्यवस्था नहीं बनती । इसी बातको मनुष्य प्रायः विषय-सुखकी तृष्णाके वश हुए दिन भर श्रमसे ग्रंयकी निम्न कारिकामे व्यक्त किया गया हैपीड़ित रहते है और रातको सो जाते है-उन्हे आत्महितको बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्चहेतू बडश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः । कोई सुधि ही नही रहती (४८) । उनका मन विषय- स्यावादिनो नाप तवैव युक्तं नकान्तवृष्टत्वमतोऽसि शास्ता॥ सुखकी अभिलाषारूप अग्निके दाहले मूछित जैसा हो जाता और यह बात बिलकुल ठीक है । इसको विशेष रूप में है (४७) । इस तरह इन्द्रिय-विषयको हेय बतलाकर उनमें सुमतिजिन आदिके स्तवनामे पाये जानेवाले तत्वज्ञानसे, आसक्तिका निषेध किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे उस जिसे ज्ञानयोगमे उद्धृत किया गया है, और स्वामी समन्तभद्र
के देवागम तया युक्त्यनुशासन-जैसे ग्रन्थोके अध्ययनसे और १. स्तुतिविद्याके पार्श्वजिन-स्तवनमें 'पुरुनिजश्रियं' दूसरे भी जैनागमोके स्वाध्यायसे भले प्रकार अनुभत किया पदके द्वारा इसी नामका उल्लेख किया गया है।
जा सकता है । अस्तु। २. "सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगणोच्छादि-दोषाप- प्रस्तुत ग्रन्थ में बन्वनको 'अचेतनकृन' (१७) बतलाया
है और उस अचेतनको जिससे चेतन (जीव) बचा है 'कर्म'
जा सकता