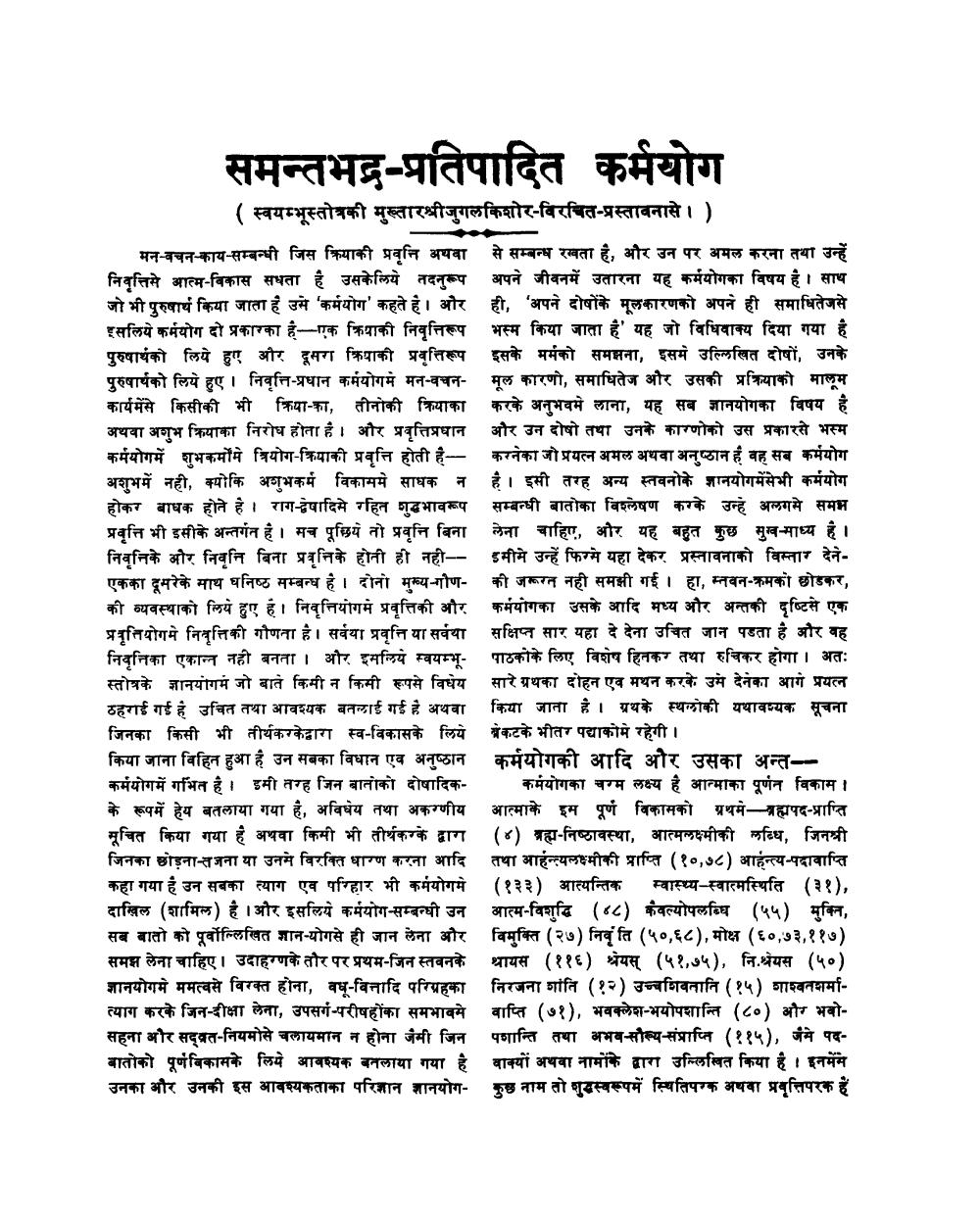________________
समन्तभद्र-प्रतिपादित कर्मयोग ( स्वयम्भूस्तोत्रकी मुख्तारश्रीजुगलकिशोर-विरचित-प्रस्तावनासे। )
मन-वचन-काय-सम्बन्धी जिस क्रियाकी प्रवृनि अथवा से सम्बन्ध रखता है, और उन पर अमल करना तथा उन्हें निवृत्तिमे आत्म-विकास सधता है उसकेलिये तदनुरूप अपने जीवनमें उतारना यह कर्मयोगका विषय है। साथ जो भी पुरुषार्थ किया जाता है उसे 'कर्मयोग' कहते है। और ही, 'अपने दोषोंके मूलकारणको अपने ही समाधितेजसे इसलिये कर्मयोग दो प्रकारका है-एक क्रियाकी निवृत्तिरूप भस्म किया जाता है' यह जो विधिवाक्य दिया गया है पुरुषार्थको लिये हुए और दूसग क्रियाकी प्रवृत्तिरूप इसके मर्मको समझना, इसमें उल्लिखित दोषों, उनके पुरुषार्थको लिये हुए। निवृत्ति-प्रधान कर्मयोगमे मन-वचन- मूल कारणो, समाधितेज और उसकी प्रक्रियाको मालूम कार्यमेंसे किसीकी भी क्रिया-का, तीनोकी क्रियाका करके अनुभवमे लाना, यह सब ज्ञानयोगका विषय है अथवा अशुभ क्रियाका निरोध होता है। और प्रवृत्तिप्रधान और उन दोषो तथा उनके कारणोको उस प्रकारसे भस्म कर्मयोगमें शुभकर्मोंमे त्रियोग-क्रियाकी प्रवृत्ति होती है- करनेका जो प्रयत्न अमल अथवा अनुष्ठान है वह सब कर्मयोग अशुभमें नही, क्योकि अशुभकर्म विकाममे साधक न है। इसी तरह अन्य स्तवनोके ज्ञानयोगमेंसेभी कर्मयोग होकर बाधक होते है। राग-द्वेषादिमे हित शुद्धभावरूप सम्बन्धी बातोका विश्लेषण करके उन्हें अलगमे समझ प्रवृत्ति भी इसीके अन्तर्गत है। मच पूछिये तो प्रवृनि बिना लेना चाहिए, और यह बहुत कुछ मुख-माध्य है। निवृनिके और निवृत्ति बिना प्रवृत्तिके होती ही नही-- इमीमे उन्हें फिग्मे यहा देकर प्रस्तावनाको विस्तार देनेएकका दूसरेके माथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनो मुख्य-गौण- की जरूरत नही समझी गई। हा, म्नवन-क्रमको छोडकर, की व्यवस्थाको लिये हुए है। निवृत्तियोगी प्रवृत्तिकी और कर्मयोगका उसके आदि मध्य और अन्तकी दृष्टिसे एक प्रवृत्तियोगमे निवृत्ति की गौणता है। सर्वया प्रवृत्ति या सर्वया सक्षिप्त सार यहा दे देना उचित जान पडता है और वह निवृतिका एकान्न नहीं बनता। और इमलिये स्वयम्भू- पाठकोके लिए विशेष हितकर तथा रुचिकर होगा। अतः स्तोत्रके ज्ञानयोगमं जो बाते किमी न किमी रूपसे विधेय सारे ग्रथका दोहन एव मथन करके उमे देनेका आगे प्रयत्न ठहराई गई है उचित तथा आवश्यक बतलाई गई है अथवा किया जाता है। प्रथके स्थलोकी यथावश्यक सूचना जिनका किसी भी तीर्थकरकेद्वारा स्व-विकासके लिये बेकटके भीतर पद्याकोमे रहेगी। किया जाना विहिन हुआ है उन सबका विधान एव अनुष्ठान कर्मयोगकी आदि और उसका अन्तकर्मयोगमें गर्भित है। इसी तरह जिन बातोको दोषादिक- कर्मयोगका चरम लक्ष्य है आत्माका पूर्णत विकाम । के रूपमें हेय बतलाया गया है, अविधेय तथा अकरणीय आत्माके इम पूर्ण विकामको प्रथमेब्रह्मपद-प्राप्ति मूचित किया गया है अथवा किसी भी तीर्थकरके द्वाग (४) ब्रह्म-निष्ठावस्था, आत्मलक्ष्मीको लब्धि, जिनश्री जिनका छोड़ना-तजना या उनमे विरक्ति धारण करना आदि तथा आहंन्यलक्ष्मीकी प्राप्ति (१०,७८) आर्हन्त्य-पदावाप्ति कहा गया है उन सबका त्याग एव परिहार भी कर्मयोगमे (१३३) आत्यन्तिक स्वास्थ्य-स्वात्मस्थिति (३१), दाखिल (शामिल) है । और इसलिये कर्मयोग-सम्बन्धी उन आत्म-विशुद्धि (४८) कैवल्योपलब्धि (५५) मुक्नि, सब बातो को पूर्वोल्लिखित ज्ञान-योगसे ही जान लेना और विमुक्ति (२७) निवृति (५०,६८), मोक्ष (६०,७३,११७) समझ लेना चाहिए। उदाहरणके तौर पर प्रथम-जिन स्तवनके थायस (११६) श्रेयस् (५१,७५), नि.श्रेयस (५०) ज्ञानयोगमे ममत्वसे विरक्त होना, वधू-वित्तादि परिग्रहका निरजना शांति (१२) उच्चशिवताति (१५) शाश्वतशर्मात्याग करके जिन-दीक्षा लेना, उपसर्ग-परीषहोंका समभावमे वाप्ति (७१), भवक्लेश-भयोपशान्ति (८०) और भवोसहना और सद्वत-नियमोसे चलायमान न होना जमी जिन पशान्ति तथा अभव-सौख्य-संप्राप्ति (११५), जैसे पदबातोको पूर्णविकामके लिये आवश्यक बतलाया गया है वाक्यों अथवा नामोंके द्वारा उल्लिखित किया है । इनमेंमे उनका और उनकी इस आवश्यकताका परिज्ञान ज्ञानयोग- कुछ नाम तो शुद्धस्वरूपमें स्थितिपरक अथवा प्रवृत्तिपरक हैं