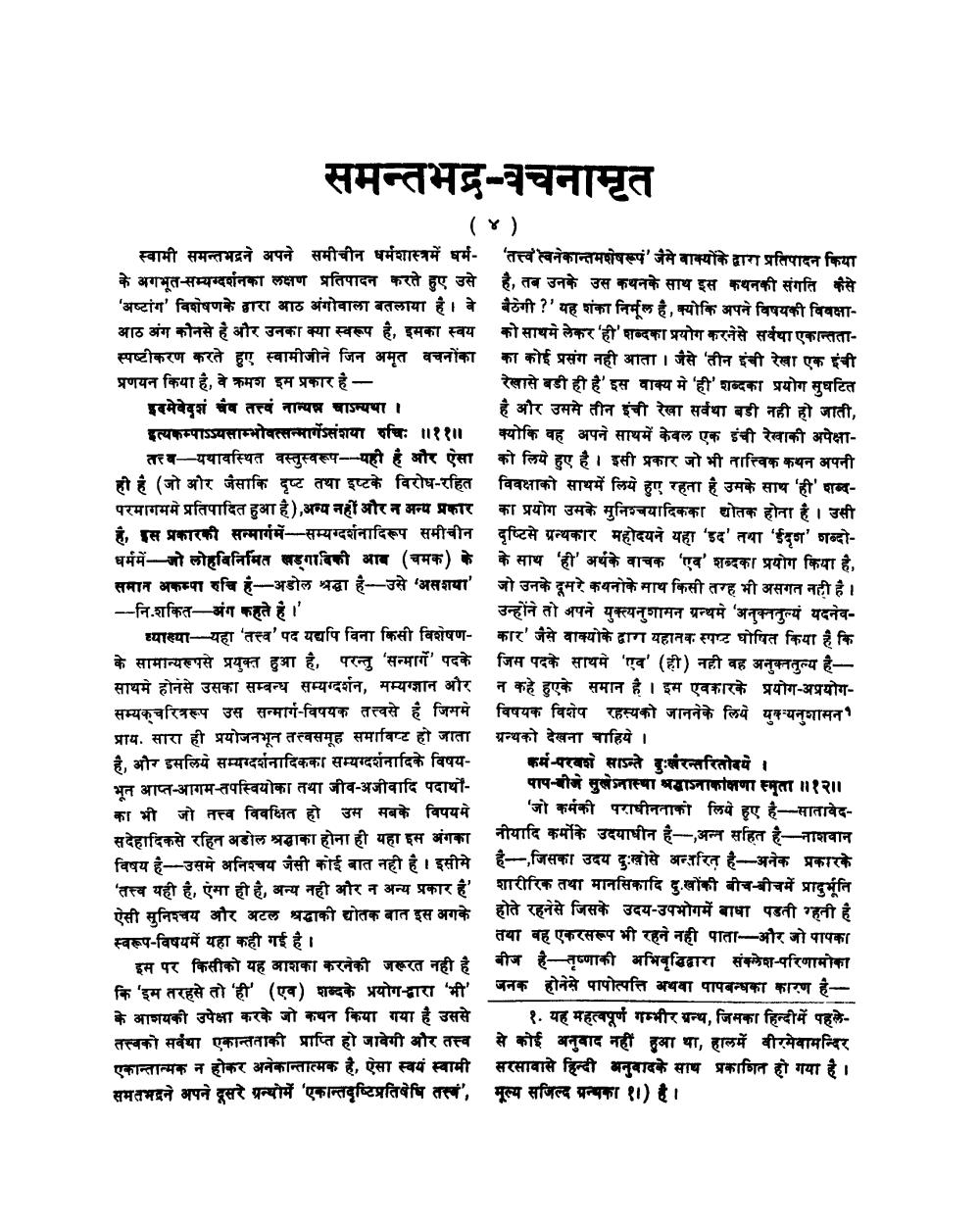________________
समन्तभद्र-वचनामृत
( ४ )
'तत्त्वं त्वनेकान्तमशेषरूपं' जैसे वाक्योंके द्वारा प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथन के साथ इस कथनकी संगति कैसे बैठेगी ?' यह शंका निर्मूल है, क्योकि अपने विषयकी विवक्षाको साथमे लेकर 'ही' शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वथा एकान्तताका कोई प्रसंग नही आता। जैसे 'तीन इंची रेखा एक इंची रेखासे बडी ही है' इस वाक्य मे 'ही' शब्दका प्रयोग सुघटित है और उसने तीन इंची रेखा सर्वधा बडी नही हो जाती, क्योंकि यह अपने साथमें केवल एक इंसी रेलाकी अपेक्षाको लिये हुए है। इसी प्रकार जो भी तात्त्विक कथन अपनी विवक्षाको साथमें लिये हुए रहता है उसके साथ 'ही' शब्दका प्रयोग उसके सुनिश्चयादिकका द्योतक होता है। उसी दृष्टिने प्रत्यकार महोदयने यहा 'डद' तथा 'ई' दोके साथ 'ही' अर्थके वाचक 'एव' शब्दका प्रयोग किया है, जो उनके दूसरे कथनोके माथ किसी तरह भी असगत नही है। उन्होंने तो अपने युक्त्यनुशासन ग्रन्थमे 'अनुक्ततुल्यं यदनेवकार' जैसे वाक्योके द्वारा यहातक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथमे 'एव' (ही) नही वह अनुक्ततुल्य है— न कहे हुएके समान है। इस एवकारके प्रयोग अप्रयोगविषयक विशेष रहस्यको जाननेके लिये ग्रन्थको देखना चाहिये ।
पनुशासन'
स्वामी समन्तभद्रने अपने समीचीन धर्मशास्त्रमें धर्मके अगभूत-सम्यदर्शनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे 'अष्टांग' विशेषणके द्वारा आठ अंगोवाला बतलाया है। वे आठ अंग कौनसे है और उनका क्या स्वरूप है, इसका स्वय स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजीने जिन अमृत वचनोंका प्रणयन किया है, वे क्रमश इम प्रकार है
-
इदमेवेशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चाऽन्यथा । इत्यकम्पाऽऽयसाम्भोवत्सन्मार्गेऽसंशया दचिः ॥११॥ तर - यथावस्थित वस्तुस्वरूप - यही है और ऐसा ही हैं (जो और जैसाकि दृष्ट तथा इष्टके विरोध - रहित परमागममे प्रतिपादित हुआ है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्ग में सम्यग्दर्शनादिरूप समीचीन धर्ममें जो लोहविनिर्मित गावकी आज ( चमक) के समान अकम्पा रुचि है—अडोल श्रद्धा है— उसे 'असशया' - नि.शक्ति अंग कहते है।'
व्याख्या—यहा 'तत्त्व' पद यद्यपि विना किसी विशेषणके सामान्यरूपसे प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 'सन्मार्गे' पदके साथमे होनेसे उसका सम्बन्ध सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकृचरित्ररूप उस सन्मार्ग-विषयक तत्व हैं जिनमे प्राय. सारा ही प्रयोजनभूत तत्वसमूह समाविष्ट हो जाता है, और इसलिये सम्यग्दर्शनादिकका सम्यग्दर्शनादिके विषयभूत आप्त-आगम- तपस्वियोका तथा जीव अजीवादि पदार्थोंका भी जो तत्त्व विवक्षित हो उस सबके विषय मे सदेहादिकसे रहिन अडोल बद्धाका होना ही यहा इस अंगका विषय है--- उसमे अनिश्चय जैसी कोई बात नही है। इसी 'तत्त्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नही और न अन्य प्रकार है' ऐसी सुनिश्चय और अटल पद्धाकी दोतक बात इस अगके स्वरूप-विषयमें यहा कही गई है।
इस पर किसीको यह आशका करनेकी जरूरत नही है कि 'इस तरहसे तो 'ही' (एव) शब्दके प्रयोग द्वारा 'भी' के आशयकी उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तत्त्वको सर्वधा एकान्तताकी प्राप्ति हो जावेगी और तस्व एकान्तात्मक न होकर अनेकान्तात्मक है, ऐसा स्वयं स्वामी समतभद्रने अपने दूसरे ग्रन्थोमें 'एकान्तदृष्टिप्रतिवेषि तस्वं
कर्म-परवसा दुरन्तरितोदये। पाप-बीने सुखेनारचा बढाउनाकांक्षा स्मृता ॥ १२ ॥ 'जो कर्मकी पराधीनताका लिये हुए है-मानावेद नीयादि कर्मोंक उपाधीन है- अन्न सहित है-नाशवान है जिसका उदय दुःखोसे अस्तरित है—अनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसिकादि दु.खोंकी बीच-बीच में प्रादुर्मूर्ति होते रहने से जिसके उदय उपभोगमें बाधा पड़ती रहती है तथा वह एकरसरूप भी रहने नही पाता और जो पापका बीज है- तृष्णाकी अभिवृद्धिद्वारा संक्मेश-परिणामका जनक होनेसे पापोत्पत्ति अथवा पापबन्धका कारण है
१. यह महत्वपूर्ण गम्भीर ग्रन्थ, जिसका हिन्दी में पहलेसे कोई अनुवाद नहीं हुआ था, हालमें वीरमेवामन्दिर सरसावासे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित हो गया है। मूल्य सजिल्द ग्रन्थका १।) है।