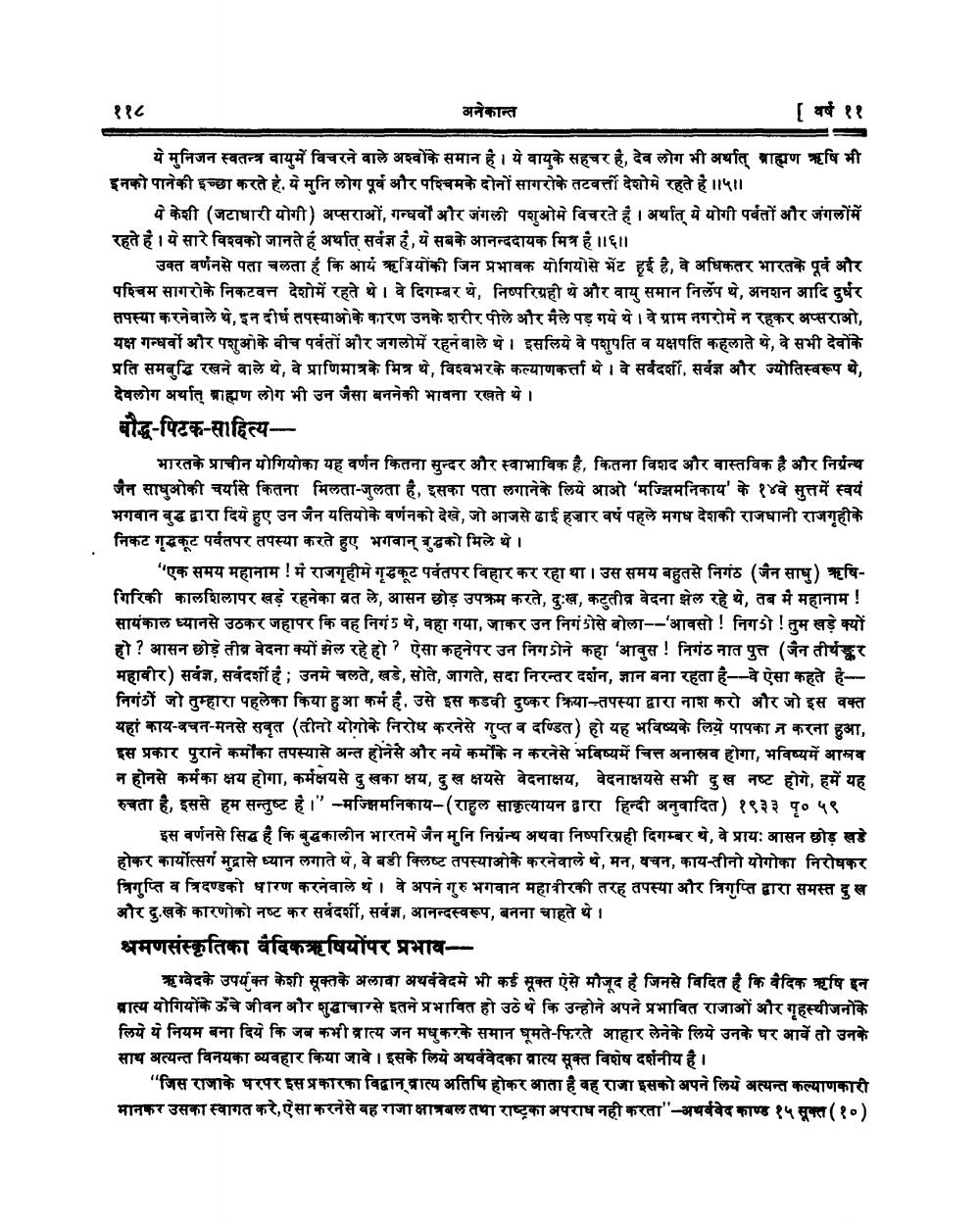________________
११८
अनेकान्त
[ वर्ष ११
ये मुनिजन स्वतन्त्र वायुमें विचरने वाले अश्वोंके समान है। ये वायुके सहचर है, देव लोग भी अर्थात् ब्राह्मण ऋषि भी इनको पानेकी इच्छा करते है. ये मुनि लोग पूर्व और पश्चिमके दोनों सागरोके तटवर्ती देशोमे रहते है ॥५॥
ये केशी (जटाधारी योगी) अप्सराओं, गन्धवों और जंगली पशुओमे विचरते है । अर्थात् ये योगी पर्वतों और जंगलोंमें रहते है। ये सारे विश्वको जानते हैं अर्थात सर्वज्ञ है, ये सबके आनन्ददायक मित्र है॥६॥
उक्त वर्णनसे पता चलता है कि आर्य ऋषियोंकी जिन प्रभावक योगियोसे भेंट हुई है, वे अधिकतर भारतके पूर्व और पश्चिम सागरोके निकटवत्त देशोमें रहते थे। वे दिगम्बर थे, निष्परिग्रही थे और वायु समान निर्लेप थे, अनशन आदि दुर्धर तपस्या करनेवाले थे, इन दीर्घ तपस्याओके कारण उनके शरीर पीले और मैले पड़ गये थे। वे ग्राम नगरोमे न रहकर अप्सराओ, यक्ष गन्धर्वो और पशुओके बीच पर्वतों और जगलोमें रहनेवाले थे। इसलिये वे पशुपति व यक्षपति कहलाते थे, वे सभी देवोंके प्रति समबुद्धि रखने वाले थे, वे प्राणिमात्रके मित्र थे, विश्वभरके कल्याणकर्ता थे । वे सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और ज्योतिस्वरूप थे, देवलोग अर्थात् ब्राह्मण लोग भी उन जैसा बननेकी भावना रखते थे। बौद्ध-पिटक-साहित्य
भारतके प्राचीन योगियोका यह वर्णन कितना सुन्दर और स्वाभाविक है, कितना विशद और वास्तविक है और निर्ग्रन्थ जैन साधुओकी चर्यासे कितना मिलता-जुलता है, इसका पता लगानेके लिये आओ 'मज्झिमनिकाय के १४वे सुत्तमें स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा दिये हुए उन जैन यतियोके वर्णनको देखे, जो आजसे ढाई हजार वर्ष पहले मगध देशको राजधानी राजगृहीके निकट गृद्धकूट पर्वतपर तपस्या करते हुए भगवान् बुद्धको मिले थे।
"एक समय महानाम ! मै राजगृहीमे गृद्धकूट पर्वतपर विहार कर रहा था। उस समय बहुतसे निगंठ (जैन साधु) ऋषिगिरिको कालशिलापर खड़े रहनेका व्रत ले, आसन छोड़ उपक्रम करते, दुःख, कटुतीव्र वेदना झेल रहे थे, तब मै महानाम ! सायंकाल ध्यानसे उठकर जहापर कि वह निगंउ थे, वहा गया, जाकर उन निगंठोसे बोला--'आवसो! निगशे! तुम खड़े क्यों हो? आसन छोड़े तीव्र वेदना क्यों झेल रहे हो? ऐसा कहनेपर उन निगडोने कहा 'आवुस ! निगंठ नात पुत्त (जैन तीर्थङ्कर महावीर) सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है ; उनमे चलते, खडे, सोते, जागते, सदा निरन्तर दर्शन, ज्ञान बना रहता है-वे ऐसा कहते हैनिगंठों जो तुम्हारा पहलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कडवी दुष्कर क्रिया-तपस्या द्वारा नाश करो और जो इस वक्त यहां काय-वचन-मनसे सवृत (तीनो योगोके निरोध करनेसे गुप्त व दण्डित) हो यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ, इस प्रकार पुराने कोका तपस्यासे अन्त होनेसे और नये कर्मोके न करनेसे भविष्यमें चित्त अनास्रव होगा, भविष्यमें आम्रव न होनसे कर्मका क्षय होगा, कर्मक्षयसे दुखका क्षय, दुख क्षयसे वेदनाक्षय, वेदनाक्षयसे सभी दुख नष्ट होगे, हमें यह रुचता है, इससे हम सन्तुष्ट है।" -मज्झिमनिकाय-(राहुल साकृत्यायन द्वारा हिन्दी अनुवादित) १९३३ पृ० ५९
इस वर्णनसे सिद्ध है कि बुद्धकालीन भारतमे जैन मुनि निग्रन्थ अथवा निष्परिग्रही दिगम्बर थे, वे प्रायः आसन छोड़ खडे होकर कार्योत्सर्ग मुद्रासे ध्यान लगाते थे, वे बडी क्लिष्ट तपस्याओके करनेवाले थे, मन, वचन, काय-तीनो योगोका निरोधकर त्रिगुप्ति व त्रिदण्डको धारण करनेवाले थे। वे अपने गुरु भगवान महावीरकी तरह तपस्या और त्रिगुप्ति द्वारा समस्त दुख और दु.खके कारणोको नष्ट कर सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, आनन्दस्वरूप, बनना चाहते थे। श्रमणसंस्कृतिका वैदिकऋषियोंपर प्रभाव
ऋग्वेदके उपर्यक्त केशी सूक्तके अलावा अथर्ववेदमे भी कई सूक्त ऐसे मौजूद है जिनसे विदित है कि वैदिक ऋषि इन व्रात्य योगियोंके ऊँचे जीवन और शुद्धाचारसे इतने प्रभावित हो उठे थे कि उन्होने अपने प्रभावित राजाओं और गृहस्थीजनोंके लिये ये नियम बना दिये कि जब कभी वात्य जन मधुकरके समान घूमते-फिरते आहार लेनेके लिये उनके घर आवें तो उनके साथ अत्यन्त विनयका व्यवहार किया जावे । इसके लिये अथर्ववेदका व्रात्य सूक्त विशेष दर्शनीय है।
"जिस राजाके घरपर इस प्रकारका विद्वान व्रात्य अतिथि होकर आता है वह राजा इसको अपने लिये अत्यन्त कल्याणकारी मानकर उसका स्वागत करे,ऐसा करनेसे वह राजा क्षात्रबल तथा राष्ट्रका अपराध नही करता"-अथर्ववेद काण्ड १५ सूक्त (१०)