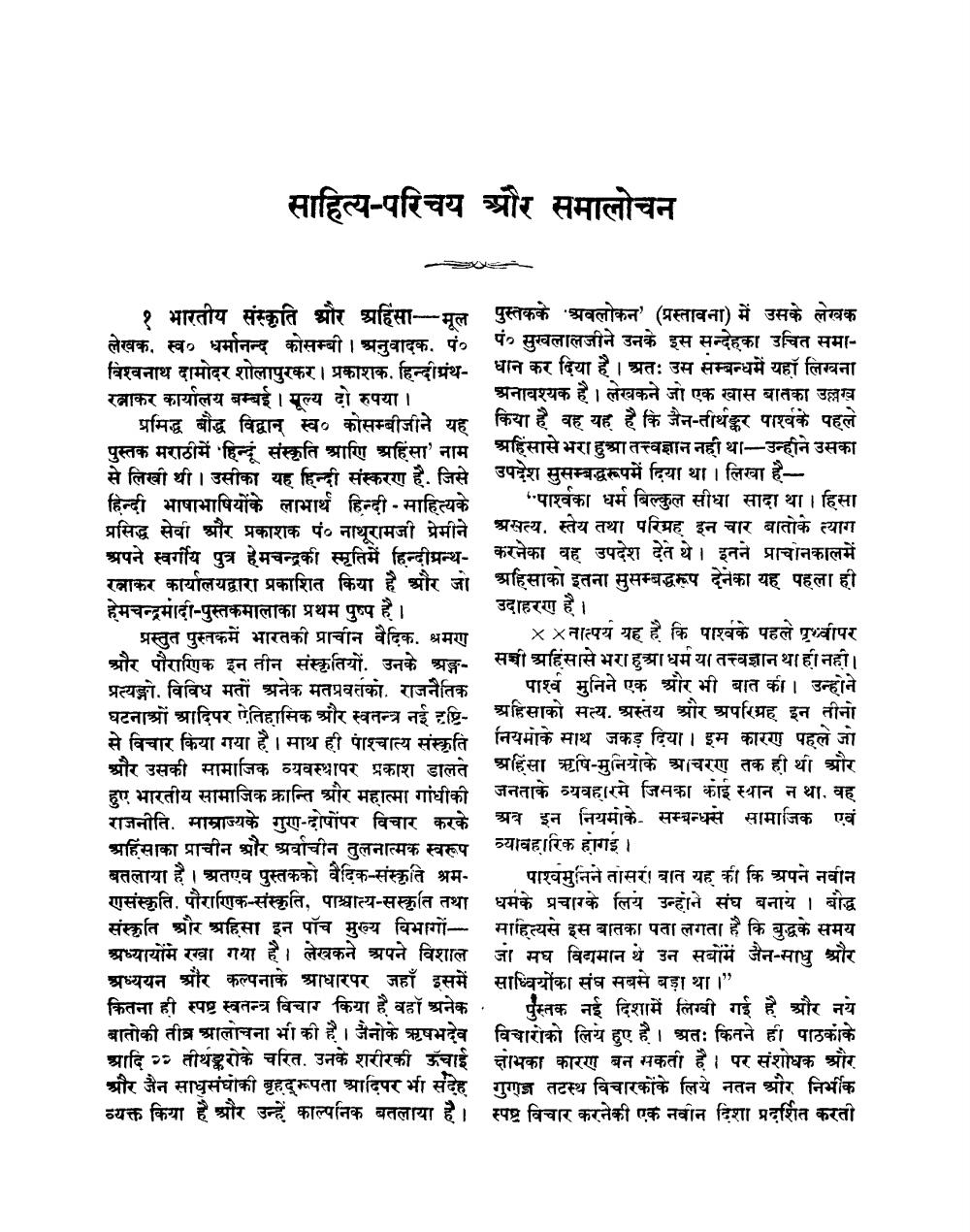________________
साहित्य - परिचय और समालोचन
१ भारतीय संस्कृति और अहिंसा - मूल लेखक, स्व० धर्मानन्द कोसम्बी । अनुवादक. पं० विश्वनाथ दामोदर शोलापुरकर। प्रकाशक. हिन्दीग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई । मूल्य दो रुपया ।
प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् स्व० कोसम्बीजीने यह पुस्तक मराठीमें 'हिन्दू संस्कृति आणि अहिंसा' नाम से लिखी थी । उसीका यह हिन्दी संस्करण है. जिसे हिन्दी भाषाभाषियोंके लाभार्थं हिन्दी - साहित्यके प्रसिद्ध सेवा और प्रकाशक पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने स्वर्गीय पुत्र हेमचन्द्रकी स्मृतिमें हिन्दीप्रन्थ रत्नाकर कार्यालयद्वारा प्रकाशित किया है और जो हेमचन्द्रमादी-पुस्तकमालाका प्रथम पुष्प है।
प्रस्तुत पुस्तक में भारत की प्राचीन वैदिक श्रमण और पौराणिक इन तीन संस्कृतियों. उनके अङ्गप्रत्यङ्गो. विविध मतों अनेक मतप्रवर्तको राजनैतिक घटनाओं आदिपर ऐतिहासिक और स्वतन्त्र नई दृष्टिसे विचार किया गया है। साथ ही पाश्चात्य संस्कृति और उसकी सामाजिक व्यवस्थापर प्रकाश डालते हुए भारतीय सामाजिक क्रान्ति और महात्मा गांधीकी राजनीति साम्राज्यके गुण-दोषोंपर विचार करके अहिंसाका प्राचीन और अर्वाचीन तुलनात्मक स्वरूप बतलाया है । अतएव पुस्तकको वैदिक-संस्कृति श्रम
संस्कृति, पौराणिक - संस्कृति, पाश्चात्य सस्कृति तथा संस्कृति और अहिसा इन पाँच मुख्य विभागोंअध्यायोंमें रखा गया है। लेखक अपने विशाल अध्ययन और कल्पनाके आधारपर जहाँ इसमें कितना ही स्पष्ट स्वतन्त्र विचार किया है वहाँ अनेक बातोकी तीव्र आलोचना भी की है। जैनोके ऋषभदेव आदि २० तीर्थङ्करो के चरित. उनके शरीरकी ऊँचाई और जैन साधुसंघकी बृहद्रूपता आदिपर भी संदेह व्यक्त किया है और उन्हें काल्पनिक बतलाया है।
पुस्तकके 'अवलोकन' (प्रस्तावना) में उसके लेखक पं० सुखलालजीने उनके इस सन्देहका उचित समाधान कर दिया है। अतः उस सम्बन्ध में यहाँ लिखना अनावश्यक है । लेखकने जो एक खास बातका उल्लेख किया है वह यह है कि जैन तीर्थङ्कर पार्श्व के पहले अहिंसासे भरा हुआ तत्त्वज्ञान नहीं था - उन्हीने उसका उपदेश सुसम्बद्धरूपमें दिया था । लिखा है
पार्श्वका धर्म बिल्कुल सीधा सादा था । हिसा असत्य स्तेय तथा परिग्रह इन चार बातो के त्याग करनेका वह उपदेश देते थे। इनने प्राचीनकालमें अहिसाको इतना सुसम्बद्धरूप देनेका यह पहला ही उदाहरण है ।
X x नात्पर्य यह है कि पार्श्वके पहले पृथ्वीपर सी अहिंसा से भरा हुआ धर्म या तत्त्वज्ञान था ही नहीं ।
पार्श्व मुनिने एक और भी बात की। उन्होंने अहिसाको सत्य अस्तंय और अपरिग्रह इन तीनो नियमोंके साथ जकड़ दिया । इस कारण पहले जो अहिंसा ऋषि-मुनियोंके आचरण तक ही थी और जनताके व्यवहारमे जिसका कोई स्थान न था. वह अव इन नियमोके सम्बन्धसे सामाजिक एवं व्यावहारिक होगई।
पाश्वमुनिने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिये उन्होंने संघ बनाये । बौद्ध साहित्यसे इस बातका पता लगता है कि बुद्धके समय जो मघ विद्यमान थे उन सबमें जैन साधु और साध्वियोंका संघ सबसे बड़ा था।"
पुस्तक नई दिशामें लिखी गई है और नये विचारोको लिये हुए है। अतः कितने ही पाठकांके क्षोभका कारण बन सकती है। पर संशोधक और गुग्न तटस्थ विचारकोंके लिये नतन और निर्भीक स्पष्ट विचार करनेकी एक नवीन दिशा प्रदर्शित करती