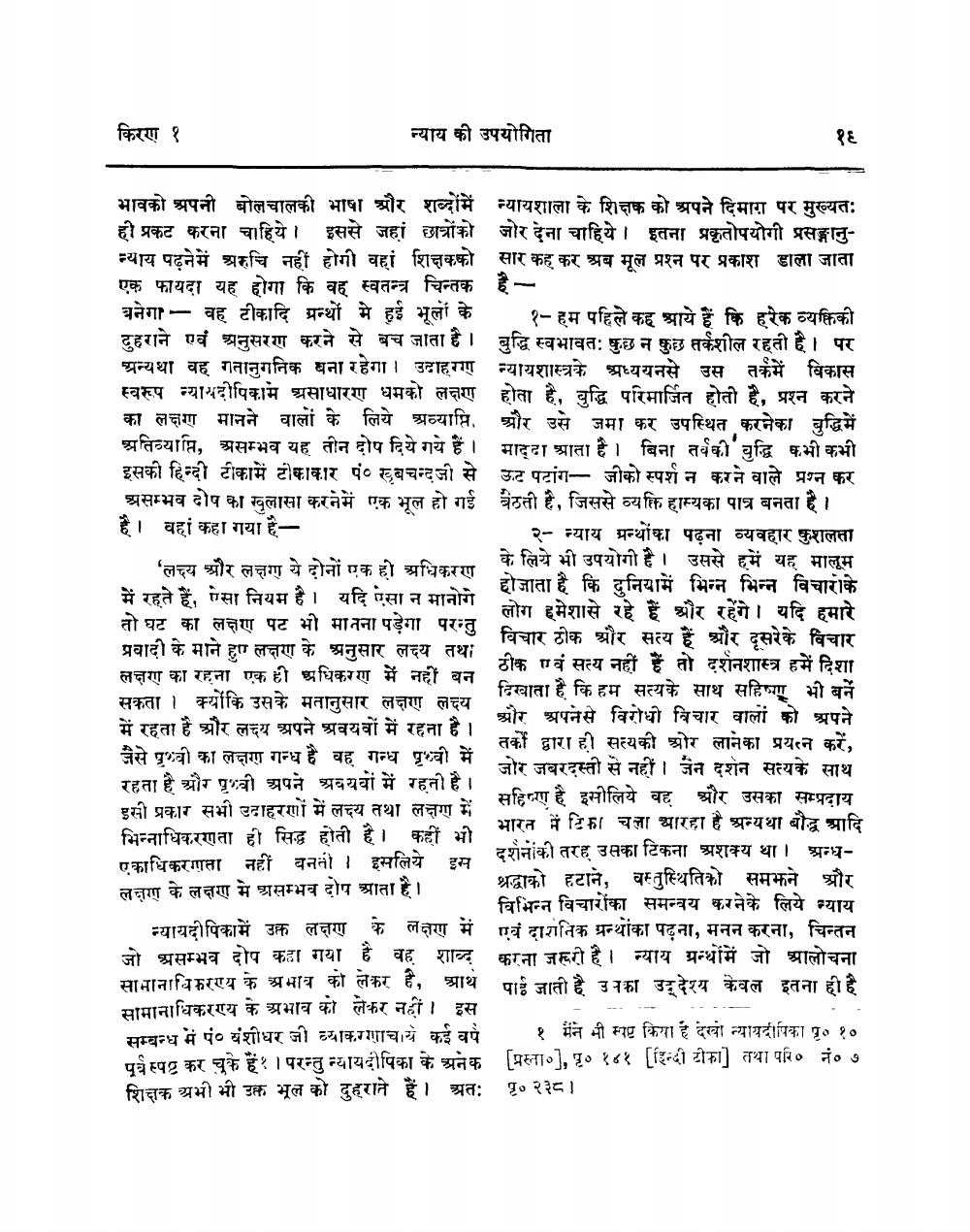________________
किरण १
न्याय की उपयोगिता
भावको अपनी बोलचालकी भाषा और शब्दों में न्यायशाला के शिक्षक को अपने दिमारा पर मुख्यतः ही प्रकट करना चाहिये। इससे जहां छात्रोंको जोर देना चाहिये। इतना प्रकृतोपयोगी प्रसङ्गानुन्याय पढ़ने में रुचि नहीं होगी वहां शिक्षकको सार कह कर अब मूल प्रश्न पर प्रकाश डाला जाता एक फायदा यह होगा कि वह स्वतन्त्र चिन्तक हैबनेगा- वह टीकादि ग्रन्थों मे हुई भूलों के १-हम पहिले कह पाये हैं कि हरेक व्यक्तिकी दहराने एवं अनुसरण करने से बच जाता है। बुद्धि स्वभावत: कुछ न कुछ तर्कशील रहती है। पर अन्यथा वह गतानुगनिक बना रहेगा। उदाहरण न्यायशास्त्रके अध्ययनसे उस तर्कमें विकास स्वरूप न्यायदोपिकाम असाधारण धमको लक्षण होता है, बुद्धि परिमार्जित होती है. प्रश्न करने का लक्षण मानने वालों के लिये अव्याप्ति, और उसे जमा कर उपस्थित करनेका बुद्धिमें अतिव्याप्ति, असम्भव यह तीन दोष दिये गये हैं। मादा पाता है। बिना तबकी बुद्धि कभी कभी इसकी हिन्दी टीकामें टीकाकार पं० खूबचन्दजी से ऊट पटांग- जीको स्पर्श न करने वाले प्रश्न कर असम्भव दोष का खुलासा करने में एक भूल हो गई बैठती है, जिससे व्यक्ति हास्यका पात्र बनता है। है। वहां कहा गया है
२- न्याय प्रन्थोंका पढ़ना व्यवहार कुशलता
के लिये भी उपयोगी है। उससे हमें यह मालूम __'लक्ष्य और लक्षण ये दोनों एक ही अधिकरण
होजाता है कि दुनिया में भिन्न भिन्न विचारोके में रहते हैं, ऐसा नियम है। यदि ऐसा न मानोगे
लोग हमेशासे रहे हैं तो घट का लक्षण पट भी मानना पड़ेगा परन्तु विचार ठीक और सत्य हैं और दूसरेके विचार
और रहेंगे। यदि हमारे प्रवादी के माने हुए लक्षण के अनुसार लक्ष्य तथा
ठीक एवं सत्य नहीं हैं तो दर्शनशास्त्र हमें दिशा लक्षण का रहना एक ही अधिकरण में नहीं बन
दिखाता है कि हम सत्यके साथ सहिषा भी बनें सकता। क्योंकि उसके मतानुसार लक्षण लक्ष्य
और अपनेसे विरोधी विचार वालों को अपने में रहता है और लक्ष्य अपने अवयवों में रहता है।
तों द्वारा ही सत्यकी ओर लाने का प्रयत्न करें, जैसे पृथ्वी का लक्षण गन्ध है वह गन्ध पृथ्वी में
जोर जबरदस्ती से नहीं। जैन दर्शन सत्यके साथ रहता है और पृथ्वी अपने अवयवों में रहती है।
सहिष्ण है इसीलिये वह और उसका सम्प्रदाय इसी प्रकार सभी उदाहरणों में लक्ष्य तथा लक्षण में
भारत में टिका चला रहा है अन्यथा बौद्ध आदि भिन्नाधिकरणता ही सिद्ध होती है। कहीं भी
दर्शन की तरह उसका टिकना अशक्य था। अन्धएकाधिकरगाता नहीं बनती। इसलिये इस
श्रद्धाको हटाने, वस्तुस्थितिको समझने और लक्षण के लक्षण मे असम्भव दोप आता है।
विभिन्न विचारोंका समन्वय करनेके लिये भ्याय न्यायदीपिकामें उक्त लक्षण के लक्षण में एवं दाशनिक ग्रन्थाका पढ़ना, मनन करना, चिन्तन जो असम्भव दोप कहा गया है वह शाब्द करना जरूरी है। न्याय ग्रन्थों में जो आलोचना सामानाधिकरण्य के अभाव को लेकर है, आथ पाई जाती है उसका उद्देश्य केवल इतना ही है सामानाधिकरण्य के अभाव को लेकर नहीं। इस सम्बन्ध में पं० वंशीधर जी व्याकरणाचाये कई वर्ष १ मैने भी स्पष्ट किया है देखो न्यायदीपिका पृ० १० पूर्व स्पष्ट कर चुके हैं। परन्तु न्यायदीपिका के अनेक [प्रस्ता०], पृ० १४१ [हिन्दी टीका] तथा परि० नं०७ शिक्षक अभी भी उक्त भूल को दुहराते हैं। अत: पृ०२३८ ।