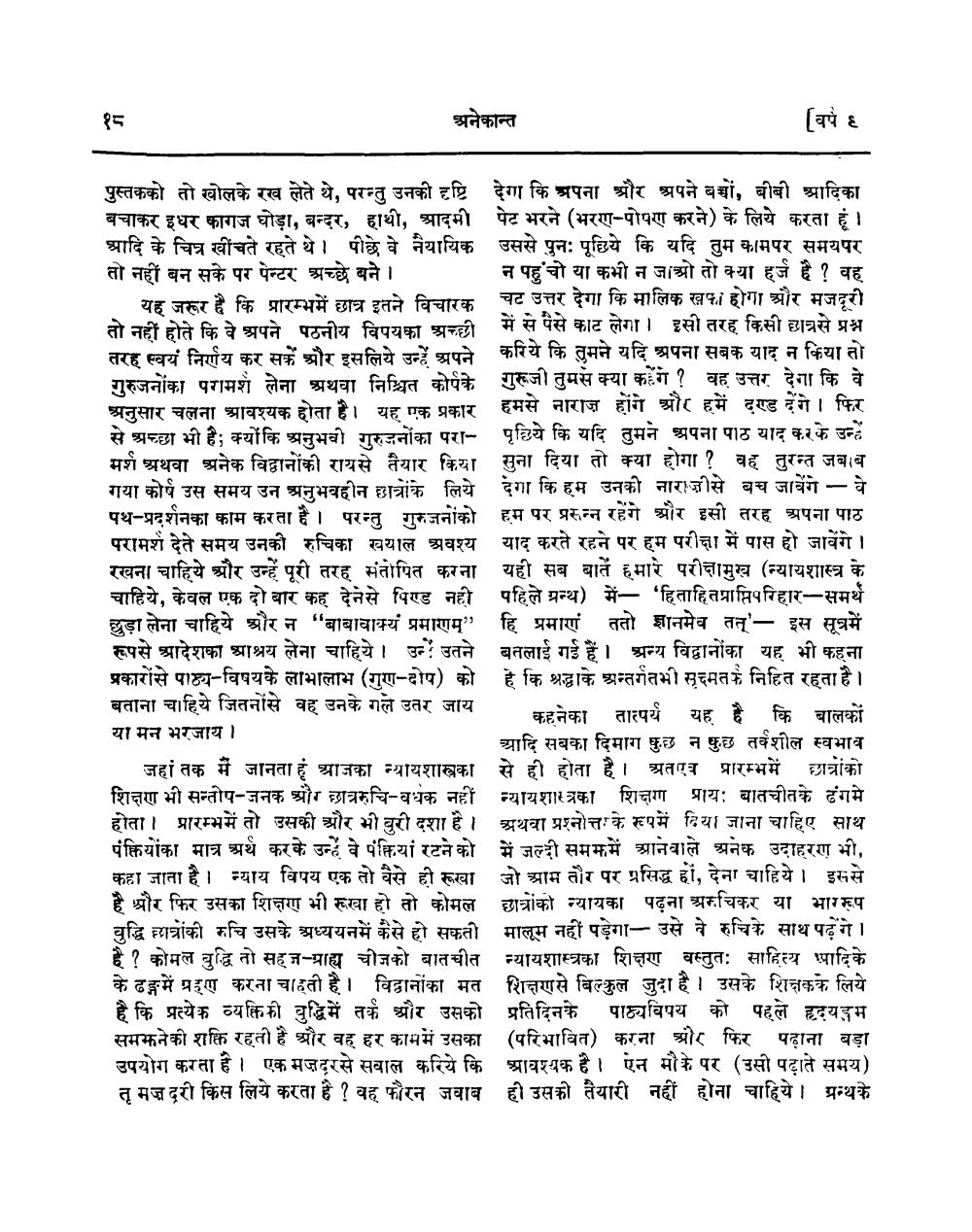________________
अनेकान्त
[वपे
पुस्तकको तो खोलके रख लेते थे, परन्तु उनकी दृष्टि देगा कि अपना और अपने बच्चों, बीबी आदिका बचाकर इधर कागज घोड़ा, बन्दर, हाथी, आदमी पेट भरने (भरण-पोपण करने) के लिये करता है। आदि के चित्र खींचते रहते थे। पीछे वे नैयायिक उससे पुनः पूछिये कि यदि तुम कामपर समयपर तो नहीं बन सके पर पेन्टर अच्छे बने।
न पहुंचो या कभी न जाओ तो क्या हर्ज है ? वह यह जरूर है कि प्रारम्भमें छात्र इतने विचारक चट उत्तर देगा कि मालिक खफा होगा और मजदरी तो नहीं होते कि वे अपने पठनीय विपयका अच्छी में से पैसे काट लेगा। इसी तरह किसी छात्रसे प्रश्न तरह स्वयं निर्णय कर सकें और इसलिये उन्हें अपने करिये कि तुमने यदि अपना सबक याद न किया तो गुरुजनोंका परामर्श लेना अथवा निश्चित कोपके गुरूजी तुमसे क्या कहेंगे ? वह उत्तर देगा कि वे अनुसार चलना आवश्यक होता है। यह एक प्रकार हमसे नाराज होंगे और हमें दण्ड देगे। फिर से अच्छा भी है। क्योंकि अनुभवी गुरुजनोंका परा- पृछिये कि यदि तुमने अपना पाठ याद करके उन्हें मर्श अथवा अनेक विद्वानोंकी रायसे तैयार किया सुना दिया तो क्या होगा? वह तुरन्त जबाब गया कोर्ष उस समय उन अनुभवहीन छात्रों के लिये दंगा कि हम उनकी नाराजीसे बच जावेंगे - वे पथ-प्रदर्शनका काम करता है। परन्तु गुरुजनोंको हम पर प्रसन्न रहेंगे और इसी तरह अपना पाठ परामर्श देते समय उनको रुचिका खयाल अवश्य याद करते रहने पर हम परीक्षा में पास हो जायेंगे। रखना चाहिये और उन्हें पूरी तरह संतोपित करना यही सब बातें हमारे परीक्षामुख (न्यायशास्त्र के चाहिये, केवल एक दो बार कह देनेसे पिण्ड नही पहिले ग्रन्थ) में- 'हिताहितप्राप्तिपरिहार-समर्थ छड़ा लेना चाहिये और न "बाबावाक्यं प्रमाणम्” हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्'- इस सूत्रमें रूपसे आदेशका श्राश्रय लेना चाहिये। उन्हें उतने बतलाई गई हैं। अन्य विद्वानोंका यह भी कहना प्रकारोंसे पाठ्य-विषयके लाभालाभ (गुण-दोप) को है कि श्रद्धाके अन्तर्गतभी सूक्ष्मतर्फ निहित रहता है। बताना चाहिये जितनोंसे वह उनके गले उतर जाय
कहनेका तात्पर्य यह है कि बालकों या मन भरजाय।
आदि सबका दिमाग कुछ न कुछ तशील स्वभाव जहां तक मैं जानता हूं आजका न्यायशास्त्रका से ही होता है। अतएव प्रारम्भमें छात्रांको शिक्षण भी सन्तोप-जनक और छात्ररुचि-वधक नहीं न्यायशास्त्रका शिक्षण प्राय: बातचीत के ढंगमे होता। प्रारम्भमें तो उसकी और भी बुरी दशा है। अथवा प्रश्नोत्ता के रूपमें दिया जाना चाहिए साथ पंक्तियोंका मात्र अर्थ करके उन्हें वे पंक्तियां रटने को में जल्दी समममें आनेवाले अनेक उदाहरण भी, कहा जाता है। न्याय विपय एक तो वैसे ही रूखा जो आम तौर पर प्रसिद्ध हों, देना चाहिये। इससे है और फिर उसका शिक्षण भी रूखा हो तो कोमल छात्रोंको न्यायका पढ़ना अरुचिकर या भाररूप बुद्धि पत्रोंकी रुचि उसके अध्ययनमें कैसे हो सकती मालूम नहीं पड़ेगा- उसे वे रुचिके साथ पढ़ेंगे। है ? कोमल बुद्धि तो सहज-ग्राह्य चीजको बातचीत न्यायशास्त्रका शिक्षण वस्तुत: साहित्य सादिके के ढङ्गमें ग्रहण करना चाहती है। विद्वानोंका मत शिक्षणसे बिल्कुल जुदा है। उसके शिक्षकके लिये है कि प्रत्येक व्यक्तिकी बुद्धि में तर्क और उसको प्रतिदिनके पाठ्यविषय को पहले हृदय इम समझने की शक्ति रहती है और वह हर काम में उसका (परिभावित) करना और फिर पढ़ाना बड़ा उपयोग करता है। एक मजदरसे सवाल करिये कि आवश्यक है। ऐन मौके पर (उसी पढ़ाते समय) त मज दरी किस लिये करता है ? वह फौरन जवाब ही उसकी तैयारी नहीं होना चाहिये। ग्रन्थके