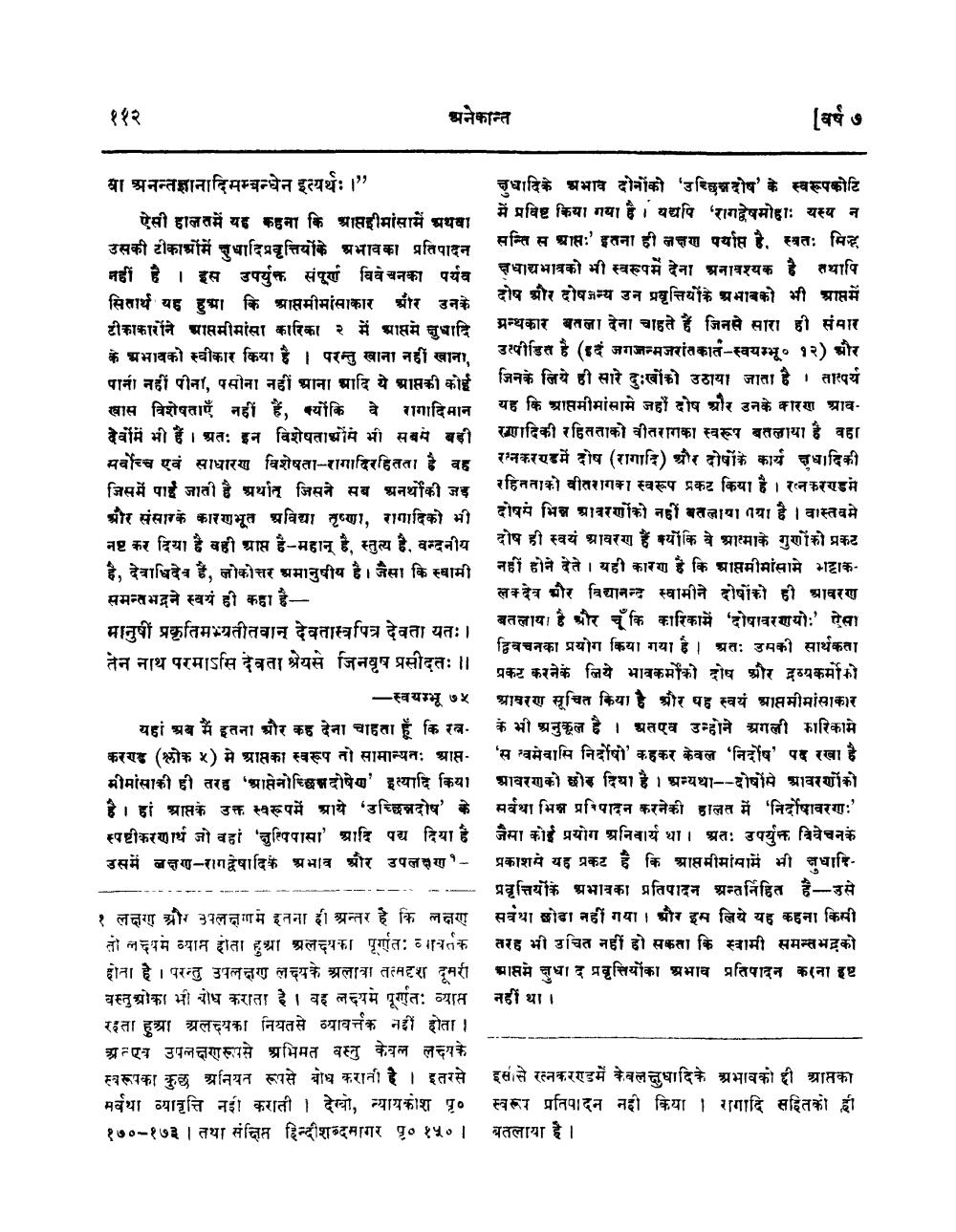________________
अनेकान्त
[वर्ष ७
या अनन्तज्ञानादिमम्बन्धेन इत्यर्थः।"
क्षुधादिके प्रभाव दोनोंको 'उरिछन्नदोष' के स्वरूपकोटि ऐसी हालतमें यह कहना कि प्राप्तडीमांसामें अथवा
में प्रविष्ट किया गया है। यद्यपि 'रागद्वेषमोहाः यस्य न उसकी टीकाओंमें सुधादिप्रवृत्तियोंके प्रभावका प्रतिपादन
सन्ति स प्रातः' इतना ही लक्षण पर्याप्त है. स्वत: मिट्ट नहीं है । इस उपर्युक्त संपूर्ण विवेचनका पर्यव
क्षधाद्यभावको भी स्वरूप में देना अनावश्यक है तथापि सितार्थ यह हुआ कि प्राप्तमीमांसाकार और उनके द
दोष और दोषजन्य उन प्रवृत्तियों के प्रभावको भी प्राप्तमें टीकाकारोंने प्राप्तमीमांसा कारिका २ में प्राप्तमे क्षुधादि
ग्रन्थकार बतला देना चाहते हैं जिनसे सारा ही संसार के अभावको स्वीकार किया है । परन्तु खाना नहीं खाना,
उत्पीडित है (इदं जगजन्मजरांतकात-स्वयम्भू. १२) और पानी नहीं पीना, सोना नहीं माना प्रादि ये प्राप्तकी कोई जिनके लिये ही सारे दुःखोंको उठाया जाता है । तात्पर्य खास विशेषताएँ नहीं हैं, क्योंकि वे रागादिमान यह कि प्राप्तमीमांसामे जहाँ दोष और उनके कारण श्रावदेवों में भी हैं। अतः इन विशेषताओंमें भी सबसे बड़ी रणादिकी रहितताको वीतरागका स्वरूप बतलाया है वहा सर्वोच्च एवं साधारण विशेषता-रागादिरहितता है वह रत्नकरण्डमें दोष (रागादि) और दोषोंके कार्य वृधादिकी जिसमें पाई जाती है अर्थात् जिसने सब अनर्थोंकी जड़ रहिनताको वीतरागका स्वरूप प्रकट किया है। रनकरण्डम और संसारके कारणभूत अविद्या तृष्णा, रागादिको भी
दोषमं भिन्न प्रावरणोंको नहीं बतलाया गया है। वास्तवमे नष्ट कर दिया है वही प्राप्त है-महान् है, स्तुत्य है. वन्दनीय
दोष ही स्वयं प्रावरण हैं क्योंकि वे प्रात्माके गुणों को प्रकट है, देवाधिदेव हैं, लोकोत्तर अमानुषीय है। जैसा कि स्वामी नहीं होने देते । यही कारण है कि प्राप्तमीमांसामे भाट्टाकसमन्तभद्र ने स्वयं ही कहा है
लकदेव और विद्यानन्द स्वामीने दोषोंको ही आवरण मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान देवतास्वपित्र देवता यतः।
बतलाया है और चूंकि कारिकामें 'दोषावरणयोः' ऐसा
द्विवचनका प्रयोग किया गया है। अत: उसकी सार्थकता तेन नाथ परमाऽसि देवता श्रेयसे जिनवृष प्रसीदतः ॥
प्रकट करनेके लिये भावकों को दोष और द्रव्यकर्मोको
-स्वयम्भू ७५ प्रावरण सूचित किया है और यह स्वयं प्राप्तमीमांसाकार यहां अब मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि स्व. के भी अनुकूल है । श्रतएव उन्होने अगली कारिकामे करण्ड (श्लोक ५) मे प्राप्तका स्वरूप तो सामान्यतः श्राप्त- 'स त्वमेवामि निर्दोषों' कहकर केवल 'निर्दोष' पद रखा है मीमांसाकी ही तरह 'प्राप्तेनोच्छिन्नदोषेण' इत्यादि किया आवरणको छोड़ दिया है। अन्यथा--दोषोंसे प्रावरणोंको है। हां प्राप्तके उक्त स्वरूपमें आये 'उच्छिन्नदोष' के सर्वथा भिन्न प्रपिपादन करनेकी हालत में 'निर्दोषावरण:' स्पष्टीकरणार्थ जो वहां 'क्षुत्पिपासा' आदि पद्य दिया है जैसा कोई प्रयोग अनिवार्य था। अत: उपर्युक्त विवेचन उसमें बक्षण-रागद्वेषादिक प्रभाव और उपलक्षण'- प्रकाशमे यह प्रकट है कि प्राप्तमीमांसा भी धारि
.--...-...-- प्रवृत्तियोंके प्रभावका प्रतिपादन अन्तर्निहित है-उसे १ लक्षण और उपलक्षण में इतना ही अन्तर है कि लक्षण सर्वथा छोढा नहीं गया। और इस लिये यह कहना किसी तो लक्ष्य में व्याम होता हुश्रा अलक्ष्यका पूर्णत: गावर्तक तरह भी उचित नहीं हो सकता कि स्वामी समन्तभद्रको होता है । परन्तु उपलक्षण लक्ष्य के अलावा तत्सदृश दूमरी प्राप्तमे क्षुधा द प्रवृत्तियोंका अभाव प्रतिपादन करना इष्ट वस्तुअोका भी बोध कराता है। वह लक्ष्यमे पूर्णत: व्याप्त नहीं था। रहता हुअा अलक्ष्यका नियतसे व्यावर्नक नहीं होता। अतएव उपलक्षणरूपसे अभिमत वस्तु केवल लक्ष्यके स्वरूपका कुछ अनियत रूपसे बोध कराती है । इतरसे इससे रत्नकरण्डमें केवलक्षुधादिके अभावको ही प्राप्तका मर्वथा व्यावृत्ति नही कराती । देखो, न्यायकोश पृ० स्वरूप प्रतिपादन नही किया । रागादि सहितको ही १७०-१७३ | तथा संक्षिप्त हिन्दीशब्दमागर पृ० १५०। बतलाया है।