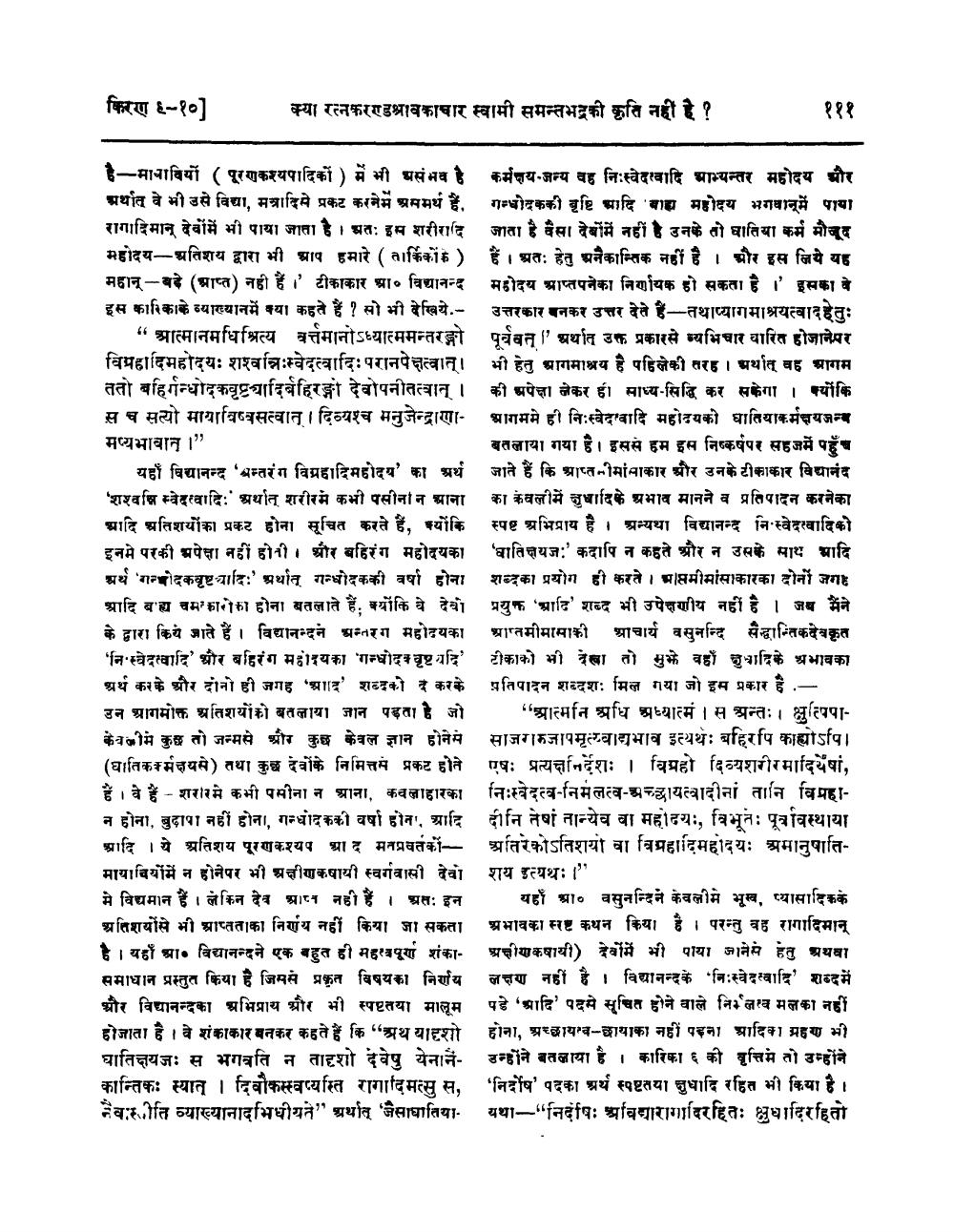________________
किरण ६-१०]
क्या रत्नकरण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है ?
१११
है-माजावियों (पूरणकश्यपादिकों) में भी असंभव है कर्मक्षय-जन्य वह निःस्वेदत्वादि भाभ्यन्तर महोदय और अर्थात वे भी उसे विद्या, मत्रादिसे प्रकट करने में असमर्थ हैं, गन्धोदककी दृष्टि प्रादि बाह्य महोदय भगवानमें पाया रागादिमान देवों में भी पाया जाता है। अत: इस शरीरादि जाता है वैसा देबों में नहीं है उनके तो घातिया कर्म मौजद महोदय-अतिशय द्वारा भी आप हमारे (तार्किकोंक) है। अत: हेतु अनेकान्तिक नहीं है । और इस लिये यह महान् -बड़े (माप्त) नही हैं।' टीकाकार प्रा. विद्यानन्द महोदय प्राप्तपनेका निर्णायक हो सकता है।' इसका वे इस कारिकाके व्याख्यानमें क्या कहते हैं ? सो भी देखिये.- उत्तरकार बनकर उत्तर देते हैं तथाप्यागमाश्रयत्वादहेतुः
"आत्मानमधिश्रित्य वर्तमानोऽध्यात्ममन्तरङ्गो पूर्ववत' अर्थात उक्त प्रकारसे व्यभिचार बारित होजानेपर विग्रहादिमहोदयः शश्वनिःस्वेदत्वादिःपरानपेक्षत्वात्। भी हेतु भागमाश्रय है पहिलेकी तरह । अर्थात् वह भागम ततो बहिर्गन्धोदकवृष्ट्यादिर्बहिरङ्गो देवोपनीतत्वात् । की अपेक्षा लेकर ही साध्य-सिद्धि कर सकेगा । क्योंकि स च सत्यो मायाविष्वसत्वात् । दिव्यश्च मनुजेन्द्राणा- भागममे ही निःस्वेदावादि महोदयको धातियाकर्मक्षयजन्य मध्यभावान।"
बतलाया गया है। इससे हम इस निष्कर्षपर सहज पहुँच यहाँ विद्यानन्द 'अन्तरंग विग्रहादिमहोदय' का अर्थ जाते हैं कि प्राप्तीमांसाकार और उनके टीकाकार विद्यानंद 'शश्वनि स्वेदस्वादिः' अर्थात् शरीरमे कभी पसीना न आना का केवलीमें जुधादिके प्रभाव मानने व प्रतिपादन करनेका प्रादि अतिशयोंका प्रकट होना सूचित करते हैं, क्योंकि स्पष्ट अभिप्राय है । अन्यथा विद्यानन्द निस्वेदस्वादिको इनमे परकी अपेक्षा नहीं होती। और बहिरंग महोदयका 'पातिक्षयज:' कदापि न कहते और न उसके माय भादि अर्थ 'गन्धोदकवृष्टयादिः' अर्थात् गन्धोदककी वर्षा होना शब्दका प्रयोग ही करते । माप्तमीमांसाकारका दोनों जगह श्रादि ब'ह्य चमकारोका होना बतलाते हैं, क्योंकि वे देवी प्रयुक 'श्रादि' शब्द भी उपेक्षणीय नहीं है । जब मैंने के द्वारा किये जाते हैं। विद्यानन्दन अन्तरग महोदयका प्राप्तमीमामाकी प्राचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकदेवकृत 'नि:स्वेदत्वादि' और बहिरंग महोदयका गन्धोदकवृष्ट यदि' टीकाको भी देखा तो मुझे वहाँ धादिके अभावका अर्थ करके और दोनो ही जगह 'प्राद' शब्दको द करके प्रतिपादन शब्दश: मिल गया जो इस प्रकार है :उन भागमोक्त अतिशयों को बतलाया जान पड़ता है जो "अात्मनि अधि अध्यात्मं । स अन्तः । क्षुत्पिपाकेवळीमे कुछ तो जन्मसे और कुछ केवल ज्ञान होनेसे साजगाजापमृत्यवाद्यभाव इत्यर्थः बहिरपि काह्योऽपि। (घातिकर्मक्षयसे) तथा कुछ देवोंके निमित्तम प्रकट होते एषः प्रत्यक्षनिर्देशः । विग्रहो दिव्यशरीरमादियषां, हैं । वे हैं - शरारमे कभी पसीना न श्राना, कवलाहारका निःस्वेदत्व-निमलत्व-अच्छायत्वादीनां तानि विमहान होना, बुढ़ापा नहीं होना, गन्धोदककी वर्षा होना, आदि दीनि तेषां नान्येव वा महोदयः, विभूत
विस्थाया श्रादि । ये अतिशय पूरणकश्यप श्राद मतप्रवर्तकों- अतिरकोऽतिशयो वा विग्रहादिमहोदयः अमानुपातिमायाचियों में न होनेपर भी अक्षीणकषायी स्वर्गवासी देवा शय इत्यथः।" मे विद्यमान हैं। लेकिन देव प्राप्त नही हैं । अत: इन यहाँ प्रा. वसुनन्दिने केवलीमे भूख, प्यासादिकके अतिशयोंसे भी प्राप्तताका निर्णय नहीं किया जा सकता अभावका मट कथन किया है । परन्तु वह रागादिमान् है। यहाँ प्रा. विद्यानन्दने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शंका- अक्षीणकषायी) देवों में भी पाया जाने से हंतु अथवा समाधान प्रस्तुत किया है जिमसे प्रकृत विषयका निर्णय लक्षण नहीं है । विद्यानन्दके नि:स्वेदस्वादि' शब्द में और विद्यानन्दका अभिप्राय और भी स्पष्टतया मालूम पडे 'श्रादि' पदमे सूचित होने वाले निलव मलका नहीं होजाता है। वे शंकाकार बनकर कहते हैं कि “अथ यादृशो होना, अच्छायाव-छायाका नहीं पड़ना आदिका ग्रहण भी घातिक्षयजः स भगवति न तादृशो देवेषु येनाने- उन्होंने बतलाया है । कारिका ६ की वृत्तिमं तो उन्होंने कान्तिकः स्यात् । दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु स, 'निर्दोष' पदका अर्थ स्पष्टतया क्षुधादि रहित भी किया है। वारुतीति व्याख्यानादभिधीयते" अर्थात् 'जैसाघातिया- यथा-"निर्दोषः अविद्यारागादिरहितः क्षुधादिरहितो