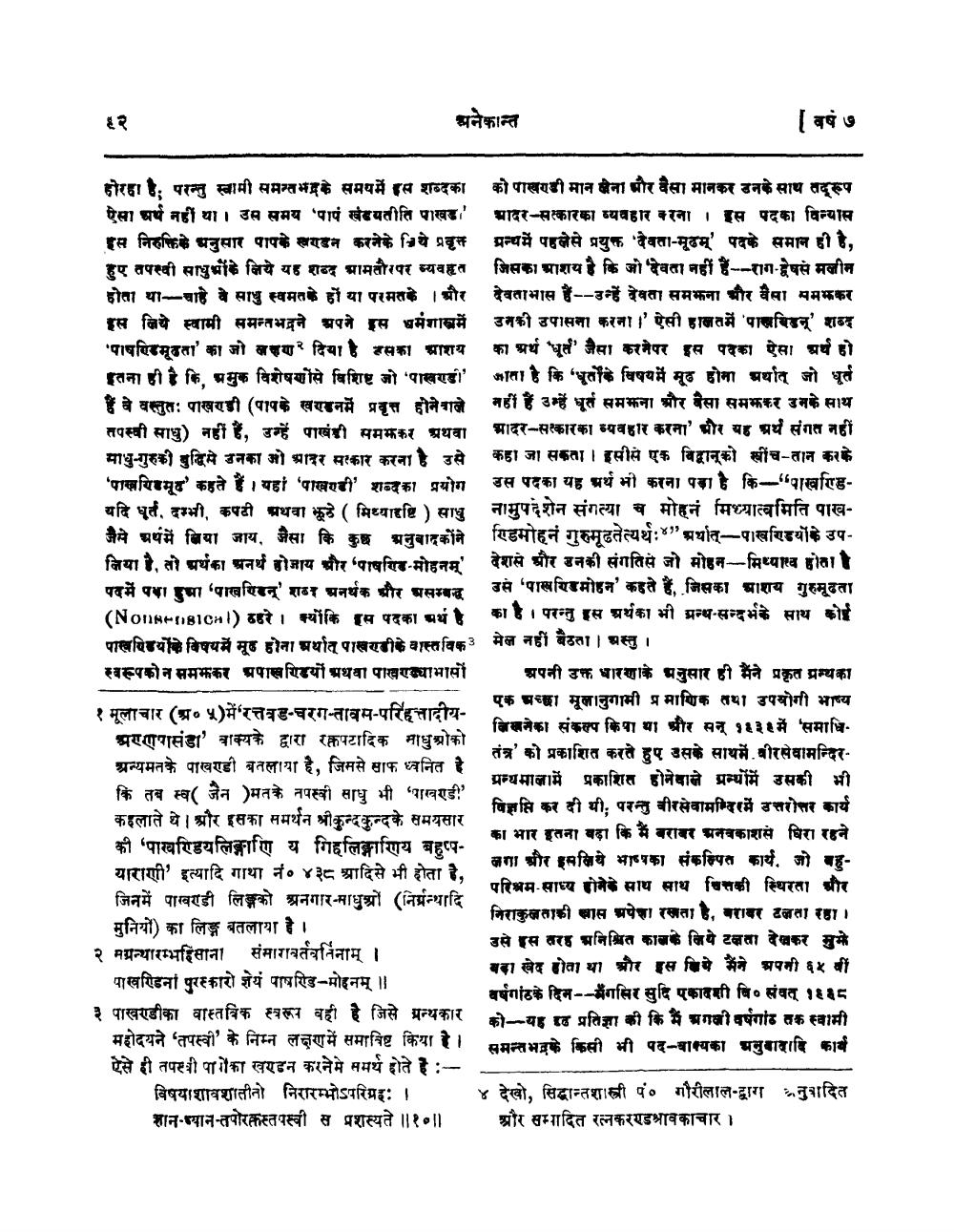________________
१२
अनेकान्त
[वर्ष ७
होरहा है। परन्तु स्वामी समन्तभद्रके समयमें इस शब्दका को पाखण्डी मान खेना और वैसा मानकर उनके साथ तद्रूप ऐसा अर्थ नहीं था। उस समय 'पापं खंब्यतीति पाखड भादर-सत्कारका व्यवहार करना । इस पदका विन्यास इस निरुक्ति के अनुसार पापके खण्डन करनेके शिये प्रवृत्त ग्रन्थ में पहलेसे प्रयुक्त देवता-मूढम्' पदके समान ही है, हुए तपस्वी साधुओंके लिये यह शब्द भामतौरपर व्यवहत जिसका प्राशय है कि जो देवतानहीं है--राग-द्वेषस मलीन होता था-चाहे वे साधु स्वमतके हों या परमतके । और देवताभास है--उन्हें देवता समझना और वैसा समझकर इस लिये स्वामी समन्तभद्रने अपने इस धर्मशास्त्रमें उनकी उपासना करना।' ऐसी हालतमें 'पाखविडन्' शब्द 'पापण्डिमूतता' का जो लक्षण दिया है उसका प्राशय का अर्थ 'धूत जैसा करमेपर इस पदका ऐसा अर्थ हो इतना ही कि.अमुक विशेषणोंसे विशिष्ट जो पाखण्डी' जाता है कि 'धूर्तीके विषय में मूढ होना अर्थात् जो धूर्त हैं वे वस्तुत: पाखण्डी (पापके खण्डनमें प्रवृत्त होनेगले महीं हैं उन्हें धूर्त समझना और बैसा समझकर उनके साथ तपस्वी साधु) नहीं हैं, उन्हें पाखंडी समझकर अथवा भादर-सत्कारका व्यवहार करना' और यह अर्थ संगत नहीं माधु-गुरुकी बुद्धिसे उनका जो श्रादर सरकार करना है उसे कहा जा सकता । इसीसे एक विद्वानको खींच-तान करके 'पाखपिसमूह' कहते हैं। यहां पाखण्डी' शब्द का प्रयोग उस पदका यह अर्थ भी करना पड़ा है कि-"पाखण्डियदि घृत, दम्भी, कपटी अथवा कुठे ( मिथ्याटि) साधु नामुपदेशेन संगत्या च मोहनं मिथ्यात्वमिति पाखजैसे अर्थ में लिया जाय, जैसा कि कुछ अनुवादकोंने एिडमोहन गुरुमढतेत्यर्थः४" अर्थात्-पाखण्डियोंके उपलिया, तो अर्थका अनर्थ होमाय और 'पाषगिड-मोहन' देशसे और उनकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्याव होता पद में पाया पाखन्'ि शब्न अनर्थक और असम्बद उसे 'पाखविडमोहन' कहते हैं, जिसका भाशय गुरुमूढता (NonSICHI) ठहरे। क्योंकि इस पदका अर्थ है का है । परन्तु इस अर्थका भी ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ कोई पाखविडयोंके विषय में मुहहोना अर्थात् पाखण्डीके वास्तविक मेल नहीं बैठता । अस्तु । स्वरूपको न समझकर अपाखण्डियों अथवा पाखरख्याभासों अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मैंने प्रकृत ग्रन्थका
एक अच्छा मूलानुगामी प्रमाणिक तथा उपयोगी भाष्य १ मूलाचार (4०५)में रत्तवड-चरग-तावम-परिहत्तादीय
लिखनेका संकल्प किया था और सन् ११३में 'समाधिअण्णासंडा' वाक्यके द्वारा रक्तपटादिक माधुरोको
तंत्र' को प्रकाशित करते हुए उसके साथ में वीरसेवामन्दिरअन्यमतके पाखण्डी बतलाया है, जिमसे साफ ध्वनित है
ग्रन्थमालामें प्रकाशित होनेवाले प्रन्योंमें उसकी भी कि तब स्व( जैन )मतके तपस्वी साधु भी 'पाखण्डी'
विज्ञप्ति कर दी थी, परन्तु वीरसेवामन्दिरमें उत्तरोत्तर कार्य कहलाते थे। और इसका समर्थन श्रीकुन्दकुन्दके समयसार
का भार इतना बढ़ा कि मैं बराबर अनवकाशसे घिरा रहने की 'पाखण्डियलिङ्गाणि य गिहलिङ्गारिणय बहुप्प
लगा और इसलिये भाष्पका संकल्पित कार्य, जो बहयाराणी' इत्यादि गाथा नं. ४३८ श्रादिसे भी होता है,
परिश्रम-साध्य होने के साथ साथ चित्तकी स्थिरता और जिनमें पाखण्डी लिङ्गको अनगार-माधुनों (निर्ग्रन्यादि
निराकुलताकी सास अपेक्षा रखता है, बराबर टलता रहा। मुनियों) का लिङ्ग बतलाया है।
उसे इस तरह अनिश्रित काल के लिये टलता देखकर मुझे २ मग्रन्यारम्भहिंसाना संमारावर्तवनिनाम् ।
बड़ा खेद होता था और इस लिये मैंने अपनी ६५ वीं पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पापण्डि-मोहनम् ॥
वर्षगांठके दिन--मंगसिर सुदि एकादशी वि० संवत् ११३ पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकार
को-यहढ प्रतिज्ञा की कि मैं अगली वर्षगांठ तक स्वामी महोदयने 'तपस्वी' के निम्न लक्षण में समाविष्ट किया है।
समन्तभद्रके किसी भी पद-बाल्यका अनुवादादि कार्य ऐसे ही तपस्थी पागेका खण्डन करनेमे समर्थ होते है:
विषयाशावशातीनो निरारम्भोऽपरिग्रहः । ४ देखो, सिद्धान्तशास्त्री पं० गौरीलाल-दाग नुवादित शान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ और समादित रत्नकरण्डश्रावकाचार ।