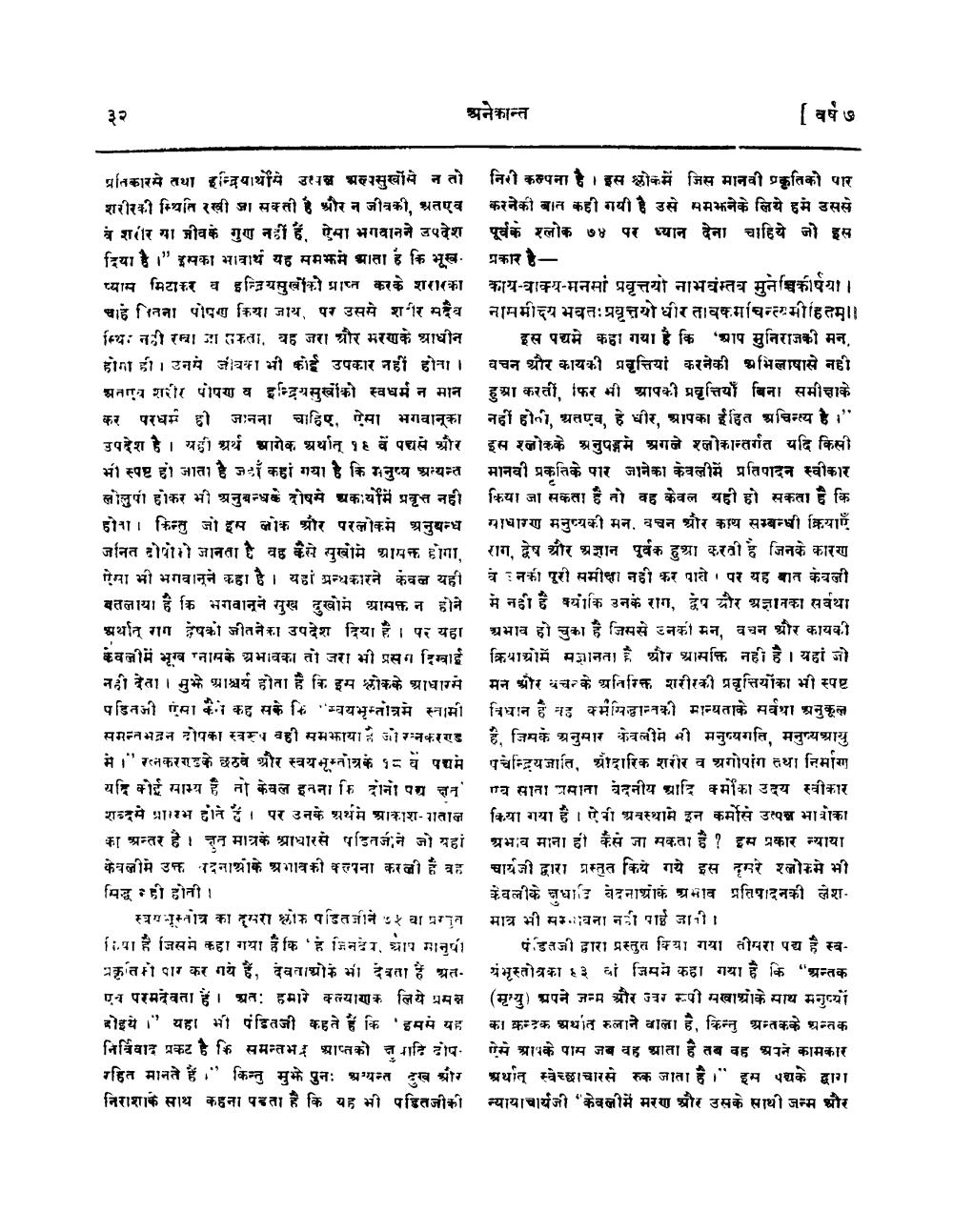________________
३२
अनेकान्त
प्रतिकार तथा इन्द्रियार्थयेउ सुखों मे न तो शरीरकी स्थिति रखी जा सकती है और न जीवकी, श्रतएव शरीर या जीवके गुण नहीं हैं ऐसा भगवानने उपदेश दिया है ।" इसका भावार्थ यह समझ मे आता है कि भूखप्यास मिटाकर व इन्द्रियसुखको प्राप्त करके शरारका चाईना पोषण किया जाय पर उससे शरीर सदैव स्थानीय जरा और मरयके आधीन होगा ही । उनमें जीवका भी कोई उपकार नहीं होना । अव शरीर पीपय व इन्द्रियमुखको स्वधर्म न मान कर परधर्म ही जानना चाहिए, ऐसा भगवान्का उपदेश है । यही अर्थ आगेक अर्थात् १६ वें पचले और भी स्पष्ट हो जाता है जहाँ कहां गया है कि मनुष्य अत्यन्त लोलुप होकर भी अनुबन्धके शेषमे अकायोंमें प्रवृत्त नही होना किन्तु जो इस लोक और परलोक अनुबन्ध जनित शेप जानता है वह कैसे होगा, सुखीमे श्रायक ऐसा भी भगवान कहा है। यहां प्रन्धकारने केवल यही बतलाया है कि भगवान सुख दुखोमं धाम न होने अर्थात् राग को जीतने उपदेश दिया है। पर यहा केवली में भूख नामके प्रभावका तो जरा भी प्रसग दिखाई नहीं देता। मुझे पार्य होता है कि इस लोकके आधार पंडितजी ऐसा कैसे कह सके कि "स्वयभृस्तोत्रमे स्वामी समन्तभद्रन दोपका स्वरूप वही समझाया है जो स्नकरण्ड मे।" रत्नकरण्डके उठने और स्वयम्ती में पथमं १८ यदि कोई साम्य है तो केवल इतना कि दोनों पक्ष शब्द मे प्रारम्भ होते हैं। पर उनके अर्थ मे श्राकाशगताल का अन्तर है। तुन मात्र के श्राधारसे पडितजी ने जो यहां केवली में उक्त वदनाशी के श्रभावकी कल्पना करती हैं वह सिद्धही होती।
का दूसरा पतीने २ किया है जिसमें कहा गया हैं कि 'हे जिनदेव, प मानुषी प्रकृति कर गये हैं, देवताओं भी देवता है अतः एव परमदेवता है। अतः हमारे कल्याणक लिये प्रपन्न होइये ।" यहां भी पंडितजी कहते हैं कि इससे यह निर्विवाद प्रकट है कि समन्तभाणको दि रहित मानते हैं" किन्तु मुके पुनः चम्पन्त दुख और निराशा के साथ कहना पडता है कि यह भी पंडितजीकी
[ वर्ष ७
निरी कल्पना है। इसमें मिस मानवी प्रकृतिको पार करने की बात कही गयी है उसे समझने के लिये हमें उससे पूर्वकं श्लोक ७४ पर ध्यान देना चाहिये जो इस प्रकार है
काय वाक्य मनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तव सुनचिकीर्षया । नाममीय भवतः प्रवृत्तयो घीर तावकमचिन्त्यमीहितम् ॥
इस पचमे कहा गया है कि आप मुनिराज की मन वचन और कार्यकी प्रवृत्तियां करनेकी अभिलाषासे नहीं हुआ करतीं, फिर भी आपकी प्रवृत्तियों बिना समीक्षा नहीं होती, सएव हे धीर, आपका ईडित थिय है।" इस श्लोक के अनुपमे अगले रोगंत यदि किसी मानवी प्रकृति के पार जानेका केवली में प्रतिपादन स्वीकार किया जा सकता है तो वह केवल यही हो सकता है कि साधारण मनुष्य की मन, वचन और काय सम्बन्धी क्रियाएँ राग, द्वेष और अज्ञान पूर्वक हुआ करती है जिनके कारण
उनकी पूरी समीक्षा नहीं कर पाये पर यह बात केवली मे नही है कि उनके राग, द्वेष और अज्ञानका सबंधा भाव हो चुका है जिससे उनकी मन, वचन और कायकी क्रियायोंमें मज्ञानता है और श्रासक्ति नहीं है। यहां जो मन और वचन के अतिरिक शरीरकी प्रवृत्तियोंका भी स्पष्ट विधान है कि मान्यतामा अनुकूल है, जिसके अनुसार केली मी मनुष्यगति, मनुष्यधायु पचेद्रियजात चारिक शरीर व गोपांग तथा निर्माण एव साता माता वेदनीय श्रादि कर्मोंका उदय स्वीकार किया गया है। ऐसी अवस्थामै इन कर्मोसे उत्पन्न भावीका श्रभाव माना ही कैसे जा सकता है ? इस प्रकार न्याया चार्यजी द्वारा प्रस्तुत किये गये इस दूसरे श्लोकमे भी केवीके के अभाव प्रतिपादनकीजेश मात्र भी सम्भावना नही पाई जाती।
पंडितजी द्वारा प्रस्तुत किया गया तीसरा पद्य है स्वस्तोत्रका ६३ व जिसमें कहा गया है कि " श्रन्तक (मृत्यु) अपने जन्म और अररूपी माधके साथ मनुष्यों का अर्थात् रुलाने वाला है, किन्तु श्रन्तकके श्रन्तक ऐसे आपके पास जब वह श्राता है तब वह अपने कामकार तारसे रुक जाता है इस पथके द्वाग वीमें मरण और उसके साथी जन्म और