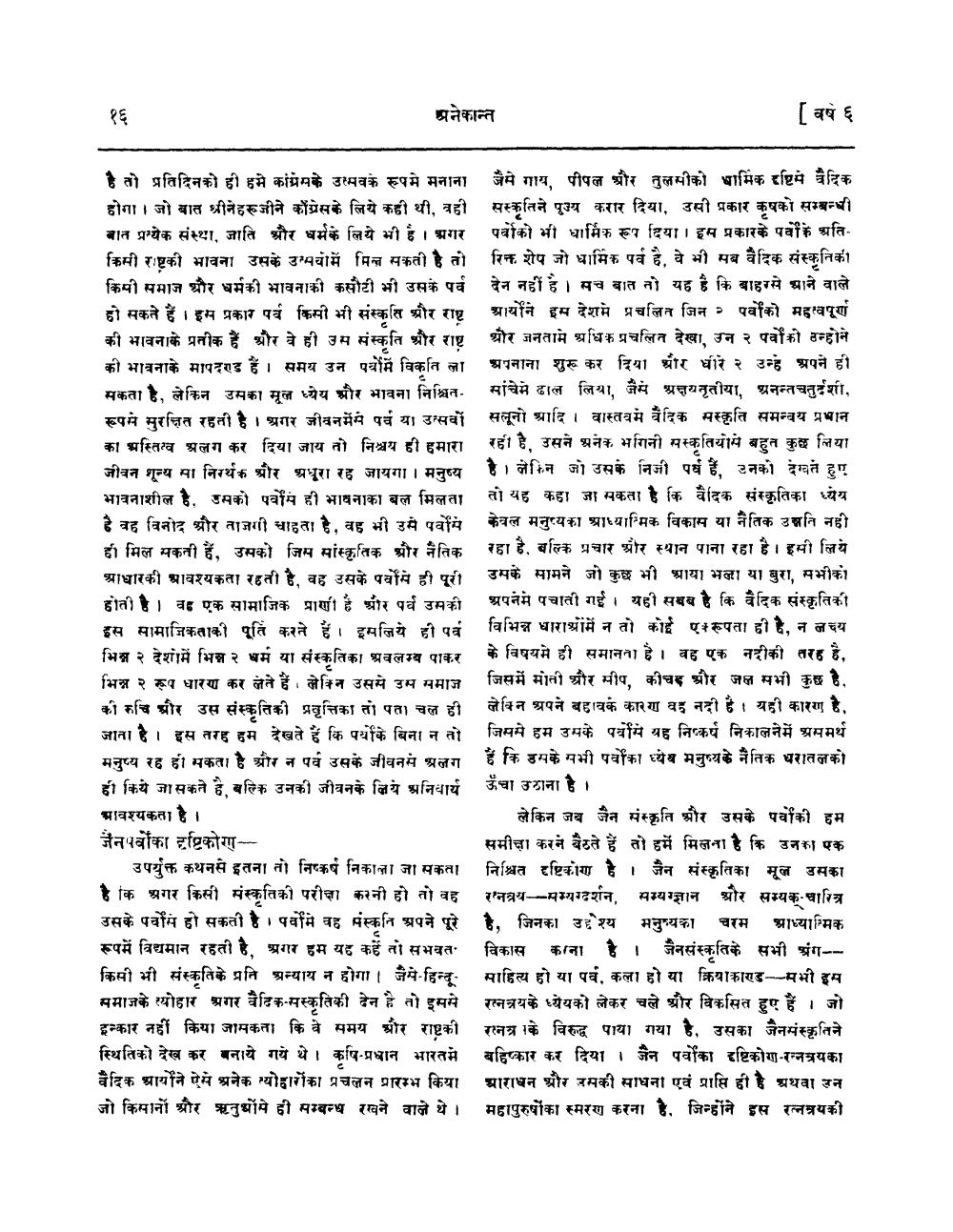________________
अनेकान्त
[वर्ष ६
है तो प्रतिदिनको ही हमे कांग्रेसके उत्मक रूपमे मनाना जैसे गाय, पीपल और तुलसीको धार्मिक दृष्टिमे वैदिक होगा। जो बात श्रीनेहरूजीने कोंग्रेसके लिये कही थी, वही सस्कृतिने पूज्य करार दिया, उसी प्रकार कृषको सम्बन्धी बात प्रत्येक संस्था, जाति और धर्मके लिये भी है । अगर पर्बोको भी धार्मिक रूप दिया। इस प्रकारके पोंके अति. किमी राष्टकी भावना उसके उन्मयों में मिल सकती है तो रिक्त शेप जो धार्मिक पर्व है, वे भी पब वैदिक संस्कृतिका किपी समाज और धर्मकी भावनाकी कसौटी भी उसके पर्व देन नहीं है। सच बात तो यह है कि बाहरसे पाने वाले हो सकते हैं । इस प्रकार पर्व किसी भी संस्कृति और राष्ट्र प्राोंने इस देशमे प्रचलित जिन • पर्वोको महत्वपूर्ण की भावनाके प्रतीक हैं और वे ही उस संस्कृति और राष्ट और जनतामे अधिक प्रचलित देखा, उन २ पर्वो को उन्होने की भावनाके मापदण्ड हैं। समय उन पोंमें विकति ला अपनाना शुरू कर दिया और धीर २ उन्हें अपने ही सकता है, लेकिन उसका मूल ध्येय और भावना निश्चित. मांचेमे ढाल लिया, जैसे अक्षय तृतीया, अनन्तचतुर्दशी, रूपसे सुरक्षित रहती है। अगर जीवन में पर्व या उत्सवों सलूनो श्रादि । वास्तव में वैदिक संस्कृति समन्वय प्रधान का अस्तित्व अलग कर दिया जाय तो निश्चय ही हमारा रही है, उसने अनेक भगिनी संस्कृतियोमे बहुत कुछ लिया जीवन शून्य मा निरर्थक और अधूरा रह जायगा। मनुष्य है। लेकिन जो उसके निजी पर्व हैं, उनको दम्यते हुए भावनाशील है. उसको पर्वोम ही भावनाका बल मिलता तो यह कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृतिका ध्येय है वह विनोद और ताजगी चाहता है, वह भी उसे पर्वो केवल मनुष्यका प्राध्यामिक विकास या नैतिक उमति नही ही मिल सकती हैं, उसको जिम सांस्कृतिक और नैतिक रहा है, बल्कि प्रचार और स्थान पाना रहा है। इसी लिये आधारकी श्रावश्यकता रहती है. वह उसके पास ही पूरी उपके सामने जो कुछ भी पाया भला या बुरा, सभीको होती है। वह एक सामाजिक प्राणी है और पर्व उपकी अपनेमे पचाती गई। यही सबब है कि वैदिक संस्कृतिकी इस सामाजिकताको प्रति करते है। इसलिये ही पर्व विभिन्न धाराओं में न तो कोई एकरूपता ही है. न ल च्य भिन्न देशों में भिन्न २ धर्म या संस्कतिका अवलम्ब पाकर के विषयमे ही समानता है। वह एक नदीकी तरह है, भिन्न २ रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन उससे उस समाज जिसमें मोती और मीप, कीचड़ और जल सभी कुछ है की रुचि और उस संस्कृतिकी प्रवृत्तिका तो पता चल ही लेकिन अपने बहावकं कारण वह नदी है। यही कारण है, जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि पोंके बिना न तो जिसमे हम उपके पर्वो यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ मनुष्य रह ही सकता है और न पर्व उसके जीवन से अलग है कि उसके सभी पर्वोका ध्येय मनुष्य के नैतिक धरातलको ही किये जा सकते है. बल्कि उनकी जीवनके लिये अनिवार्य ऊँचा उठाना है। आवश्यकता है।
लेकिन जब जैन संस्कृति और उसके पर्वोकी हम जैनपोंका दृष्टिकोण
समीक्षा करने बैठते हैं तो हमें मिलना है कि उनका एक __उपर्युक्त कथनसे इतना तो निष्कर्ष निकाला जा सकता निश्चित दृष्टिकोण है । जैन संस्कृतिका मूल उसका है कि अगर किसी संस्कृतिकी परीक्षा करनी हो तो वह स्नत्रय-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक-चारित्र उसके पास हो सकती है। पर्वोमे वह संस्कान अपने पूरे है, जिनका उद्देश्य मनुष्यका चरम आध्यात्मिक रूपमें विद्यमान रहती है, अगर हम यह कहें तो सभवतः विकास काना है। जैनसंस्कतिके सभी अंग-- किसी भी संस्कृतिके प्रति अन्याय न होगा। जैसे-हिन्द- साहित्य हो या पर्व, कला हो या क्रियाकाण्ड-सभी इस समाजके त्योहार अगर वैदिक-सस्कृतिकी देन है तो इससे रत्नत्रयके ध्येयको लेकर चले और विकसित हुए हैं । जो इन्कार नहीं किया जामकता कि वे समय और राष्ट्रकी रत्नत्र के विरुद्ध पाया गया है, उसका जैनसंस्कृतिने स्थितिको देख कर बनाये गये थे। कृषि प्रधान भारतमे बहिष्कार कर दिया । जैन पर्वोका दृष्टिकोण-रन्नत्रयका वैदिक पार्योंने ऐसे अनेक त्योहारोंका प्रचलन प्रारम्भ किया पाराधन और उसकी साधना एवं प्राप्ति ही है अथवा उन जो किसानों और ऋतुभोंसे ही सम्बन्ध रखने वाले थे। महापुरुषों का स्मरण करना है, जिन्होंने इस रत्नत्रयकी