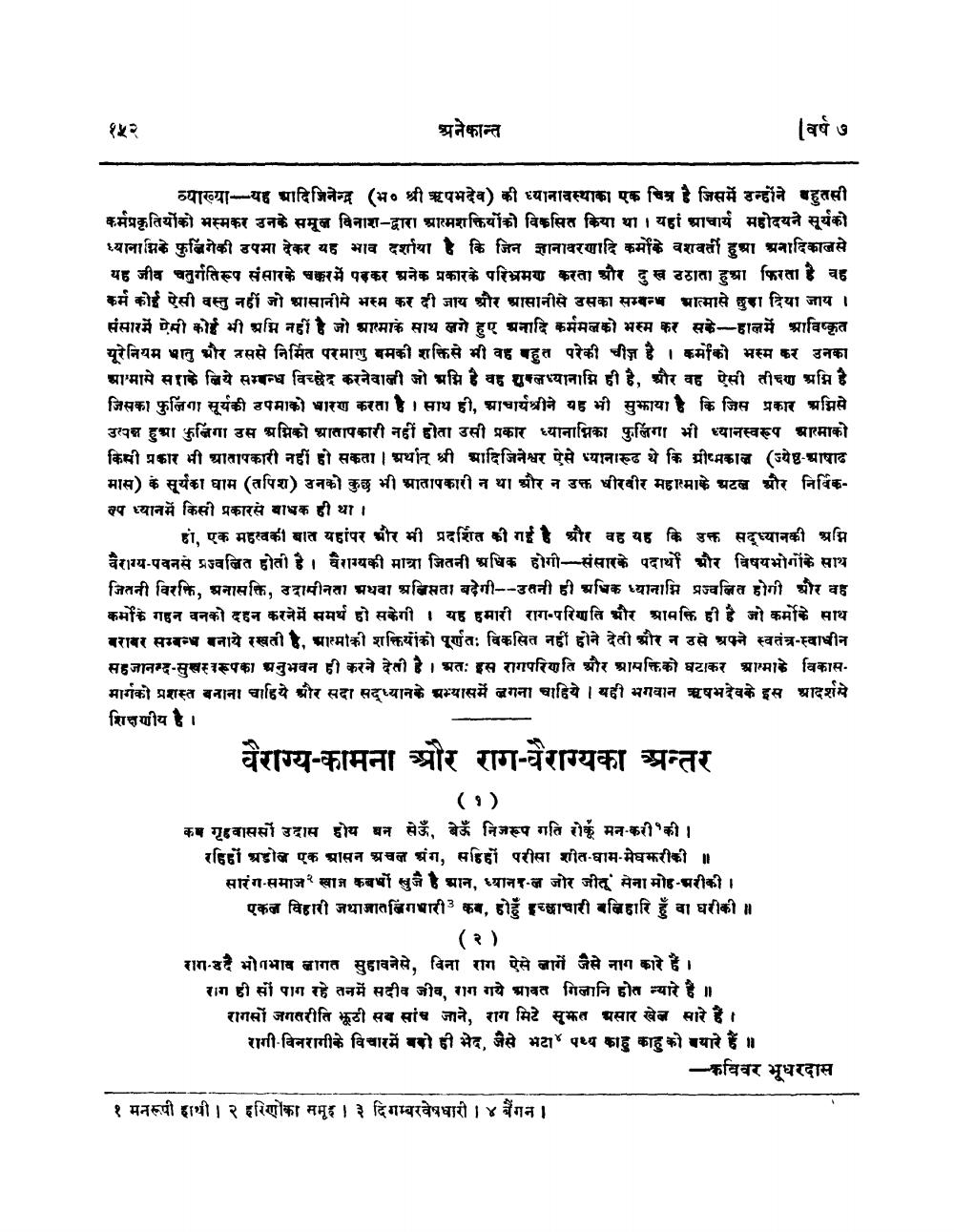________________
अनेकान्त
वर्ष ७
व्याख्या-यह प्रादिजिनेन्द्र (भ. श्री ऋषभदेव) की ध्यानावस्थाका एक चित्र है जिसमें उन्होंने बहुतसी कर्मप्रकृतियोंको भस्मकर उनके समूल विनाश-द्वारा प्रारमशक्तियों को विकसित किया था। यहां प्राचार्य महोदयने सूर्यको ध्यानामिके फुलिंगेकी उपमा देकर यह भाव दर्शाया है कि जिन ज्ञानावरणादि कर्मों के वशवर्ती हुआ अनादिकालसे यह जीव चतुर्गतिरूप संसारके चक्कर में पड़कर अनेक प्रकारके परिभ्रमण करता और दुख उठाता हुश्रा फिरताहे वह कर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं जो श्रासानीमे भस्म कर दी जाय और प्रासानीसे उसका सम्बन्ध भात्मासे छुड़ा दिया जाय । संसारमें ऐसी कोई भी अग्नि नहीं है जो प्रात्माके साथ लगे हुए अनादि कर्ममलको भस्म कर सके-हाल में आविष्कृत यूरेनियम धातु और उससे निर्मित परमाणु बमकी शक्तिसे भी वह बहुत परेकी चीज़ है । कर्माको भस्म कर उनका
आमासे सके लिये सम्बन्ध विच्छेद करनेवाली जो भग्नि है वह शुक्लध्यानाग्नि ही है, और वह ऐसी तीक्ष्ण अग्नि है जिसका फुलिंगा सूर्यकी उपमाको धारण करता है। साथ ही, प्राचार्यश्रीने यह भी सुझाया है कि जिस प्रकार अग्निसे उत्पन्न हुआ कुलिंगा उस अग्निको प्रातापकारी नहीं होता उसी प्रकार ध्यानाग्निका फुलिंगा भी ध्यानस्वरूप प्रारमाको किसी प्रकार भी श्रातापकारी नहीं हो सकता | अर्थात् श्री आदिजिनेश्वर ऐसे ध्यानारूढ थे कि ग्रीष्मकाल (ज्येष्ट-प्राषाढ मास) के सूर्यका घाम (तपिश) उनको कुछ भी आतापकारी न था और न उक्त धीरवीर महात्माके अटल और निर्विकरूप ध्यानमें किसी प्रकारसे वाधक ही था।
हो, एक महत्वकी बात यहांपर और भी प्रदर्शित की गई है और वह यह कि उक्त सद्ध्यानकी अग्नि वैराग्य-पवनसे प्रज्वलित होती है। वैराग्यकी मात्रा जितनी अधिक होगी-संसारके पदार्थों और विषयभोगोंके साथ जितनी विरक्ति, अनासक्ति, उदासीनता अथवा अलिप्तता बढ़ेगी--उतनी ही अधिक ध्यानानि प्रज्वलित होगी और वह कर्मोंके गहन वनको दहन करने में समर्थ हो सकेगी । यह हमारी राग-परिणति और आसक्ति ही है जो कर्मोके साथ बराबर सम्बन्ध बनाये रखती है, मात्माकी शक्तियोंको पूर्णत: विकसित नहीं होने देती और न उसे अपने स्वतंत्र-स्वाधीन सहजानन्द-सुखस्वरूपका अनुभवन ही करने देती। अत: इस रागपरियाति और श्रापक्तिको घटाकर आत्माके विकास. मार्गको प्रशस्त बनाना चाहिये और सदा सद्ध्यानके अभ्यासमें बगना चाहिये । यही भगवान ऋषभदेवके इस आदर्शमे शिक्षणीय है।
वैराग्य-कामना और राग-वैराग्यका अन्तर
कर गृहवाससों उदास होय धन सेऊँ, बेऊँ निजरूप गति रोक मन-करी की। रहिहों अडोल एक प्रासन अचल अंग, सहिहों परीसा शीत-धाम-मेघमरीकी ॥ सारंग-समाज खान कबर्षों खुजै है मान, ध्याना-ल जोर जीतू सेना मोह-परीकी।
एकल विहारी जथाजातलिंगधारी कब, होहुँ इच्छाचारी बलिहारि हुँ वा घरीकी।
गग-उदै भोगभाव लागत सुहावनेसे, विना राग ऐसे लागें जैसे नाग कारे हैं। राग ही सी पाग रहे तनमें सदीव जीव, गग गये पावत गिलानि होत न्यारे है॥ रागसों जगतरीति झूठी सब सांच जाने, राग मिटे सूझत असार खेज सारे है। रागी-विनरागीके विचारमें बदो ही भेद, जैसे भटा पथ्य काहु काहु को ग्यारे हैं।
कविवर भूधरदास
१ मनरूपी हाथी। २ हरिणोंका ममूह | ३ दिगम्बरवेषधारी। ४ बैंगन ।