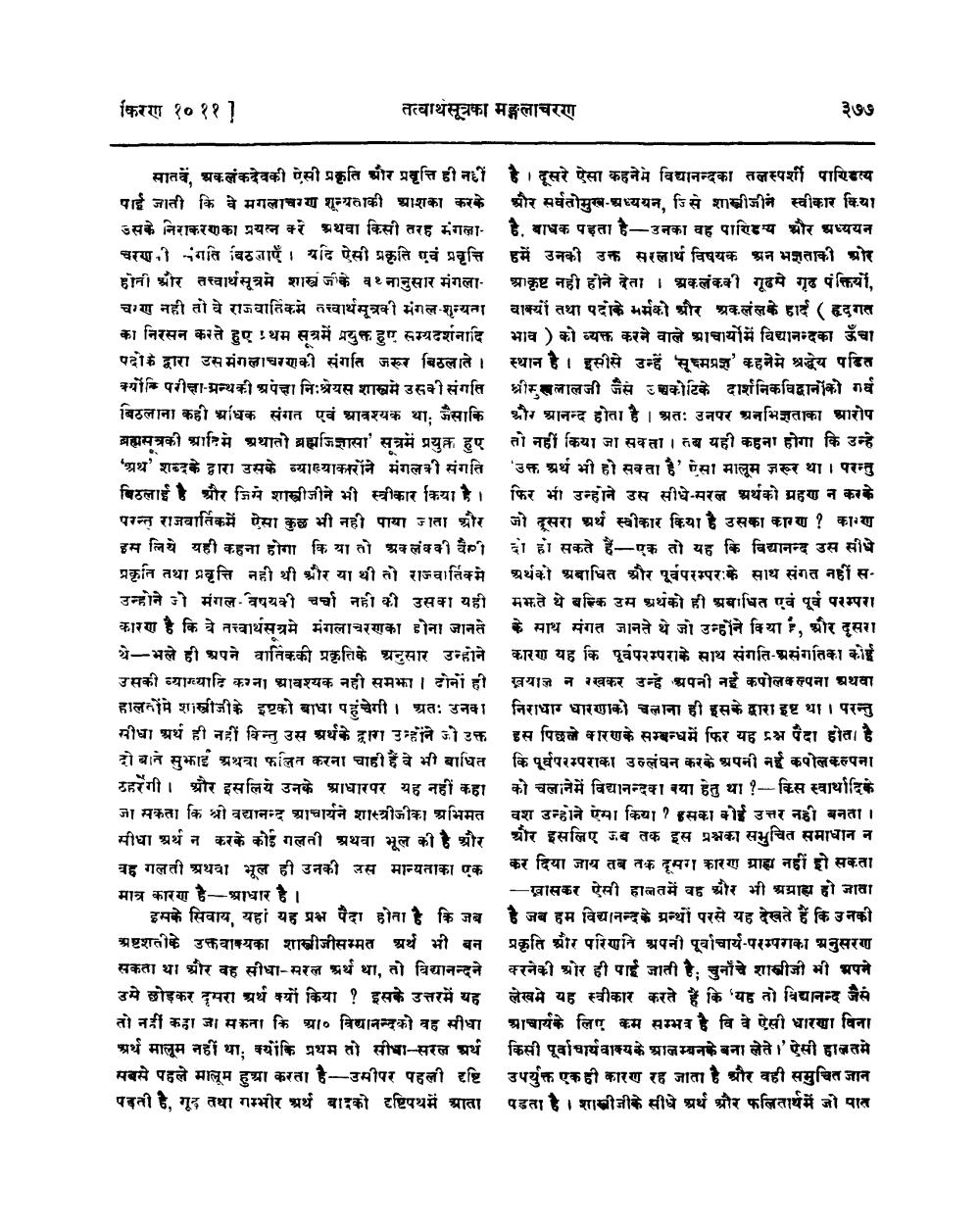________________
किरण १०११]
तत्वार्थसूत्रका मङ्गलाचरण
३७७
सातवें, अकलंकदेवकी ऐसी प्रकृति और प्रवृत्ति ही नहीं है। दूसरे ऐसा कहनेमे विद्यानन्दका तलस्पर्शी पाण्डित्य पाई जाती कि वे मगलाचरण शून्यताकी श्राशका करके और सर्वतोमुख-अध्ययन, जिसे शास्त्रीजीने स्वीकार किया उसके निराकरणका प्रयत्न करे अथवा किसी तरह मंगला- है. बाधक पड़ता है-उनका वह पाण्डिन्य और अध्ययन चरणी गति बिठ जाएँ। यदि ऐसी प्रकृति एवं प्रवृत्ति हमें उनकी उक्त सरलार्थ विषयक अन भज्ञताकी ओर होती और तत्वार्थसूत्रमे शास्त्रं जीके व नानुसार मंगला- अाकृष्ट नहीं होने देता । अकलंककी गूढमे गृढ पंक्तियों, चरण नही तो वे राजवार्तिकमे तत्वार्थमूत्रकी मंगल-शून्यता वाक्यों तथा पदोके मर्मको और अकलंलके हार्द (हृदगत का निरसन करते हुए 'थम सूत्रमें प्रयुक्त हुए सम्प्रदर्शनादि भाव ) को व्यक्त करने वाले श्राचार्यो में विद्यानन्दका ऊँचा पदोके द्वारा उस मंगलाचरणकी संगति जरूर बिठलाते। स्थान है। इसीसे उन्हें 'सूक्ष्मप्रज्ञ' कहनेमे श्रद्धेय पडित क्योंकि परीक्षा-ग्रन्थकी अपेक्षा निःश्रेयस शास्त्रमे उसकी संगति श्रीमुखलालजी जैसे उच्चकोटिके दार्शनिकविद्वानोंको गर्व बिठलाना कही अधिक संगत एवं श्रावश्यक था; जैसाकि और प्रानन्द होता है। अत: उनपर अनभिज्ञताका आरोप ब्रह्मसत्रकी प्रातिमे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा सत्रमें प्रयुक्त हुए तो नहीं किया जा सकता । तब यही कहना होगा कि उन्हें 'अथ' शब्दके द्वारा उसके व्याख्याकारोंने मंगलकी संगति 'उक्त अर्थ भी हो सकता है। ऐसा मालूम जरूर था। परन्तु बिठलाई है और जिसे शास्त्रीजीने भी स्वीकार किया है। फिर भी उन्होंने उस सीधे-सरल अर्थको ग्रहण न करके परन्त राजवार्तिकमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता और जो दूसरा अर्थ स्वीकार किया है उसका कारण ? कारण इस लिये यही कहना होगा कि या तो अकलंककी वैली दो हो सकते हैं-एक तो यह कि विद्यानन्द उस सीधे प्रकृति तथा प्रवृत्ति नही थी और या थी तो राजवार्तिकमे अर्थको अबाधित और पूर्वपरम्पर के साथ संगत नहीं स. उन्होने जो मंगल वषयकी चर्चा नहीं की उसका यही मझते थे बल्कि उस प्रथको ही अबाधित एवं पूर्व परम्परा कारण है कि वे तत्त्वार्थसग्रमे मंगलाचरणका होना जानते के साथ संगत जानते थे जो उन्होंने विया, और दूसरा थे-भले ही अपने वार्तिककी प्रकृति के अनुसार उन्होने कारण यह कि पूर्वपरम्पराके साथ संगति-प्रसंगतिका कोई उसकी व्याख्यादि करना प्रावश्यक नही समझा। दोनों ही खयाज न रखकर उन्हें अपनी नई कपोलकल्पना अथवा हाललोंमे शास्त्रीजीके इष्टको बाधा पहुंचेगी। अत: उनका निराधार धारणाको चलाना ही इसके द्वारा इष्ट था। परन्तु सीधा अर्थ ही नहीं विन्तु उस अर्थके द्वारा उन्होंने जो उक्त इस पिछले कारण के सम्बन्धमें फिर यह प्रश्न पैदा होता है दो बाने सुझाई अथवा फलित करना चाही हैं वे भी बाधित कि पूर्वपरम्पराका उल्लंघन करके अपनी नई कपोलकल्पना ठहरेगी। और इसलिये उनके आधारपर यह नहीं कहा को चलानेमें विद्यानन्दका क्या हेतु था ?--किस स्वार्थादिके जा सकता कि श्री वद्यानन्द प्राचार्यने शास्त्रीजीका अभिमत वश उन्होंने ऐसा किया इसका कोई उत्तर नहीं बनता। सीधा अर्थ न करके कोई गलती अथवा भूल की है और और इसलिए जब तक इस प्रश्नका समुचित समाधान न वह गलती अथवा भूल ही उनकी उस मान्यताका एक कर दिया जाय तब तक दूसग कारण ग्राह्य नहीं हो सकता मात्र कारण है-श्राधार है।
-खासकर ऐसी हालतमें वह और भी अग्राह्य हो जाता इसके सिवाय, यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि जब है जब हम विद्यानन्दके ग्रन्थों परसे यह देखते हैं कि उनकी अष्टशतीके उक्तवाक्यका शास्त्रीजीसम्मत अर्थ भी बन प्रकृति और परिणति अपनी पूर्वाचार्य-परम्पगका अनुसरण सकता था और वह सीधा-सरल अर्थ था, तो विद्यानन्दने करनेकी ओर ही पाई जाती है। चुनाँचे शास्त्रीजी भी अपने उसे छोड़कर दूसरा अर्थ क्यों किया ? इसके उत्तरमें यह लेखमे यह स्वीकार करते हैं कि 'यह तो विद्यानन्द जैसे तो नहीं कहा जा सकता कि प्रा. विद्यानन्दको वह सीधा प्राचार्यके लिए कम सम्भव है वि वे ऐसी धारणा विना अर्थ मालूम नहीं था, क्योंकि प्रथम तो सीधा-सरल अर्थ किसी पूर्वाधार्यवाक्य के पालम्बनके बना लेते।' ऐसी हालतमे सबसे पहले मालूम हुआ करता है-उसीपर पहली दृष्टि उपर्युक्त एकही कारण रह जाता है और वही समुचित जान पड़ती है, गूढ तथा गम्भीर अर्थ बादको दृष्टिपथमें आता पडता है। शास्त्रीजीके सीधे अर्थ और फलितार्थमें जो पात