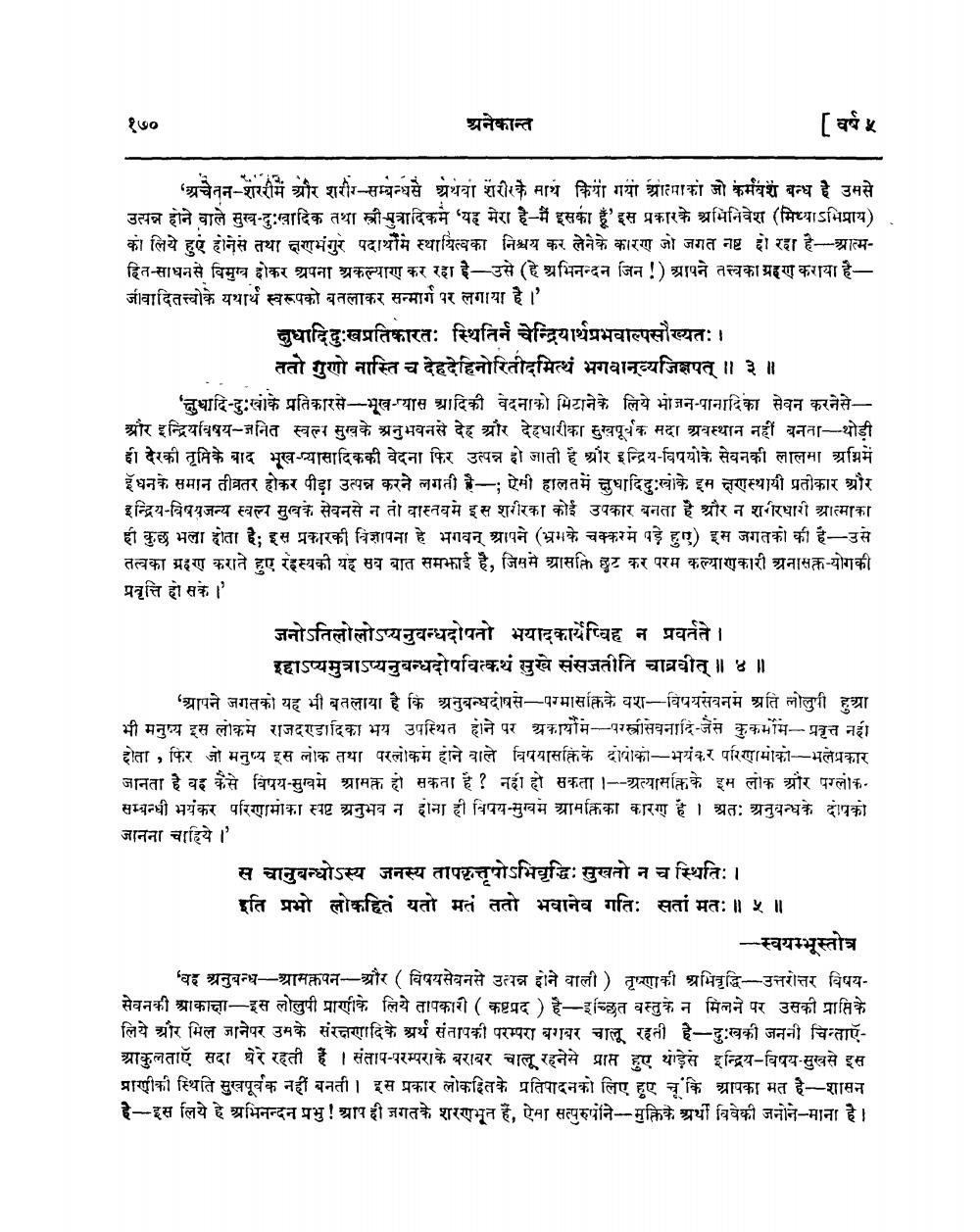________________
१७०
अनेकान्त
[वर्ष ५
'अचेतन-शररीमें और शरीर-सम्बन्धसै अथवा शरीरके माय किया गया श्रात्मा को जो कर्मवश बन्ध है उससे उत्पन्न होने वाले सुख-दुःखादिक तथा स्त्री पुत्रादिकमे 'यह मेरा है-मैं इसका हूँ' इस प्रकार के अभिनिवेश (मिथ्याऽभिप्राय) को लिये हुए होनेसे तथा क्षणभंगुर पदाथोंमे स्थायित्वका निश्चय कर लेनेके कारण जो जगत नष्ट हो रहा है-श्रात्महित-साधनसे विमुग्व होकर अपना अकल्याण कर रहा है-उसे (हे अभिनन्दन जिन !) अापने तत्त्वका ग्रहण कराया हैजीवादितत्त्वोके यथार्थ स्वरूपको बतलाकर सन्मार्ग पर लगाया है।'
तुधादिदुःखप्रतिकारतः स्थितिन चेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसौख्यतः ।
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीदमित्थं भगवानव्यजिशपत् ॥ ३ ॥ 'क्षुधादि-दु:खांके प्रतिकारसे-भूख-ग्यास प्रादिकी वेदनाको मिटाने के लिये भोजन-पानादिका सेवन करनेसेऔर इन्द्रियविषय-जनित स्वल्ल सुखके अनुभवनसे देह और देहधारीका सुखपूर्वक मदा अवस्थान नहीं बनता-थोड़ी ही देरकी तृप्तिके बाद भूख-ग्यासादिककी वेदना फिर उत्पन्न हो जाती है और इन्द्रिय-विषयोके सेवनकी लालमा अग्निमें
धन के समान तीव्रतर होकर पीड़ा उत्पन्न करने लगती है- ऐमी हालत में सुधादिदुःखोके इम क्षणस्थायी प्रतीकार और इन्द्रिय-विषयजन्य स्वल्य सुखके सेवनसे न तो वास्तवमे इस शरीरका कोई उपकार बनता है और न शरीरधारी अात्माका ही कुछ भला होता है; इस प्रकारकी विज्ञापना हे भगवन् अापने (भ्रमके चक्कर में पड़े हुए) इस जगतको की है-उसे तत्वका ग्रहण कराते हुए रहस्यकी यह सब बात समझाई है, जिससे ग्रासक्ति छुट कर परम कल्याणकारी अनासक्त-योगकी प्रवृत्ति हो सके।
जनोऽतिलोलोऽप्यनुवन्धदोपतो भयादकार्येप्विह न प्रवर्तते ।
इहाऽप्यमुत्राऽप्यनुबन्धदोपवित्कथं सुखे संसजतीति चाब्रवीत ॥४॥ 'अापने जगतको यह भी बतलाया है कि अनुबन्धदोषसे-पग्मासक्तिके वश-विषयसवनम अति लोलुपी हुया भी मनुष्य इस लोकम राजदण्डादिका भय उपस्थित होने पर अकार्योम-परस्त्रीसवनादि-जेंस कुकर्मोम-प्रवृत्त नही दोता , फिर जो मनुष्य इस लोक तथा परलोकम होने वाले विषयासक्ति के दायोको-भयंकर परिणामोको-मलेप्रकार जानता है वह कैसे विषय-सुग्वमे श्रामक्त हो सकता है ? नही हो सकता।--अत्याक्ति के इम लोक और पग्लीक. सम्बन्धी भयंकर परिणामोका स्पष्ट अनुभव न होना ही विषय-मुग्वमे अामक्तिका कारण है । अत: अनुवन्धके दोपको जानना चाहिये।
स चानुबन्धोऽस्य जनस्य तापमृत्तृपोऽभिवृद्धिः सुखतो न च स्थितिः । इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गतिः सतां मतः ॥ ५ ॥
-स्वयम्भूस्तोत्र 'वह अनुबन्ध-श्रामक्तपन-और ( विषयसेवनसे उत्पन्न होने वाली) तृष्णाकी अभिवृद्धि-उत्तरोत्तर विषयसेवनकी श्राकाक्षा-इस लोलुपी प्राणीके लिये तापकारी ( कष्टप्रद ) है-इच्छित वस्तु के न मिलने पर उसकी प्राप्ति के लिये और मिल जानेपर उसके संरक्षणादिके अर्थ संतापकी परम्परा बगबर चालू रहती है-दुःखकी जननी चिन्ताएँअाकुलताएँ सदा घेरे रहती हैं । संताप-परम्पराके बराबर चालू रहनेसे प्रास हुए थोड़ेसे इन्द्रिय-विषय-सुखसे इस प्राणीकी स्थिति सुखपूर्वक नहीं बनती। इस प्रकार लोकहितके प्रतिपादनको लिए हुए चुकि अापका मत है-शासन है-इस लिये हे अभिनन्दन प्रभु ! श्राप ही जगतके शरणभूत हैं, ऐमा सत्पुरुषोंने-मुक्तिके अर्थी विवेकी जनोने-माना है।