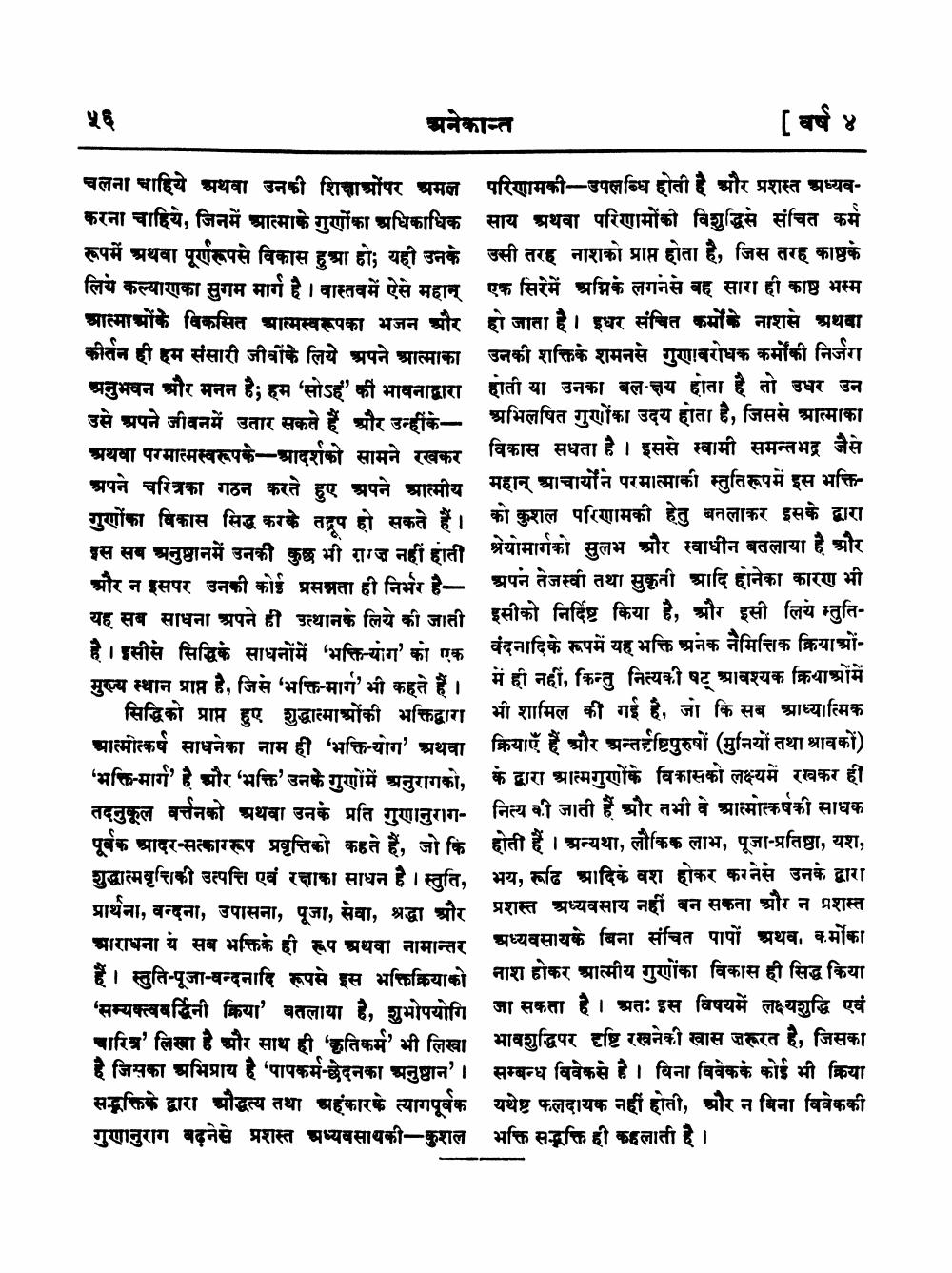________________
अनेकान्त
[वर्ष ४
चलना चाहिये अथवा उनकी शिक्षाओंपर अमल परिणामकी-उपलब्धि होती है और प्रशस्त अध्यवकरना चाहिये, जिनमें आत्माके गुणों का अधिकाधिक साय अथवा परिणामोंको विशुद्धिसे संचित कर्म रूपमें अथवा पूर्णरूपसे विकास हुआ हो; यही उनके उसी तरह नाशको प्राप्त होता है, जिस तरह काष्ठक लिये कल्याणका सुगम मार्ग है । वास्तवमें ऐसे महान् एक सिरेमें अग्निक लगनसे वह साग ही काष्ठ भस्म
आत्माओंके विकसित आत्मस्वरूपका भजन और हो जाता है। इधर संचित कोंके नाशसे अथवा कीर्तन ही हम संसारी जीवोंके लिये अपने आत्माका उनकी शक्तिक शमनसे गुणावरोधक कर्मोकी निर्जग अनुभवन और मनन है। हम 'सोऽह' की भावनाद्वारा होती या उनका बल-क्षय होता है तो उधर उन उसे अपने जीवनमें उतार सकते हैं और उन्हींक- अभिलषित गुणोंका उदय होता है, जिससे आत्माका अथवा परमात्मस्वरूपके-आदर्शको सामने रखकर विकास सधता है । इससे स्वामी समन्तभद्र जैसे अपने चरित्रका गठन करते हुए अपने आत्मीय महान् प्राचार्यों ने परमात्माकी स्तुतिरूपमें इस भक्तिगुणोंका विकास सिद्ध करके तद्रप हो सकते हैं। को कुशल परिणामकी हेतु बतलाकर इसके द्वारा इस सब अनुष्ठानमें उनकी कुछ भी राज नहीं हाती श्रेयोमार्गको सुलभ और स्वाधीन बतलाया है और
और न इसपर उनकी कोई प्रसन्नता ही निर्भर है- अपनं तेजस्वी तथा सुकृनी आदि होनेका कारण भी यह सब साधना अपने ही उत्थानके लिये की जाती इसीको निर्दिष्ट किया है, और इसी लिये स्तुतिहै । इसीसे सिद्धिक साधनोंमें 'भक्ति-योग' को एक वंदनादिके रूपमें यह भक्ति अनेक नैमित्तिक क्रियाओंमुख्य स्थान प्राप्त है, जिस 'भक्ति-मार्ग' भी कहते हैं। में ही नहीं, किन्तु नित्यकी षट् श्रावश्यक क्रियाओंमें
सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओंकी भक्तिद्वारा भी शामिल की गई है, जो कि सब आध्यात्मिक मात्मोत्कर्ष साधनेका नाम ही 'भक्ति-योग' अथवा क्रियाएँ हैं और अन्तर्दृष्टिपुरुषों (मुनियों तथा श्रावकों) 'भक्ति-मार्ग' है और 'भक्ति' उनके गुणोंमें अनुरागको, के द्वारा आत्मगुणोंके विकासको लक्ष्यमें रखकर ही तदनुकूल वर्तनको अथवा उनके प्रति गुणानुराग- नित्य की जाती हैं और तभी वे आत्मोत्कर्षकी साधक पूर्वक आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते हैं, जो कि होती हैं । अन्यथा, लौकिक लाभ, पूजा-प्रतिष्ठा, यश, शुद्धात्मवृत्तिकी उत्पत्ति एवं रक्षाका साधन है । स्तुति, भय, रूढि श्रादिकं वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रार्थना, वन्दना, उपासना, पूजा, सेवा, श्रद्धा और प्रशस्त अध्यवसाय नहीं बन सकता और न प्रशस्त भाराधना ये सब भक्तिक ही रूप अथवा नामान्तर अध्यवसायके बिना संचित पापों अथव, कर्मोका हैं। स्तुति-पूजा-वन्दनादि रूपसे इस भक्तिक्रियाको नाश होकर आत्मीय गुणोंका विकास ही सिद्ध किया 'सम्यक्त्ववर्दिनी क्रिया' बतलाया है, शुभोपयोगि जा सकता है। अतः इस विषयमें लक्ष्यशुद्धि एवं चारित्र' लिखा है और साथ ही 'कृतिकर्म' भी लिखा भावशुद्धिपर दृष्टि रखनेकी खास जरूरत है, जिसका है जिसका अभिप्राय है 'पापकर्म-छेदनका अनुष्ठान'। सम्बन्ध विवेकसे है। विना विवेककं कोई भी क्रिया सद्भक्तिके द्वारा प्रौद्धत्य तथा अहंकारके त्यागपूर्वक यथेष्ट फलदायक नहीं होती, और न बिना विवेककी गुणानुराग बढ़नेसे प्रशस्त अध्यवसायकी-कुशल भक्ति सद्भक्ति ही कहलाती है।